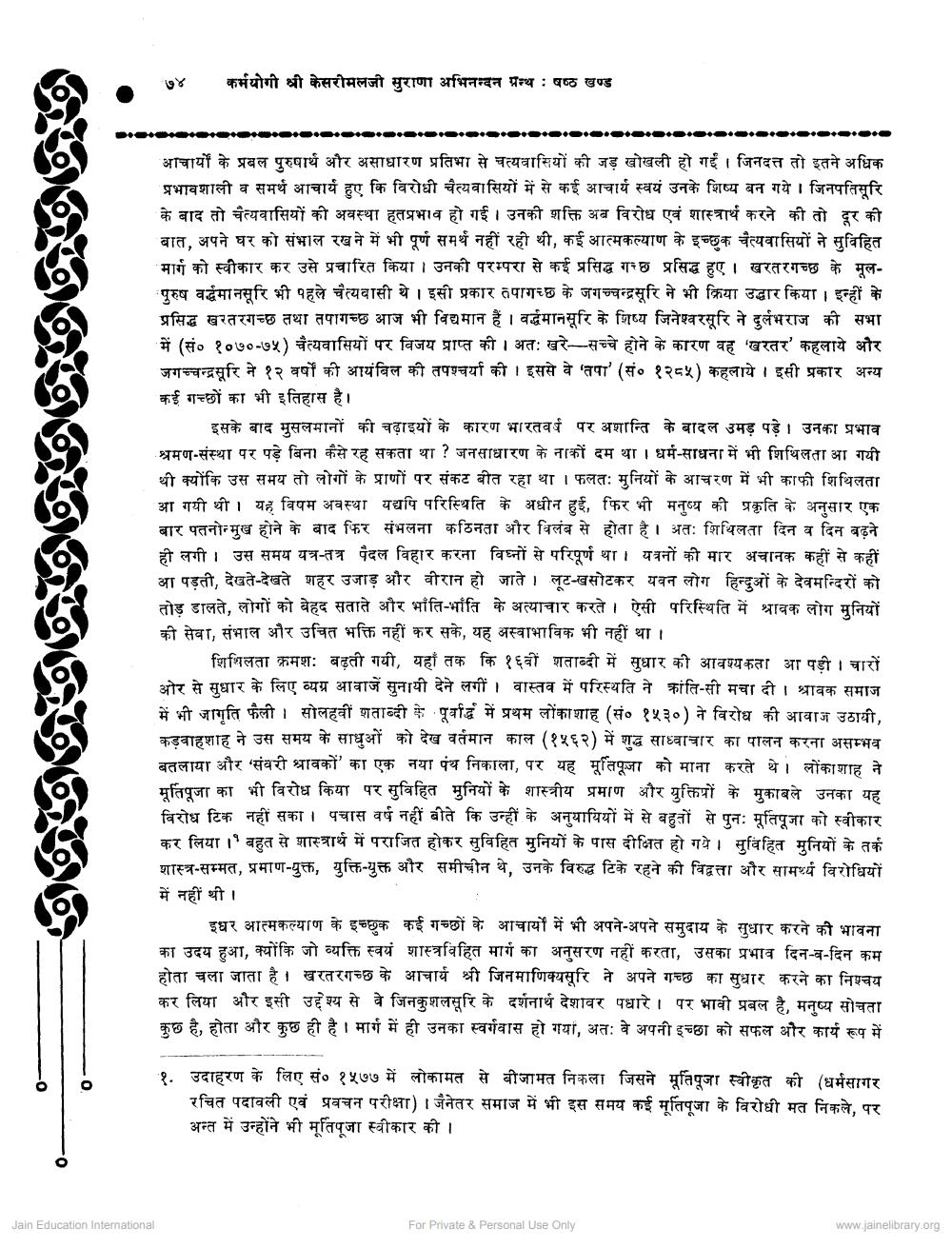________________
कर्मयोगी श्री केसरीमलजी सुराणा अभिनन्दन ग्रन्थ : षष्ठ खण्ड
आचार्यों के प्रबल पुरुषार्थ और असाधारण प्रतिभा से चत्यवासियों की जड़ खोखली हो गई । जिनदत्त तो इतने अधिक प्रभावशाली व समर्थ आचार्य हुए कि विरोधी चैत्यवासियों में से कई आचार्य स्वयं उनके शिष्य बन गये । जिनपतिसरि के बाद तो चैत्यवासियों की अवस्था हतप्रभाव हो गई । उनकी शक्ति अब विरोध एवं शास्त्रार्थ करने की तो दूर की बात, अपने घर को संभाल रखने में भी पूर्ण समर्थ नहीं रही थी, कई आत्मकल्याण के इच्छुक चैत्यवासियों ने सुविहित मार्ग को स्वीकार कर उसे प्रचारित किया। उनकी परम्परा से कई प्रसिद्ध गन्छ प्रसिद्ध हुए। खरतरगच्छ के मूलपुरुष वर्द्धमानसूरि भी पहले चैत्यवासी थे । इसी प्रकार तपागच्छ के जगच्चन्द्रसूरि ने भी क्रिया उद्धार किया। इन्हीं के प्रसिद्ध खरतरगच्छ तथा तपागच्छ आज भी विद्यमान हैं । वर्द्धमानसूरि के शिष्य जिनेश्वरसूरि ने दुर्लभराज की सभा में (सं० १०७०-७५) चैत्यवासियों पर विजय प्राप्त की। अत: खरे-सच्चे होने के कारण वह 'खरतर' कहलाये और जगच्चन्द्रसूरि ने १२ वर्षों की आयंबिल की तपश्चर्या की । इससे वे 'तपा' (सं० १२८५) कहलाये । इसी प्रकार अन्य कई गच्छों का भी इतिहास है।।
इसके बाद मुसलमानों की चढ़ाइयों के कारण भारतवर्ष पर अशान्ति के बादल उमड़ पड़े। उनका प्रभाव श्रमण-संस्था पर पड़े बिना कैसे रह सकता था? जनसाधारण के नाकों दम था । धर्म-साधना में भी शिथिलता आ गयी थी क्योंकि उस समय तो लोगों के प्राणों पर संकट बीत रहा था । फलत: मुनियों के आचरण में भी काफी शिथिलता आ गयी थी। यह विषम अवस्था यद्यपि परिस्थिति के अधीन हुई, फिर भी मनुष्य की प्रकृति के अनुसार एक बार पतनोन्मुख होने के बाद फिर संभलना कठिनता और विलंब से होता है। अत: शिथिलता दिन ब दिन बढ़ने ही लगी। उस समय यत्र-तत्र पैदल विहार करना विघ्नों से परिपूर्ण था। यवनों की मार अचानक कहीं से कहीं आ पड़ती, देखते-देखते शहर उजाड़ और वीरान हो जाते । लूट-खसोटकर यवन लोग हिन्दुओं के देवमन्दिरों को तोड़ डालते, लोगों को बेहद सताते और भाँति-भाँति के अत्याचार करते। ऐसी परिस्थिति में श्रावक लोग मुनियों की सेवा, संभाल और उचित भक्ति नहीं कर सके, यह अस्वाभाविक भी नहीं था।
शिथिलता क्रमशः बढ़ती गयी, यहाँ तक कि १६वीं शताब्दी में सुधार की आवश्यकता आ पड़ी। चारों ओर से सुधार के लिए व्यग्र आवाजें सुनायी देने लगीं। वास्तव में परिस्थति ने क्रांति-सी मचा दी। श्रावक समाज में भी जागति फैली। सोलहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में प्रथम लोंका शाह (सं० १५३०) ने विरोध की आवाज उठायी, कड़वाहशाह ने उस समय के साधुओं को देख वर्तमान काल (१५६२) में शुद्ध साध्वाचार का पालन करना असम्भव बतलाया और संवरी श्रावकों' का एक नया पंथ निकाला, पर यह मूर्तिपूजा को माना करते थे। लोंका शाह ने मर्तिपूजा का भी विरोध किया पर सुविहित मुनियों के शास्त्रीय प्रमाण और युक्तियों के मुकाबले उनका यह विरोध टिक नहीं सका। पचास वर्ष नहीं बीते कि उन्हीं के अनुयायियों में से बहुतों से पुन: मूर्तिपूजा को स्वीकार कर लिया। बहुत से शास्त्रार्थ में पराजित होकर सुविहित मुनियों के पास दीक्षित हो गये। सुविहित मुनियों के तर्क शास्त्र-सम्मत, प्रमाण-युक्त, युक्ति-युक्त और समीचीन थे, उनके विरुद्ध टिके रहने की विद्वत्ता और सामर्थ्य विरोधियों में नहीं थी।
इधर आत्मकल्याण के इच्छुक कई गच्छों के आचार्यों में भी अपने-अपने समुदाय के सुधार करने की भावना का उदय हआ, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं शास्त्रविहित मार्ग का अनुसरण नहीं करता, उसका प्रभाव दिन-ब-दिन कम होता चला जाता है। खरतरगच्छ के आचार्य श्री जिनमाणिक्यसूरि ने अपने गच्छ का सुधार करने का निश्चय कर लिया और इसी उद्देश्य से वे जिनकुशलसूरि के दर्शनार्थ देशावर पधारे। पर भावी प्रबल है, मनुष्य सोचता कुछ है, होता और कुछ ही है। मार्ग में ही उनका स्वर्गवास हो गया, अत: वे अपनी इच्छा को सफल और कार्य रूप में
१. उदाहरण के लिए सं० १५७७ में लोकामत से बीजामत निकला जिसने मूर्तिपूजा स्वीकृत की (धर्मसागर
रचित पदावली एवं प्रवचन परीक्षा)। जैनेतर समाज में भी इस समय कई मूर्तिपूजा के विरोधी मत निकले, पर अन्त में उन्होंने भी मूर्तिपूजा स्वीकार की।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org