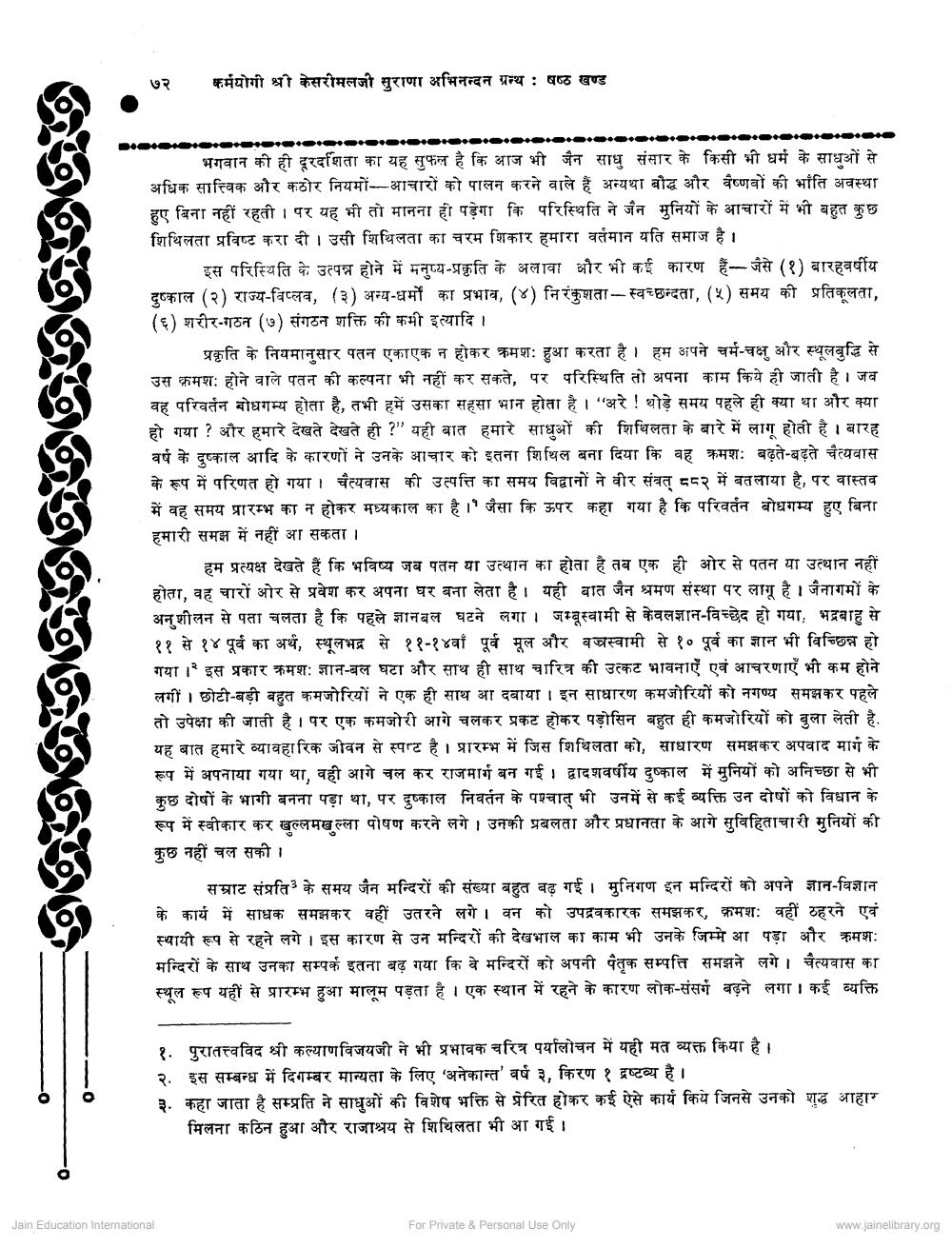________________
७२
कर्मयोगी श्री केसरीमलजी सुराणा अभिनन्दन ग्रन्थ : षष्ठ खण्ड
भगवान की ही दूरदशिता का यह सुफल है कि आज भी जैन साधु संसार के किसी भी धर्म के साधुओं से अधिक सात्त्विक और कठोर नियमों-आचारों को पालन करने वाले हैं अन्यथा बौद्ध और वैष्णवों की भांति अवस्था हुए बिना नहीं रहती । पर यह भी तो मानना ही पड़ेगा कि परिस्थिति ने जैन मुनियों के आचारों में भी बहुत कुछ शिथिलता प्रविष्ट करा दी। उसी शिथिलता का चरम शिकार हमारा वर्तमान यति समाज है।
इस परिस्थिति के उत्पन्न होने में मनुष्य-प्रकृति के अलावा और भी कई कारण हैं- जैसे (१) बारहवर्षीय दुष्काल (२) राज्य-विप्लव, (३) अन्य-धर्मों का प्रभाव, (४) निरंकुशता-स्वच्छन्दता, (५) समय की प्रतिकूलता, (६) शरीर-गठन (७) संगठन शक्ति की कमी इत्यादि ।
प्रकृति के नियमानुसार पतन एकाएक न होकर क्रमशः हुआ करता है। हम अपने चर्म-चक्षु और स्थूलबुद्धि से उस क्रमश: होने वाले पतन की कल्पना भी नहीं कर सकते, पर परिस्थिति तो अपना काम किये ही जाती है। जब वह परिवर्तन बोधगम्य होता है, तभी हमें उसका सहसा भान होता है । “अरे ! थोड़े समय पहले ही क्या था और क्या हो गया? और हमारे देखते देखते ही ?" यही बात हमारे साधुओं की शिथिलता के बारे में लागू होती है । बारह वर्ष के दुष्काल आदि के कारणों ने उनके आचार को इतना शिथिल बना दिया कि वह क्रमशः बढ़ते-बढ़ते चैत्यवास के रूप में परिणत हो गया। चैत्यवास की उत्पत्ति का समय विद्वानों ने वीर संवत् ८८२ में बतलाया है, पर वास्तव में वह समय प्रारम्भ का न होकर मध्यकाल का है। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि परिवर्तन बोधगम्य हुए बिना हमारी समझ में नहीं आ सकता ।
हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि भविष्य जब पतन या उत्थान का होता है तब एक ही ओर से पतन या उत्थान नहीं होता, वह चारों ओर से प्रवेश कर अपना घर बना लेता है। यही बात जैन श्रमण संस्था पर लागू है । जैनागमों के अनुशीलन से पता चलता है कि पहले ज्ञानबल घटने लगा। जम्बूस्वामी से केवलज्ञान-विच्छेद हो गया, भद्रबाहु से ११ से १४ पूर्व का अर्थ, स्थूलभद्र से ११-१४वाँ पूर्व मूल और वज्रस्वामी से १० पूर्व का ज्ञान भी विच्छिन्न हो गया। इस प्रकार क्रमश: ज्ञान-बल घटा और साथ ही साथ चारित्र की उत्कट भावनाएँ एवं आचरणाएँ भी कम होने लगीं। छोटी-बड़ी बहुत कमजोरियों ने एक ही साथ आ दबाया । इन साधारण कमजोरियों को नगण्य समझकर पहले तो उपेक्षा की जाती है । पर एक कमजोरी आगे चलकर प्रकट होकर पड़ोसिन बहुत ही कमजोरियों को बुला लेती है. यह बात हमारे व्यावहारिक जीवन से स्पाट है। प्रारम्भ में जिस शिथिलता को, साधारण समझकर अपवाद मार्ग के रूप में अपनाया गया था, वही आगे चल कर राजमार्ग बन गई। द्वादशवर्षीय दुष्काल में मुनियों को अनिच्छा से भी कुछ दोषों के भागी बनना पड़ा था, पर दुष्काल निवर्तन के पश्चात् भी उनमें से कई व्यक्ति उन दोषों को विधान के रूप में स्वीकार कर खुल्लमखुल्ला पोषण करने लगे। उनकी प्रबलता और प्रधानता के आगे सुविहिताचारी मुनियों की कुछ नहीं चल सकी।
सम्राट संप्रति के समय जैन मन्दिरों की संख्या बहुत बढ़ गई। मुनिगण इन मन्दिरों को अपने ज्ञान-विज्ञान के कार्य में साधक समझकर वहीं उतरने लगे। वन को उपद्रवकारक समझकर, क्रमश: वहीं ठहरने एवं स्थायी रूप से रहने लगे। इस कारण से उन मन्दिरों की देखभाल का काम भी उनके जिम्मे आ पड़ा और क्रमशः मन्दिरों के साथ उनका सम्पर्क इतना बढ़ गया कि वे मन्दिरों को अपनी पैतृक सम्पत्ति समझने लगे। चैत्यवास का स्थूल रूप यहीं से प्रारम्भ हुआ मालूम पड़ता है । एक स्थान में रहने के कारण लोक-संसर्ग बढ़ने लगा। कई व्यक्ति
१. पुरातत्त्वविद श्री कल्याणविजयजी ने भी प्रभावक चरित्र पर्यालोचन में यही मत व्यक्त किया है। २. इस सम्बन्ध में दिगम्बर मान्यता के लिए 'अनेकान्त' वर्ष ३, किरण १ द्रष्टव्य है। ३. कहा जाता है सम्प्रति ने साधुओं की विशेष भक्ति से प्रेरित होकर कई ऐसे कार्य किये जिनसे उनको शुद्ध आहार
मिलना कठिन हुआ और राजाश्रय से शिथिलता भी आ गई।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org