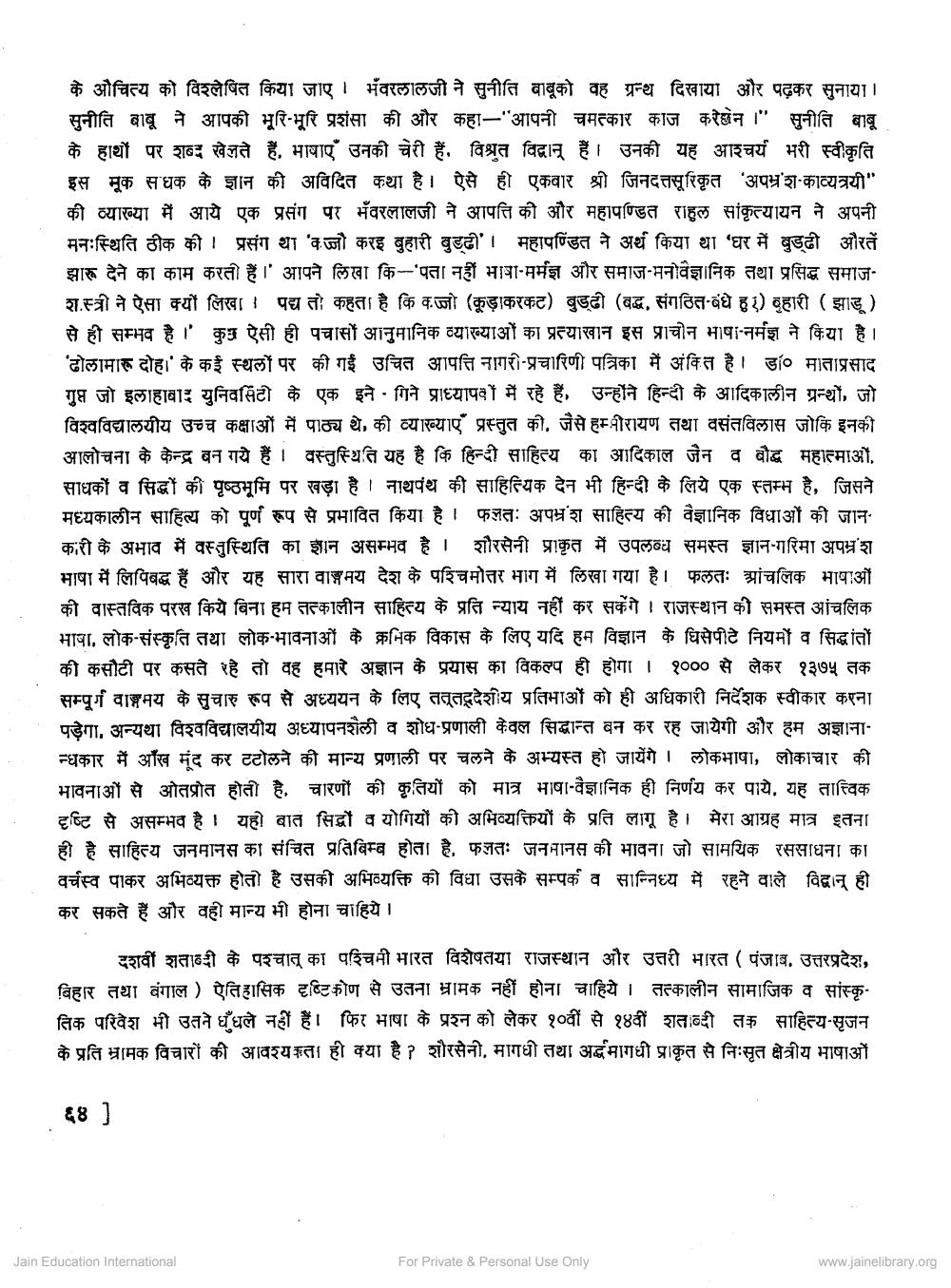________________
के औचित्य को विश्लेषित किया जाए। भंवरलालजी ने सुनीति बाबूको वह ग्रन्थ दिखाया और पढ़कर सुनाया। सुनीति बाबू ने आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा की और कहा-"आपनी चमत्कार काज करेछन ।" सुनीति बाबू के हाथों पर शब्द खेलते हैं. भाषाएं उनकी चेरी हैं, विश्रुत विद्वान् हैं। उनकी यह आश्चर्य भरी स्वीकृति इस मूक सधक के ज्ञान की अविदित कथा है। ऐसे ही एकवार श्री जिनदत्तसूरिकृत 'अपभ्रश-काव्यत्रयी" की व्याख्या में आये एक प्रसंग पर भंवरलालजी ने आपत्ति की और महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने अपनी मनःस्थिति ठीक की। प्रसंग था 'वज्जो करइ बुहारी बुड्ढी'। महापण्डित ने अर्थ किया था 'घर में बुड्ढी औरतें झारू देने का काम करती हैं।' आपने लिखा कि-'पता नहीं भाषा-मर्मज्ञ और समाज-मनोवैज्ञानिक तथा प्रसिद्ध समाजश.स्त्री ने ऐसा क्यों लिखा । पद्य तो कहता है कि कज्जो (कूड़ाकरकट) बुड्डी (बद्ध, संगठित बंधे हुए) बुहारी (झाडू ) से ही सम्भव है।' कुछ ऐसी ही पचासों आनुमानिक व्याख्याओं का प्रत्याखान इस प्राचीन भाषा-नर्मज्ञ ने किया है। 'ढोलामारू दोहा के कई स्थलों पर की गई उचित आपत्ति नागरी-प्रचारिणी पत्रिका में अंकित है। डॉ० माताप्रसाद गुप्त जो इलाहाबाद युनिवर्सिटी के एक इने - गिने प्राध्यापकों में रहे हैं, उन्होंने हिन्दी के आदिकालीन ग्रन्थों, जो विश्वविद्यालयीय उच्च कक्षाओं में पाठ्य थे, की व्याख्याएं प्रस्तुत की, जैसे हम्मीरायण तथा वसंतविलास जोकि इनकी आलोचना के केन्द्र बन गये हैं। वस्तुस्थिति यह है कि हिन्दी साहित्य का आदिकाल जैन व बौद्ध महात्माओं, साधकों व सिद्धों की पृष्ठभूमि पर खड़ा है। नाथपंथ की साहित्यिक देन भी हिन्दी के लिये एक स्तम्भ है, जिसने मध्यकालीन साहित्य को पूर्ण रूप से प्रभावित किया है। फलतः अपभ्रंश साहित्य की वैज्ञानिक विधाओं की जान कारी के अभाव में वस्तुस्थिति का ज्ञान असम्भव है। शौरसेनी प्राकृत में उपलब्ध समस्त ज्ञान-गरिमा अपभ्रंश भाषा में लिपिबद्ध हैं और यह सारा वाङ्गमय देश के पश्चिमोत्तर भाग में लिखा गया है। फलतः आंचलिक भाषाओं की वास्तविक परख किये बिना हम तत्कालीन साहित्य के प्रति न्याय नहीं कर सकेंगे । राजस्थान की समस्त आंचलिक भाषा, लोक-संस्कृति तथा लोक-भावनाओं के क्रमिक विकास के लिए यदि हम विज्ञान के घिसेपीटे नियमों व सिद्धांतों की कसौटी पर कसते रहे तो वह हमारे अज्ञान के प्रयास का विकल्प ही होगा । १००० से लेकर १३७५ तक सम्पूर्ण वाङ्गमय के सुचारु रूप से अध्ययन के लिए तत्तद्देशीय प्रतिभाओं को ही अधिकारी निर्देशक स्वीकार करना पडेगा. अन्यथा विश्वविद्यालयीय अध्यापनशैली व शोध-प्रणाली केवल सिद्धान्त बन कर रह जायेगी और हम अज्ञानान्धकार में आँख मूंद कर टटोलने की मान्य प्रणाली पर चलने के अभ्यस्त हो जायेंगे । लोकभाषा, लोकाचार की भावनाओं से ओतप्रोत होती है, चारणों की कृतियों को मात्र भाषा-वैज्ञानिक ही निर्णय कर पाये, यह तात्विक दृष्टि से असम्भव है। यही बात सिद्धों व योगियों की अभिव्यक्तियों के प्रति लागू है। मेरा आग्रह मात्र इतना ही है साहित्य जनमानस का संचित प्रतिबिम्ब होता है, फलतः जनमानस की भावना जो सामयिक रससाधना का वर्चस्व पाकर अभिव्यक्त होती है उसकी अभिव्यक्ति को विधा उसके सम्पर्क व सान्निध्य में रहने वाले विद्वान ही कर सकते हैं और वही मान्य भी होना चाहिये।
दशवीं शताब्दी के पश्चात् का पश्चिमी भारत विशेषतया राजस्थान और उत्तरी भारत (पंजाब, उत्तरप्रदेश, बिहार तथा बंगाल ) ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उतना भ्रामक नहीं होना चाहिये । तत्कालीन सामाजिक व सांस्कृ. तिक परिवेश भी उतने घंधले नहीं हैं। फिर भाषा के प्रश्न को लेकर १०वीं से १४वीं शताब्दी तक साहित्य-सजन के प्रति भ्रामक विचारों की आवश्यकता ही क्या है? शौरसेनी, मागधी तथा अर्द्धमागधी प्राकृत से निःसृत क्षेत्रीय भाषाओं
६४ ]
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org