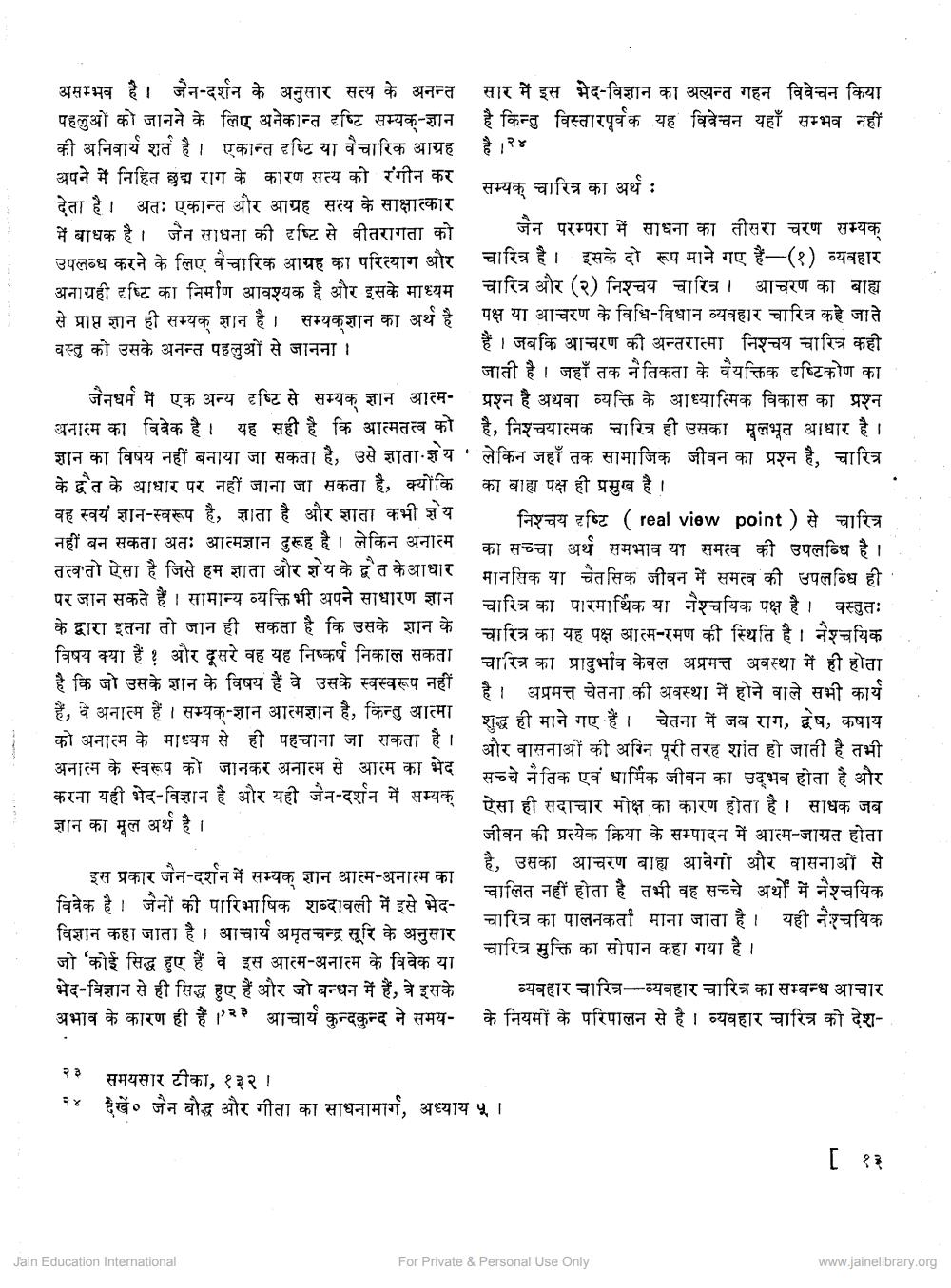________________
असम्भव है। जैन दर्शन के अनुसार सत्य के अनन्त पहलुओं को जानने के लिए अनेकान्त दृष्टि सम्यक् ज्ञान की अनिवार्य शर्त है। एकान्त दृष्टि या वैचारिक आग्रह अपने में निहित छद्म राग के कारण सत्य को रंगीन कर देता है । अतः एकान्त और आग्रह सत्य के साक्षात्कार में बाधक है। जैन साधना की दृष्टि से वीतरागता को उपलब्ध करने के लिए वैचारिक आग्रह का परित्याग और अनाग्रही दृष्टि का निर्माण आवश्यक है और इसके माध्यम से प्राप्त ज्ञान ही सम्यक् ज्ञान है । सम्यक्ज्ञान का अर्थ है सम्पज्ञान का अर्थ है वस्तु को उसके अनन्त पहलुओं से जानना ।
I
जैनधर्म में एक अन्य दृष्टि से सम्यक् ज्ञान आत्मअनात्म का विवेक है । यह सही है कि आत्मतत्व को ज्ञान का विषय नहीं बनाया जा सकता है, उसे ज्ञाता ज्ञेय' केत के आधार पर नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है, शाता है और शाता कभी शेय नहीं बन सकता अतः आत्मज्ञान दुरूह है लेकिन अनात्म तरवतो ऐसा है जिसे हम ज्ञाता और शेय के द्व ेत के आधार पर जान सकते हैं। सामान्य व्यक्ति भी अपने साधारण ज्ञान के द्वारा इतना तो जान ही सकता है कि उसके ज्ञान के विषय क्या हैं ? और दूसरे वह यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि जो उसके ज्ञान के विषय हैं वे उसके स्वस्वरूप नहीं हैं, वे अनात्म हैं। सम्यक् ज्ञान आत्मज्ञान है, किन्तु आत्मा को अनात्म के माध्यम से ही पहचाना जा सकता है । अनात्म के स्वरूप को जानकर अनात्म से आत्म का भेद करना यही भेद-विज्ञान है और यही जैन दर्शन में सम्ब ज्ञान का मूल अर्थ है।
इस प्रकार जैन दर्शन में सम्यक ज्ञान आत्म-अनात्म का विवेक है। जैनों की पारिभाषिक शब्दावली में इसे भेदविज्ञान कहा जाता है। आचार्य अमृतचन्द्र सूरि के अनुसार जो 'कोई सिद्ध हुए हैं वे इस आत्म-अनात्म के विवेक या भेद-विज्ञान से ही सिद्ध हुए हैं और जो बन्धन में हैं, वे इसके अभाव के कारण ही हैं। २० आचार्य कुन्दकुन्द ने समय
२३ समयसार टीका, १३२ ।
२४
सार में इस भेद - विज्ञान का अत्यन्त गहन विवेचन किया है किन्तु विस्तारपूर्वक यह विवेचन यहाँ सम्भव नहीं है २४
Jain Education International
सम्यक् चारित्र का चारित्र का अर्थ
जैन परम्परा में साधना का तीसरा चरण सम्यक् चारित्र है । इसके दो रूप माने गए हैं - ( १ ) व्यवहार चारित्र और (२) निश्चय चारित्र आचरण का बाह्य पक्ष या आचरण के विधि-विधान व्यवहार चारित्र कहे जाते है। जबकि आचरण की अन्तरात्मा निश्चय चारित्र कही जाती है। जहाँ तक नैतिकता के वैयक्तिक दृष्टिकोण का प्रश्न है अथवा व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास का प्रश्न है, निश्चयात्मक चारित्र ही उसका मूलभूत आधार है । लेकिन जहाँ तक सामाजिक जीवन का प्रश्न है, चारित्र का बाह्य पक्ष ही प्रमुख है !
निश्चय दृष्टि (real view point ) से चारित्र का सच्चा अर्थ समभाव या समत्व की उपलब्धि है । मानसिक या चैत सिक जीवन में समत्व की उपलब्धि ही चारित्र का पारमार्थिक या नेश्वयिक पक्ष है। वस्तुतः चारित्र का यह पक्ष आत्म-रमण की स्थिति है। नेश्चयिक चारित्र का प्रादुर्भाव केवल अप्रमत्त अवस्था में ही होता है। अप्रमत्त चेतना की अवस्था में होने वाले सभी कार्य शुद्ध ही माने गए हैं। चेतना में जब राग, द्वेष, कपाय और वासनाओं की अग्नि पूरी तरह शांत हो जाती है तभी सच्चे नैतिक एवं धार्मिक जीवन का उद्भव होता है और ऐसा ही सदाचार मोक्ष का कारण होता है । साधक जब जीवन की प्रत्येक क्रिया के सम्पादन में आत्म जाग्रत होता है, उसका आचरण बाह्य आवेगों और वासनाओं से चालित नहीं होता है तभी वह सच्चे अर्थों में नैश्चयिक चारित्र का पालनकर्ता माना जाता है । यही नैश्चयिक चारित्र मुक्ति का सोपान कहा गया है।
व्यवहार चारित्र - व्यवहार चारित्र का सम्बन्ध आचार के नियमों के परिपालन से है। व्यवहार चारित्र को देश
देखें ० जैन बौद्ध और गीता का साधनामार्ग, अध्याय ५ ।
For Private & Personal Use Only
[ १२
www.jainelibrary.org