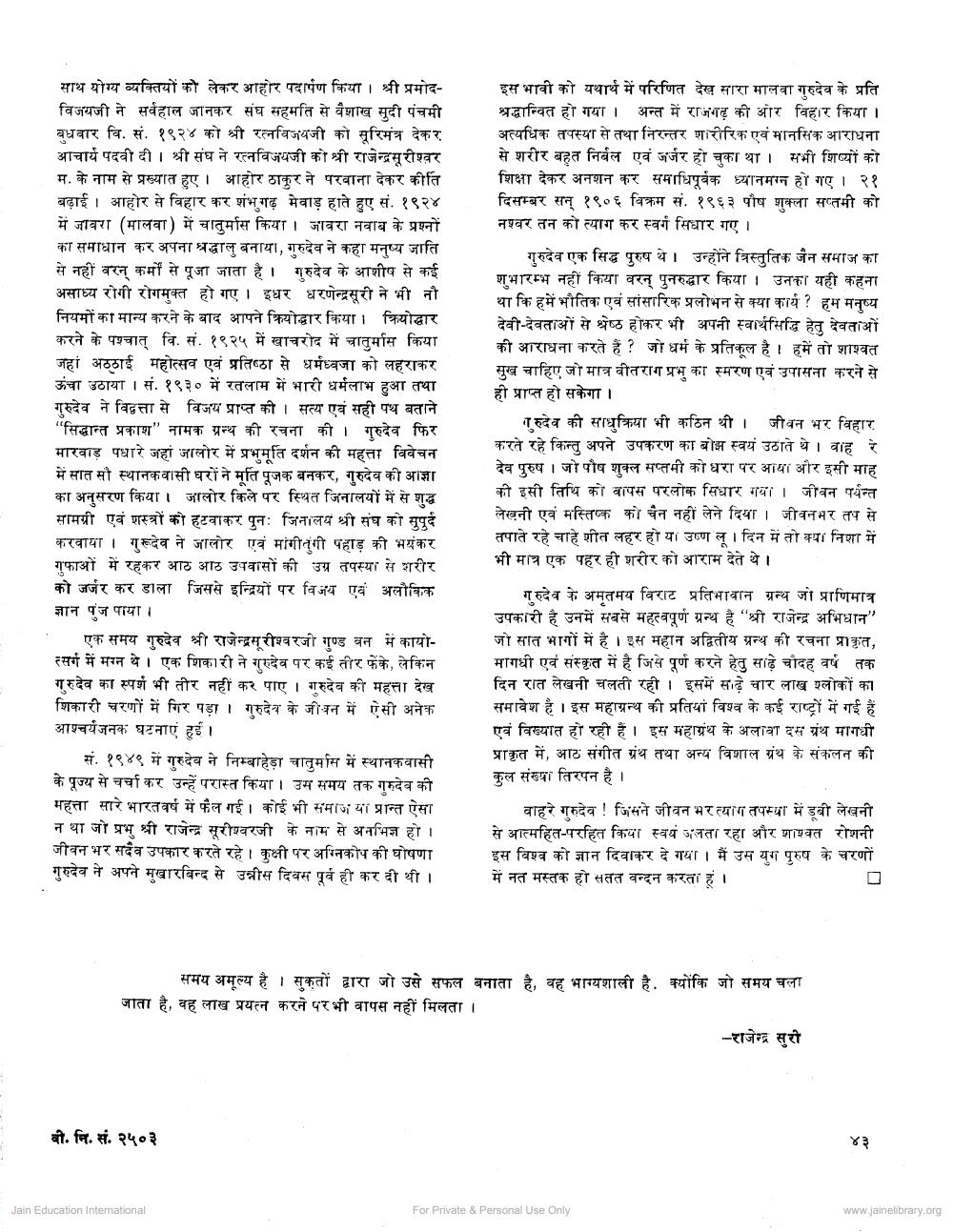________________
साथ योग्य व्यक्तियों को लेकर आहोर पदार्पण किया। श्री प्रमोदविजयजी ने सर्वहाल जानकर संघ सहमति से वैशाख सुदी पंचमी बुधवार वि. सं. १९२४ को श्री रत्नविजयजी को सूरिमंत्र देकर आचार्य पदवी दी। श्री संघ ने रत्नविजयजी को श्री राजेन्द्रसूरीश्वर म. के नाम से प्रख्यात हुए। आहोर ठाकुर ने परवाना देकर कीर्ति बढ़ाई। आहोर से विहार कर शंभु गढ़ मेवाड़ हाते हुए सं. १९२४ में जावरा (मालवा) में चातुर्मास किया। जावरा नवाब के प्रश्नों का समाधान कर अपना श्रद्धालु बनाया, गुरुदेव ने कहा मनुष्य जाति से नहीं वरन् कर्मों से पूजा जाता है। गुरुदेव के आशीष से कई असाध्य रोगी रोगमुक्त हो गए। इधर धरणेन्द्रसूरी ने भी नौ नियमों का मान्य करने के बाद आपने क्रियोद्धार किया। क्रियोद्धार करने के पश्चात् वि. सं. १९२५ में खाचरोद में चातुर्मास किया जहां अट्ठाई महोत्सव एवं प्रतिष्ठा से धर्मध्वजा को लहराकर ऊंचा उठाया । सं. १९३० में रतलाम में भारी धर्मलाभ हुआ तथा गुरुदेव ने विद्वत्ता से विजय प्राप्त की। सत्य एवं सही पथ बताने "सिद्धान्त प्रकाश" नामक ग्रन्थ की रचना की । गुरुदेव फिर मारवाड़ पधारे जहां जालोर में प्रभुमूर्ति दर्शन की महत्ता विवेचन में सात सौ स्थानकवासी घरों ने मूर्ति पूजक बनकर, गुरुदेव की आज्ञा का अनुसरण किया। जालोर किले पर स्थित जिनालयों में से शुद्ध सामग्री एवं शस्त्रों को हटवाकर पुनः जिनालय श्री संघ को सुपुर्द करवाया । गुरूदेव ने जालोर एवं मांगीतुंगी पहाड़ की भयंकर गुफाओं में रहकर आठ आठ उपवासों की उग्र तपस्या से शरीर को जर्जर कर डाला जिससे इन्द्रियों पर विजय एवं अलौकिक ज्ञान पुंज पाया।
एक समय गुरुदेव श्री राजेन्द्रसूरीश्वरजी गुण्ड वन में कायोत्सर्ग में मग्न थे। एक शिकारी ने गुरुदेव पर कई तीर फेंके, लेकिन गरुदेव का स्पर्श भी तीर नहीं कर पाए। गरुदेव की महत्ता देख शिकारी चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव के जीवन में ऐसी अनेक आश्चर्यजनक घटनाएं हुई।
सं. १९४९ में गुरुदेव ने निम्बाहेड़ा चातुर्मास में स्थानकवासी के पूज्य से चर्चा कर उन्हें परास्त किया। उस समय तक गुरुदेव की महत्ता सारे भारतवर्ष में फैल गई। कोई भी समाज या प्रान्त ऐसा न था जो प्रभु श्री राजेन्द्र सूरीश्वरजी के नाम से अनभिज्ञ हो । जीवन भर सदैव उपकार करते रहे। कुक्षी पर अग्निकोप की घोषणा गरुदेव ने अपने मुखारबिन्द से उन्नीस दिवस पूर्व ही कर दी थी।
इस भावी को यथार्थ में परिणित देख सारा मालवा गुरुदेव के प्रति श्रद्धान्वित हो गया । अन्त में राजगढ़ की ओर विहार किया। अत्यधिक तपस्या से तथा निरन्तर शारीरिक एवं मानसिक आराधना से शरीर बहुत निर्बल एवं जर्जर हो चुका था। सभी शिष्यों को शिक्षा देकर अनशन कर समाधिपूर्वक ध्यानमग्न हो गए। २१ दिसम्बर सन् १९०६ विक्रम सं. १९६३ पौष शुक्ला सप्तमी को नश्वर तन को त्याग कर स्वर्ग सिधार गए।
गुरुदेव एक सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने त्रिस्तुतिक जैन समाज का शुभारम्भ नहीं किया वरन् पुनरुद्धार किया । उनका यही कहना था कि हमें भौतिक एवं सांसारिक प्रलोभन से क्या कार्य ? हम मनुष्य देवी-देवताओं से श्रेष्ठ होकर भी अपनी स्वार्थसिद्धि हेतु देवताओं की आराधना करते हैं ? जो धर्म के प्रतिकूल है। हमें तो शाश्वत सुख चाहिए जो मात्र वीतराग प्रभु का स्मरण एवं उपासना करने से ही प्राप्त हो सकेगा।
गुरुदेव की साधुक्रिया भी कठिन थी। जीवन भर विहार करते रहे किन्तु अपने उपकरण का बोझ स्वयं उठाते थे। वाह रे देव पुरुष । जो पौष शुक्ल सप्तमी को धरा पर आया और इसी माह की इसी तिथि को वापस परलोक सिधार गया । जीवन पर्यन्त लेखनी एवं मस्तिष्क को चैन नहीं लेने दिया । जीवनभर तप से तपाते रहे चाहे शीत लहर हो या उष्ण लू । दिन में तो क्या निशा में भी मात्र एक पहर ही शरीर को आराम देते थे।
गुरुदेव के अमृतमय विराट प्रतिभावान ग्रन्थ जो प्राणिमात्र उपकारी है उनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ है “श्री राजेन्द्र अभिधान" जो सात भागों में है। इस महान अद्वितीय ग्रन्थ की रचना प्राकृत, मागधी एवं संस्कृत में है जिसे पूर्ण करने हेतु साढ़े चौदह वर्ष तक दिन रात लेखनी चलती रही। इसमें साढ़े चार लाख श्लोकों का समावेश है । इस महाग्रन्थ की प्रतियां विश्व के कई राष्ट्रों में गई हैं एवं विख्यात हो रही हैं। इस महाग्रंथ के अलावा दस ग्रंथ मागधी प्राकृत में, आठ संगीत ग्रंथ तथा अन्य विशाल ग्रंथ के संकलन की कुल संख्या तिरपन है।
वाहरे गुरुदेव ! जिसने जीवन भर त्याग तपस्या में डूबी लेखनी से आत्महित-परहित किया स्वयं जलता रहा और शाश्वत रोशनी इस विश्व को ज्ञान दिवाकर दे गया । मैं उस युग पुरुष के चरणों में नत मस्तक हो सतत वन्दन करता हूँ।
समय अमूल्य है । सुकतों द्वारा जो उसे सफल बनाता है, वह भाग्यशाली है. क्योंकि जो समय चला जाता है, वह लाख प्रयत्न करने पर भी वापस नहीं मिलता।
-राजेन्द्र सुरी
वी.नि.सं. २५०३
४३
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org