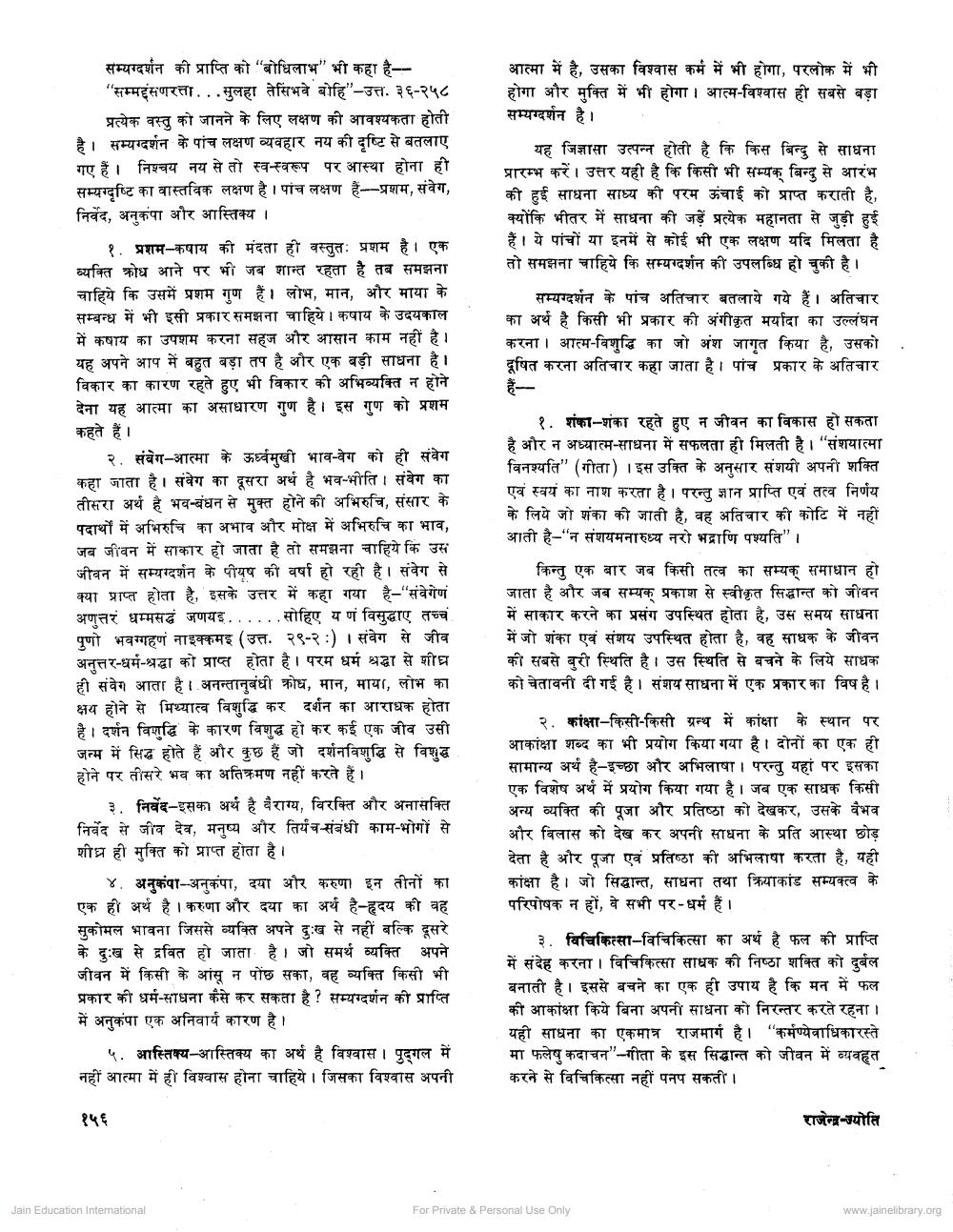________________
सम्यग्दर्शन की प्राप्ति को “बोधिलाभ" भी कहा है "सम्म सगरता... मुलहा तेहिभने बोहि" उत्त. ३६-२५८
प्रत्येक वस्तु को जानने के लिए लक्षण की आवश्यकता होती है । सम्यग्दर्शन के पांच लक्षण व्यवहार नय की दृष्टि से बतलाए गए हैं। निश्चय नय से तो स्व-स्वरूप पर आस्था होना ही सम्यग्दृष्टि का वास्तविक लक्षण है। पांच लक्षण हैं- प्रशम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य ।
१. प्रशम - कषाय की मंदता ही वस्तुतः प्रशम है। एक व्यक्ति क्रोध आने पर भी जब शान्त रहता है तब समझना चाहिये कि उसमें प्रशम गुण हैं। लोभ, मान, और माया के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार समझना चाहिये । कषाय के उदयकाल में कषाय का उपशम करना सहज और आसान काम नहीं है । यह अपने आप में बहुत बड़ा तप है और एक बड़ी साधना है। विकार का कारण रहते हुए भी विकार की अभिव्यक्ति न होने देना यह आत्मा का असाधारण गुण है। इस गुण को प्रथम कहते हैं।
२. संवेग आत्मा के ऊर्ध्वमुखी भाव-वे को ही संवेग कहा जाता है। संवेग का दूसरा अर्थ है भव-भीति । संवेग का तीसरा अर्थ है भव-बंधन से मुक्त होने की अभिरुचि, संसार के पदार्थों में अभिरुचि का अभाव और मोक्ष में अभिरुचि का भाव, जब जीवन में साकार हो जाता है तो समझना चाहिये कि उस जीवन में सम्यग्दर्शन के पीयूष की वर्षा हो रही है। संवेग से क्या प्राप्त होता है, इसके उत्तर में कहा गया है- "संवेगेणं अणुत्तरं धम्मसद्धं जणयइ. . सोहिए य णं विसुद्धाए तच्च पुणो भवग्गहणं नाइक्कमइ ( उत्त. २९-२ ) । संवेग से जीव अनुत्तर-धर्म-श्रद्धा को प्राप्त होता है। परम धर्म श्रद्धा से शीघ्र ही संवेग आता है । अनन्तानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का क्षय होने से मिथ्यात्व विशुद्धि कर दर्शन का आराधक होता है। दर्शन विशुद्धि के कारण विशुद्ध हो कर कई एक जीव उसी जन्म में सिद्ध होते हैं और कुछ हैं जो दर्शनविशुद्धि से विशुद्ध होने पर तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करते हैं।
३. निर्वेद - इसका अर्थ है वैराग्य, विरक्ति और अनासक्ति निर्वेद से जीव देव, मनुष्य और तिर्यंच-संबंधी काम-भोगों से शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त होता है।
४. अनुकंपा अनुकंपा, दया और करुणा इन तीनों का एक ही अर्थ है । करुणा और दया का अर्थ है - हृदय की वह सुकोमल भावना जिससे व्यक्ति अपने दुःख से नहीं बल्कि दूसरे के दुःख से द्रवित हो जाता है। जो समर्थ व्यक्ति अपने जीवन में किसी के आंसू न पोंछ सका, वह व्यक्ति किसी भी प्रकार की धर्म-साधना कैसे कर सकता है ? सम्यग्दर्शन की प्राप्ति में अनुकंपा एक अनिवार्य कारण है।
५. आस्तिक्य - आस्तिक्य का अर्थ है विश्वास । पुद्गल में नहीं आत्मा में ही विश्वास होना चाहिये। जिसका विश्वास अपनी
१५६
Jain Education International
आत्मा में है, उसका विश्वास कर्म में भी होगा, परलोक में भी होगा और मुक्ति में भी होगा । आत्म-विश्वास ही सबसे बड़ा सम्यग्दर्शन है।
यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि किस बिन्दु से साधना प्रारम्भ करें। उत्तर यही है कि किसी भी सम्यक् बिन्दु से आरंभ की हुई साधना साध्य की परम ऊंचाई को प्राप्त कराती है, क्योंकि भीतर में साधना की जड़ें प्रत्येक महानता से जुड़ी हुई हैं। ये पांचों या इनमें से कोई भी एक लक्षण यदि मिलता है। तो समझना चाहिये कि सम्यग्दर्शन की उपलब्धि हो चुकी है ।
सम्यग्दर्शन के पांच अतिचार बतलाये गये हैं। अतिचार का अर्थ है किसी भी प्रकार की अंगीकृत मर्यादा का उल्लंघन करना। आत्म-विशुद्धि का जो अंश जागृत किया है, उसको दूषित करना अतिचार कहा जाता है। पांच प्रकार के अतिचार है
१. शंका - शंका रहते हुए न जीवन का विकास हो सकता है और न अध्यात्म-साधना में सफलता ही मिलती है। "संशयात्मा विनश्यति' ( गीता) । इस उक्ति के अनुसार संशयी अपनी शक्ति एवं स्वयं का नाश करता है । परन्तु ज्ञान प्राप्ति एवं तत्व निर्णय के लिये जो शंका की जाती है, वह अतिचार की कोटि में नहीं आती है- "न संशयमनारुध्य नरो भद्राणि पश्यति" ।
किन्तु एक बार जब किसी तत्व का सम्यक् समाधान हो जाता है और जब सम्यक् प्रकाश से स्वीकृत सिद्धान्त को जीवन में साकार करने का प्रसंग उपस्थित होता है, उस समय साधना में जो शंका एवं संशय उपस्थित होता है, वह साधक के जीवन की सबसे बुरी स्थिति है । उस स्थिति से बचने के लिये साधक को चेतावनी दी गई है। संशय साधना में एक प्रकार का विष है।
२. कांक्षा- किसी-किसी ग्रन्थ में कांक्षा के स्थान पर आकांक्षा शब्द का भी प्रयोग किया गया है। दोनों का एक ही सामान्य अर्थ है - इच्छा और अभिलाषा । परन्तु यहां पर इसका एक विशेष अर्थ में प्रयोग किया गया है। जब एक साधक किसी अन्य व्यक्ति की पूजा और प्रतिष्ठा को देखकर, उसके वैभव और विलास को देख कर अपनी साधना के प्रति आस्था छोड़ देता है और पूजा एवं प्रतिष्ठा की अभिलाषा करता है, यही कांक्षा है। जो सिद्धान्त, साधना तथा क्रियाकांड सम्यक्त्व के परिपोषक न हों, वे सभी पर धर्म हैं ।
३. विचिकित्सा - विचिकित्सा का अर्थ है फल की प्राप्ति में संदेह करना । विचिकित्सा साधक की निष्ठा शक्ति को दुर्बल बनाती है। इससे बचने का एक ही उपाय है कि मन में फल hat आकांक्षा किये बिना अपनी साधना को निरन्तर करते रहना । यही साधना का एकमात्र राजमार्ग है। "कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन" - गीता के इस सिद्धान्त को जीवन में व्यवहृत करने से विचिकित्सा नहीं पनप सकती ।
For Private & Personal Use Only
राजेन्द्र ज्योति
www.jainelibrary.org