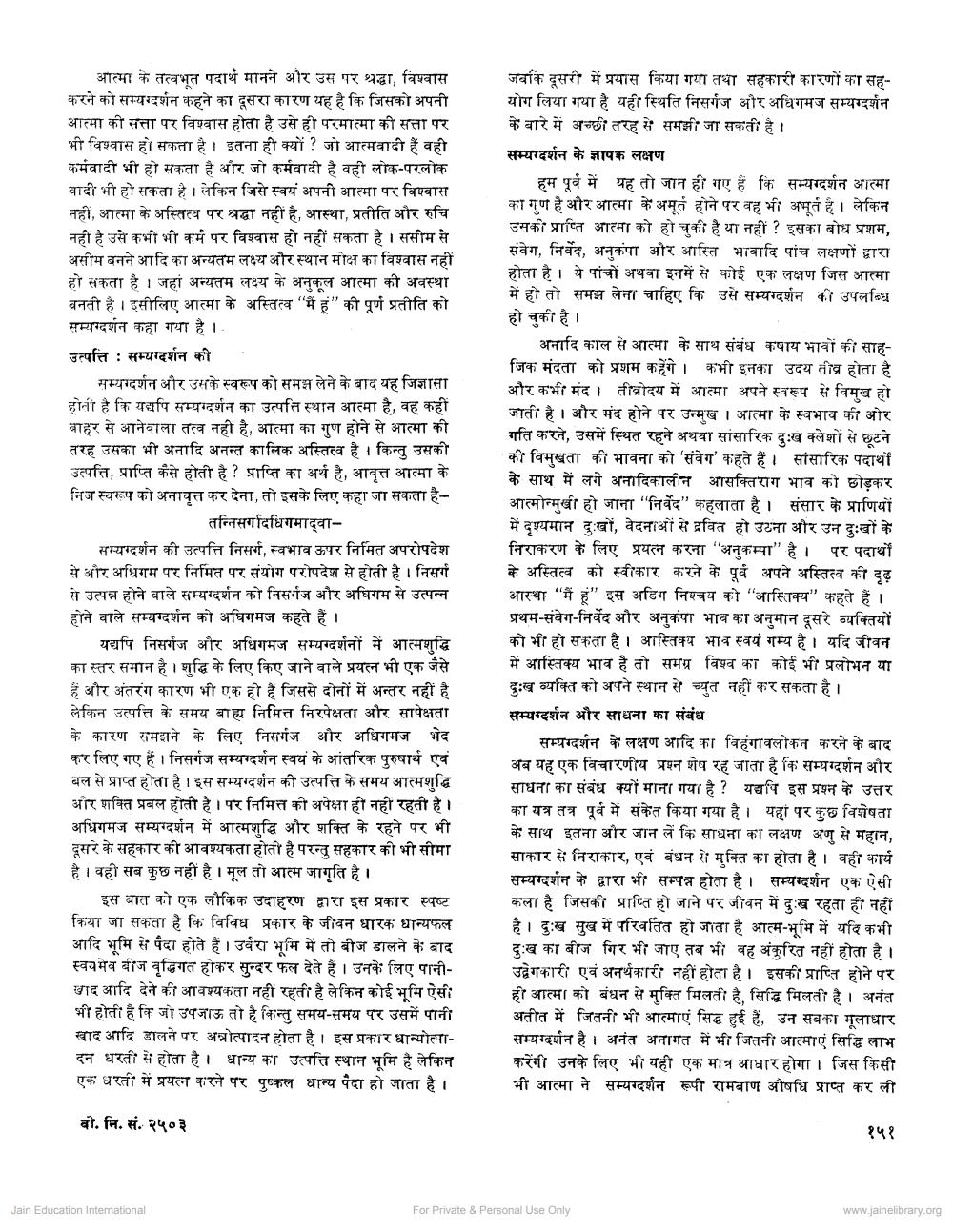________________
आत्मा के तत्वभूत पदार्थ मानने और उस पर श्रद्धा, विश्वास करने को सम्यग्दर्शन कहने का दूसरा कारण यह है कि जिसको अपनी आत्मा की सत्ता पर विश्वास होता है उसे ही परमात्मा की सत्ता पर भी विश्वास हो सकता है। इतना ही क्यों? जो आत्मवादी हैं वही कर्मवादी भी हो सकता है और जो कर्मवादी है वही लोक-परलोक वादी भी हो सकता है। लेकिन जिसे स्वयं अपनी आत्मा पर विश्वास नहीं, आत्मा के अस्तित्व पर श्रद्धा नहीं है, आस्था, प्रतीति और रुचि नहीं है उसे कभी भी कर्म पर विश्वास हो नहीं सकता है । ससीम से असीम बनने आदि का अन्यतम लक्ष्य और स्थान मोक्ष का विश्वास नहीं हो सकता है । जहां अन्यतम लक्ष्य के अनुकूल आत्मा की अवस्था बनती है। इसीलिए आत्मा के अस्तित्व "मैं हूं" की पूर्ण प्रतीति को सम्यग्दर्शन कहा गया है। उत्पत्ति : सम्यग्दर्शन की
सम्यग्दर्शन और उसके स्वरूप को समझ लेने के बाद यह जिज्ञासा होती है कि यद्यपि सम्यग्दर्शन का उत्पत्ति स्थान आत्मा है, वह कहीं बाहर से आनेवाला तत्व नहीं है, आत्मा का गुण होने से आत्मा की तरह उसका भी अनादि अनन्त कालिक अस्तित्व है । किन्तु उसकी उत्पत्ति, प्राप्ति कैसे होती है ? प्राप्ति का अर्थ है, आवृत्त आत्मा के निज स्वरूप को अनावृत्त कर देना, तो इसके लिए कहा जा सकता है
तन्निसर्गादधिगमाद्वासम्यग्दर्शन की उत्पत्ति निसर्ग, स्वभाव ऊपर निर्मित अपरोपदेश से और अधिगम पर निर्मित पर संयोग परोपदेश से होती है । निसर्ग से उत्पन्न होने वाले सम्यग्दर्शन को निसर्गज और अधिगम से उत्पन्न होने वाले सम्यग्दर्शन को अधिगमज कहते हैं ।
यद्यपि निसर्गज और अधिगमज सम्यग्दर्शनों में आत्मशुद्धि का स्तर समान है। शुद्धि के लिए किए जाने वाले प्रयत्न भी एक जैसे हैं और अंतरंग कारण भी एक ही हैं जिससे दोनों में अन्तर नहीं है लेकिन उत्पत्ति के समय बाह्य निमित्त निरपेक्षता और सापेक्षता के कारण समझने के लिए निसर्गज और अधिगमज भेद कर लिए गए हैं । निसर्गज सम्यग्दर्शन स्वयं के आंतरिक पुरुषार्थ एवं बल से प्राप्त होता है। इस सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति के समय आत्मशुद्धि और शक्ति प्रबल होती है। पर निमित्त की अपेक्षा ही नहीं रहती है। अधिगमज सम्यग्दर्शन में आत्मशुद्धि और शक्ति के रहने पर भी दूसरे के सहकार की आवश्यकता होती है परन्तु सहकार की भी सीमा है । वही सब कुछ नहीं है । मूल तो आत्म जागृति है।
इस बात को एक लौकिक उदाहरण द्वारा इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि विविध प्रकार के जीवन धारक धान्यफल आदि भूमि से पैदा होते हैं । उर्वरा भूमि में तो बीज डालने के बाद स्वयमेव बीज वृद्धिगत होकर सुन्दर फल देते हैं । उनके लिए पानीखाद आदि देने की आवश्यकता नहीं रहती है लेकिन कोई भूमि ऐसी भी होती है कि जो उपजाऊ तो है किन्तु समय-समय पर उसमें पानी खाद आदि डालने पर अन्नोत्पादन होता है। इस प्रकार धान्योत्पादन धरती से होता है। धान्य का उत्पत्ति स्थान भूमि है लेकिन एक धरती में प्रयत्न करने पर पुष्कल धान्य पैदा हो जाता है।
जबकि दूसरी में प्रयास किया गया तथा सहकारी कारणों का सहयोग लिया गया है यही स्थिति निसर्गज और अधिगमज सम्यग्दर्शन के बारे में अच्छी तरह से समझी जा सकती है। सम्यग्दर्शन के ज्ञापक लक्षण
हम पूर्व में यह तो जान ही गए हैं कि सम्यग्दर्शन आत्मा का गुण है और आत्मा के अमूर्त होने पर वह भी अमूर्त है । लेकिन उसकी प्राप्ति आत्मा को हो चुकी है या नहीं? इसका बोध प्रशम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्ति भावादि पांच लक्षणों द्वारा होता है। ये पांचों अथवा इनमें से कोई एक लक्षण जिस आत्मा में हो तो समझ लेना चाहिए कि उसे सम्यग्दर्शन की उपलब्धि हो चुकी है।
अनादि काल से आत्मा के साथ संबंध कषाय भावों की साहजिक मंदता को प्रशम कहेंगे। कभी इनका उदय तीव्र होता है और कभी मंद। तीवोदय में आत्मा अपने स्वरूप से विमुख हो जाती है। और मंद होने पर उन्मुख । आत्मा के स्वभाव की ओर गति करने, उसमें स्थित रहने अथवा सांसारिक दुःख क्लेशों से छूटने की विमुखता की भावना को 'संवेग' कहते हैं। सांसारिक पदार्थों के साथ में लगे अनादिकालीन आसक्तिराग भाव को छोड़कर आत्मोन्मुखी हो जाना "निर्वेद" कहलाता है। संसार के प्राणियों में दश्यमान दुःखों, वेदनाओं से द्रवित हो उठना और उन दुःखों के निराकरण के लिए प्रयत्न करना "अनुकम्पा" है। पर पदार्थों के अस्तित्व को स्वीकार करने के पूर्व अपने अस्तित्व की दृढ़ आस्था "मैं हूं" इस अडिग निश्चय को "आस्तिक्य" कहते हैं । प्रथम-संवेग-निर्वेद और अनुकंपा भाव का अनुमान दूसरे व्यक्तियों को भी हो सकता है। आस्तिक्य भाव स्वयं गम्य है। यदि जीवन में आस्तिक्य भाव है तो समग्र विश्व का कोई भी प्रलोभन या दुःख व्यक्ति को अपने स्थान से च्युत नहीं कर सकता है। सम्यग्दर्शन और साधना का संबंध
सम्यग्दर्शन के लक्षण आदि का विहंगावलोकन करने के बाद अब यह एक विचारणीय प्रश्न शेष रह जाता है कि सम्यग्दर्शन और साधना का संबंध क्यों माना गया है ? यद्यपि इस प्रश्न के उत्तर का यत्र तत्र पूर्व में संकेत किया गया है। यहां पर कुछ विशेषता के साथ इतना और जान लें कि साधना का लक्षण अणु से महान, साकार से निराकार, एवं बंधन से मुक्ति का होता है। वहीं कार्य सम्यग्दर्शन के द्वारा भी सम्पन्न होता है। सम्यग्दर्शन एक ऐसी कला है जिसकी प्राप्ति हो जाने पर जीवन में दुःख रहता ही नहीं है। दुःख सुख में परिवर्तित हो जाता है आत्म-भूमि में यदि कभी दुःख का बीज गिर भी जाए तब भी वह अंकुरित नहीं होता है। उद्वेगकारी एवं अनर्थकारी नहीं होता है। इसकी प्राप्ति होने पर ही आत्मा को बंधन से मुक्ति मिलती है, सिद्धि मिलती है। अनंत अतीत में जितनी भी आत्माएं सिद्ध हुई हैं, उन सबका मूलाधार सम्यग्दर्शन है। अनंत अनागत में भी जितनी आत्माएं सिद्धि लाभ करेंगी उनके लिए भी यही एक मात्र आधार होगा। जिस किसी भी आत्मा ने सम्यग्दर्शन रूपी रामबाण औषधि प्राप्त कर ली
वो. नि. सं. २५०३
१५१
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org