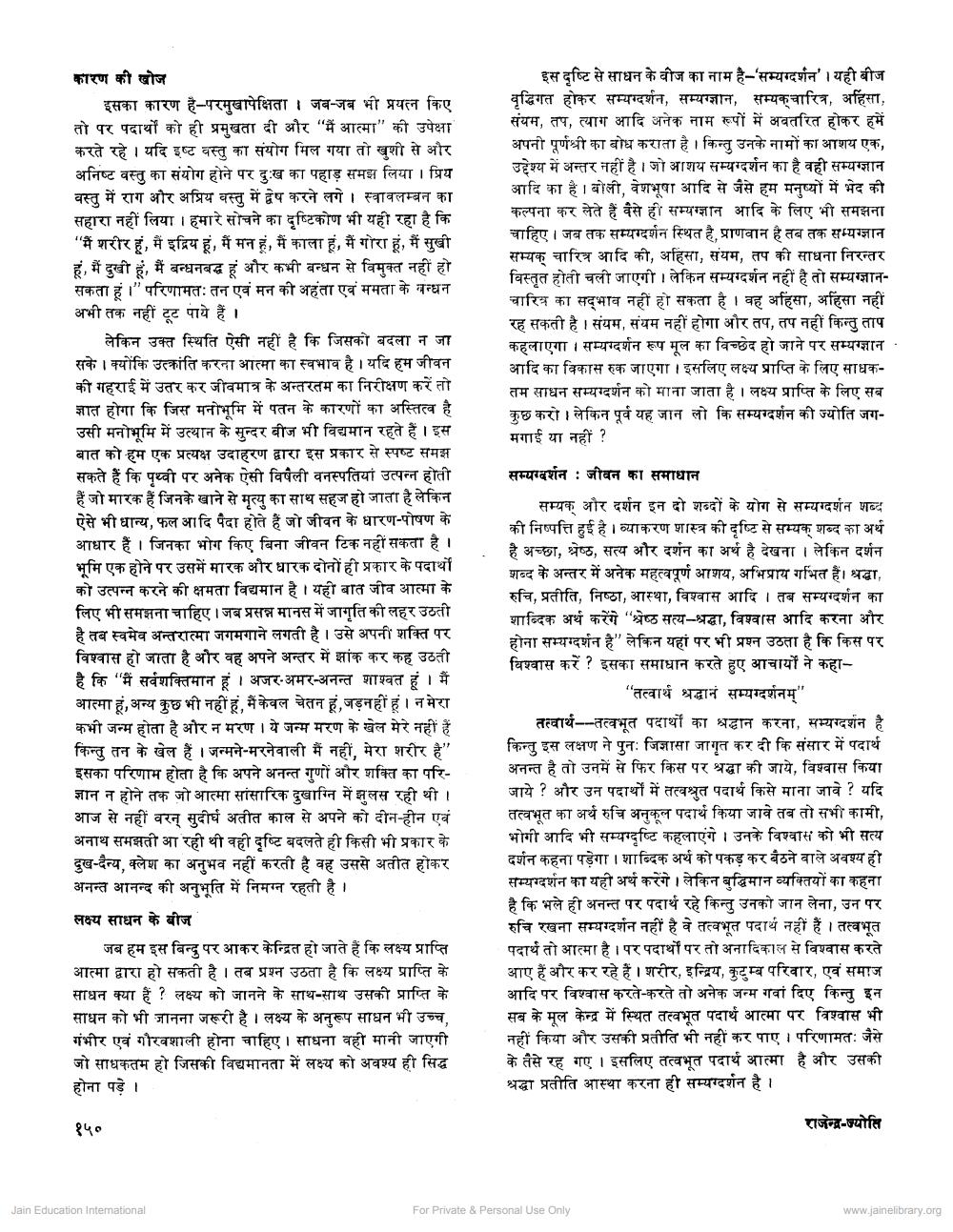________________
कारण की खोज
इसका कारण है - परमुखापेक्षिता । जब जब भी प्रयत्न किए तो पर पदार्थों को ही प्रमुखता दी और "मैं आत्मा" की उपेक्षा' करते रहे । यदि इष्ट वस्तु का संयोग मिल गया तो खुशी से और अनिष्ट वस्तु का संयोग होने पर दुःख का पहाड़ समझ लिया । प्रिय वस्तु में राग और अप्रिय वस्तु में द्वेष करने लगे। स्वावलम्बन का सहारा नहीं लिया । हमारे सोचने का दृष्टिकोण भी यही रहा है कि "मैं शरीर हूं, मैं इद्रिय हूं, मैं मन हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूँ, मैं बन्धनबद्ध हूं और कभी बन्धन से विमुक्त नहीं हो सकता हूं ।" परिणामतः तन एवं मन की अहंता एवं ममता के बन्धन अभी तक नहीं टूट पाये हैं ।
लेकिन उक्त स्थिति ऐसी नहीं है कि जिसको बदला न जा सके। क्योंकि उत्क्रांति करना आत्मा का स्वभाव है। यदि हम जीवन की गहराई में उतर कर जीवमात्र के अन्तरतम का निरीक्षण करें तो ज्ञात होगा कि जिस मनोभूमि में पतन के कारणों का अस्तित्व है उसी मनोभूमि में उत्थान के सुन्दर बीज भी विद्यमान रहते हैं । इस बात को हम एक प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा इस प्रकार से स्पष्ट समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर अनेक ऐसी विषैली वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं जो मारक हैं जिनके खाने से मृत्यु का साथ सहज हो जाता है लेकिन ऐसे भी धान्य, फल आदि पैदा होते हैं जो जीवन के धारण-पोषण के आधार हैं। जिनका भोग किए बिना जीवन टिक नहीं सकता है । भूमि एक होने पर उसमें मारक और धारक दोनों ही प्रकार के पदार्थों को उत्पन्न करने की क्षमता विद्यमान है। यही बात जीव आत्मा के लिए भी समझना चाहिए। जब प्रसन्न मानस में जागृति की लहर उठती है तब स्वमेव अन्तरात्मा जगमगाने लगती है । उसे अपनी शक्ति पर विश्वास हो जाता है और वह अपने अन्तर में झांक कर कह उठती है कि " में सर्वशक्तिमान हूं । अजर-अमर - अनन्त शाश्वत हूं । मैं आत्मा है, अन्य कुछ भी नहीं हूं. मैं केवल चेतन है, नहीं है। नमेरा कभी जन्म होता है और न मरण । ये जन्म मरण के खेल मेरे नहीं हैं। किन्तु तन के खेल हैं। जन्मने मरनेवाली में नहीं, मेरा शरीर है" इसका परिणाम होता है कि अपने अनन्त गुणों और शक्ति का परिज्ञान न होने तक जो आत्मा सांसारिक दुखाग्नि में झुलस रही थी । आज से नहीं वरन् सुदीर्घ अतीत काल से अपने को दीन-हीन एवं अनाथ समझती आ रही थी वही दृष्टि बदलते ही किसी भी प्रकार के दुख-दैन्य, क्लेश का अनुभव नहीं करती है वह उससे अतीत होकर अनन्त आनन्द की अनुभूति में निमग्न रहती है ।
लक्ष्य साधन के बीज
जब हम इस बिन्दु पर आकर केन्द्रित हो जाते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति आत्मा द्वारा हो सकती है । तब प्रश्न उठता है कि लक्ष्य प्राप्ति के साधन क्या हैं? लक्ष्य को जानने के साथ-साथ उसकी प्राप्ति के साधन को भी जानना जरूरी है । लक्ष्य के अनुरूप साधन भी उच्च, गंभीर एवं गौरवशाली होना चाहिए। साधना वही मानी जाएगी। जो साधकतम हो जिसकी विद्यमानता में लक्ष्य को अवश्य ही सिद्ध होना पड़े ।
१५०
Jain Education International
इस दृष्टि से साधन के बीज का नाम है- 'सम्यग्दर्शन' । यही बीज वृद्धिगत होकर सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्र, अहिंसा, संयम, तप, त्याग आदि अनेक नाम रूपों में अवतरित होकर हमें अपनी पूर्णश्री का बोध कराता है। किन्तु उनके नामों का आशय एक, उद्देश्य में अन्तर नहीं है। जो आशय सम्यग्दर्शन का है वही सम्यग्ज्ञान आदि का हैं। बोली, वेशभूषा आदि से जैसे हम मनुष्यों में भेद की कल्पना कर लेते हैं वैसे ही सम्यग्ज्ञान आदि के लिए भी समझना चाहिए । जब तक सम्यग्दर्शन स्थित है, प्राणवान है तब तक सम्यग्ज्ञान सम्यक् चारित्र आदि की, अहिंसा, संयम, तप की साधना निरन्तर विस्तृत होती चली जाएगी। लेकिन सम्यग्दर्शन नहीं है तो सम्यग्ज्ञानचारि का सद्भाव नहीं हो सकता है। वह अहिंसा, अहिंसा नहीं रह सकती है । संयम, संयम नहीं होगा और तप, तप नहीं किन्तु ताप कहलाएगा । सम्यग्दर्शन रूप मूल का विच्छेद हो जाने पर सम्यग्ज्ञान आदि का विकास रुक जाएगा। इसलिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधकतम साधन सम्यग्दर्शन को माना जाता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सब कुछ करो। लेकिन पूर्व यह जान लो कि सम्यग्दर्शन की ज्योति जगमगाई या नहीं ?
सम्यग्दर्शन : जीवन का समाधान
सम्यक् और दर्शन इन दो शब्दों के योग से सम्यग्दर्शन शब्द की निष्पत्ति हुई है । व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से सम्यक् शब्द का अर्थ है अच्छा, श्रेष्ठ, सत्य और दर्शन का अर्थ है देखना । लेकिन दर्शन शब्द के अन्तर में अनेक महत्वपूर्ण आशय, अभिप्राय गर्भित हैं। श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, निष्ठा, आस्था, विश्वास आदि । तब सम्यग्दर्शन का शाब्दिक अर्थ करेंगे "श्रेष्ठ सत्य-श्रद्धा, विश्वास आदि करना और होना सम्यग्दर्शन है" लेकिन यहां पर भी प्रश्न उठता है कि किस पर विश्वास करें ? इसका समाधान करते हुए आचार्यों ने कहा
"तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् "
तत्वार्थ -- तत्वभूत पदार्थों का श्रद्धान करना, सम्यग्दर्शन है किन्तु इस लक्षण ने पुनः जिज्ञासा जागृत कर दी कि संसार में पदार्थ अनन्त है तो उनमें से फिर किस पर श्रद्धा की जाये, विश्वास किया जाये ? और उन पदार्थों में तत्वश्रुत पदार्थ किसे माना जावे ? यदि तत्वभूत का अर्थ रुचि अनुकूल पदार्थ किया जावे तब तो सभी कामी, भोगी आदि भी सम्यग्दृष्टि कहलाएंगे। उनके विश्वास की भी सत्य दर्शन कहना पड़ेगा। शाब्दिक अर्थ को पकड़ कर बैठने वाले अवश्य ही सम्यग्दर्शन का यही अर्थ करेंगे लेकिन बुद्धिमान व्यक्तियों का कहना है कि भले ही अनन्त पर पदार्थ रहे किन्तु उनको जान लेना, उन पर रुचि रखना सम्यग्दर्शन नहीं है वे तत्वभूत पदार्थ नहीं हैं। तस्वभूत पदार्थ तो आत्मा है । पर पदार्थों पर तो अनादिकाल से विश्वास करते आए हैं और कर रहे हैं । शरीर, इन्द्रिय, कुटुम्ब परिवार, एवं समाज आदि पर विश्वास करते-करते तो अनेक जन्म गवां दिए किन्तु इन सब के मूल केन्द्र में स्थित तत्वभूत पदार्थ आत्मा पर विश्वास भी नहीं किया और उसकी प्रतीति भी नहीं कर पाए । परिणामतः जैसे के तैसे रह गए । इसलिए तत्वभूत पदार्थ आत्मा है और उसकी श्रद्धा प्रतीति आस्था करना ही सम्यग्दर्शन है ।
For Private & Personal Use Only
राजेन्द्र- ज्योति
www.jainelibrary.org