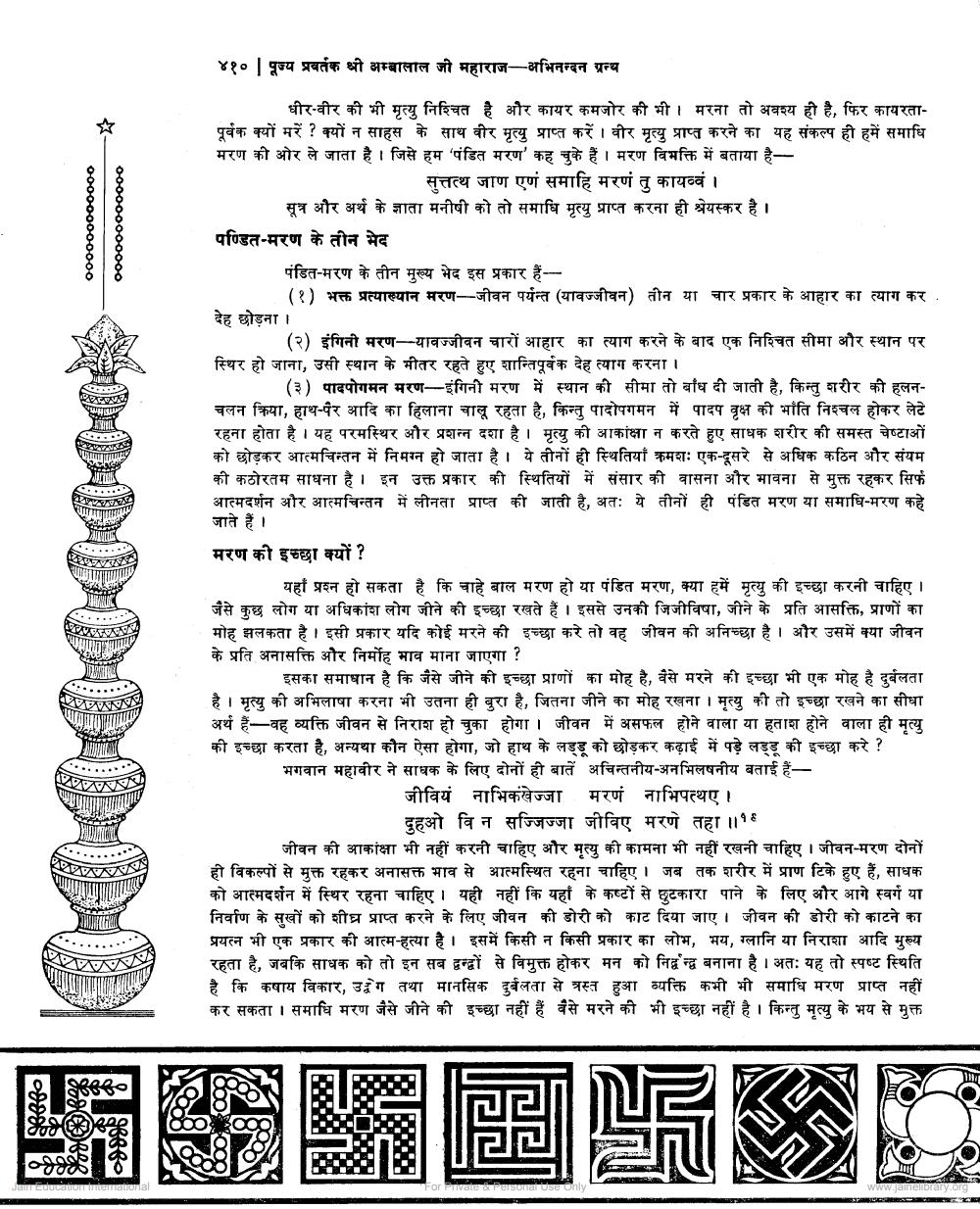________________
४१० | पूज्य प्रवर्तक श्री अम्बालाल जी महाराज-अभिनन्दन ग्रन्थ
000000000000
000000000000
MHAR
a
स
धीर-वीर की भी मृत्यु निश्चित है और कायर कमजोर की भी। मरना तो अवश्य ही है, फिर कायरतापूर्वक क्यों मरें ? क्यों न साहस के साथ वीर मृत्यु प्राप्त करें। वीर मृत्यु प्राप्त करने का यह संकल्प ही हमें समाधि मरण की ओर ले जाता है । जिसे हम 'पंडित मरण' कह चुके हैं । मरण विभक्ति में बताया है
सुत्तत्थ जाण एणं समाहि मरणं तु कायव्वं । सूत्र और अर्थ के ज्ञाता मनीषी को तो समाधि मृत्यु प्राप्त करना ही श्रेयस्कर है। पण्डित-मरण के तीन भेद
पंडित-मरण के तीन मुख्य भेद इस प्रकार हैं
(१) भक्त प्रत्याख्यान मरण-जीवन पर्यन्त (यावज्जीवन) तीन या चार प्रकार के आहार का त्याग कर . देह छोड़ना।
(२) इंगिनी मरण-यावज्जीवन चारों आहार का त्याग करने के बाद एक निश्चित सीमा और स्थान पर स्थिर हो जाना, उसी स्थान के भीतर रहते हुए शान्तिपूर्वक देह त्याग करना ।
(३) पादपोगमन मरण-इंगिनी मरण में स्थान की सीमा तो बाँध दी जाती है, किन्तु शरीर की हलनचलन क्रिया, हाथ-पैर आदि का हिलाना चालू रहता है, किन्तु पादोपगमन में पादप वृक्ष की भांति निश्चल होकर लेटे रहना होता है । यह परमस्थिर और प्रशन्न दशा है। मृत्यु की आकांक्षा न करते हुए साधक शरीर की समस्त चेष्टाओं को छोड़कर आत्मचिन्तन में निमग्न हो जाता है। ये तीनों ही स्थितियाँ क्रमशः एक-दूसरे से अधिक कठिन और संयम की कठोरतम साधना है। इन उक्त प्रकार की स्थितियों में संसार की वासना और भावना से मुक्त रहकर सिर्फ आत्मदर्शन और आत्मचिन्तन में लीनता प्राप्त की जाती है, अत: ये तीनों ही पंडित मरण या समाधि-मरण कहे जाते हैं। मरण की इच्छा क्यों?
यहाँ प्रश्न हो सकता है कि चाहे बाल मरण हो या पंडित मरण, क्या हमें मृत्यु की इच्छा करनी चाहिए। जैसे कुछ लोग या अधिकांश लोग जीने की इच्छा रखते हैं। इससे उनकी जिजीविषा, जीने के प्रति आसक्ति, प्राणों का मोह झलकता है। इसी प्रकार यदि कोई मरने की इच्छा करे तो वह जीवन की अनिच्छा है। और उसमें क्या जीवन के प्रति अनासक्ति और निर्मोह भाव माना जाएगा?
इसका समाधान है कि जैसे जीने की इच्छा प्राणों का मोह है, वैसे मरने की इच्छा भी एक मोह है दुर्बलता है । मृत्यु की अभिलाषा करना भी उतना ही बुरा है, जितना जीने का मोह रखना । मृत्यु की तो इच्छा रखने का सीधा अर्थ हैं-वह व्यक्ति जीवन से निराश हो चुका होगा। जीवन में असफल होने वाला या हताश होने वाला ही मृत्यु की इच्छा करता है, अन्यथा कौन ऐसा होगा, जो हाथ के लड्डू को छोड़कर कढ़ाई में पड़े लड्डू की इच्छा करे ? भगवान महावीर ने साधक के लिए दोनों ही बातें अचिन्तनीय-अनभिलषनीय बताई हैं
जीवियं नाभिकखेज्जा मरणं नाभिपत्थए।
दुहओ विन सज्जिज्जा जीविए मरणे तहा ॥१६ जीवन की आकांक्षा भी नहीं करनी चाहिए और मृत्यु की कामना भी नहीं रखनी चाहिए । जीवन-मरण दोनों ही विकल्पों से मुक्त रहकर अनासक्त भाव से आत्मस्थित रहना चाहिए। जब तक शरीर में प्राण टिके हुए हैं, साधक को आत्मदर्शन में स्थिर रहना चाहिए। यही नहीं कि यहाँ के कष्टों से छुटकारा पाने के लिए और आगे स्वर्ग या निर्वाण के सुखों को शीघ्र प्राप्त करने के लिए जीवन की डोरी को काट दिया जाए। जीवन की डोरी को काटने का प्रयत्न भी एक प्रकार की आत्म-हत्या है। इसमें किसी न किसी प्रकार का लोभ, भय, ग्लानि या निराशा आदि मुख्य रहता है, जबकि साधक को तो इन सब द्वन्द्वों से विमुक्त होकर मन को निर्द्वन्द्व बनाना है । अत: यह तो स्पष्ट स्थिति है कि कषाय विकार, उद्वेग तथा मानसिक दुर्बलता से त्रस्त हुआ व्यक्ति कभी भी समाधि मरण प्राप्त नहीं कर सकता । समाधि मरण जैसे जीने की इच्छा नहीं हैं वैसे मरने की भी इच्छा नहीं है । किन्तु मृत्यु के भय से मुक्त
CO300
MERA
म्या
Jan Education international
For PrivatePersar
only
www.jamenbally.org नाम