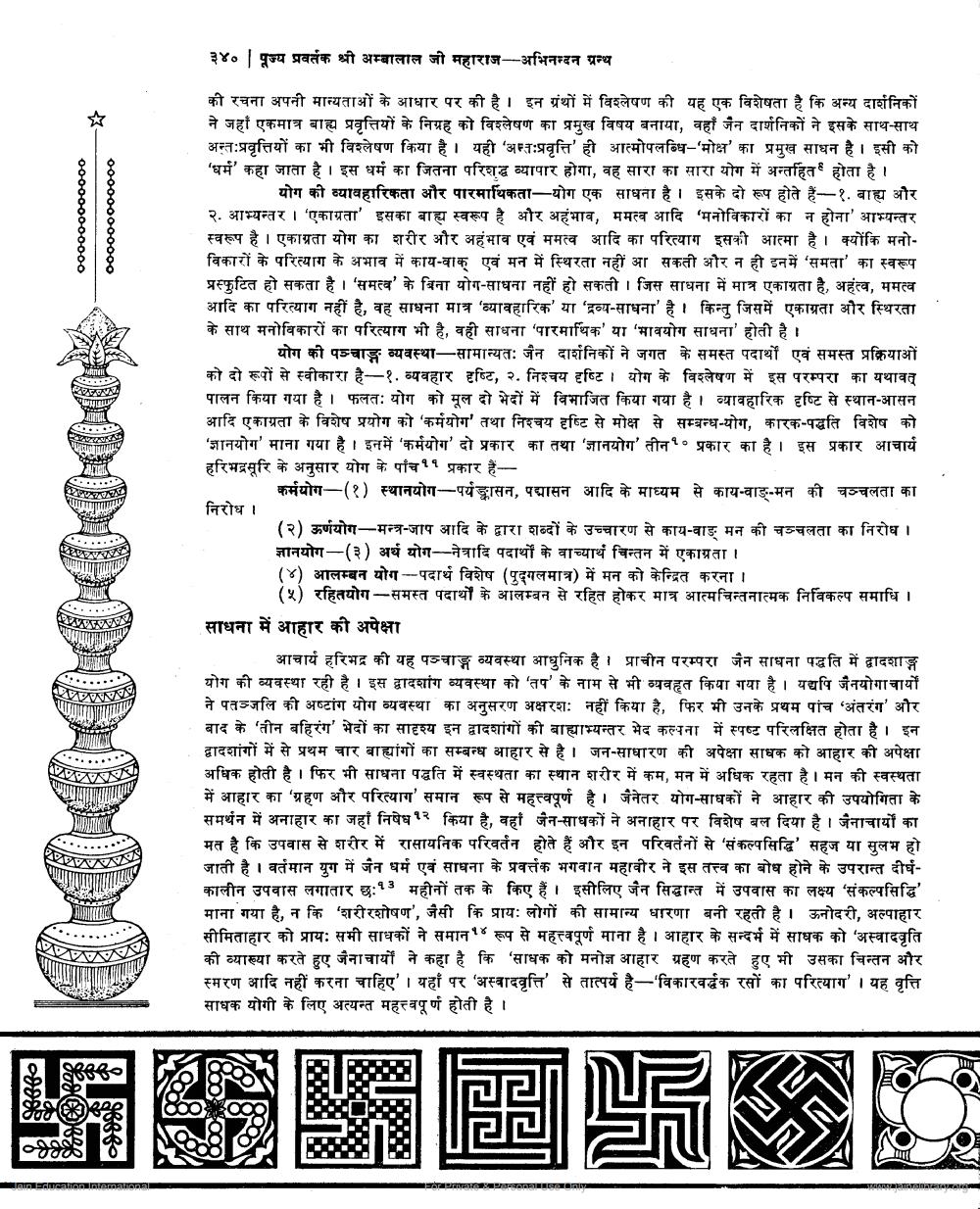________________
३४० | पूज्य प्रवर्तक श्री अम्बालाल जी महाराज-अभिनन्दन ग्रन्थ
000000000000
००००००००००००
A
ARTIL
RAN
TITION
की रचना अपनी मान्यताओं के आधार पर की है। इन ग्रंथों में विश्लेषण की यह एक विशेषता है कि अन्य दार्शनिकों ने जहाँ एकमात्र बाह्य प्रवृत्तियों के निग्रह को विश्लेषण का प्रमुख विषय बनाया, वहाँ जैन दार्शनिकों ने इसके साथ-साथ अन्तःप्रवृत्तियों का भी विश्लेषण किया है। यही 'अन्तःप्रवृत्ति' ही आत्मोपलब्धि-'मोक्ष' का प्रमुख साधन है। इसी को 'धर्म' कहा जाता है । इस धर्म का जितना परिशद्ध व्यापार होगा, वह सारा का सारा योग में अन्तर्हित होता है।
योग की व्यावहारिकता और पारमार्थिकता-योग एक साधना है। इसके दो रूप होते हैं-१. बाह्य और २. आभ्यन्तर । 'एकाग्रता' इसका बाह्य स्वरूप है और अहंभाव, ममत्व आदि 'मनोविकारों का न होना' आभ्यन्तर स्वरूप है । एकाग्रता योग का शरीर और अहंभाव एवं ममत्व आदि का परित्याग इसकी आत्मा है। क्योंकि मनोविकारों के परित्याग के अभाव में काय-वाक् एवं मन में स्थिरता नहीं आ सकती और न ही इनमें 'समता' का स्वरूप प्रस्फुटित हो सकता है । 'समत्व' के बिना योग-साधना नहीं हो सकती । जिस साधना में मात्र एकाग्रता है, अहंत्व, ममत्व आदि का परित्याग नहीं है, वह साधना मात्र 'व्यावहारिक' या 'द्रव्य-साधना' है। किन्तु जिसमें एकाग्रता और स्थिरता के साथ मनोविकारों का परित्याग भी है, वही साधना 'पारमार्थिक' या 'मावयोग साधना' होती है।
योग को पञ्चाङ्ग व्यवस्था सामान्यतः जैन दार्शनिकों ने जगत के समस्त पदार्थों एवं समस्त प्रक्रियाओं को दो रूपों से स्वीकारा है-१. व्यवहार दृष्टि, २. निश्चय दृष्टि । योग के विश्लेषण में इस परम्परा का यथावत् पालन किया गया है। फलत: योग को मूल दो भेदों में विभाजित किया गया है। व्यावहारिक दृष्टि से स्थान-आसन आदि एकाग्रता के विशेष प्रयोग को 'कर्मयोग' तथा निश्चय दृष्टि से मोक्ष से सम्बन्ध-योग, कारक-पद्धति विशेष को 'ज्ञानयोग' माना गया है। इनमें 'कर्मयोग' दो प्रकार का तथा 'ज्ञानयोग' तीन प्रकार का है। इस प्रकार आचार्य हरिभद्रसूरि के अनुसार योग के पाँच११ प्रकार हैं
कर्मयोग-(१) स्थानयोग-पर्यङ्कासन, पद्मासन आदि के माध्यम से काय-वाङ्-मन की चञ्चलता का निरोध ।
(२) ऊर्णयोग-मन्त्र-जाप आदि के द्वारा शब्दों के उच्चारण से काय-वाङ् मन की चञ्चलता का निरोध । ज्ञानयोग-(३) अर्थ योग-नेवादि पदार्थों के वाच्यार्थ चिन्तन में एकाग्रता । (४) आलम्बन योग-पदार्थ विशेष (पूगलमात्र) में मन को केन्द्रित करना ।
(५) रहितयोग-समस्त पदार्थों के आलम्बन से रहित होकर मात्र आत्मचिन्तनात्मक निविकल्प समाधि । साधना में आहार की अपेक्षा
आचार्य हरिभद्र की यह पञ्चाङ्ग व्यवस्था आधुनिक है। प्राचीन परम्परा जैन साधना पद्धति में द्वादशाङ्ग योग की व्यवस्था रही है। इस द्वादशांग व्यवस्था को 'तप' के नाम से भी व्यवहृत किया गया है। यद्यपि जैनयोगाचार्यों ने पतञ्जलि की अष्टांग योग व्यवस्था का अनुसरण अक्षरशः नहीं किया है, फिर भी उनके प्रथम पांच 'अंतरंग' और बाद के 'तीन बहिरंग' भेदों का सादृश्य इन द्वादशांगों की बाह्याभ्यन्तर भेद कल्पना में स्पष्ट परिलक्षित होता है। इन द्वादशांगों में से प्रथम चार बाह्यांगों का सम्बन्ध आहार से है। जन-साधारण की अपेक्षा साधक को आहार की अपेक्षा अधिक होती है। फिर भी साधना पद्धति में स्वस्थता का स्थान शरीर में कम, मन में अधिक रहता है। मन की स्वस्थता में आहार का 'ग्रहण और परित्याग' समान रूप से महत्त्वपूर्ण है। जैनेतर योग-साधकों ने आहार की उपयोगिता के समर्थन में अनाहार का जहाँ निषेध१२ किया है, वहाँ जैन-साधकों ने अनाहार पर विशेष बल दिया है। जैनाचार्यों का मत है कि उपवास से शरीर में रासायनिक परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों से 'संकल्पसिद्धि' सहज या सुलभ हो जाती है। वर्तमान युग में जैन धर्म एवं साधना के प्रवर्तक भगवान महावीर ने इस तत्त्व का बोध होने के उपरान्त दीर्घकालीन उपवास लगातार छ:१३ महीनों तक के किए हैं। इसीलिए जैन सिद्धान्त में उपवास का लक्ष्य 'संकल्पसिद्धि' माना गया है, न कि 'शरीरशोषण', जैसी कि प्रायः लोगों की सामान्य धारणा बनी रहती है। ऊनोदरी, अल्पाहार सीमिताहार को प्रायः सभी साधकों ने समान ४ रूप से महत्त्वपूर्ण माना है । आहार के सन्दर्भ में साधक को 'अस्वादवृति की व्याख्या करते हुए जैनाचार्यों ने कहा है कि 'साधक को मनोज्ञ आहार ग्रहण करते हुए भी उसका चिन्तन और स्मरण आदि नहीं करना चाहिए'। यहाँ पर 'अस्वादवृत्ति' से तात्पर्य है-'विकारवर्द्धक रसों का परित्याग' । यह वृत्ति साधक योगी के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती है ।
00088
.
Pal200 UUUUK
..
Radmaansaamaa
TAT RANSPORTERRA