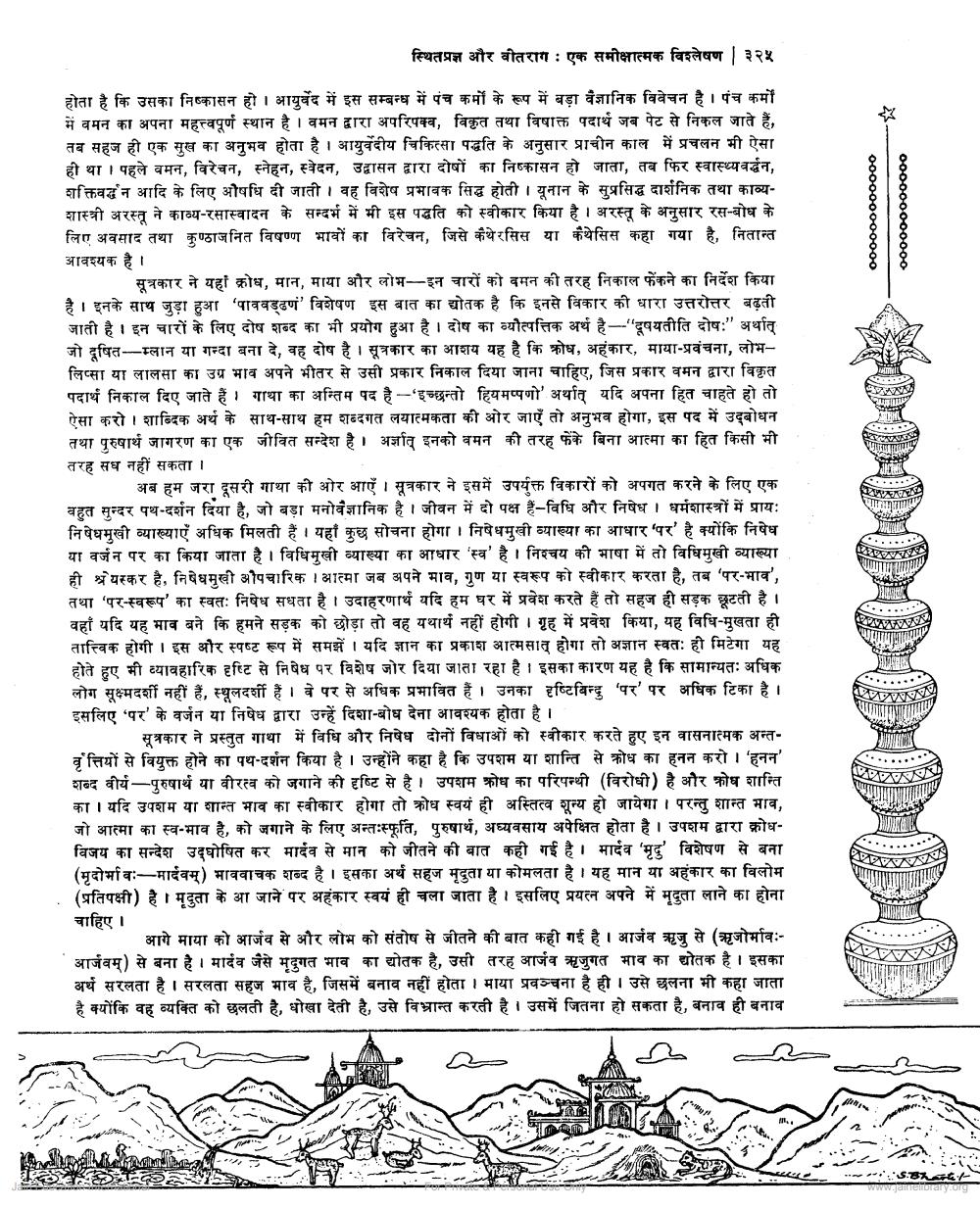________________
स्थितप्रज्ञ और वीतराग : एक समीक्षात्मक विश्लेषण | ३२५
००००००००००००
००००००००००००
RAWHA
CILMS
HTMINS
CRPATTER
होता है कि उसका निष्कासन हो । आयुर्वेद में इस सम्बन्ध में पंच कर्मों के रूप में बड़ा वैज्ञानिक विवेचन है । पंच कर्मों में वमन का अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है । वमन द्वारा अपरिपक्व, विकृत तथा विषाक्त पदार्थ जब पेट से निकल जाते हैं, तब सहज ही एक सुख का अनुभव होता है । आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति के अनुसार प्राचीन काल में प्रचलन भी ऐसा ही था। पहले वमन, विरेचन, स्नेहन, स्वेदन, उद्वासन द्वारा दोषों का निष्कासन हो जाता, तब फिर स्वास्थ्यवर्द्धन, शक्तिवर्द्धन आदि के लिए औषधि दी जाती। वह विशेष प्रभावक सिद्ध होती । यूनान के सुप्रसिद्ध दार्शनिक तथा काव्यशास्त्री अरस्तू ने काव्य-रसास्वादन के सन्दर्भ में भी इस पद्धति को स्वीकार किया है । अरस्तू के अनुसार रस-बोध के लिए अवसाद तथा कुण्ठाजनित विषण्ण भावों का विरेचन, जिसे कैथेरसिस या कैथेसिस कहा गया है, नितान्त आवश्यक है।
सूत्रकार ने यहां क्रोध, मान, माया और लोभ-इन चारों को दमन की तरह निकाल फेंकने का निर्देश किया है। इनके साथ जुड़ा हुआ 'पाववड्ढणं' विशेषण इस बात का द्योतक है कि इनसे विकार की धारा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है । इन चारों के लिए दोष शब्द का भी प्रयोग हुआ है । दोष का व्योत्पत्तिक अर्थ है-"दूषयतीति दोषः" अर्थात् जो दूषित-म्लान या गन्दा बना दे, वह दोष है। सूत्रकार का आशय यह है कि क्रोध, अहंकार, माया-प्रवंचना, लोभलिप्सा या लालसा का उग्र भाव अपने भीतर से उसी प्रकार निकाल दिया जाना चाहिए, जिस प्रकार वमन द्वारा विकृत पदार्थ निकाल दिए जाते हैं। गाथा का अन्तिम पद है -'इच्छन्तो हियमप्पणो' अर्थात् यदि अपना हित चाहते हो तो ऐसा करो । शाब्दिक अर्थ के साथ-साथ हम शब्दगत लयात्मकता की ओर जाएँ तो अनुभव होगा, इस पद में उद्बोधन तथा पुरुषार्थ जागरण का एक जीवित सन्देश है। अर्शात् इनको वमन की तरह फेंके बिना आत्मा का हित किसी भी तरह सध नहीं सकता।
अब हम जरा दूसरी गाथा की ओर आएँ । सूत्रकार ने इसमें उपर्युक्त विकारों को अपगत करने के लिए एक बहुत सुन्दर पथ-दर्शन दिया है, जो बड़ा मनोवैज्ञानिक है । जीवन में दो पक्ष हैं-विधि और निषेध । धर्मशास्त्रों में प्रायः निषेधमुखी व्याख्याएँ अधिक मिलती हैं । यहाँ कुछ सोचना होगा । निषेधमुखी व्याख्या का आधार 'पर' है क्योंकि निषेध या वर्जन पर का किया जाता है। विधिमुखी व्याख्या का आधार 'स्व' है। निश्चय की भाषा में तो विधिमुखी व्याख्या ही श्रेयस्कर है, निषेधमुखी औपचारिक । आत्मा जब अपने माव, गुण या स्वरूप को स्वीकार करता है, तब 'पर-भाव', तथा 'पर-स्वरूप' का स्वतः निषेध सधता है। उदाहरणार्थ यदि हम घर में प्रवेश करते हैं तो सहज ही सड़क छूटती है। वहाँ यदि यह भाव बने कि हमने सड़क को छोड़ा तो वह यथार्थ नहीं होगी । गृह में प्रवेश किया, यह विधि-मुखता ही तात्त्विक होगी। इस और स्पष्ट रूप में समझें । यदि ज्ञान का प्रकाश आत्मसात् होगा तो अज्ञान स्वतः ही मिटेगा यह होते हुए भी व्यावहारिक दृष्टि से निषेध पर विशेष जोर दिया जाता रहा है। इसका कारण यह है कि सामान्यतः अधिक लोग सूक्ष्मदर्शी नहीं हैं, स्थूलदर्शी हैं। वे पर से अधिक प्रभावित हैं। उनका दृष्टिबिन्दु 'पर' पर अधिक टिका है। इसलिए 'पर' के वर्जन या निषेध द्वारा उन्हें दिशा-बोध देना आवश्यक होता है।
सूत्रकार ने प्रस्तुत गाथा में विधि और निषेध दोनों विधाओं को स्वीकार करते हुए इन वासनात्मक अन्तवृत्तियों से वियुक्त होने का पथ-दर्शन किया है। उन्होंने कहा है कि उपशम या शान्ति से क्रोध का हनन करो । 'हनन' शब्द वीर्य-पुरुषार्थ या वीरत्व को जगाने की दृष्टि से है। उपशम क्रोध का परिपन्थी (विरोधी) है और क्रोध शान्ति का । यदि उपशम या शान्त भाव का स्वीकार होगा तो क्रोध स्वयं ही अस्तित्व शून्य हो जायेगा। परन्तु शान्त भाव, जो आत्मा का स्व-भाव है, को जगाने के लिए अन्तःस्फूर्ति, पुरुषार्थ, अध्यवसाय अपेक्षित होता है । उपशम द्वारा क्रोधविजय का सन्देश उद्घोषित कर मार्दव से मान को जीतने की बात कही गई है। मार्दव 'मृदु' विशेषण से बना (मृदोर्भावः-मार्दवम्) भाववाचक शब्द है । इसका अर्थ सहज मृदुता या कोमलता है। यह मान या अहंकार का विलोम (प्रतिपक्षी) है। मृदुता के आ जाने पर अहंकार स्वयं ही चला जाता है । इसलिए प्रयत्न अपने में मृदुता लाने का होना चाहिए।
आगे माया को आर्जव से और लोभ को संतोष से जीतने की बात कही गई है । आर्जव ऋजु से (ऋजोर्भाव:आर्जवम्) से बना है । मार्दव जैसे मृदुगत भाव का द्योतक है, उसी तरह आर्जव ऋजुगत भाव का द्योतक है। इसका अर्थ सरलता है । सरलता सहज भाव है, जिसमें बनाव नहीं होता । माया प्रवञ्चना है ही। उसे छलना भी कहा जाता है क्योंकि वह व्यक्ति को छलती है, धोखा देती है, उसे विभ्रान्त करती है। उसमें जितना हो सकता है, बनाव ही बनाव
। इस और हमने सड़क को छोड़ा ताणार्थ यदि हम घर में स्वरूप को स्वीकार के
..--.:58
www.norary.org