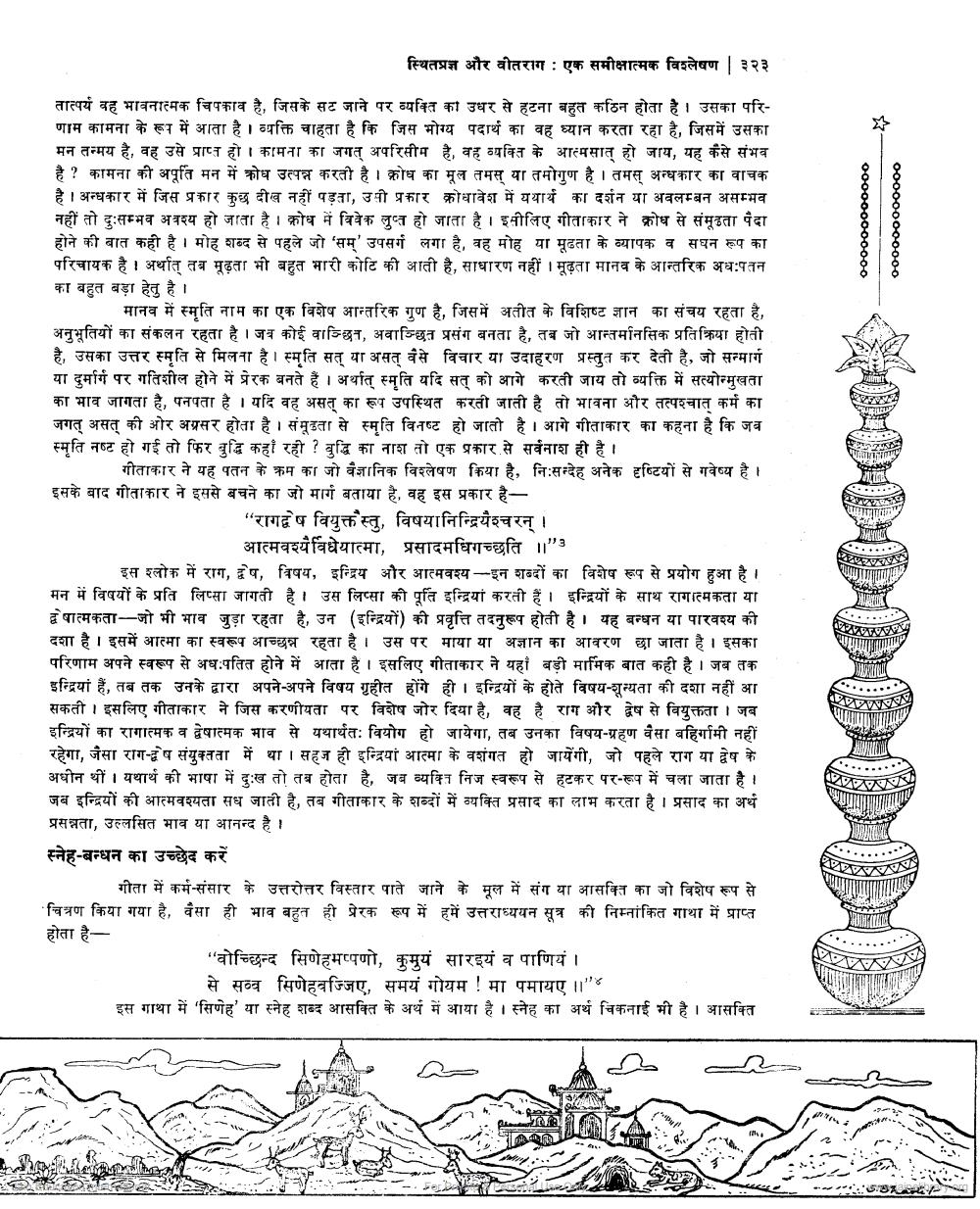________________
स्थितप्रज्ञ और वीतराग : एक समीक्षात्मक विश्लेषण | ३२३
तात्पर्य वह भावनात्मक चिपकाव है, जिसके सट जाने पर व्यक्ति का उधर से हटना बहुत कठिन होता है । उसका परिणाम कामना के रूप में आता है। व्यक्ति चाहता है कि जिस भोग्य पदार्थ का वह ध्यान करता रहा है, जिसमें उसका मन तन्मय है, वह उसे प्राप्त हो । कामता का जगत् अपरिसीम है, वह व्यक्ति के आत्मसात् हो जाय, यह कैसे संभव है ? कामना की अपूर्ति मन में क्रोध उत्पन्न करती है। क्रोध का मूल तमस् या तमोगुण है । तमस् अन्धकार का वाचक है । अन्धकार में जिस प्रकार कुछ दीख नहीं पड़ता, उसी प्रकार क्रोधावेश में यथार्थ का दर्शन या अवलम्बन असम्भव नहीं तो दुःसम्भव अवश्य हो जाता है। क्रोध में विवेक लुप्त हो जाता है । इसीलिए गीताकार ने क्रोध से संमूढता पैदा होने की बात कही है । मोह शब्द से पहले जो 'सम्' उपसर्ग लगा है, वह मोह या मूढता के व्यापक व सघन रूप का परिचायक है । अर्थात् तब मूढ़ता भी बहुत भारी कोटि की आती है, साधारण नहीं । मूढ़ता मानव के आन्तरिक अधःपतन का बहुत बड़ा हेतु है ।
मानव में स्मृति नाम का एक विशेष आन्तरिक गुण है, जिसमें अतीत के विशिष्ट ज्ञान का संचय रहता है, अनुभूतियों का संकलन रहता है । जब कोई वाञ्छित, अवाञ्छित प्रसंग बनता है, तब जो आन्तर्मानसिक प्रतिक्रिया होती है, उसका उत्तर स्मृति से मिलता है। स्मृति सत् या असत् वैसे विचार या उदाहरण प्रस्तुत कर देती है, जो सन्मार्ग या दुर्मार्ग पर गतिशील होने में प्रेरक बनते हैं । अर्थात् स्मृति यदि सत् को आगे करती जाय तो व्यक्ति में सत्योन्मुखता का भाव जागता है, पनपता है । यदि वह असत् का रूप उपस्थित करती जाती है तो भावना और तत्पश्चात् कर्म का जगत् असत् की ओर अग्रसर होता है। संमूढता से स्मृति विनष्ट हो जाती है। आगे गीताकार का कहना है कि जब स्मृति नष्ट हो गई तो फिर बुद्धि कहाँ रही ? बुद्धि का नाश तो एक प्रकार से सर्वनाश ही है ।
गीताकार ने यह पतन के क्रम का जो वैज्ञानिक विश्लेषण किया है, निःसन्देह अनेक दृष्टियों से गवेष्य है । इसके बाद गीताकार ने इससे बचने का जो मार्ग बताया है, वह इस प्रकार है
"रागद्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् । आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादमधिगणाति ॥"
इस श्लोक में राग, द्वेष, विषय, इन्द्रिय और आत्मवश्य - इन शब्दों का
विशेष रूप से प्रयोग हुआ है ।
मन में विषयों के प्रति लिप्सा जागती है । उस लिप्सा की पूर्ति इन्द्रियां करती हैं । इन्द्रियों के साथ रागात्मकता या द्वेषात्मकता - जो भी भाव जुड़ा रहता है, उन ( इन्द्रियों) की प्रवृत्ति तदनुरूप होती है। यह बन्धन या पारवश्य की दशा है । इसमें आत्मा का स्वरूप आच्छन्न रहता है। उस पर माया या अज्ञान का आवरण छा जाता है । इसका परिणाम अपने स्वरूप से अध:पतित होने में आता है। इसलिए गीताकार ने यहाँ बड़ी मार्मिक बात कही है। जब तक इन्द्रियां हैं, तब तक उनके द्वारा अपने-अपने विषय गृहीत होंगे ही। इन्द्रियों के होते विषय शुन्यता की दशा नहीं आ सकती। इसलिए गीताकार ने जिस करणीयता पर विशेष जोर दिया है, वह है राग और द्वेष से वियुक्तता । जब इन्द्रियों का रागात्मक व द्वेषात्मक भाव से यथार्थतः वियोग हो जायेगा, तब उनका विषय ग्रहण वैसा बहिर्गामी नहीं रहेगा, जैसा राग-द्वेष संयुक्तता में था । सहज ही इन्द्रियां आत्मा के वशंगत हो जायेंगी, जो पहले राग या द्वेष के अधीन थीं । यथार्थ की भाषा में दुःख तो तब होता है, जब व्यक्ति निज स्वरूप से हटकर पर-रूप में चला जाता है । जब इन्द्रियों की आत्मवश्यता सध जाती है, तब गीताकार के शब्दों में व्यक्ति प्रसाद का लाभ करता है । प्रसाद का अर्थ प्रसन्नता, उल्लसित भाव या आनन्द है ।
स्नेह-बन्धन का उच्छेद करें
गीता में कर्म-संसार के उत्तरोत्तर विस्तार पाते जाने के मूल में संग या आसक्ति का जो विशेष रूप से 'चित्रण किया गया है, वैसा ही भाव बहुत ही प्रेरक रूप में हमें उत्तराध्ययन सूत्र की निम्नांकित गाथा में प्राप्त होता है
"वोच्छिन्द सिणेहमण्यणो कुमयं सारद व पाणिवं ।
से सम्व सिणेहवज्जिए, समय गोयम मा पमायए ।। ४
इस गाथा में 'सिणेह' या स्नेह शब्द आसक्ति के अर्थ में आया है । स्नेह का अर्थ चिकनाई भी है । आसक्ति
000000000000
★
000000000000
ACORDOODED
1