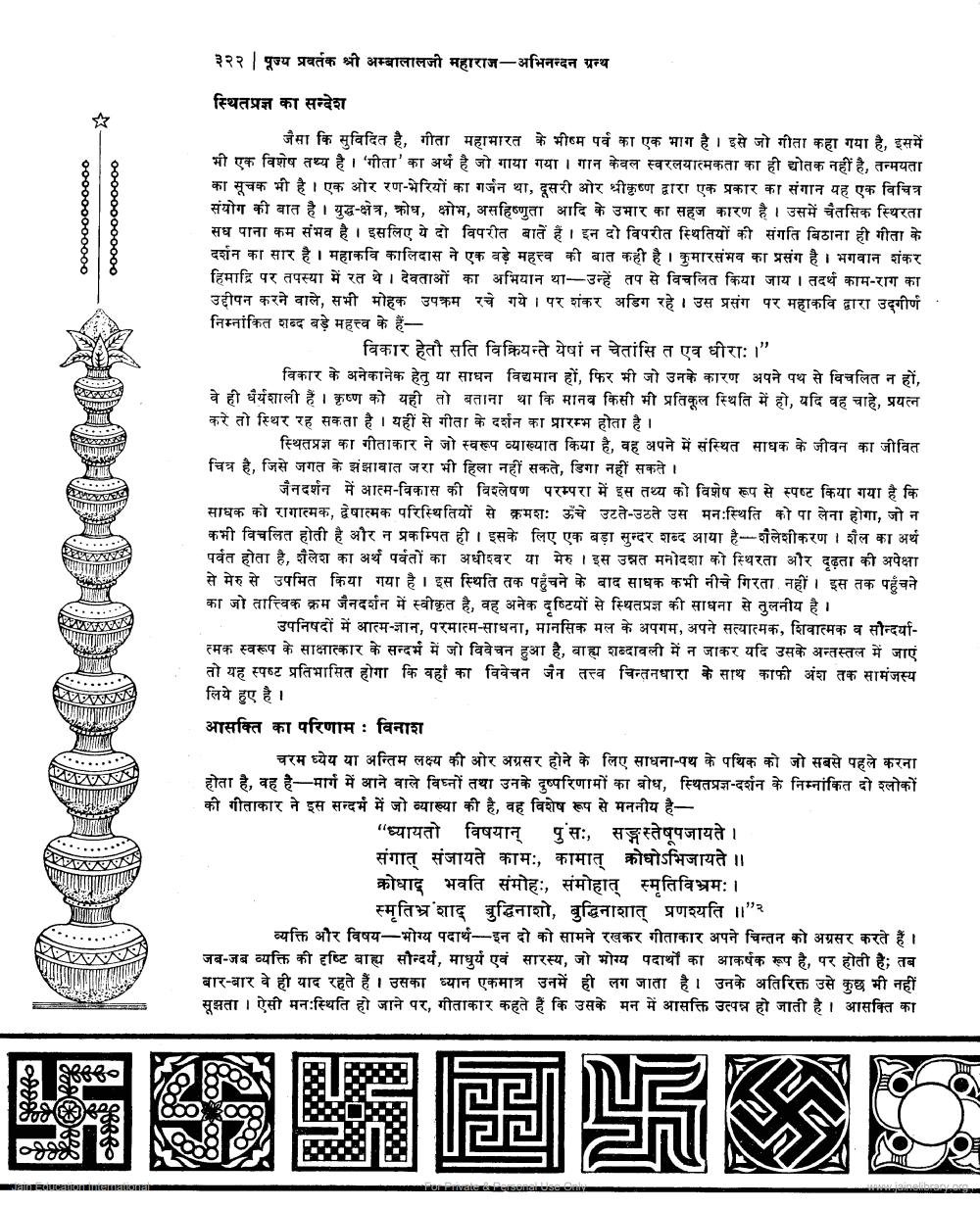________________
*
000000000000
000000000000
CODODDDDD
३२२ | पूज्य प्रवर्तक श्री अम्बालालजी महाराज - अभिनन्दन ग्रन्थ
स्थितप्रज्ञ का सन्देश
जैसा कि सुविदित है, गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है। इसे जो गीता कहा गया है, इसमें भी एक विशेष तथ्य है। 'गीता' का अर्थ है जो गाया गया। गान केवल स्वरलयात्मकता का ही द्योतक नहीं है, तन्मयता का सूचक भी है। एक ओर रण-भेरियों का गर्जन था, दूसरी ओर श्रीकृष्ण द्वारा एक प्रकार का संगान यह एक विचित्र संयोग की बात है। युद्ध क्षेत्र, क्रोध, क्षोभ, असहिष्णुता आदि के उभार का सहज कारण है। उसमें चैतसिक स्थिरता संघ पाना कम संभव है । इसलिए ये दो विपरीत बातें हैं । इन दो विपरीत स्थितियों की संगति बिठाना ही गीता के दर्शन का सार है। महाकवि कालिदास ने एक बड़े महत्त्व की बात कही है। कुमारसंभव का प्रसंग है। भगवान शंकर हिमाद्रि पर तपस्या में रत थे। देवताओं का अभियान था — उन्हें तप से विचलित किया जाय । तदर्थ काम-राग का उद्दीपन करने वाले सभी मोहक उपक्रम रचे गये । पर शंकर अडिग रहे । उस प्रसंग पर महाकवि द्वारा उद्गीर्ण निम्नांकित शब्द बड़े महत्व के हैं
विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः । "
वे ही धैर्यशाली हैं । कृष्ण को करें तो स्थिर रह सकता है ।
विकार के अनेकानेक हेतु या साधन विद्यमान हों, फिर भी जो उनके कारण अपने पथ से विचलित न हों, यही तो बताना था कि मानव किसी भी प्रतिकूल स्थिति में हो, यदि वह चाहे, प्रयत्न यहीं से गीता के दर्शन का प्रारम्भ होता है ।
स्थितप्रज्ञ का गीताकार ने जो स्वरूप व्याख्यात किया है, वह अपने में संस्थित साधक के जीवन का जीवित चित्र है, जिसे जगत के झंझावात जरा भी हिला नहीं सकते, डिगा नहीं सकते ।
जैनदर्शन में आत्म - विकास की विश्लेषण परम्परा में इस तथ्य को विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है कि साधक को रागात्मक, द्वेषात्मक परिस्थितियों से क्रमशः ऊँचे उटते-उठते उस मनःस्थिति को पा लेना होगा, जो न कभी विचलित होती है और न प्रकम्पित ही । इसके लिए एक बड़ा सुन्दर शब्द आया है- शैलेशीकरण । शैल का अर्थ पर्वत होता है, शैलेश का अर्थ पर्वतों का अधीश्वर या मेरु । इस उन्नत मनोदशा को स्थिरता और दृढ़ता की अपेक्षा से मेरु से उपमित किया गया है। इस स्थिति तक पहुँचने के बाद साधक कभी नीचे गिरता नहीं। इस तक पहुँचने का जो तात्त्विक क्रम जैनदर्शन में स्वीकृत है, वह अनेक दृष्टियों से स्थितप्रज्ञ की साधना से तुलनीय है ।
उपनिषदों में आत्म-ज्ञान, परमात्म-साधना, मानसिक मल के अपगम, अपने सत्यात्मक, शिवात्मक व सौन्दर्यात्मक स्वरूप के साक्षात्कार के सन्दर्भ में जो विवेचन हुआ है, बाह्य शब्दावली में न जाकर यदि उसके अन्तस्तल में जाएं तो यह स्पष्ट प्रतिभासित होगा कि वहाँ का विवेचन जैन तत्त्व चिन्तनधारा के साथ काफी अंश तक सामंजस्य लिये हुए है ।
आसक्ति का परिणाम : विनाश
चरम ध्येय या अन्तिम लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए साधना-पथ के पथिक को जो सबसे पहले करना होता है, वह है— मार्ग में आने वाले विघ्नों तथा उनके दुष्परिणामों का बोध, स्थितप्रज्ञ दर्शन के निम्नांकित दो श्लोकों की गीताकार ने इस सन्दर्भ में जो व्याख्या की है, वह विशेष रूप से मननीय है
"ध्यायतो विषयान् पुसः, सङ्गस्तेषूपजायते । संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते ॥
क्रोधाद् भवति संमोहः, संमोहात् स्मृतिविभ्रमः ।
स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ॥ २
व्यक्ति और विषय — भोग्य पदार्थ इन दो को सामने रखकर गीताकार अपने चिन्तन को अग्रसर करते हैं । जब-जब व्यक्ति की दृष्टि बाह्य सौन्दर्य, माधुर्य एवं सारस्य, जो भोग्य पदार्थों का आकर्षक रूप है, पर होती है; तब बार-बार वे ही याद रहते हैं । उसका ध्यान एकमात्र उनमें ही लग जाता है । उनके अतिरिक्त उसे कुछ भी नहीं सूझता । ऐसी मनःस्थिति हो जाने पर, गीताकार कहते हैं कि उसके मन में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है । आसक्ति का
IF Y
ठ
«Faisona