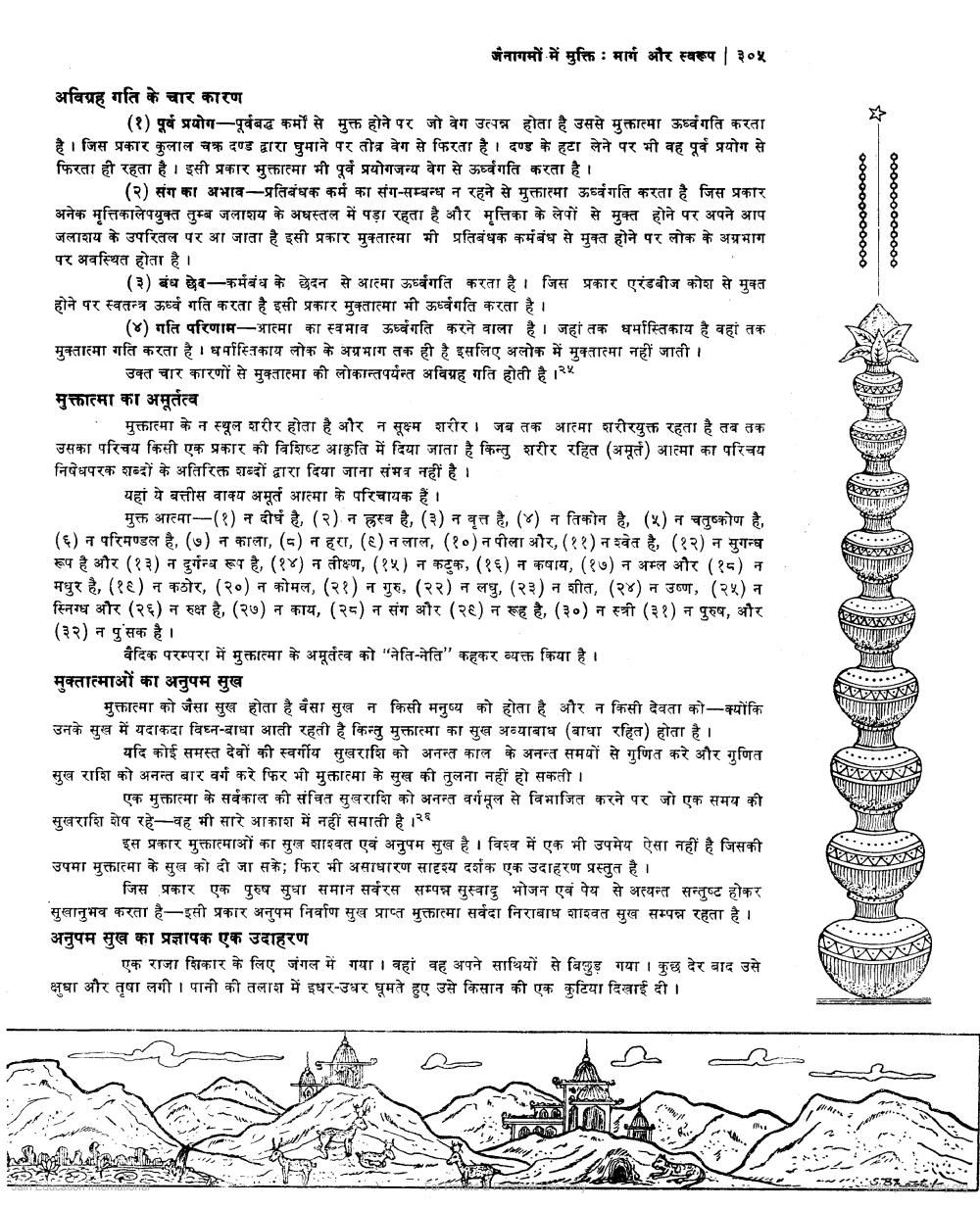________________
जैनागमों में मुक्ति : मार्ग और स्वरूप | ३०५
000000000000
००००००००००००
अविग्रह गति के चार कारण
(१) पूर्व प्रयोग-पूर्वबद्ध कर्मों से मुक्त होने पर जो वेग उत्पन्न होता है उससे मुक्तात्मा ऊर्ध्वगति करता है। जिस प्रकार कुलाल चक्र दण्ड द्वारा घुमाने पर तीव्र वेग से फिरता है । दण्ड के हटा लेने पर भी वह पूर्व प्रयोग से फिरता ही रहता है। इसी प्रकार मुक्तात्मा भी पूर्व प्रयोगजन्य वेग से ऊर्ध्वगति करता है।
(२) संग का अभाव-प्रतिबंधक कर्म का संग-सम्बन्ध न रहने से मुक्तात्मा ऊर्ध्वगति करता है जिस प्रकार अनेक मृत्तिकालेपयुक्त तुम्ब जलाशय के अधस्तल में पड़ा रहता है और मृत्तिका के लेपों से मुक्त होने पर अपने आप जलाशय के उपरितल पर आ जाता है इसी प्रकार मुक्तात्मा भी प्रतिबंधक कर्मबंध से मुक्त होने पर लोक के अग्रभाग पर अवस्थित होता है।
(३) बंध छेव-कर्मबंध के छेदन से आत्मा ऊर्ध्वगति करता है। जिस प्रकार एरंडबीज कोश से मुक्त होने पर स्वतन्त्र ऊर्ध्व गति करता है इसी प्रकार मुक्तात्मा भी ऊर्ध्वगति करता है।
(४) गति परिणाम-आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगति करने वाला है। जहां तक धर्मास्तिकाय है वहां तक मुक्तात्मा गति करता है । धर्मास्तिकाय लोक के अग्रभाग तक ही है इसलिए अलोक में मुक्तात्मा नहीं जाती।
उक्त चार कारणों से मुक्तात्मा की लोकान्तपर्यन्त अविग्रह गति होती है ।२५. मुक्तात्मा का अमूर्तत्व
- मुक्तात्मा के न स्थूल शरीर होता है और न सूक्ष्म शरीर । जब तक आत्मा शरीरयुक्त रहता है तब तक उसका परिचय किसी एक प्रकार की विशिष्ट आकृति में दिया जाता है किन्तु शरीर रहित (अमूर्त) आत्मा का परिचय निषेधपरक शब्दों के अतिरिक्त शब्दों द्वारा दिया जाना संभव नहीं है।
यहां ये बत्तीस वाक्य अमूर्त आत्मा के परिचायक हैं।
मुक्त आत्मा-(१) न दीर्घ है, (२) न ह्रस्व है, (३) न वृत्त है, (४) न तिकोन है, (५) न चतुष्कोण है, (६) न परिमण्डल है, (७) न काला, (८) न हरा, (8) न लाल, (१०) न पीला और, (११) न श्वेत है, (१२) न सुगन्ध रूप है और (१३) न दुर्गन्ध रूप है, (१४) न तीक्ष्ण, (१५) न कटुक, (१६) न कषाय, (१७) न अम्ल और (१८) न.. मधुर है, (१६) न कठोर, (२०) न कोमल, (२१) न गुरु, (२२) न लघु, (२३) न शीत, (२४) न उष्ण, (२५) न स्निग्ध और (२६) न रुक्ष है, (२७) न काय, (२८) न संग और (२६) न रूह है, (३०) न स्त्री (३१) न पुरुष, और (३२) न पुंसक है।
वैदिक परम्परा में मुक्तात्मा के अमूर्तत्व को “नेति-नेति" कहकर व्यक्त किया है। मुक्तात्माओं का अनुपम सुख ।
मुक्तात्मा को जैसा सुख होता है वैसा सुख न किसी मनुष्य को होता है और न किसी देवता को-क्योंकि उनके सुख में यदाकदा विघ्न-बाधा आती रहती है किन्तु मुक्तात्मा का सुख अव्याबाध (बाधा रहित) होता है।
यदि कोई समस्त देवों की स्वर्गीय सुखराशि को अनन्त काल के अनन्त समयों से गुणित करे और गुणित सुख राशि को अनन्त बार वर्ग करे फिर भी मुक्तात्मा के सुख की तुलना नहीं हो सकती।
एक मुक्तात्मा के सर्वकाल की संचित सुखराशि को अनन्त वर्गमूल से विभाजित करने पर जो एक समय की सुखराशि शेष रहे-वह भी सारे आकाश में नहीं समाती है ।२६
इस प्रकार मुक्तात्माओं का सुख शाश्वत एवं अनुपम सुख है। विश्व में एक भी उपमेय ऐसा नहीं है जिसकी उपमा मुक्तात्मा के सुख को दी जा सके, फिर भी असाधारण सादृश्य दर्शक एक उदाहरण प्रस्तुत है।
जिस प्रकार एक पुरुष सुधा समान सर्वरस सम्पन्न सुस्वादु भोजन एवं पेय से अत्यन्त सन्तुष्ट होकर सुखानुभव करता है-इसी प्रकार अनुपम निर्वाण सुख प्राप्त मुक्तात्मा सर्वदा निराबाध शाश्वत सुख सम्पन्न रहता है । अनुपम सुख का प्रज्ञापक एक उदाहरण
एक राजा शिकार के लिए जंगल में गया। वहां वह अपने साथियों से बिछुड़ गया । कुछ देर बाद उसे क्षुधा और तृषा लगी। पानी की तलाश में इधर-उधर घूमते हुए उसे किसान की एक कुटिया दिखाई दी।
.......
:
CAT
m
ucatomimitemation