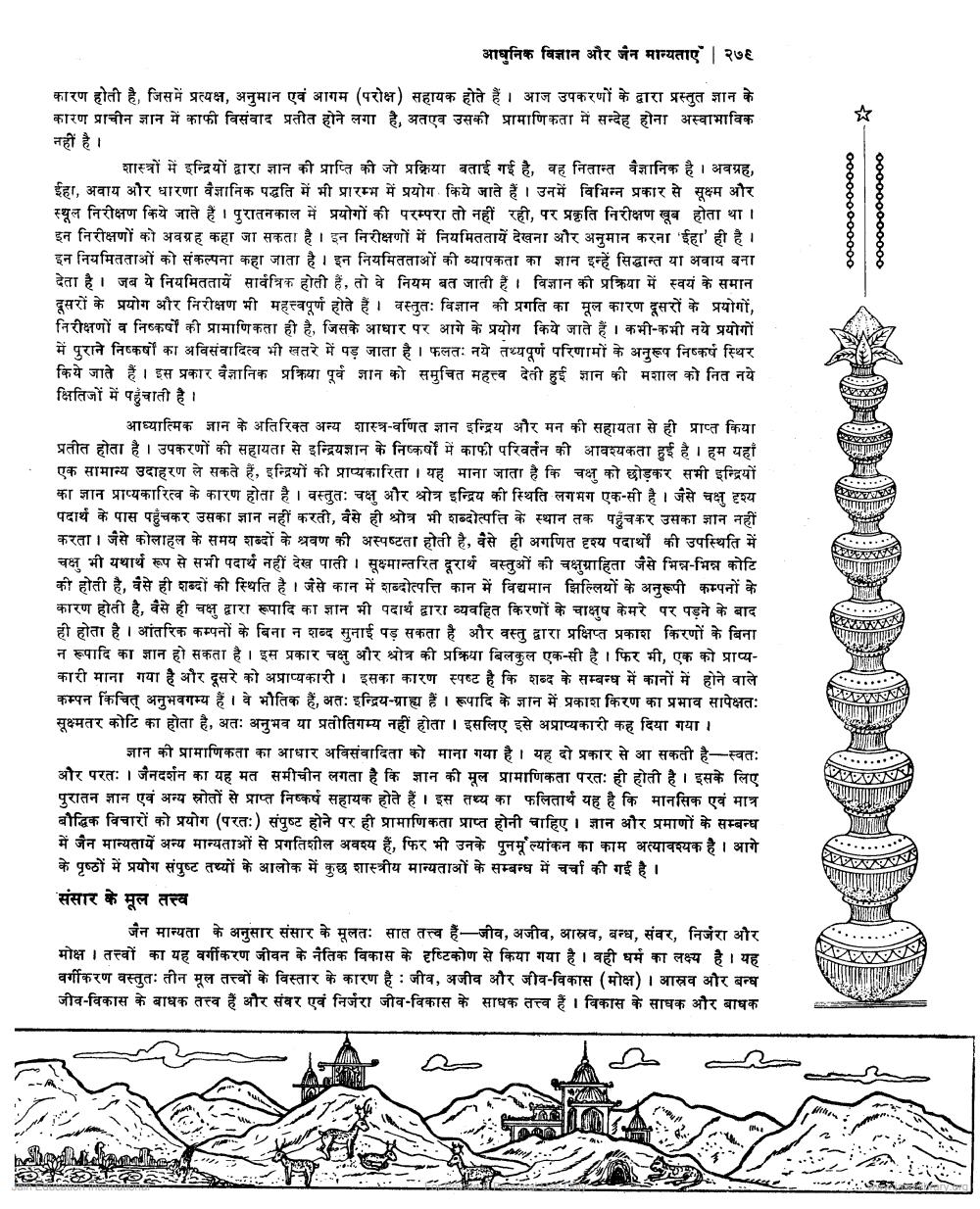________________
आधुनिक विज्ञान और जैन मान्यताएं। २७६
000000000000
000000000000
कारण होती है, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आगम (परोक्ष) सहायक होते हैं। आज उपकरणों के द्वारा प्रस्तुत ज्ञान के कारण प्राचीन ज्ञान में काफी विसंवाद प्रतीत होने लगा है, अतएव उसकी प्रामाणिकता में सन्देह होना अस्वाभाविक नहीं है।
शास्त्रों में इन्द्रियों द्वारा ज्ञान की प्राप्ति की जो प्रक्रिया बताई गई है, वह नितान्त वैज्ञानिक है । अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा वैज्ञानिक पद्धति में भी प्रारम्भ में प्रयोग किये जाते हैं। उनमें विभिन्न प्रकार से सूक्ष्म और स्थूल निरीक्षण किये जाते हैं। पुरातनकाल में प्रयोगों की परम्परा तो नहीं रही, पर प्रकृति निरीक्षण खूब होता था। इन निरीक्षणों को अवग्रह कहा जा सकता है । इन निरीक्षणों में नियमिततायें देखना और अनुमान करना ईहा' ही है । इन नियमितताओं को संकल्पना कहा जाता है। इन नियमितताओं की व्यापकता का ज्ञान इन्हें सिद्धान्त या अवाय बना देता है। जब ये नियमिततायें सार्वत्रिक होती हैं, तो वे नियम बत जाती हैं। विज्ञान की प्रक्रिया में स्वयं के समान दूसरों के प्रयोग और निरीक्षण भी महत्त्वपूर्ण होते हैं। वस्तुतः विज्ञान की प्रगति का मूल कारण दूसरों के प्रयोगों, निरीक्षणों व निष्कर्षों की प्रामाणिकता ही है, जिसके आधार पर आगे के प्रयोग किये जाते हैं । कभी-कभी नये प्रयोगों में पुराने निष्कर्षों का अविसंवादित्व भी खतरे में पड़ जाता है । फलतः नये तथ्यपूर्ण परिणामों के अनुरूप निष्कर्ष स्थिर किये जाते हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रक्रिया पूर्व ज्ञान को समुचित महत्त्व देती हुई ज्ञान की मशाल को नित नये क्षितिजों में पहुँचाती है।
आध्यात्मिक ज्ञान के अतिरिक्त अन्य शास्त्र-वर्णित ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता से ही प्राप्त किया प्रतीत होता है। उपकरणों की सहायता से इन्द्रियज्ञान के निष्कर्षों में काफी परिवर्तन की आवश्यकता हुई है । हम यहाँ एक सामान्य उदाहरण ले सकते हैं, इन्द्रियों की प्राप्यकारिता । यह माना जाता है कि चक्षु को छोड़कर सभी इन्द्रियों का ज्ञान प्राप्यकारित्व के कारण होता है । वस्तुतः चक्षु और श्रोत्र इन्द्रिय की स्थिति लगभग एक-सी है । जैसे चक्षु दृश्य पदार्थ के पास पहुंचकर उसका ज्ञान नहीं करती, वैसे ही श्रोत्र भी शब्दोत्पत्ति के स्थान तक पहुँचकर उसका ज्ञान नहीं करता। जैसे कोलाहल के समय शब्दों के श्रवण की अस्पष्टता होती है, वैसे ही अगणित दृश्य पदार्थों की उपस्थिति में चक्षु भी यथार्थ रूप से सभी पदार्थ नहीं देख पाती। सूक्ष्मान्तरित दूरार्थ वस्तुओं की चक्षुग्राहिता जैसे भिन्न-भिन्न कोटि की होती है, वैसे ही शब्दों की स्थिति है । जैसे कान में शब्दोत्पत्ति कान में विद्यमान झिल्लियों के अनुरूपी कम्पनों के कारण होती है, वैसे ही चक्षु द्वारा रूपादि का ज्ञान भी पदार्थ द्वारा व्यवहित किरणों के चाक्षुष केमरे पर पड़ने के बाद ही होता है । आंतरिक कम्पनों के बिना न शब्द सुनाई पड़ सकता है और वस्तु द्वारा प्रक्षिप्त प्रकाश किरणों के बिना न रूपादि का ज्ञान हो सकता है । इस प्रकार चक्षु और श्रोत्र की प्रक्रिया बिलकुल एक-सी है। फिर भी, एक को प्राप्यकारी माना गया है और दूसरे को अप्राप्यकारी। इसका कारण स्पष्ट है कि शब्द के सम्बन्ध में कानों में होने वाले कम्पन किंचित् अनुभवगम्य हैं। वे भौतिक हैं, अत: इन्द्रिय-ग्राह्य हैं । रूपादि के ज्ञान में प्रकाश किरण का प्रभाव सापेक्षतः सूक्ष्मतर कोटि का होता है, अतः अनुभव या प्रतीतिगम्य नहीं होता । इसलिए इसे अप्राप्यकारी कह दिया गया।
ज्ञान की प्रामाणिकता का आधार अविसंवादिता को माना गया है। यह दो प्रकार से आ सकती है-स्वतः और परतः । जैनदर्शन का यह मत समीचीन लगता है कि ज्ञान की मूल प्रामाणिकता परतः ही होती है । इसके लिए पुरातन ज्ञान एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त निष्कर्ष सहायक होते हैं । इस तथ्य का फलितार्थ यह है कि मानसिक एवं मात्र बौद्धिक विचारों को प्रयोग (परतः) संपुष्ट होने पर ही प्रामाणिकता प्राप्त होनी चाहिए । ज्ञान और प्रमाणों के सम्बन्ध में जैन मान्यतायें अन्य मान्यताओं से प्रगतिशील अवश्य हैं, फिर भी उनके पुनर्मूल्यांकन का काम अत्यावश्यक है । आगे के पृष्ठों में प्रयोग संपुष्ट तथ्यों के आलोक में कुछ शास्त्रीय मान्यताओं के सम्बन्ध में चर्चा की गई है। संसार के मूल तत्त्व
जैन मान्यता के अनुसार संसार के मूलतः सात तत्त्व हैं—जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष । तत्त्वों का यह वर्गीकरण जीवन के नैतिक विकास के दृष्टिकोण से किया गया है । वही धर्म का लक्ष्य है। यह वर्गीकरण वस्तुतः तीन मूल तत्त्वों के विस्तार के कारण है : जीव, अजीव और जीव-विकास (मोक्ष) । आस्रव और बन्ध जीव-विकास के बाधक तत्त्व हैं और संवर एवं निर्जरा जीव-विकास के साधक तत्त्व हैं । विकास के साधक और बाधक
SARO
SURESS
KADI
Mail
Di/ATTATRO