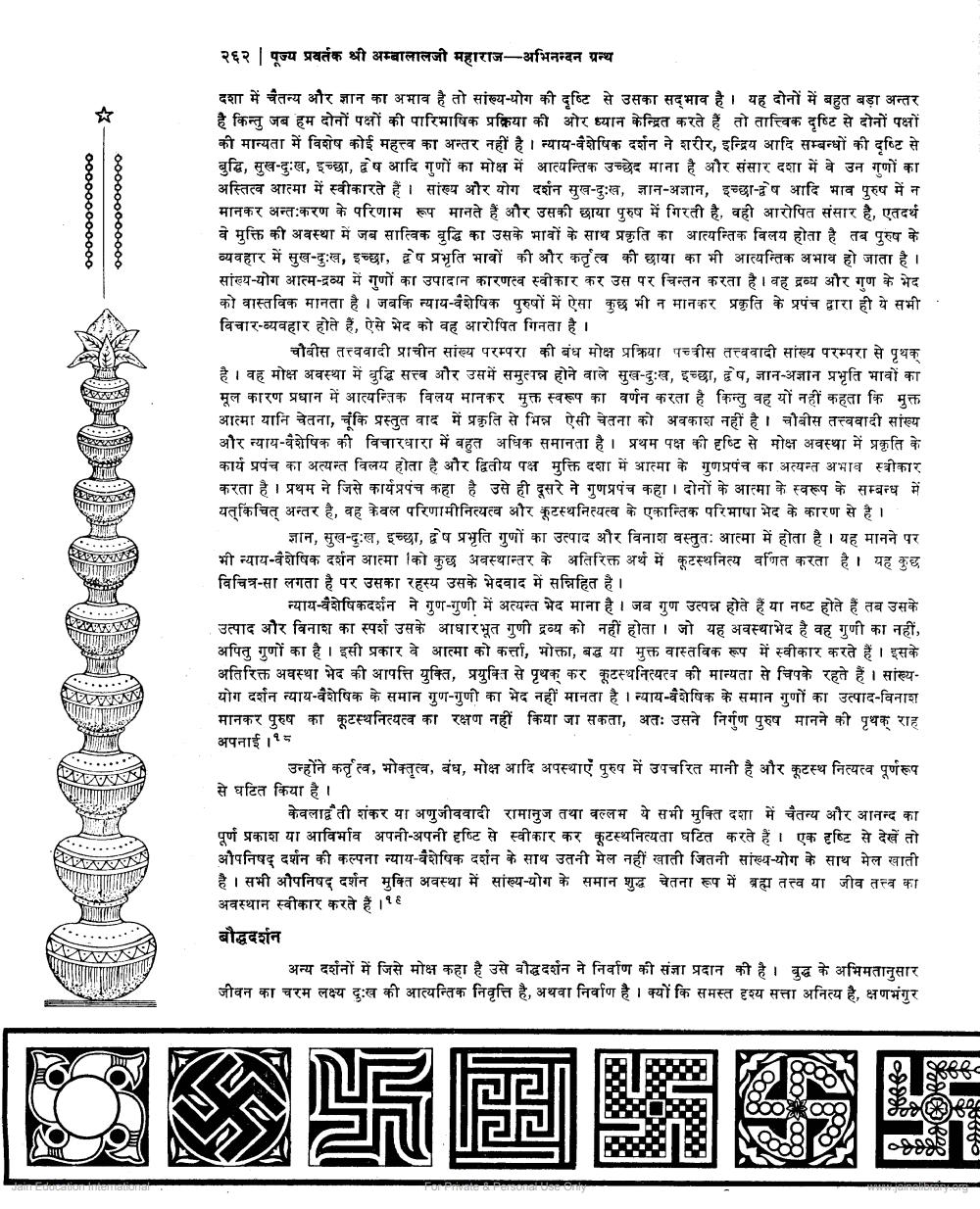________________
२६२ | पूज्य प्रवर्तक श्री अम्बालालजी महाराज-अभिनन्दन ग्रन्थ
000000000000
००००००००००००
दशा में चैतन्य और ज्ञान का अभाव है तो सांख्य-योग की दृष्टि से उसका सद्भाव है। यह दोनों में बहुत बड़ा अन्तर है किन्तु जब हम दोनों पक्षों की पारिभाषिक प्रक्रिया की ओर ध्यान केन्द्रित करते हैं तो तात्त्विक दृष्टि से दोनों पक्षों की मान्यता में विशेष कोई महत्त्व का अन्तर नहीं है । न्याय-वैशेषिक दर्शन ने शरीर, इन्द्रिय आदि सम्बन्धों की दृष्टि से बुद्धि, सुख-दुःख, इच्छा, द्वेष आदि गुणों का मोक्ष में आत्यन्तिक उच्छेद माना है और संसार दशा में वे उन गणों का अस्तित्व आत्मा में स्वीकारते हैं। सांख्य और योग दर्शन सुख-दुःख, ज्ञान-अज्ञान, इच्छा-द्वष आदि भाव पुरुष में न मानकर अन्तःकरण के परिणाम रूप मानते हैं और उसकी छाया पुरुष में गिरती है, वही आरोपित संसार है, एतदर्थ वे मुक्ति की अवस्था में जब सात्विक बुद्धि का उसके भावों के साथ प्रकृति का आत्यन्तिक विलय होता है तब पुरुष के व्यवहार में सुख-दुःख, इच्छा, द्वेष प्रभृति भावों की और कर्तृत्व की छाया का भी आत्यन्तिक अभाव हो जाता है। सांख्य-योग आत्म-द्रव्य में गुणों का उपादान कारणत्व स्वीकार कर उस पर चिन्तन करता है । वह द्रव्य और गुण के भेद को वास्तविक मानता है । जबकि न्याय-वैशेषिक पुरुषों में ऐसा कुछ भी न मानकर प्रकृति के प्रपंच द्वारा ही ये सभी । विचार-व्यवहार होते हैं, ऐसे भेद को वह आरोपित गिनता है।
चौबीस तत्त्ववादी प्राचीन सांख्य परम्परा की बंध मोक्ष प्रक्रिया पच्चीस तत्त्ववादी सांख्य परम्परा से पृथक है । वह मोक्ष अवस्था में बुद्धि सत्त्व और उसमें समुत्पन्न होने वाले सुख-दुःख, इच्छा, द्वेष, ज्ञान-अज्ञान प्रभृति भावों का मूल कारण प्रधान में आत्यन्तिक विलय मानकर मुक्त स्वरूप का वर्णन करता है किन्तु वह यों नहीं कहता कि मुक्त आत्मा यानि चेतना, चूंकि प्रस्तुत वाद में प्रकृति से भिन्न ऐसी चेतना को अवकाश नहीं है। चौबीस तत्त्ववादी सांख्य और न्याय-वैशेषिक की विचारधारा में बहुत अधिक समानता है। प्रथम पक्ष की दृष्टि से मोक्ष अवस्था में प्रकृति के कार्य प्रपंच का अत्यन्त विलय होता है और द्वितीय पक्ष मुक्ति दशा में आत्मा के गुणप्रपंच का अत्यन्त अभाव स्वीकार करता है । प्रथम ने जिसे कार्यप्रपंच कहा है उसे ही दूसरे ने गुणप्रपंच कहा । दोनों के आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में यत्किंचित् अन्तर है, वह केवल परिणामीनित्यत्व और कूटस्थनित्यत्व के एकान्तिक परिभाषा भेद के कारण से है।
ज्ञान, सुख-दुःख, इच्छा, द्वष प्रभृति गुणों का उत्पाद और विनाश वस्तुतः आत्मा में होता है । यह मानने पर भी न्याय-वैशेषिक दर्शन आत्मा को कुछ अवस्थान्तर के अतिरिक्त अर्थ में कूटस्थनित्य वणित करता है। यह कुछ विचित्र-सा लगता है पर उसका रहस्य उसके भेदवाद में सन्निहित है।
न्याय-वैशेषिकदर्शन ने गुण-गुणी में अत्यन्त भेद माना है । जब गुण उत्पन्न होते हैं या नष्ट होते हैं तब उसके उत्पाद और विनाश का स्पर्श उसके आधारभूत गुणी द्रव्य को नहीं होता । जो यह अवस्थाभेद है वह गुणी का नहीं, अपितु गुणों का है । इसी प्रकार वे आत्मा को कर्त्ता, भोक्ता, बद्ध या मुक्त वास्तविक रूप में स्वीकार करते हैं । इसके अतिरिक्त अवस्था भेद की आपत्ति युक्ति, प्रयुक्ति से पृथक् कर कूटस्थनित्यत्व की मान्यता से चिपके रहते हैं । सांख्ययोग दर्शन न्याय-वैशेषिक के समान गुण-गुणी का भेद नहीं मानता है । न्याय-वैशेषिक के समान गुणों का उत्पाद-विनाश मानकर पुरुष का कूटस्थनित्यत्व का रक्षण नहीं किया जा सकता, अतः उसने निर्गुण पुरुष मानने की पृथक् राह अपनाई।१६
___ उन्होंने कर्तृत्व, भोक्तृत्व, बंध, मोक्ष आदि अपस्थाएं पुरुष में उपचरित मानी है और कूटस्थ नित्यत्व पूर्णरूप से घटित किया है।
केवलाद्व ती शंकर या अणुजीववादी रामानुज तथा वल्लम ये सभी मुक्ति दशा में चैतन्य और आनन्द का पूर्ण प्रकाश या आविर्भाव अपनी-अपनी दृष्टि से स्वीकार कर कूटस्थनित्यता घटित करते हैं। एक दृष्टि से देखें तो
औपनिषद् दर्शन की कल्पना न्याय-वैशेषिक दर्शन के साथ उतनी मेल नहीं खाती जितनी सांख्ययोग के साथ मेल खाती है। सभी औपनिषद् दर्शन मुक्ति अवस्था में सांख्य-योग के समान शुद्ध चेतना रूप में ब्रह्म तत्त्व या जीव तत्त्व का अवस्थान स्वीकार करते हैं । १६ बौद्धदर्शन
अन्य दर्शनों में जिसे मोक्ष कहा है उसे बौद्ध दर्शन ने निर्वाण की संज्ञा प्रदान की है। बुद्ध के अभिमतानुसार जीवन का चरम लक्ष्य दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति है, अथवा निर्वाण है । क्यों कि समस्त दृश्य सत्ता अनित्य है, क्षणभंगुर
Samducation international