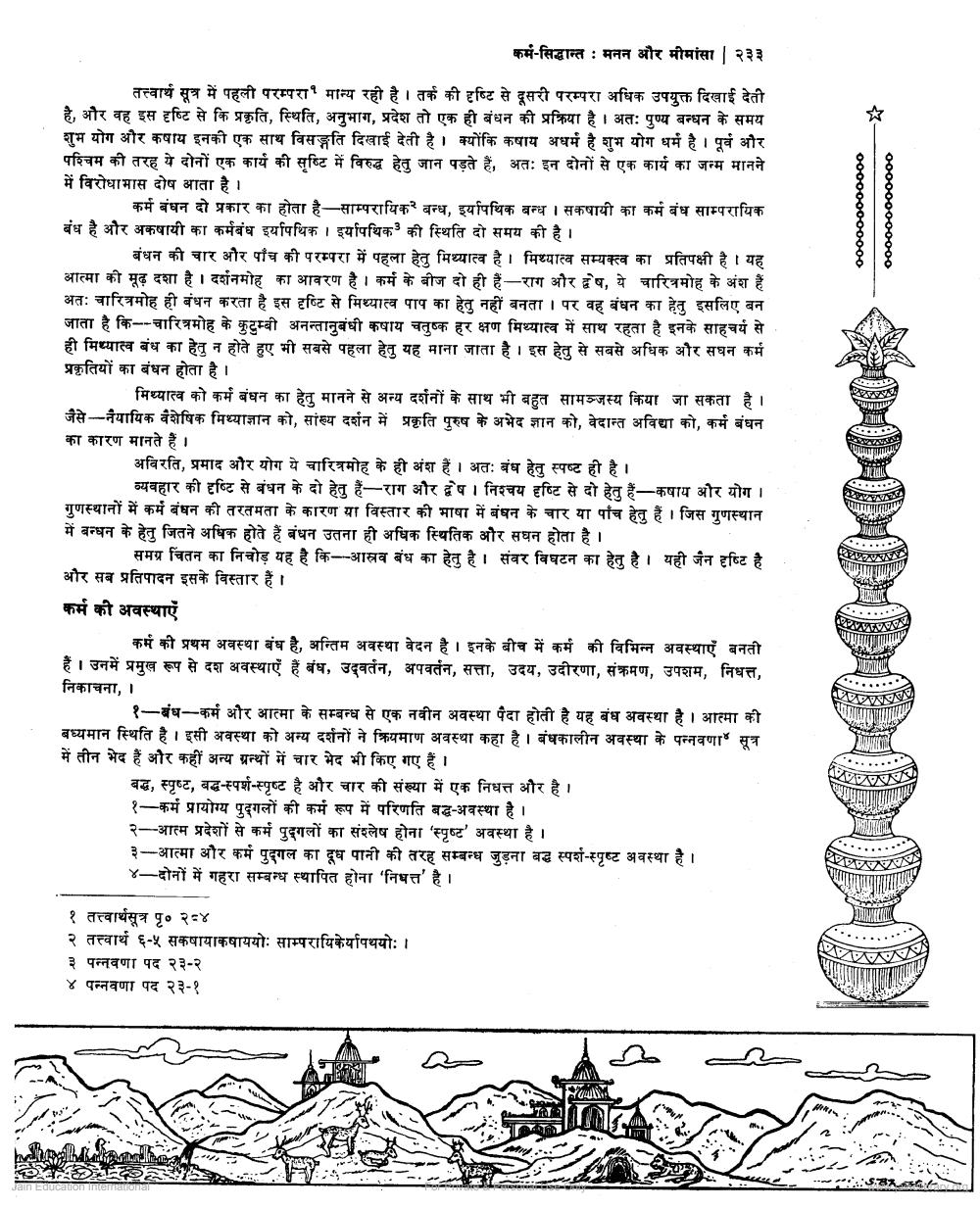________________
कर्म-सिद्धान्त : मनन और मीमांसा | २३३
000000000000
प्रणाम
TA
तत्त्वार्थ सूत्र में पहली परम्परा' मान्य रही है । तर्क की दृष्टि से दूसरी परम्परा अधिक उपयुक्त दिखाई देती है, और वह इस दृष्टि से कि प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश तो एक ही बंधन की प्रक्रिया है । अतः पुण्य बन्धन के समय शुभ योग और कषाय इनकी एक साथ विसङ्गति दिखाई देती है। क्योंकि कषाय अधर्म है शुभ योग धर्म है । पूर्व और पश्चिम की तरह ये दोनों एक कार्य की सृष्टि में विरुद्ध हेतु जान पड़ते हैं, अतः इन दोनों से एक कार्य का जन्म मानने में विरोधाभास दोष आता है।
कर्म बंधन दो प्रकार का होता है-साम्परायिक बन्ध, इपिथिक बन्ध । सकषायी का कर्म बंध साम्परायिक बंध है और अकषायी का कर्मबंध इपिथिक । इपिथिक' की स्थिति दो समय की है।
बंधन की चार और पाँच की परम्परा में पहला हेतु मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व सम्यक्त्व का प्रतिपक्षी है । यह आत्मा की मूढ़ दशा है । दर्शनमोह का आवरण है । कर्म के बीज दो ही हैं-राग और द्वेष, ये चारित्रमोह के अंश हैं अतः चारित्रमोह ही बंधन करता है इस दृष्टि से मिथ्यात्व पाप का हेतु नहीं बनता । पर वह बंधन का हेतु इसलिए बन जाता है कि--चारित्रमोह के कुटुम्बी अनन्तानुबंधी कषाय चतुष्क हर क्षण मिथ्यात्व में साथ रहता है इनके साहचर्य से ही मिथ्यात्व बंध का हेतु न होते हुए भी सबसे पहला हेतु यह माना जाता है । इस हेतु से सबसे अधिक और सघन कर्म प्रकृतियों का बंधन होता है।
मिथ्यात्व को कर्म बंधन का हेतु मानने से अन्य दर्शनों के साथ भी बहुत सामञ्जस्य किया जा सकता है। जैसे-नैयायिक वैशेषिक मिथ्याज्ञान को, सांख्य दर्शन में प्रकृति पुरुष के अभेद ज्ञान को, वेदान्त अविद्या को, कर्म बंधन का कारण मानते हैं।
अविरति, प्रमाद और योग ये चारित्रमोह के ही अंश हैं । अतः बंध हेतु स्पष्ट ही है।
व्यवहार की दृष्टि से बंधन के दो हेतु हैं-राग और द्वेष । निश्चय दृष्टि से दो हेतु हैं-कषाय और योग । गुणस्थानों में कर्म बंधन की तरतमता के कारण या विस्तार की भाषा में बंधन के चार या पांच हेतु हैं । जिस गुणस्थान में बन्धन के हेतु जितने अधिक होते हैं बंधन उतना ही अधिक स्थितिक और सघन होता है ।
समग्र चिंतन का निचोड़ यह है कि--आस्रव बंध का हेतु है। संवर विघटन का हेतु है। यही जैन दृष्टि है और सब प्रतिपादन इसके विस्तार हैं। कर्म की अवस्थाएं
कर्म की प्रथम अवस्था बंध है, अन्तिम अवस्था वेदन है। इनके बीच में कर्म की विभिन्न अवस्थाएँ बनती हैं। उनमें प्रमुख रूप से दश अवस्थाएँ हैं बंध, उद्वर्तन, अपवर्तन, सत्ता, उदय, उदीरणा, संक्रमण, उपशम, निधत्त, निकाचना, ।
१-बंध-कर्म और आत्मा के सम्बन्ध से एक नवीन अवस्था पैदा होती है यह बंध अवस्था है। आत्मा की बध्यमान स्थिति है । इसी अवस्था को अन्य दर्शनों ने क्रियमाण अवस्था कहा है । बंधकालीन अवस्था के पन्नवणा' सूत्र में तीन भेद हैं और कहीं अन्य ग्रन्थों में चार भेद भी किए गए हैं ।
बद्ध, स्पृष्ट, बद्ध-स्पर्श-स्पृष्ट है और चार की संख्या में एक निधत्त और है। १-कर्म प्रायोग्य पुद्गलों की कर्म रूप में परिणति बद्ध-अवस्था है। २--आत्म प्रदेशों से कर्म पुद्गलों का संश्लेष होना 'स्पृष्ट' अवस्था है। ३-आत्मा और कर्म पुद्गल का दूध पानी की तरह सम्बन्ध जुड़ना बद्ध स्पर्श-स्पृष्ट अवस्था है। ४-दोनों में गहरा सम्बन्ध स्थापित होना 'निधत्त' है।
CDA
१ तत्त्वार्थसूत्र पृ० २०४ २ तत्त्वार्थ ६-५ सकषायाकषाययोः साम्परायिकेर्यापथयोः । ३ पन्नवणा पद २३-२ ४ पन्नवणा पद २३-१
-
NhoealhaKARAN-
Jan Education memo