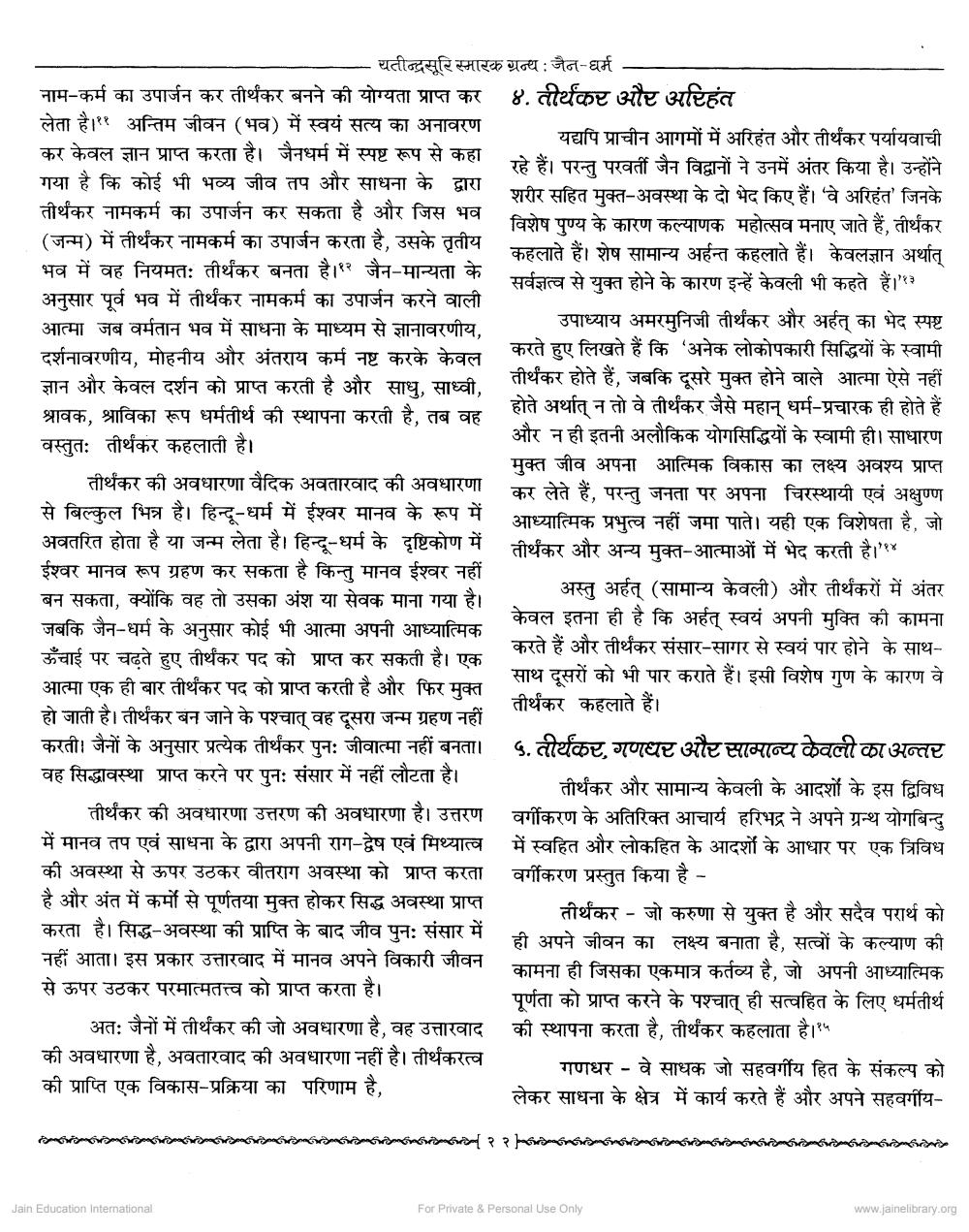________________
- यतीन्द्रसूरि स्मारक ग्रन्थ : जैन-धर्म नाम-कर्म का उपार्जन कर तीर्थंकर बनने की योग्यता प्राप्त कर ४. तीर्थंकर और अरिहंत लेता है।१९ अन्तिम जीवन (भव) में स्वयं सत्य का अनावरण
यद्यपि प्राचीन आगमों में अरिहंत और तीर्थंकर पर्यायवाची कर केवल ज्ञान प्राप्त करता है। जैनधर्म में स्पष्ट रूप से कहा
रहे हैं। परन्तु परवर्ती जैन विद्वानों ने उनमें अंतर किया है। उन्होंने गया है कि कोई भी भव्य जीव तप और साधना के द्वारा
शरीर सहित मुक्त-अवस्था के दो भेद किए हैं। वे अरिहंत' जिनके तीर्थंकर नामकर्म का उपार्जन कर सकता है और जिस भव
विशेष पुण्य के कारण कल्याणक महोत्सव मनाए जाते हैं, तीर्थंकर (जन्म) में तीर्थंकर नामकर्म का उपार्जन करता है, उसके तृतीय
कहलाते हैं। शेष सामान्य अर्हन्त कहलाते हैं। केवलज्ञान अर्थात् भव में वह नियमतः तीर्थंकर बनता है।१२ जैन-मान्यता के
सर्वज्ञत्व से युक्त होने के कारण इन्हें केवली भी कहते हैं। ५३ अनुसार पूर्व भव में तीर्थंकर नामकर्म का उपार्जन करने वाली आत्मा जब वर्मतान भव में साधना के माध्यम से ज्ञानावरणीय,
उपाध्याय अमरमुनिजी तीर्थंकर और अर्हत् का भेद स्पष्ट दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय कर्म नष्ट करके केवल
करते हुए लिखते हैं कि 'अनेक लोकोपकारी सिद्धियों के स्वामी ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त करती है और साधु, साध्वी,
तीर्थंकर होते हैं, जबकि दूसरे मुक्त होने वाले आत्मा ऐसे नहीं
होते अर्थात् न तो वे तीर्थंकर जैसे महान् धर्म-प्रचारक ही होते हैं श्रावक, श्राविका रूप धर्मतीर्थ की स्थापना करती है, तब वह
और न ही इतनी अलौकिक योगसिद्धियों के स्वामी ही। साधारण वस्तुतः तीर्थंकर कहलाती है।
मुक्त जीव अपना आत्मिक विकास का लक्ष्य अवश्य प्राप्त तीर्थंकर की अवधारणा वैदिक अवतारवाद की अवधारणा
कर लेते हैं, परन्तु जनता पर अपना चिरस्थायी एवं अक्षुण्ण से बिल्कुल भिन्न है। हिन्दू-धर्म में ईश्वर मानव के रूप में आध्यात्मिक प्रभत्व नहीं जमा पाते। यही एक विशेषता है, जो अवतरित होता है या जन्म लेता है। हिन्दू-धर्म के दृष्टिकोण में तीर्थंकर और अन्य मक्त-आत्माओं में भेद करती है। १४ ईश्वर मानव रूप ग्रहण कर सकता है किन्तु मानव ईश्वर नहीं
अस्तु अर्हत् (सामान्य केवली) और तीर्थंकरों में अंतर बन सकता, क्योंकि वह तो उसका अंश या सेवक माना गया है।
केवल इतना ही है कि अर्हत् स्वयं अपनी मुक्ति की कामना जबकि जैन-धर्म के अनुसार कोई भी आत्मा अपनी आध्यात्मिक
करते हैं और तीर्थंकर संसार-सागर से स्वयं पार होने के साथऊँचाई पर चढ़ते हुए तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सकती है। एक
साथ दूसरों को भी पार कराते हैं। इसी विशेष गुण के कारण वे आत्मा एक ही बार तीर्थंकर पद को प्राप्त करती है और फिर मुक्त
तीर्थंकर कहलाते हैं। हो जाती है। तीर्थंकर बन जाने के पश्चात् वह दूसरा जन्म ग्रहण नहीं करती। जैनों के अनुसार प्रत्येक तीर्थंकर पुन: जीवात्मा नहीं बनता। ५.तीर्थंकर, गणधर और सामान्य केवली का अन्तर वह सिद्धावस्था प्राप्त करने पर पुनः संसार में नहीं लौटता है।
तीर्थंकर और सामान्य केवली के आदशों के इस द्विविध तीर्थंकर की अवधारणा उत्तरण की अवधारणा है। उत्तरण वर्गीकरण के अतिरिक्त आचार्य हरिभद्र ने अपने ग्रन्थ योगबिन्दु में मानव तप एवं साधना के द्वारा अपनी राग-द्वेष एवं मिथ्यात्व में स्वहित और लोकहित के आदर्शों के आधार पर एक त्रिविध की अवस्था से ऊपर उठकर वीतराग अवस्था को प्राप्त करता वर्गीकरण प्रस्तुत किया है - है और अंत में कर्मों से पूर्णतया मुक्त होकर सिद्ध अवस्था प्राप्त
तीर्थंकर - जो करुणा से युक्त है और सदैव परार्थ को करता है। सिद्ध-अवस्था की प्राप्ति के बाद जीव पुन: संसार में
__ ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है, सत्वों के कल्याण की नहीं आता। इस प्रकार उत्तारवाद में मानव अपने विकारी जीवन
कामना ही जिसका एकमात्र कर्तव्य है, जो अपनी आध्यात्मिक से ऊपर उठकर परमात्मतत्त्व को प्राप्त करता है।
पूर्णता को प्राप्त करने के पश्चात् ही सत्वहित के लिए धर्मतीर्थ अत: जैनों में तीर्थंकर की जो अवधारणा है, वह उत्तारवाद की स्थापना करता है, तीर्थंकर कहलाता है।१५। की अवधारणा है, अवतारवाद की अवधारणा नहीं है। तीर्थंकरत्व
गणधर - वे साधक जो सहवर्गीय हित के संकल्प को की प्राप्ति एक विकास-प्रक्रिया का परिणाम है,
लेकर साधना के क्षेत्र में कार्य करते हैं और अपने सहवर्गीय
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org