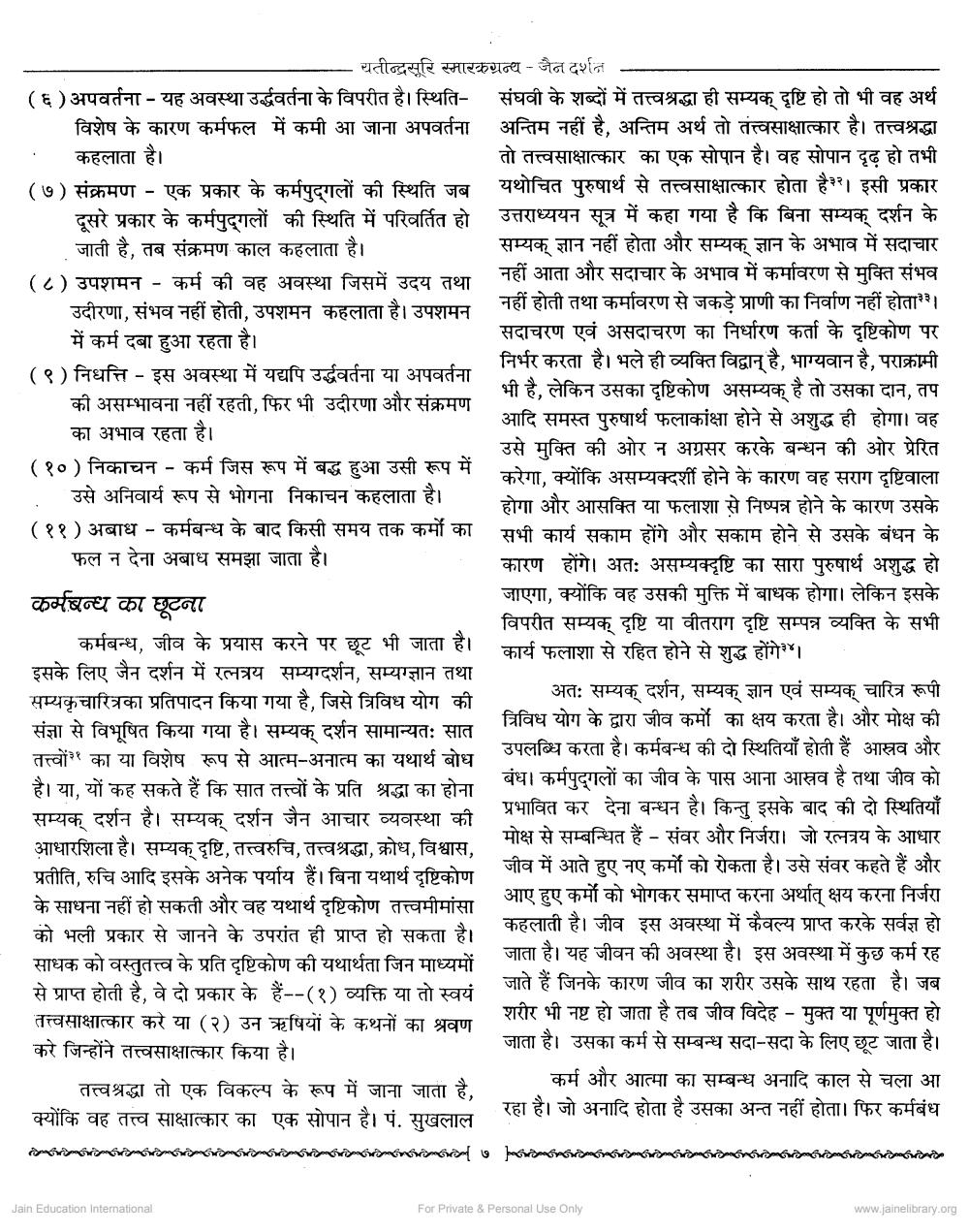________________
यतीन्द्रसूरि स्मारकग्रन्थ जैन दर्शन
( ६ ) अपवर्तना - यह अवस्था उर्द्धवर्तना के विपरीत है। स्थितिविशेष के कारण कर्मफल में कमी आ जाना अपवर्तना कहलाता है।
(७) संक्रमण - एक प्रकार के कर्मपुद्गलों की स्थिति जब दूसरे प्रकार के कर्मपुद्गलों की स्थिति में परिवर्तित हो जाती है, तब संक्रमण काल कहलाता है।
(८) उपशमन - कर्म की वह अवस्था जिसमें उदय तथा उदीरणा, संभव नहीं होती, उपशमन कहलाता है । उपशमन में कर्म दबा हुआ रहता है।
( ९ ) निधत्ति - इस अवस्था में यद्यपि उर्द्धवर्तना या अपवर्तना की असम्भावना नहीं रहती, फिर भी उदीरणा और संक्रमण का अभाव रहता है।
( १० ) निकाचन - कर्म जिस रूप में बद्ध हुआ उसी रूप में उसे अनिवार्य रूप से भोगना निकाचन कहलाता है।
( ११ ) अबाध - कर्मबन्ध के बाद किसी समय तक कर्मों का फल न देना अबाध समझा जाता है।
कर्मबन्ध का छूटना
कर्मबन्ध, जीव के प्रयास करने पर छूट भी जाता है । इसके लिए जैन दर्शन में रत्नत्रय सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यकृचारित्रका प्रतिपादन किया गया है, जिसे त्रिविध योग की संज्ञा से विभूषित किया गया है। सम्यक् दर्शन सामान्यतः सात तत्त्वों का या विशेष रूप से आत्म-अनात्म का यथार्थ बोध है। या, यों कह सकते हैं कि सात तत्त्वों के प्रति श्रद्धा का होना सम्यक् दर्शन है। सम्यक् दर्शन जैन आचार व्यवस्था की आधारशिला है। सम्यक् दृष्टि, तत्त्वरुचि, तत्त्वश्रद्धा, क्रोध, विश्वास, प्रतीति, रुचि आदि इसके अनेक पर्याय हैं। बिना यथार्थ दृष्टिकोण
साधना नहीं हो सकती और वह यथार्थ दृष्टिकोण तत्त्वमीमांसा को भली प्रकार से जानने के उपरांत ही प्राप्त हो सकता है। साधक को वस्तुतत्त्व के प्रति दृष्टिकोण की यथार्थता जिन माध्यमों से प्राप्त होती है, वे दो प्रकार के हैं-- (१) व्यक्ति या तो स्वयं तत्त्वसाक्षात्कार करे या (२) उन ऋषियों के कथनों का श्रवण करे जिन्होंने तत्त्वसाक्षात्कार किया है।
तत्त्वश्रद्धा तो एक विकल्प के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह तत्त्व साक्षात्कार का एक सोपान है। पं. सुखलाल
Jain Education International
संघवी के शब्दों में तत्त्वश्रद्धा ही सम्यक् दृष्टि हो तो भी वह अर्थ अन्तिम नहीं है, अन्तिम अर्थ तो तत्त्वसाक्षात्कार है । तत्त्वश्रद्धा तो तत्त्वसाक्षात्कार का एक सोपान है। वह सोपान दृढ़ हो तभी यथोचित पुरुषार्थ से तत्त्वसाक्षात्कार होता है । इसी प्रकार उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है कि बिना सम्यक् दर्शन के सम्यक् ज्ञान नहीं होता और सम्यक् ज्ञान के अभाव में सदाचार नहीं आता और सदाचार के अभाव में कर्मावरण से मुक्ति संभव नहीं होती तथा कर्मावरण से जकड़े प्राणी का निर्वाण नहीं होता। सदाचरण एवं असदाचरण का निर्धारण कर्ता के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। भले ही व्यक्ति विद्वान् है, भाग्यवान है, पराक्रमी भी है, लेकिन उसका दृष्टिकोण असम्यक् है तो उसका दान, तप आदि समस्त पुरुषार्थ फलाकांक्षा होने से अशुद्ध ही होगा। वह उसे मुक्ति की ओर न अग्रसर करके बन्धन की ओर प्रेरित करेगा, क्योंकि असम्यक्दर्शी होने के कारण वह सराग दृष्टिवाला होगा और आसक्ति या फलाशा से निष्पन्न होने के कारण उसके सभी कार्य सकाम होंगे और सकाम होने से उसके बंधन के कारण होंगे। अतः असम्यक्दृष्टि का सारा पुरुषार्थ अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि वह उसकी मुक्ति में बाधक होगा। लेकिन इसके विपरीत सम्यक् दृष्टि या वीतराग दृष्टि सम्पन्न व्यक्ति के सभी कार्य फलाशा से रहित होने से शुद्ध होंगे।
अतः सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान एवं सम्यक् चारित्र रूपी त्रिविध योग के द्वारा जीव कर्मों का क्षय करता है । और मोक्ष की उपलब्धि करता है। कर्मबन्ध की दो स्थितियाँ होती हैं आस्रव और बंध। कर्मपुद्गलों का जीव के पास आना आस्रव है तथा जीव को प्रभावित कर देना बन्धन है । किन्तु इसके बाद की दो स्थितियाँ मोक्ष से सम्बन्धित हैं- संवर और निर्जरा। जो रत्नत्रय के आधार जीव में आते हुए नए कर्मों को रोकता है। उसे संवर कहते हैं और आए हुए कर्मों को भोगकर समाप्त करना अर्थात् क्षय करना निर्जरा कहलाती है। जीव इस अवस्था में कैवल्य प्राप्त करके सर्वज्ञ हो जाता है। यह जीवन की अवस्था है। इस अवस्था में कुछ कर्म रह जाते हैं जिनके कारण जीव का शरीर उसके साथ रहता है। जब शरीर भी नष्ट हो जाता है तब जीव विदेह मुक्त या पूर्णमुक्त हो जाता है। उसका कर्म से सम्बन्ध सदा-सदा के लिए छूट जाता
कर्म और आत्मा का सम्बन्ध अनादि काल से चला आ रहा है। जो अनादि होता है उसका अन्त नहीं होता । फिर कर्मबंध
mensamsad v porns
-
For Private Personal Use Only
www.jainelibrary.org