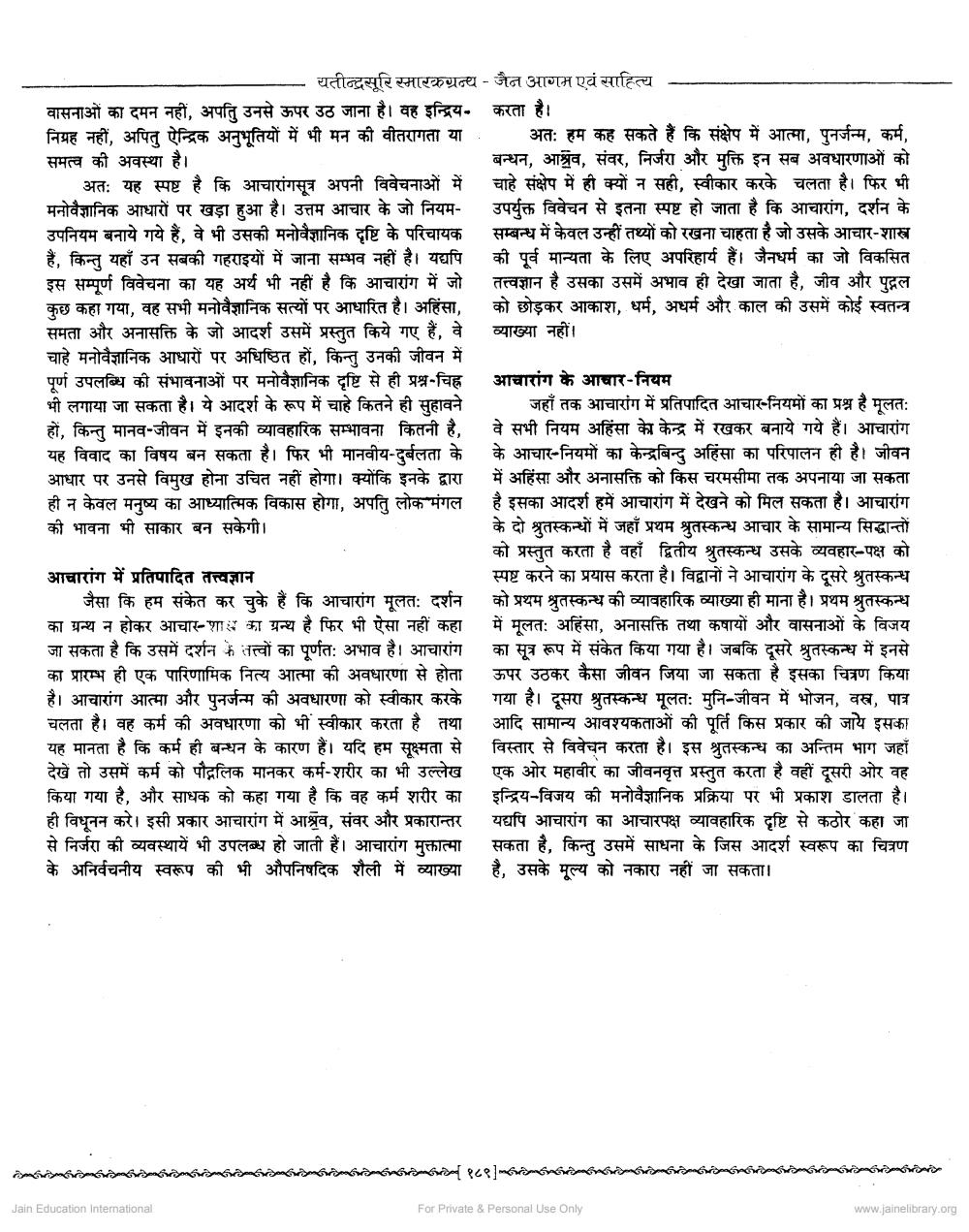________________
यतीन्द्रसूरि स्मारकग्रन्य - जैन आगम एवं साहित्य वासनाओं का दमन नहीं, अपतुि उनसे ऊपर उठ जाना है। वह इन्द्रिय. करता है। निग्रह नहीं, अपितु ऐन्द्रिक अनुभूतियों में भी मन की वीतरागता या . अत: हम कह सकते हैं कि संक्षेप में आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, समत्व की अवस्था है।
बन्धन, आश्रृंव, संवर, निर्जरा और मुक्ति इन सब अवधारणाओं को अत: यह स्पष्ट है कि आचारांगसूत्र अपनी विवेचनाओं में चाहे संक्षेप में ही क्यों न सही, स्वीकार करके चलता है। फिर भी मनोवैज्ञानिक आधारों पर खड़ा हुआ है। उत्तम आचार के जो नियम- उपर्युक्त विवेचन से इतना स्पष्ट हो जाता है कि आचारांग, दर्शन के उपनियम बनाये गये हैं, वे भी उसकी मनोवैज्ञानिक दृष्टि के परिचायक सम्बन्ध में केवल उन्हीं तथ्यों को रखना चाहता है जो उसके आचार-शास्त्र हैं, किन्तु यहाँ उन सबकी गहराइयों में जाना सम्भव नहीं है। यद्यपि की पूर्व मान्यता के लिए अपरिहार्य हैं। जैनधर्म का जो विकसित इस सम्पूर्ण विवेचना का यह अर्थ भी नहीं है कि आचारांग में जो तत्त्वज्ञान है उसका उसमें अभाव ही देखा जाता है, जीव और पुद्गल कुछ कहा गया, वह सभी मनोवैज्ञानिक सत्यों पर आधारित है। अहिंसा, को छोड़कर आकाश, धर्म, अधर्म और काल की उसमें कोई स्वतन्त्र समता और अनासक्ति के जो आदर्श उसमें प्रस्तुत किये गए हैं, वे व्याख्या नहीं। चाहे मनोवैज्ञानिक आधारों पर अधिष्ठित हों, किन्तु उनकी जीवन में पूर्ण उपलब्धि की संभावनाओं पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ही प्रश्न-चिह्न आचारांग के आचार-नियम भी लगाया जा सकता है। ये आदर्श के रूप में चाहे कितने ही सुहावने जहाँ तक आचारांग में प्रतिपादित आचार-नियमों का प्रश्न है मूलतः हों, किन्तु मानव-जीवन में इनकी व्यावहारिक सम्भावना कितनी है, वे सभी नियम अहिंसा का केन्द्र में रखकर बनाये गये हैं। आचारांग यह विवाद का विषय बन सकता है। फिर भी मानवीय-दुर्बलता के के आचार-नियमों का केन्द्रबिन्दु अहिंसा का परिपालन ही है। जीवन आधार पर उनसे विमुख होना उचित नहीं होगा। क्योंकि इनके द्वारा में अहिंसा और अनासक्ति को किस चरमसीमा तक अपनाया जा सकता ही न केवल मनुष्य का आध्यात्मिक विकास होगा, अपतुि लोक मंगल है इसका आदर्श हमें आचारांग में देखने को मिल सकता है। आचारांग की भावना भी साकार बन सकेगी।
के दो श्रुतस्कन्धों में जहाँ प्रथम श्रुतस्कन्ध आचार के सामान्य सिद्धान्तों
को प्रस्तुत करता है वहाँ द्वितीय श्रुतस्कन्ध उसके व्यवहार-पक्ष को आचारांग में प्रतिपादित तत्त्वज्ञान
स्पष्ट करने का प्रयास करता है। विद्वानों ने आचारांग के दूसरे श्रुतस्कन्ध जैसा कि हम संकेत कर चुके हैं कि आचारांग मूलत: दर्शन को प्रथम श्रुतस्कन्ध की व्यावहारिक व्याख्या ही माना है। प्रथम श्रुतस्कन्ध का ग्रन्थ न होकर आचार-शास का ग्रन्थ है फिर भी ऐसा नहीं कहा में मूलत: अहिंसा, अनासक्ति तथा कषायों और वासनाओं के विजय जा सकता है कि उसमें दर्शन के तत्वों का पूर्णत: अभाव है। आचारांग का सूत्र रूप में संकेत किया गया है। जबकि दूसरे श्रुतस्कन्ध में इनसे का प्रारम्भ ही एक पारिणामिक नित्य आत्मा की अवधारणा से होता ऊपर उठकर कैसा जीवन जिया जा सकता है इसका चित्रण किया है। आचारांग आत्मा और पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार करके गया है। दूसरा श्रुतस्कन्ध मूलतः मुनि-जीवन में भोजन, वस्त्र, पात्र चलता है। वह कर्म की अवधारणा को भी स्वीकार करता है तथा आदि सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार की जाये इसका यह मानता है कि कर्म ही बन्धन के कारण हैं। यदि हम सूक्ष्मता से । विस्तार से विवेचन करता है। इस श्रुतस्कन्ध का अन्तिम भाग जहाँ देखें तो उसमें कर्म को पौद्गलिक मानकर कर्म-शरीर का भी उल्लेख एक ओर महावीर का जीवनवृत्त प्रस्तुत करता है वहीं दूसरी ओर वह किया गया है, और साधक को कहा गया है कि वह कर्म शरीर का इन्द्रिय-विजय की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया पर भी प्रकाश डालता है। ही विधूनन करे। इसी प्रकार आचारांग में आश्रव, संवर और प्रकारान्तर यद्यपि आचारांग का आचारपक्ष व्यावहारिक दृष्टि से कठोर कहा जा से निर्जरा की व्यवस्थायें भी उपलब्ध हो जाती हैं। आचारांग मुक्तात्मा सकता है, किन्तु उसमें साधना के जिस आदर्श स्वरूप का चित्रण के अनिर्वचनीय स्वरूप की भी औपनिषदिक शैली में व्याख्या है, उसके मूल्य को नकारा नहीं जा सकता।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org