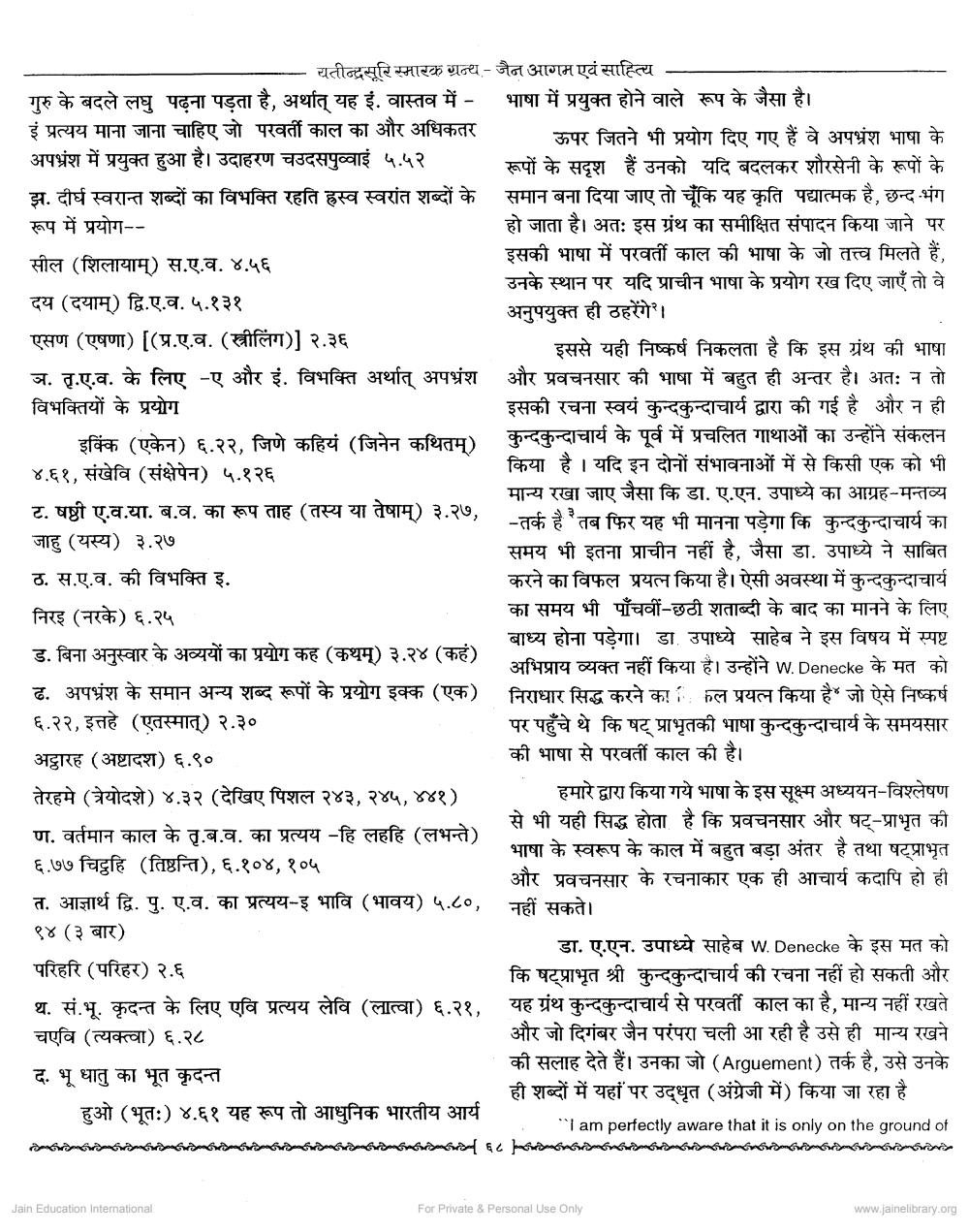________________
- यतीन्द्रसूरिस्मारक ग्रन्थ - जैन आगम एवं साहित्य - गुरु के बदले लघु पढ़ना पड़ता है, अर्थात् यह ई. वास्तव में - भाषा में प्रयुक्त होने वाले रूप के जैसा है। इं प्रत्यय माना जाना चाहिए जो परवर्ती काल का और अधिकतर
ऊपर जितने भी प्रयोग दिए गए हैं वे अपभ्रंश भाषा के अपभ्रंश में प्रयुक्त हुआ है। उदाहरण चउदसपुव्वाइ ५.५२ रूपों के सदश हैं उनको यदि बदलकर शौरसेनी के रूपों के झ. दीर्घ स्वरान्त शब्दों का विभक्ति रहति ह्रस्व स्वरांत शब्दों के समान बना दिया जाए तो चूँकि यह कृति पद्यात्मक है, छन्द भंग रूप में प्रयोग--
हो जाता है। अतः इस ग्रंथ का समीक्षित संपादन किया जाने पर सील (शिलायाम्) स.ए.व. ४.५६
इसकी भाषा में परवर्ती काल की भाषा के जो तत्त्व मिलते हैं,
उनके स्थान पर यदि प्राचीन भाषा के प्रयोग रख दिए जाएँ तो वे दय (दयाम्) द्वि.ए.व. ५.१३१
अनुपयुक्त ही ठहरेंगे। एसण (एषणा) [(प्र.ए.व. (स्त्रीलिंग)] २.३६
इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि इस ग्रंथ की भाषा ञ. तृ.ए.व. के लिए -ए और इं. विभक्ति अर्थात् अपभ्रंश और प्रवचनसार की भाषा में बहुत ही अन्तर है। अतः न तो विभक्तियों के प्रयोग
इसकी रचना स्वयं कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा की गई है और न ही इक्कि (एकेन) ६.२२. जिणे कहियं (जिनेन कथितम) कुन्दकुन्दाचार्य के पूर्व में प्रचलित गाथाओं का उन्होंने संकलन ४.६१, संखेवि (संक्षेपेन) ५.१२६
किया है। यदि इन दोनों संभावनाओं में से किसी एक को भी
मान्य रखा जाए जैसा कि डा. ए.एन. उपाध्ये का आग्रह-मन्तव्य ट. षष्ठी ए.व.या. ब.व. का रूप ताह (तस्य या तेषाम्) ३.२७,
-तर्क है तब फिर यह भी मानना पड़ेगा कि कुन्दकुन्दाचार्य का जाहु (यस्य) ३.२७
समय भी इतना प्राचीन नहीं है, जैसा डा. उपाध्ये ने साबित ठ. स.ए.व. की विभक्ति इ.
करने का विफल प्रयत्न किया है। ऐसी अवस्था में कुन्दकुन्दाचार्य निरइ (नरके) ६.२५
का समय भी पाँचवीं-छठी शताब्दी के बाद का मानने के लिए
बाध्य होना पड़ेगा। डा. उपाध्ये साहेब ने इस विषय में स्पष्ट ड. बिना अनुस्वार के अव्ययों का प्रयोग कह (कथम्) ३.२४ (कह)
अभिप्राय व्यक्त नहीं किया है। उन्होंने W. Denecke के मत को ढ. अपभ्रंश के समान अन्य शब्द रूपों के प्रयोग इक्क (एक) निराधार सिद्ध करने का कल प्रयत्न किया है जो ऐसे निष्कर्ष ६.२२, इत्तहे (एतस्मात्) २.३०
पर पहुँचे थे कि षट् प्राभृतकी भाषा कुन्दकुन्दाचार्य के समयसार अट्ठारह (अष्टादश) ६.९०
की भाषा से परवर्ती काल की है। तेरहमे (त्रेयोदशे) ४.३२ (देखिए पिशल २४३, २४५, ४४१)
हमारे द्वारा किया गये भाषा के इस सूक्ष्म अध्ययन-विश्लेषण
से भी यही सिद्ध होता है कि प्रवचनसार और षट्-प्राभृत की ण. वर्तमान काल के तृ.ब.व. का प्रत्यय -हि लहहि (लभन्ते)
भाषा के स्वरूप के काल में बहुत बड़ा अंतर है तथा षट्प्राभृत ६.७७ चिट्ठहि (तिष्ठन्ति), ६.१०४,१०५ ।।
और प्रवचनसार के रचनाकार एक ही आचार्य कदापि हो ही त. आज्ञार्थ द्वि. प. ए.व. का प्रत्यय-इ भावि (भावय) ५.८०, नहीं सकते। ९४ (३ बार)
डा. ए.एन. उपाध्ये साहेब W. Denecke के इस मत को परिहरि (परिहर) २.६
कि षट्प्राभृत श्री कुन्दकुन्दाचार्य की रचना नहीं हो सकती और थ. सं.भू. कृदन्त के लिए एवि प्रत्यय लेवि (लात्वा) ६.२१, यह ग्रंथ कुन्दकुन्दाचार्य से परवर्ती काल का है, मान्य नहीं रखते चएवि (त्यक्त्वा ) ६.२८
और जो दिगंबर जैन परंपरा चली आ रही है उसे ही मान्य रखने
की सलाह देते हैं। उनका जो (Arguement) तर्क है, उसे उनके द. भू धातु का भूत कृदन्त
ही शब्दों में यहां पर उद्धृत (अंग्रेजी में) किया जा रहा है हुओ (भूतः) ४.६१ यह रूप तो आधुनिक भारतीय आर्य
"I am perfectly aware that it is only on the ground of
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org