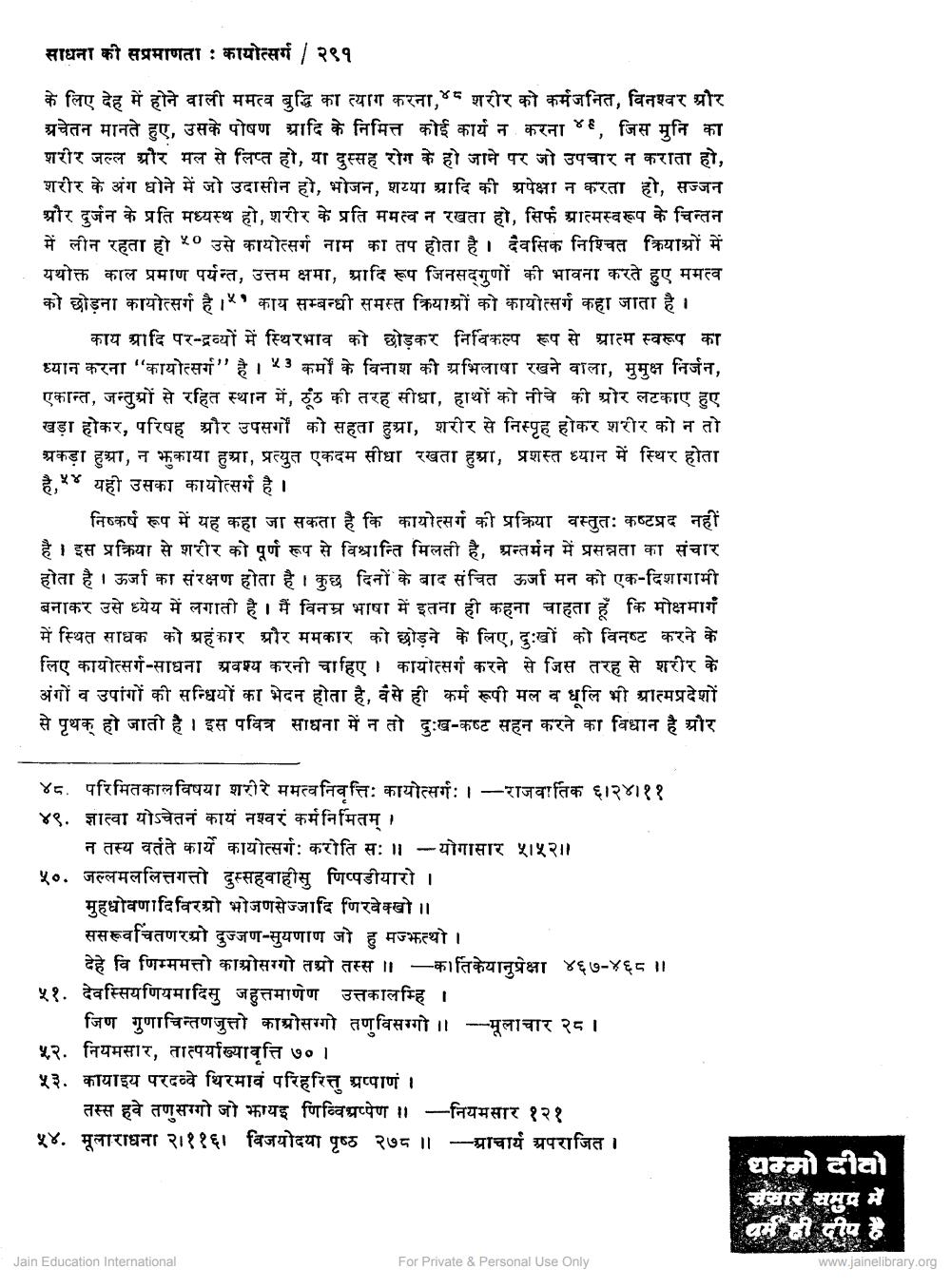________________
साधना की सप्रमाणता : कायोत्सर्ग / २९१
के लिए देह में होने वाली ममत्व बुद्धि का त्याग करना, ४६ शरीर को कर्मजनित, विनश्वर और अचेतन मानते हुए, उसके पोषण आदि के निमित्त कोई कार्य न करना ४६, जिस मुनि का शरीर जल और मल से लिप्त हो, या दुस्सह रोग के हो जाने पर जो उपचार न कराता हो, शरीर के अंग धोने में जो उदासीन हो, भोजन, शय्या आदि की अपेक्षा न करता हो, सज्जन और दुर्जन के प्रति मध्यस्थ हो, शरीर के प्रति ममत्व न रखता हो, सिर्फ आत्मस्वरूप के चिन्तन में लीन रहता हो ५० उसे कायोत्सर्ग नाम का तप होता है । दैवसिक निश्चित क्रियाओं में वोक्त काल प्रमाण पर्यन्त उत्तम क्षमा, प्रादि रूप जिनसद्गुणों की भावना करते हुए ममत्व को छोड़ना कायोत्सर्ग है । " काय सम्बन्धी समस्त क्रियाओं को कायोत्सर्ग कहा जाता है ।
7
काय आदि पर द्रव्यों में स्थिरभाव को छोड़कर निर्विकल्प रूप से प्रात्म स्वरूप का ध्यान करना " कायोत्सर्ग" है । ५३ कर्मों के विनाश की अभिलाषा रखने वाला, मुमुक्ष निर्जन, एकान्त, जन्तुओं से रहित स्थान में, ठूंठ की तरह सीधा, हाथों को नीचे की ओर लटकाए हुए खड़ा होकर, परिषह और उपसर्गों को सहता हुआ, शरीर से निस्पृह होकर शरीर को न तो अकड़ा हुआ, न झुकाया हुआ, प्रत्युत एकदम सीधा रखता हुआ प्रशस्त ध्यान में स्थिर होता है, ५४ यही उसका कायोत्सर्ग है।
1
श्रन्तर्मन में प्रसन्नता का संचार
ऊर्जा मन को एक दिशागामी
निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि कायोत्सर्ग की प्रक्रिया वस्तुतः कष्टप्रद नहीं है । इस प्रक्रिया से शरीर को पूर्ण रूप से विश्रान्ति मिलती है, होता है । ऊर्जा का संरक्षण होता है । कुछ दिनों के बाद संचित बनाकर उसे ध्येय में लगाती है । मैं विनम्र भाषा में इतना ही कहना चाहता हूँ कि मोक्षमार्ग में स्थित साधक को अहंकार और ममकार को छोड़ने के लिए दुःखों को विनष्ट करने के लिए कायोत्सर्ग साधना प्रवश्य करनी चाहिए। कायोत्सर्ग करने से जिस तरह से शरीर के अंगों व उपांगों की सन्धियों का भेदन होता है, वैसे ही कर्म रूपी मल व धूलि भी आत्मप्रदेशों से पृथक् हो जाती है। इस पवित्र साधना में न तो दुःख कष्ट सहन करने का विधान है और
४८. परिमितकालविषया शरीरे ममत्वनिवृत्तिः कायोत्सर्गः राजवार्तिक ६।२४।११ ४९. ज्ञात्वा योऽचेतनं कार्य नश्वरं कर्म निर्मितम् ।
न तस्य वर्तते कार्ये कायोत्सर्गः करोति सः ॥ - योगासार ५। ५२ ।।
५०. जल्वमललितगत्तो दुस्सहवाहीसु णिप्पडीयारो । मुहघोषणादिविरयो भोजणसेज्जादि णिरवेक्खो ॥
ससरूवचितणर दुज्जण सुयणाण जो हु मज्झत्थो । देहे वणिग्ममतो काम्रोसग्गो तम्रो तस्स ॥ ५१. देवस्सियणियमादिसु जहत्तमाणेण उत्तकालम्हि ।
|
कार्तिकेयानुप्रेक्षा ४६७-४६८ ।।
जिण गुणाचिन्तणजुत्तो काधीसम्मो तणुविसम्गो । मूलाचार २६ ।
५२. नियमसार, तात्पर्याख्यावृत्ति ७० ।
५३. कायाइय परदव्वे थिरमावं परिहरितु अप्पाणं । तस्स हवे तणुसग्गो जो कायइ णिविप्पेण | ५४. मूलाराधना २।११६ | विजयोदया पृष्ठ २७८ ।।
||
Jain Education International
नियमसार १२१ प्राचार्य अपराजित ।
For Private & Personal Use Only
धम्मो दोवो संचार समुद्र में धर्म ही दीप है
www.jainelibrary.org