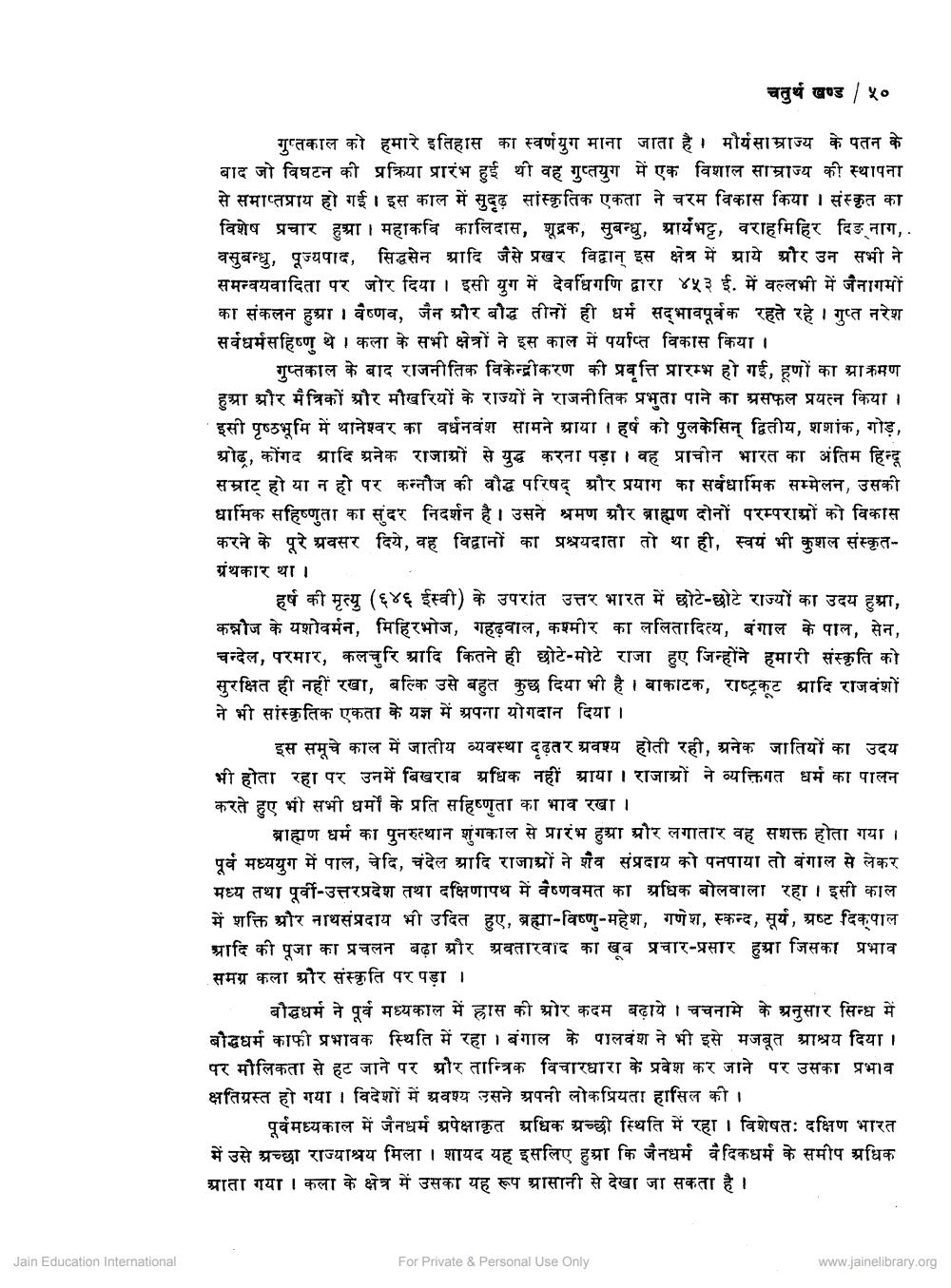________________
चतुर्थ खण्ड | ५०
गुप्तकाल को हमारे इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी वह गुप्तयुग में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना से समाप्तप्राय हो गई। इस काल में सुदृढ़ सांस्कृतिक एकता ने चरम विकास किया । संस्कृत का विशेष प्रचार हुआ। महाकवि कालिदास, शूद्रक, सुबन्धु, आर्यभट्ट, वराहमिहिर दिङ नाग, . वसुबन्धु, पूज्यपाद, सिद्धसेन आदि जैसे प्रखर विद्वान इस क्षेत्र में पाये और उन सभी ने समन्वयवादिता पर जोर दिया। इसी युग में देवधिगणि द्वारा ४५३ ई. में वल्लभी में जैनागमों का संकलन हुआ। वैष्णव, जैन और बौद्ध तीनों ही धर्म सद्भावपूर्वक रहते रहे । गुप्त नरेश सर्वधर्मसहिष्ण थे। कला के सभी क्षेत्रों ने इस काल में पर्याप्त विकास किया।
गुप्तकाल के बाद राजनीतिक विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति प्रारम्भ हो गई, हणों का आक्रमण हा और मैत्रिकों और मौखरियों के राज्यों ने राजनीतिक प्रभुता पाने का असफल प्रयत्न किया। इसी पृष्ठभूमि में थानेश्वर का वर्धनवंश सामने आया। हर्ष को पुलकेसिन् द्वितीय, शशांक, गोड़, अोढ, कोंगद आदि अनेक राजाओं से युद्ध करना पड़ा। वह प्राचीन भारत का अंतिम हिन्दू सम्राट हो या न हो पर कन्नौज की वौद्ध परिषद् और प्रयाग का सर्वधार्मिक सम्मेलन, उसकी धार्मिक सहिष्णुता का संदर निदर्शन है। उसने श्रमण और ब्राह्मण दोनों परम्पराओं को विकास करने के पूरे अवसर दिये, वह विद्वानों का प्रश्रयदाता तो था ही, स्वयं भी कुशल संस्कृतग्रंथकार था।
हर्ष की मृत्यु (६४६ ईस्वी) के उपरांत उत्तर भारत में छोटे-छोटे राज्यों का उदय हमा, कन्नौज के यशोवर्मन, मिहिरभोज, गहढ़वाल, कश्मीर का ललितादित्य, बंगाल के पाल, सेन, चन्देल, परमार, कलचुरि आदि कितने ही छोटे-मोटे राजा हुए जिन्होंने हमारी संस्कृति को सुरक्षित ही नहीं रखा, बल्कि उसे बहुत कुछ दिया भी है । बाकाटक, राष्ट्रकूट आदि राजवंशों ने भी सांस्कृतिक एकता के यज्ञ में अपना योगदान दिया।
इस समूचे काल में जातीय व्यवस्था दृढ़तर अवश्य होती रही, अनेक जातियों का उदय भी होता रहा पर उनमें बिखराब अधिक नहीं आया। राजाओं ने व्यक्तिगत धर्म का पालन करते हुए भी सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखा।
ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान शुंगकाल से प्रारंभ हुआ और लगातार वह सशक्त होता गया। पूर्व मध्ययुग में पाल, चेदि, चंदेल आदि राजाओं ने शैव संप्रदाय को पनपाया तो बंगाल से लेकर मध्य तथा पूर्वी-उत्तरप्रदेश तथा दक्षिणापथ में वैष्णवमत का अधिक बोलवाला रहा । इसी काल में शक्ति और नाथसंप्रदाय भी उदित हुए, ब्रह्मा-विष्णु-महेश, गणेश, स्कन्द, सूर्य, अष्ट दिक्पाल श्रादि की पूजा का प्रचलन बढ़ा और अवतारवाद का खूब प्रचार-प्रसार हुआ जिसका प्रभाव समग्र कला और संस्कृति पर पड़ा ।
बौद्धधर्म ने पूर्व मध्यकाल में ह्रास की ओर कदम बढ़ाये । चचनामे के अनुसार सिन्ध में बौद्धधर्म काफी प्रभावक स्थिति में रहा । बंगाल के पालवंश ने भी इसे मजबूत आश्रय दिया। पर मौलिकता से हट जाने पर और तान्त्रिक विचारधारा के प्रवेश कर जाने पर उसका प्रभाव क्षतिग्रस्त हो गया। विदेशों में अवश्य उसने अपनी लोकप्रियता हासिल की।
पूर्वमध्यकाल में जैनधर्म अपेक्षाकृत अधिक अच्छी स्थिति में रहा । विशेषतः दक्षिण भारत में उसे अच्छा राज्याश्रय मिला । शायद यह इसलिए हुआ कि जैनधर्म वैदिकधर्म के समीप अधिक प्राता गया । कला के क्षेत्र में उसका यह रूप आसानी से देखा जा सकता है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org