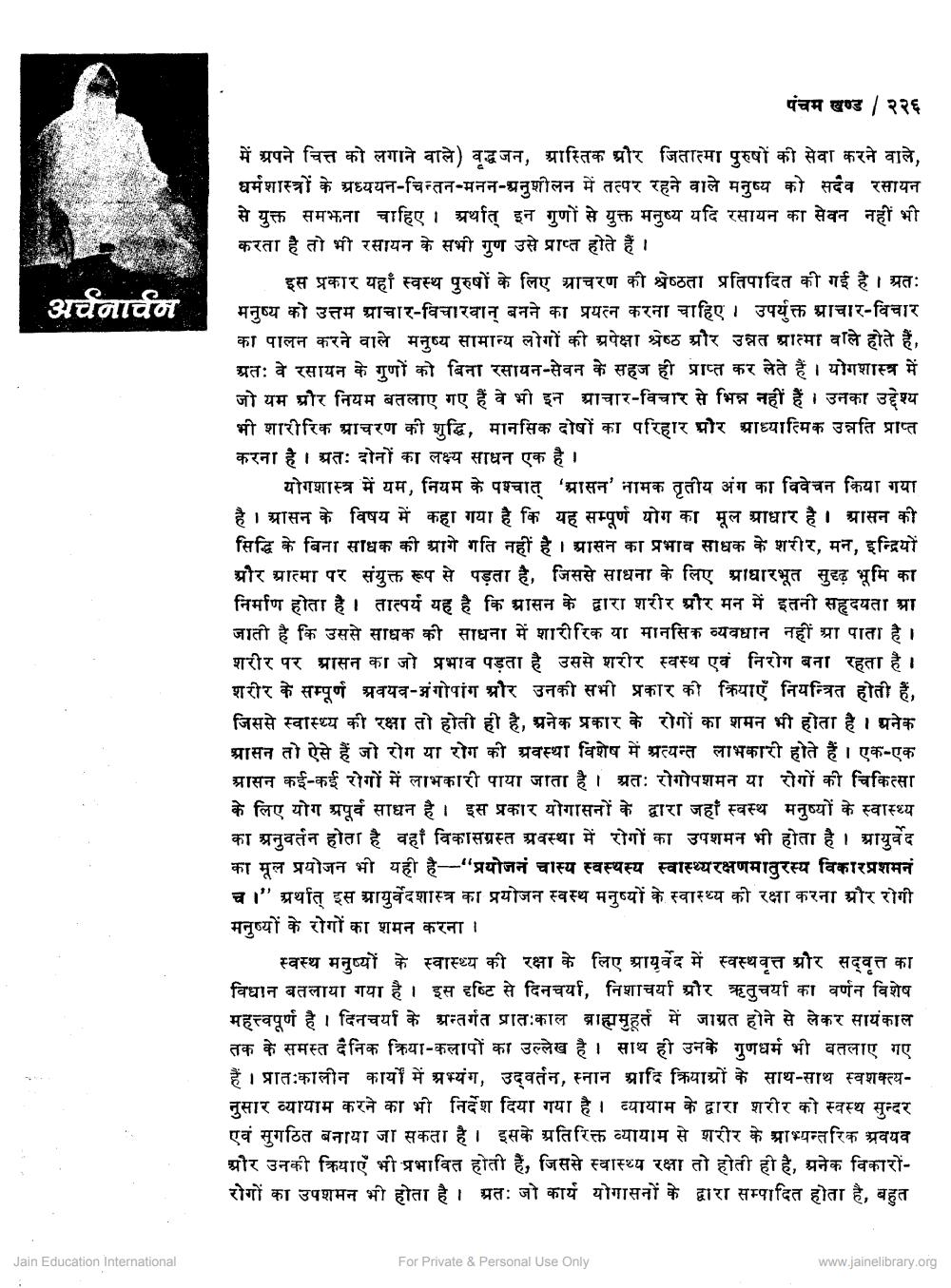________________
पंचम खण्ड | २२६
अर्चनार्चन
में अपने चित्त को लगाने वाले) वद्ध जन, आस्तिक और जितात्मा पुरुषों की सेवा करने वाले, धर्मशास्त्रों के अध्ययन-चिन्तन-मनन-अनुशीलन में तत्पर रहने वाले मनुष्य को सदैव रसायन से युक्त समझना चाहिए। अर्थात् इन गुणों से युक्त मनुष्य यदि रसायन का सेवन नहीं भी करता है तो भी रसायन के सभी गुण उसे प्राप्त होते हैं ।
इस प्रकार यहाँ स्वस्थ पुरुषों के लिए ग्राचरण की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है। अतः मनुष्य को उत्तम प्राचार-विचारवान बनने का प्रयत्न करना चाहिए। उपर्युक्त आचार-विचार का पालन करने वाले मनुष्य सामान्य लोगों की अपेक्षा श्रेष्ठ और उन्नत प्रात्मा वाले होते हैं, अत: वे रसायन के गुणों को बिना रसायन-सेवन के सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। योगशास्त्र में जो यम और नियम बतलाए गए हैं वे भी इन प्राचार-विचार से भिन्न नहीं हैं। उनका उद्देश्य भी शारीरिक आचरण की शुद्धि, मानसिक दोषों का परिहार पोर आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना है। अतः दोनों का लक्ष्य साधन एक है।
योगशास्त्र में यम, नियम के पश्चात 'पासन' नामक तृतीय अंग का विवेचन किया गया है । आसन के विषय में कहा गया है कि यह सम्पूर्ण योग का मूल आधार है। आसन की सिद्धि के बिना साधक की आगे गति नहीं है । आसन का प्रभाव साधक के शरीर, मन, इन्द्रियों
और प्रात्मा पर संयुक्त रूप से पड़ता है, जिससे साधना के लिए प्राधारभूत सुदृढ़ भूमि का निर्माण होता है। तात्पर्य यह है कि प्रासन के द्वारा शरीर और मन में इतनी सहृदयता प्रा जाती है कि उससे साधक की साधना में शारीरिक या मानसिक व्यवधान नहीं आ पाता है। शरीर पर प्रासन का जो प्रभाव पड़ता है उससे शरीर स्वस्थ एवं निरोग बना रहता है। शरीर के सम्पूर्ण अवयव-अंगोपांग और उनकी सभी प्रकार की क्रियाएँ नियन्त्रित होती हैं, जिससे स्वास्थ्य की रक्षा तो होती ही है, अनेक प्रकार के रोगों का शमन भी होता है। अनेक प्रासन तो ऐसे हैं जो रोग या रोग की अवस्था विशेष में अत्यन्त लाभकारी होते हैं। एक-एक प्रासन कई-कई रोगों में लाभकारी पाया जाता है। अतः रोगोपशमन या रोगों की चिकित्सा के लिए योग अपूर्व साधन है। इस प्रकार योगासनों के द्वारा जहाँ स्वस्थ मनुष्यों के स्वास्थ्य का अनुवर्तन होता है वहाँ विकासग्रस्त अवस्था में रोगों का उपशमन भी होता है। आयुर्वेद का मूल प्रयोजन भी यही है-"प्रयोजनं चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणमातुरस्य विकारप्रशमनं च।" अर्थात् इस आयुर्वेदशास्त्र का प्रयोजन स्वस्थ मनुष्यों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी मनुष्यों के रोगों का शमन करना ।
स्वस्थ मनुष्यों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आयुर्वेद में स्वस्थवृत्त और सद्वत्त का विधान बतलाया गया है। इस दृष्टि से दिनचर्या, निशाचर्या और ऋतुचर्या का वर्णन विशेष महत्त्वपूर्ण है । दिनचर्या के अन्तर्गत प्रातःकाल ब्राह्ममुहूर्त में जाग्रत होने से लेकर सायंकाल तक के समस्त दैनिक क्रिया-कलापों का उल्लेख है। साथ ही उनके गुणधर्म भी बतलाए गए हैं। प्रातःकालीन कार्यों में अभ्यंग, उद्वर्तन, स्नान आदि क्रियाओं के साथ-साथ स्वशक्त्यनुसार व्यायाम करने का भी निर्देश दिया गया है। व्यायाम के द्वारा शरीर को स्वस्थ सुन्दर एवं सुगठित बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त व्यायाम से शरीर के प्राभ्यन्तरिक अवयव और उनकी क्रियाएँ भी प्रभावित होती हैं, जिससे स्वास्थ्य रक्षा तो होती ही है, अनेक विकारोंरोगों का उपशमन भी होता है। अतः जो कार्य योगासनों के द्वारा सम्पादित होता है, बहुत
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org