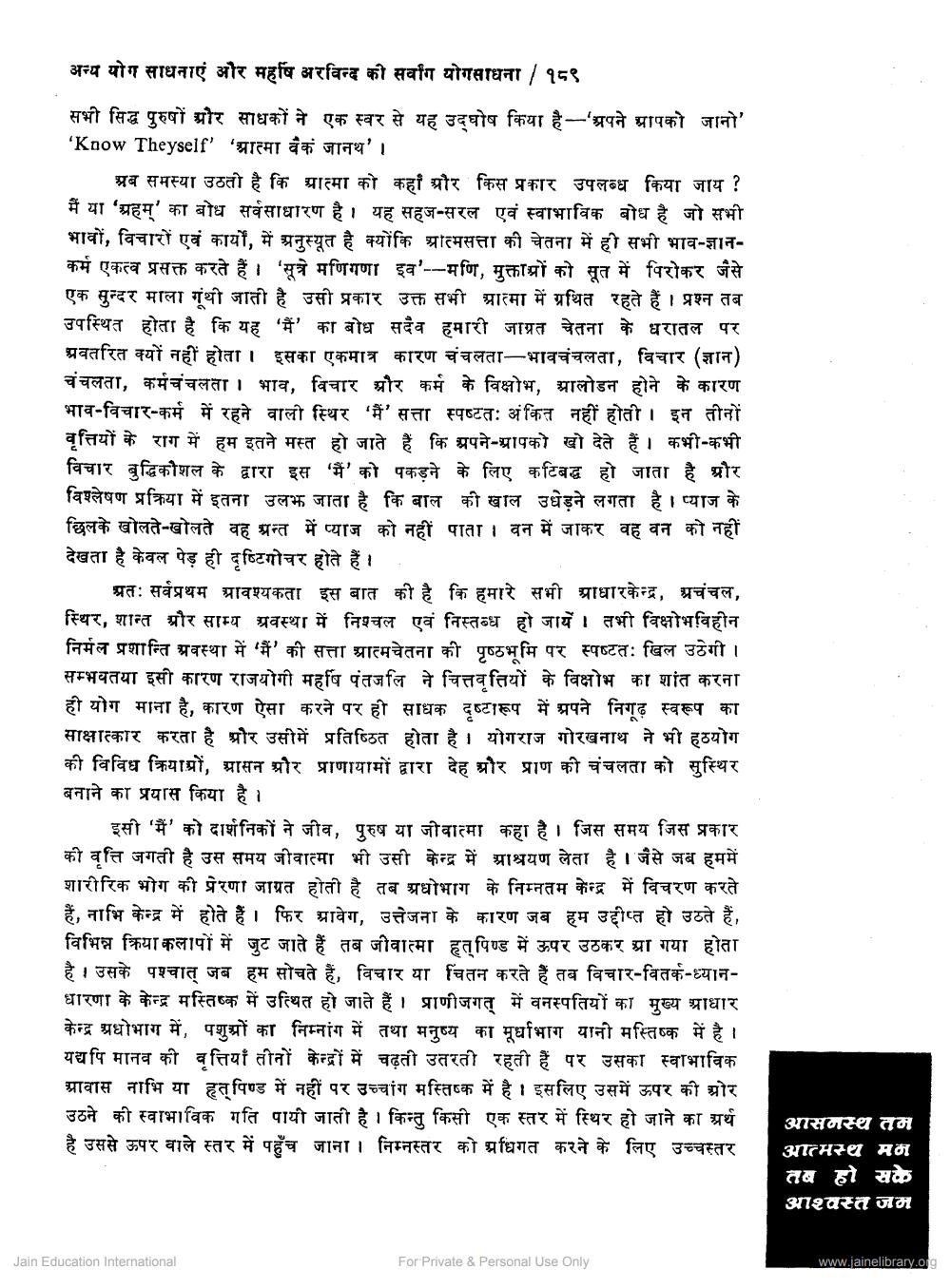________________
अन्य योग साधनाएं और महर्षि अरविन्द की सर्वांग योगसाधना / १८९
सभी सिद्ध पुरुषों और साधकों ने एक स्वर से यह उद्घोष किया है-'अपने पापको जानो' 'Know Theyself' 'आत्मा वैकं जानथ' ।
अब समस्या उठती है कि प्रात्मा को कहाँ और किस प्रकार उपलब्ध किया जाय ? मैं या 'अहम्' का बोध सर्वसाधारण है। यह सहज-सरल एवं स्वाभाविक बोध है जो सभी भावों, विचारों एवं कार्यों, में अनुस्यूत है क्योंकि आत्मसत्ता की चेतना में ही सभी भाव-ज्ञानकर्म एकत्व प्रसक्त करते हैं। 'सूत्रे मणिगणा इव'--मणि, मुक्तानों को सूत में पिरोकर जैसे एक सुन्दर माला गंथी जाती है उसी प्रकार उक्त सभी आत्मा में ग्रथित रहते हैं। प्रश्न तब उपस्थित होता है कि यह 'मैं' का बोध सदैव हमारी जाग्रत चेतना के धरातल पर प्रवतरित क्यों नहीं होता। इसका एकमात्र कारण चंचलता-भावचंचलता, विचार (ज्ञान) चंचलता, कर्मचंचलता। भाव, विचार और कर्म के विक्षोभ, आलोडन होने के कारण भाव-विचार-कर्म में रहने वाली स्थिर 'मैं' सत्ता स्पष्टतः अंकित नहीं होती। इन तीनों वृत्तियों के राग में हम इतने मस्त हो जाते हैं कि अपने-पापको खो देते हैं। कभी-कभी विचार बुद्धिकौशल के द्वारा इस 'मैं' को पकड़ने के लिए कटिबद्ध हो जाता है और विश्लेषण प्रक्रिया में इतना उलझ जाता है कि बाल की खाल उधेड़ने लगता है। प्याज के छिलके खोलते-खोलते वह अन्त में प्याज को नहीं पाता। वन में जाकर वह वन को नहीं देखता है केवल पेड़ ही दृष्टिगोचर होते हैं।
अतः सर्वप्रथम आवश्यकता इस बात की है कि हमारे सभी प्राधारकेन्द्र, अचंचल, स्थिर, शान्त और साम्य अवस्था में निश्चल एवं निस्तब्ध हो जायें। तभी विक्षोभविहीन निर्मल प्रशान्ति अवस्था में 'मैं' की सत्ता आत्मचेतना की पृष्ठभमि पर स्पष्टत: खिल उठेगी। सम्भवतया इसी कारण राजयोगी महर्षि पंतजलि ने चित्तवत्तियों के विक्षोभ का शांत करना ही योग माना है, कारण ऐसा करने पर ही साधक दृष्टारूप में अपने निगूढ़ स्वरूप का साक्षात्कार करता है और उसीमें प्रतिष्ठित होता है। योगराज गोरखनाथ ने भी हठयोग की विविध क्रियानों, ग्रासन और प्राणायामों द्वारा देह और प्राण की चंचलता को सुस्थिर बनाने का प्रयास किया है।
इसी 'मैं' को दार्शनिकों ने जीव, पुरुष या जीवात्मा कहा है। जिस समय जिस प्रकार की वत्ति जगती है उस समय जीवात्मा भी उसी केन्द्र में प्राश्रयण लेता है। जैसे जब हममें शारीरिक भोग की प्रेरणा जाग्रत होती है तब अधोभाग के निम्नतम केन्द्र में विचरण करते हैं, नाभि केन्द्र में होते हैं। फिर आवेग, उत्तेजना के कारण जब हम उद्दीप्त हो उठते हैं, विभिन्न क्रियाकलापों में जुट जाते हैं तब जीवात्मा हृत पिण्ड में ऊपर उठकर पा गया होता है। उसके पश्चात् जब हम सोचते हैं, विचार या चितन करते हैं तब विचार-वितर्क-ध्यानधारणा के केन्द्र मस्तिष्क में उत्थित हो जाते हैं। प्राणीजगत् में वनस्पतियों का मुख्य आधार केन्द्र अधोभाग में, पशुओं का निम्नांग में तथा मनुष्य का मूर्धाभाग यानी मस्तिष्क में है। यद्यपि मानव की वृत्तियाँ तीनों केन्द्रों में चढ़ती उतरती रहती हैं पर उसका स्वाभाविक आवास नाभि या हृत पिण्ड में नहीं पर उच्चांग मस्तिष्क में है। इसलिए उसमें ऊपर की ओर उठने की स्वाभाविक गति पायी जाती है। किन्तु किसी एक स्तर में स्थिर हो जाने का अर्थ है उससे ऊपर वाले स्तर में पहुँच जाना। निम्नस्तर को अधिगत करने के लिए उच्चस्तर
आसनस्थ तम आत्मस्थ मन तब हो सके आश्वस्त जम
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org