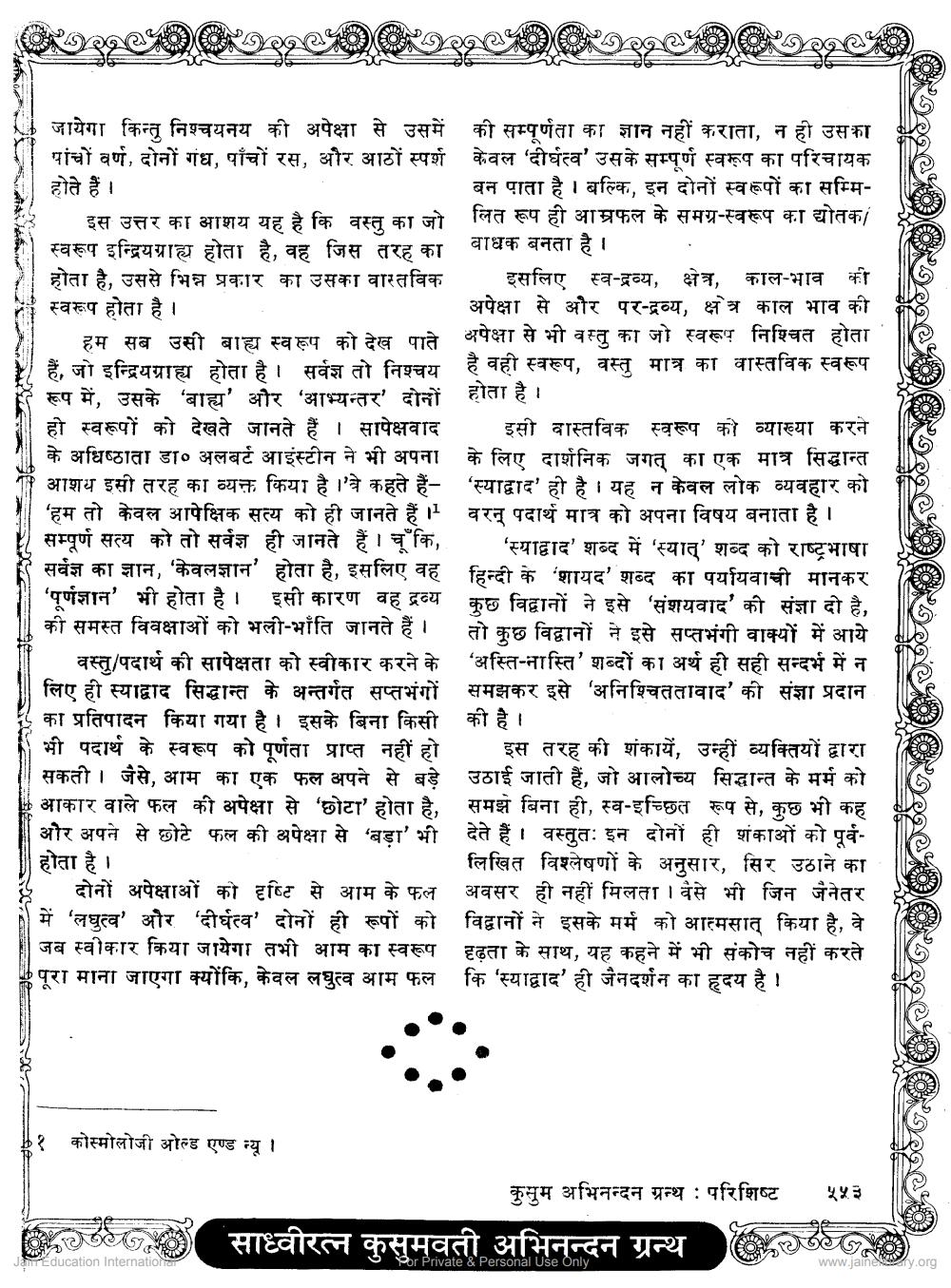________________
KO जायेगा किन्तु निश्चयनय की अपेक्षा से उसमें की सम्पूर्णता का ज्ञान नहीं कराता, न ही उसका
पांचों वर्ण, दोनों गंध, पाँचों रस, और आठों स्पर्श केवल 'दीर्घत्व' उसके सम्पूर्ण स्वरूप का परिचायक होते हैं।
बन पाता है । बल्कि, इन दोनों स्वरूपों का सम्मिइस उत्तर का आशय यह है कि वस्त का जो लित रूप ही आम्रफल के समग्र-स्वरूप का द्योतका स्वरूप इन्द्रियग्राह्य होता है, वह जिस तरह का बाधक बनता है। होता है, उससे भिन्न प्रकार का उसका वास्तविक इसलिए स्व-द्रव्य, क्षेत्र, काल-भाव की । स्वरूप होता है।
अपेक्षा से और पर-द्रव्य, क्षेत्र काल भाव की हम सब उसी बाह्य स्वरूप को देख पाते अपेक्षा से भी वस्तु का जो स्वरूप निश्चित होता 1 हैं, जो इन्द्रियग्राह्य होता है। सर्वज्ञ तो निश्चय है वही स्वरूप, वस्तु मात्र का वास्तविक स्वरूप
रूप में, उसके 'बाह्य' और 'आभ्यन्तर' दोनों होता है। हो स्वरूपों को देखते जानते हैं । सापेक्षवाद इसी वास्तविक स्वरूप को व्याख्या करने के अधिष्ठाता डा० अलबर्ट आइंस्टीन ने भी अपना के लिए दार्शनिक जगत का एक मात्र सिद्धान्त । आशय इसी तरह का व्यक्त किया है । वे कहते हैं- 'स्याद्वाद' ही है। यह न केवल लोक व्यवहार को 'हम तो केवल आपेक्षिक सत्य को ही जानते हैं। वरन् पदार्थ मात्र को अपना विषय बनाता है। । सम्पूर्ण सत्य को तो सर्वज्ञ ही जानते हैं। चू कि, 'स्याद्वाद' शब्द में 'स्यात' शब्द को राष्ट्रभाषा
सर्वज्ञ का ज्ञान, 'केवलज्ञान' होता है, इसलिए वह हिन्दी के 'शायद' शब्द का पर्यायवाची मानकर 'पूर्णज्ञान' भी होता है। इसी कारण वह द्रव्य कुछ विद्वानों ने इसे 'संशयवाद' की संज्ञा दो है, की समस्त विवक्षाओं को भली-भाँति जानते हैं। तो कुछ विद्वानों ने इसे सप्तभंगी वाक्यों में आये ___वस्तु/पदार्थ की सापेक्षता को स्वीकार करने के अस्ति-नास्ति' शब्दों का अर्थ ही सही सन्दर्भ में न लिए ही स्याद्वाद सिद्धान्त के अन्तर्गत सप्तभंगों समझकर इसे 'अनिश्चिततावाद' की संज्ञा प्रदान का प्रतिपादन किया गया है। इसके बिना किसी की है। भी पदार्थ के स्वरूप को पूर्णता प्राप्त नहीं हो इस तरह की शंकायें, उन्हीं व्यक्तियों द्वारा सकती। जैसे, आम का एक फल अपने से बड़े उठाई जाती हैं, जो आलोच्य सिद्धान्त के मर्म को आकार वाले फल की अपेक्षा से 'छोटा होता है, समझ बिना ही, स्व-इच्छित रूप से, कुछ भी कह और अपने से छोटे फल की अपेक्षा से 'बड़ा' भी देते हैं । वस्तुतः इन दोनों ही शंकाओं को पूर्वहोता है।
लिखित विश्लेषणों के अनुसार, सिर उठाने का दोनों अपेक्षाओं को दृष्टि से आम के फल अवसर ही नहीं मिलता। वैसे भी जिन जैनेतर में 'लघुत्व' और 'दीर्घत्व' दोनों ही रूपों को विद्वानों ने इसके मर्म को आत्मसात् किया है, वे जब स्वीकार किया जायेगा तभी आम का स्वरूप दृढता के साथ, यह कहने में भी संकोच नहीं करते पूरा माना जाएगा क्योंकि, केवल लघुत्व आम फल कि 'स्याद्वाद' ही जैनदर्शन का हृदय है।
१ कोस्मोलोजी ओल्ड एण्ड न्यू ।
५५३
2.
कुसुम अभिनन्दन ग्रन्थ : परिशिष्ट साध्वीरत्न कुसुमवती अभिनन्दन ग्रन्थ
Jan Education Internatione
Por Private & Personal Use Only
v.jainenery.org