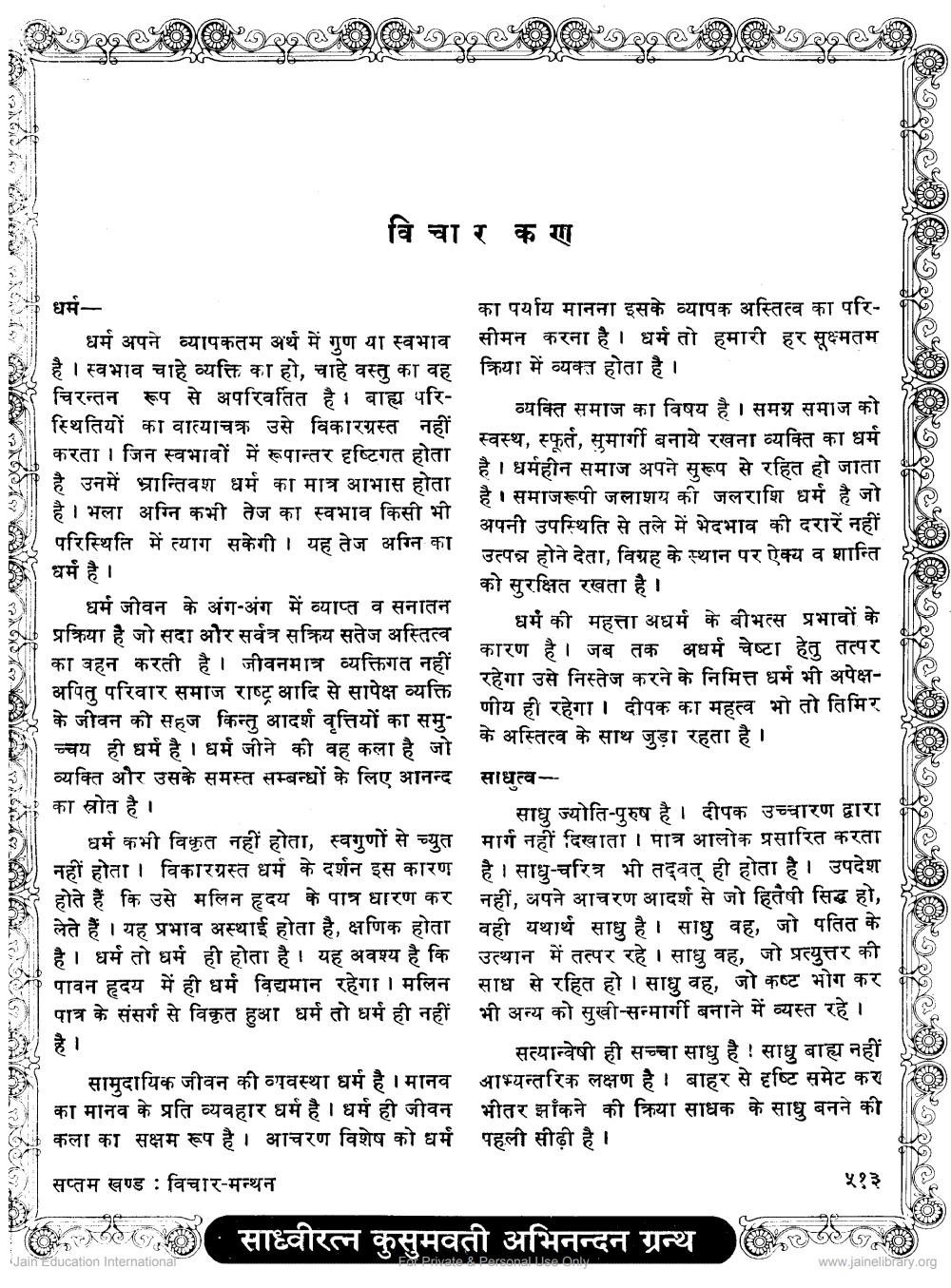________________
%
80
वि चा र
क
ण
धर्म
का पर्याय मानना इसके व्यापक अस्तित्व का परिधर्म अपने व्यापकतम अर्थ में गुण या स्वभाव सीमन करना है। धर्म तो हमारी हर सूक्ष्मतम है । स्वभाव चाहे व्यक्ति का हो, चाहे वस्तु का वह क्रिया में व्यक्त होता है । चिरन्तन रूप से अपरिवर्तित है। बाह्य परि- व्यक्ति समाज का विषय है । समग्र समाज को स्थितियों का वात्याचक्र उसे विकारग्रस्त नहीं करता । जिन स्वभावों में रूपान्तर दृष्टिगत होता
- स्वस्थ, स्फूर्त, सुमार्गी बनाये रखना व्यक्ति का धर्म है उनमें भ्रान्तिवश धर्म का मात्र आभास होता
है। धर्महीन समाज अपने सुरूप से रहित हो जाता
है। समाजरूपी जलाशय की जलराशि धर्म है जो है । भला अग्नि कभी तेज का स्वभाव किसी भी
अपनी उपस्थिति से तले में भेदभाव की दरारें नहीं परिस्थिति में त्याग सकेगी। यह तेज अग्नि का
उत्पन्न होने देता, विग्रह के स्थान पर ऐक्य व शान्ति धर्म है।
को सुरक्षित रखता है। धर्म जीवन के अंग-अंग में व्याप्त व सनातन
धर्म की महत्ता अधर्म के बीभत्स प्रभावों के प्रक्रिया है जो सदा और सर्वत्र सक्रिय सतेज अस्तित्व का वहन करती है। जीवनमात्र व्यक्तिगत नहीं
* कारण है। जब तक अधर्म चेष्टा हेतु तत्पर
रहेगा उसे निस्तेज करने के निमित्त धर्म भी अपेक्षअपितु परिवार समाज राष्ट्र आदि से सापेक्ष व्यक्ति के जीवन को सहज किन्तु आदर्श वत्तियों का सम- णाय हो रहेगा। दीपक का महत्व भो तो तिमिर च्चय ही धर्म है। धर्म जीने की वह कला है जो
के अस्तित्व के साथ जुड़ा रहता है। व्यक्ति और उसके समस्त सम्बन्धों के लिए आनन्द साधुत्वका स्रोत है।
साधु ज्योति-पुरुष है। दीपक उच्चारण द्वारा का धर्म कभी विकृत नहीं होता, स्वगुणों से च्युत मार्ग नहीं दिखाता । मात्र आलोक प्रसारित करता नहीं होता। विकारग्रस्त धर्म के दर्शन इस कारण है। साधु-चरित्र भी तद्वत् ही होता है। उपदेश होते हैं कि उसे मलिन हृदय के पात्र धारण कर नहीं, अपने आचरण आदर्श से जो हितैषी सिद्ध हो, लेते हैं । यह प्रभाव अस्थाई होता है, क्षणिक होता वही यथार्थ साधु है । साधु वह, जो पतित के है। धर्म तो धर्म ही होता है। यह अवश्य है कि उत्थान में तत्पर रहे । साधु वह, जो प्रत्युत्तर की पावन हृदय में ही धर्म विद्यमान रहेगा। मलिन साध से रहित हो । साधु वह, जो कष्ट भोग कर पात्र के संसर्ग से विकृत हुआ धर्म तो धर्म ही नहीं भी अन्य को सुखी-सन्मार्गी बनाने में व्यस्त रहे।
सत्यान्वेषी ही सच्चा साधु है ! साधु बाह्य नहीं सामुदायिक जीवन की व्यवस्था धर्म है । मानव आभ्यन्तरिक लक्षण है। बाहर से दृष्टि समेट कर का मानव के प्रति व्यवहार धर्म है । धर्म ही जीवन भीतर झाँकने की क्रिया साधक के साधु बनने की कला का सक्षम रूप है। आचरण विशेष को धर्म पहली सीढ़ी है। सप्तम खण्ड : विचार-मन्थन
५१३
CHASE
(ONE
60 साध्वीरत्न कुसुमवती अभिनन्दन ग्रन्थ
Jain Education International
private
Personalilse.Only
www.jainelibrary.org