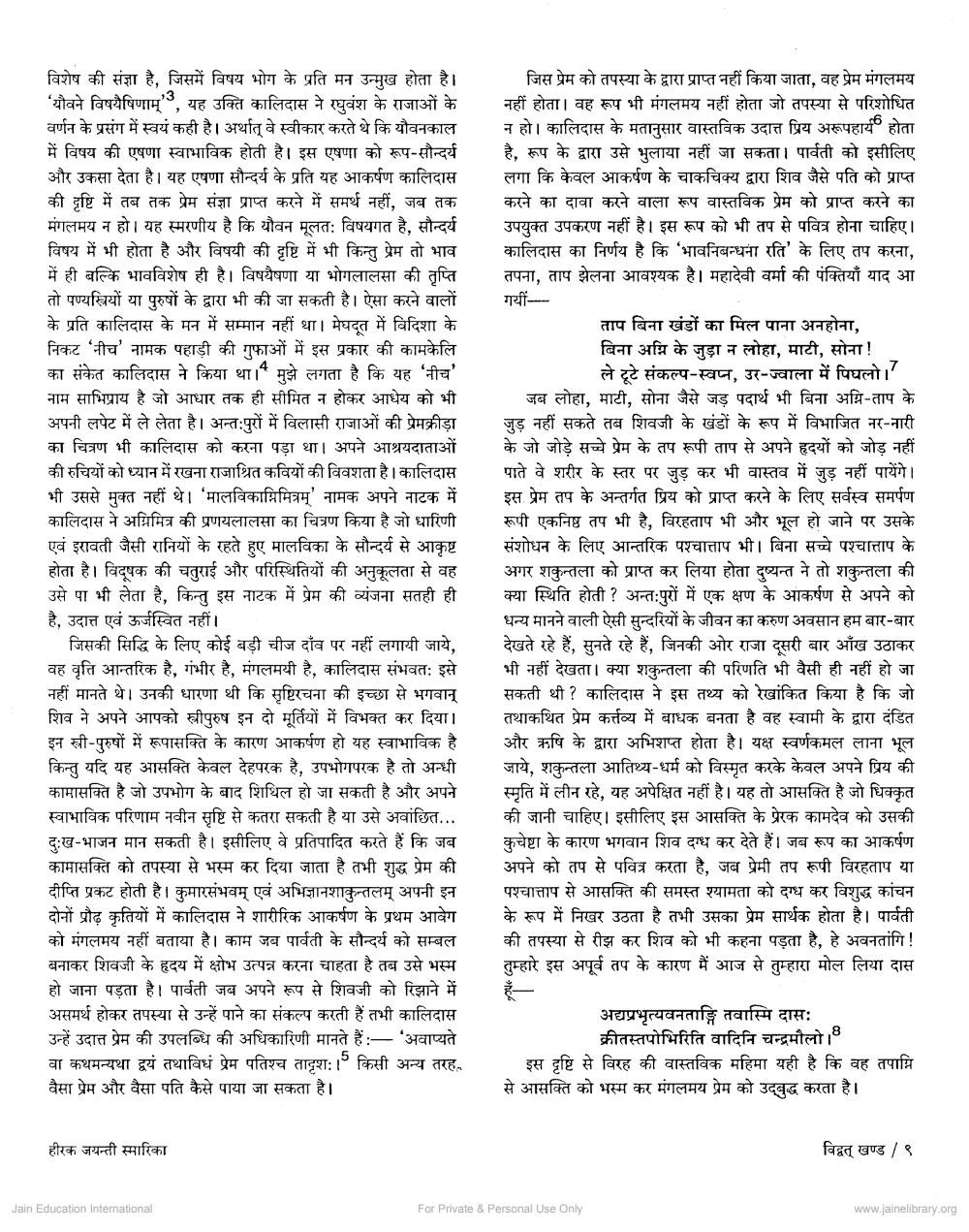________________
विशेष की संज्ञा है, जिसमें विषय भोग के प्रति मन उन्मुख होता है। 'यौवने विषयैषिणाम्'3, यह उक्ति कालिदास ने रघुवंश के राजाओं के वर्णन के प्रसंग में स्वयं कही है। अर्थात् वे स्वीकार करते थे कि यौवनकाल में विषय की एषणा स्वाभाविक होती है। इस एषणा को रूप-सौन्दर्य और उकसा देता है। यह एषणा सौन्दर्य के प्रति यह आकर्षण कालिदास की दृष्टि में तब तक प्रेम संज्ञा प्राप्त करने में समर्थ नहीं, जब तक मंगलमय न हो। यह स्मरणीय है कि यौवन मूलत: विषयगत है, सौन्दर्य विषय में भी होता है और विषयी की दृष्टि में भी किन्तु प्रेम तो भाव में ही बल्कि भावविशेष ही है। विषयैषणा या भोगलालसा की तृप्ति तो पण्यस्त्रियों या पुरुषों के द्वारा भी की जा सकती है। ऐसा करने वालों के प्रति कालिदास के मन में सम्मान नहीं था। मेघदूत में विदिशा के निकट 'नीच' नामक पहाड़ी की गुफाओं में इस प्रकार की कामकेलि का संकेत कालिदास ने किया था। मुझे लगता है कि यह 'नीच' नाम साभिप्राय है जो आधार तक ही सीमित न होकर आधेय को भी अपनी लपेट में ले लेता है। अन्त:पुरों में विलासी राजाओं की प्रेमक्रीड़ा का चित्रण भी कालिदास को करना पड़ा था। अपने आश्रयदाताओं की रुचियों को ध्यान में रखना राजाश्रित कवियों की विवशता है। कालिदास भी उससे मुक्त नहीं थे। 'मालविकाग्निमित्रम्' नामक अपने नाटक में कालिदास ने अग्निमित्र की प्रणयलालसा का चित्रण किया है जो धारिणी एवं इरावती जैसी रानियों के रहते हुए मालविका के सौन्दर्य से आकृष्ट होता है। विदूषक की चतुराई और परिस्थितियों की अनुकूलता से वह उसे पा भी लेता है, किन्तु इस नाटक में प्रेम की व्यंजना सतही ही है, उदात्त एवं ऊर्जस्वित नहीं।
जिसकी सिद्धि के लिए कोई बड़ी चीज दाँव पर नहीं लगायी जाये, वह वृत्ति आन्तरिक है, गंभीर है, मंगलमयी है, कालिदास संभवत: इसे नहीं मानते थे। उनकी धारणा थी कि सृष्टिरचना की इच्छा से भगवान् शिव ने अपने आपको स्त्रीपुरुष इन दो मूर्तियों में विभक्त कर दिया। इन स्त्री-पुरुषों में रूपासक्ति के कारण आकर्षण हो यह स्वाभाविक है किन्तु यदि यह आसक्ति केवल देहपरक है, उपभोगपरक है तो अन्धी कामासक्ति है जो उपभोग के बाद शिथिल हो जा सकती है और अपने स्वाभाविक परिणाम नवीन सृष्टि से कतरा सकती है या उसे अवांछित... दुःख-भाजन मान सकती है। इसीलिए वे प्रतिपादित करते हैं कि जब कामासक्ति को तपस्या से भस्म कर दिया जाता है तभी शुद्ध प्रेम की दीप्ति प्रकट होती है। कुमारसंभवम् एवं अभिज्ञानशाकुन्तलम् अपनी इन दोनों प्रौढ़ कृतियों में कालिदास ने शारीरिक आकर्षण के प्रथम आवेग को मंगलमय नहीं बताया है। काम जब पार्वती के सौन्दर्य को सम्बल बनाकर शिवजी के हृदय में क्षोभ उत्पन्न करना चाहता है तब उसे भस्म हो जाना पड़ता है। पार्वती जब अपने रूप से शिवजी को रिझाने में असमर्थ होकर तपस्या से उन्हें पाने का संकल्प करती हैं तभी कालिदास उन्हें उदात्त प्रेम की उपलब्धि की अधिकारिणी मानते हैं:- 'अवाप्यते वा कथमन्यथा द्वयं तथाविधं प्रेम पतिश्च तादृशः। किसी अन्य तरह.. वैसा प्रेम और वैसा पति कैसे पाया जा सकता है।
जिस प्रेम को तपस्या के द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता, वह प्रेम मंगलमय नहीं होता। वह रूप भी मंगलमय नहीं होता जो तपस्या से परिशोधित न हो। कालिदास के मतानुसार वास्तविक उदात्त प्रिय अरूपहार्य होता है, रूप के द्वारा उसे भुलाया नहीं जा सकता। पार्वती को इसीलिए लगा कि केवल आकर्षण के चाकचिक्य द्वारा शिव जैसे पति को प्राप्त करने का दावा करने वाला रूप वास्तविक प्रेम को प्राप्त करने का उपयुक्त उपकरण नहीं है। इस रूप को भी तप से पवित्र होना चाहिए। कालिदास का निर्णय है कि 'भावनिबन्धना रति' के लिए तप करना, तपना, ताप झेलना आवश्यक है। महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ याद आ गयीं
ताप बिना खंडों का मिल पाना अनहोना, बिना अग्नि के जुड़ा न लोहा, माटी, सोना!
ले टूटे संकल्प-स्वप्न, उर-ज्वाला में पिघलो।' जब लोहा, माटी, सोना जैसे जड़ पदार्थ भी बिना अग्नि-ताप के जुड़ नहीं सकते तब शिवजी के खंडों के रूप में विभाजित नर-नारी के जो जोड़े सच्चे प्रेम के तप रूपी ताप से अपने हृदयों को जोड़ नहीं पाते वे शरीर के स्तर पर जुड़ कर भी वास्तव में जुड़ नहीं पायेंगे। इस प्रेम तप के अन्तर्गत प्रिय को प्राप्त करने के लिए सर्वस्व समर्पण रूपी एकनिष्ठ तप भी है, विरहताप भी और भूल हो जाने पर उसके संशोधन के लिए आन्तरिक पश्चात्ताप भी। बिना सच्चे पश्चात्ताप के अगर शकुन्तला को प्राप्त कर लिया होता दुष्यन्त ने तो शकुन्तला की क्या स्थिति होती ? अन्त:पुरों में एक क्षण के आकर्षण से अपने को धन्य मानने वाली ऐसी सुन्दरियों के जीवन का करुण अवसान हम बार-बार देखते रहे हैं, सुनते रहे हैं, जिनकी ओर राजा दूसरी बार आँख उठाकर भी नहीं देखता। क्या शकुन्तला की परिणति भी वैसी ही नहीं हो जा सकती थी? कालिदास ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि जो तथाकथित प्रेम कर्त्तव्य में बाधक बनता है वह स्वामी के द्वारा दंडित
और ऋषि के द्वारा अभिशप्त होता है। यक्ष स्वर्णकमल लाना भूल जाये, शकुन्तला आतिथ्य-धर्म को विस्मृत करके केवल अपने प्रिय की स्मृति में लीन रहे, यह अपेक्षित नहीं है। यह तो आसक्ति है जो धिक्कृत की जानी चाहिए। इसीलिए इस आसक्ति के प्रेरक कामदेव को उसकी कुचेष्टा के कारण भगवान शिव दग्ध कर देते हैं। जब रूप का आकर्षण अपने को तप से पवित्र करता है, जब प्रेमी तप रूपी विरहताप या पश्चात्ताप से आसक्ति की समस्त श्यामता को दग्ध कर विशुद्ध कांचन के रूप में निखर उठता है तभी उसका प्रेम सार्थक होता है। पार्वती की तपस्या से रीझ कर शिव को भी कहना पड़ता है, हे अवनतांगि! तुम्हारे इस अपूर्व तप के कारण मैं आज से तुम्हारा मोल लिया दास
अद्यप्रभृत्यवनतानि तवास्मि दास:
क्रीतस्तपोभिरिति वादिनि चन्द्रमौलो। इस दृष्टि से विरह की वास्तविक महिमा यही है कि वह तपाग्नि से आसक्ति को भस्म कर मंगलमय प्रेम को उबुद्ध करता है।
हीरक जयन्ती स्मारिका
विद्वत् खण्ड /९
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org