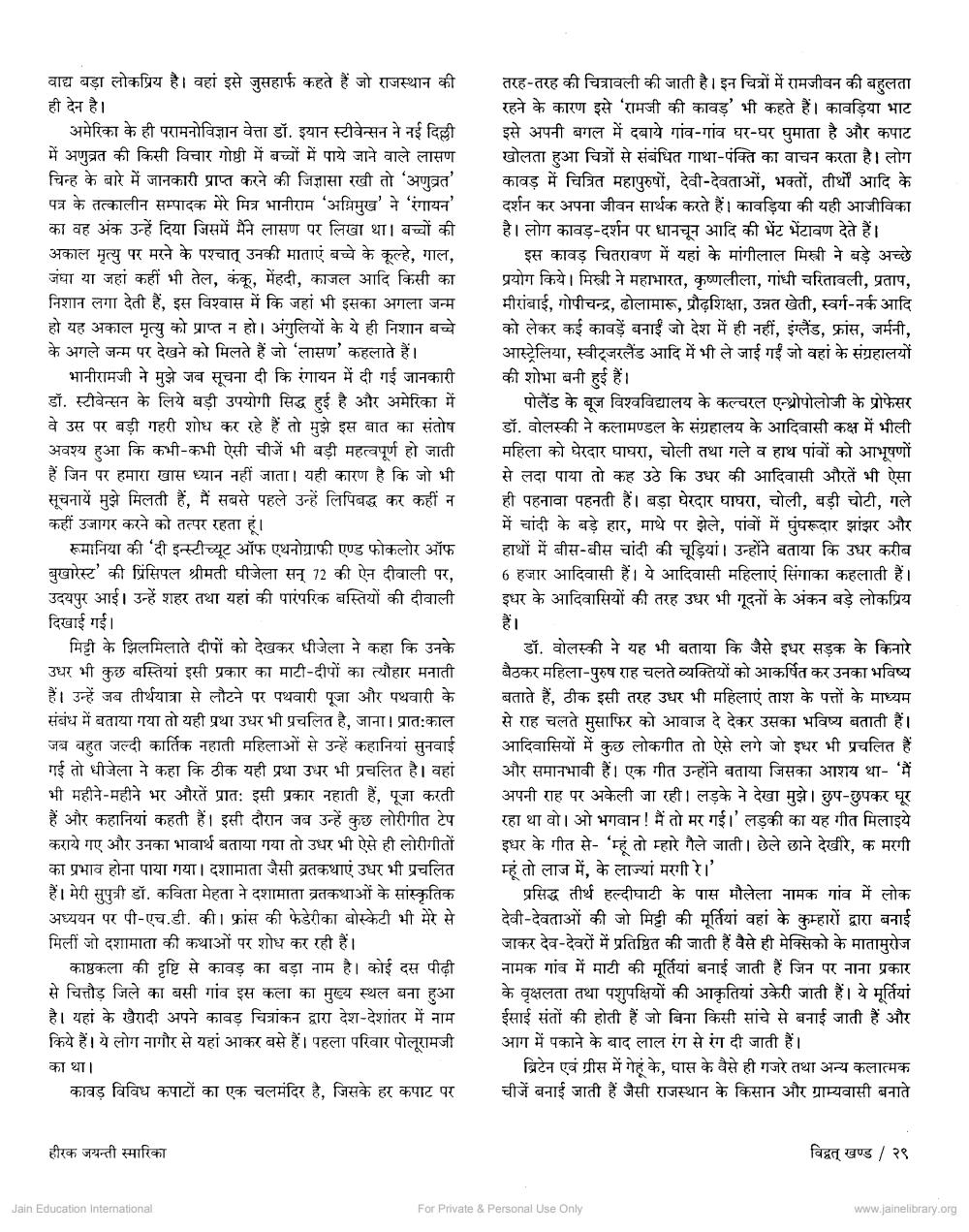________________
वाद्य बड़ा लोकप्रिय है। वहां इसे जुसहार्फ कहते हैं जो राजस्थान की ही देन है।
अमेरिका के ही परामनोविज्ञान वेत्ता डॉ. इयान स्टीवेन्सन ने नई दिल्ली में अणुव्रत की किसी विचार गोष्ठी में बच्चों में पाये जाने वाले लासण चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा रखी तो 'अणुव्रत' पत्र के तत्कालीन सम्पादक मेरे मित्र भानीराम 'अग्निमुख' ने 'रंगायन' का वह अंक उन्हें दिया जिसमें मैने लासण पर लिखा था। बच्चों की अकाल मृत्यु पर मरने के पश्चात् उनकी माताएं बच्चे के कूल्हे, गाल, जंघा या जहां कहीं भी तेल, कंकू, मेंहदी, काजल आदि किसी का निशान लगा देती हैं, इस विश्वास में कि जहां भी इसका अगला जन्म हो यह अकाल मृत्यु को प्राप्त न हो। अंगुलियों के ये ही निशान बच्चे के अगले जन्म पर देखने को मिलते हैं जो 'लासण' कहलाते हैं।
भानीरामजी ने मुझे जब सूचना दी कि रंगायन में दी गई जानकारी डी. स्टीवेन्सन के लिये बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई है और अमेरिका में वे उस पर बड़ी गहरी शोध कर रहे हैं तो मुझे इस बात का संतोष अवश्य हुआ कि कभी-कभी ऐसी चीजें भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं जिन पर हमारा खास ध्यान नहीं जाता। यही कारण है कि जो भी सूचनायें मुझे मिलती हैं, मैं सबसे पहले उन्हें लिपिबद्ध कर कहीं न कहीं उजागर करने को तत्पर रहता हूं।
रूमानिया की 'दी इन्स्टीच्यूट ऑफ एथनोग्राफी एण्ड फोकलोर ऑफ बुखारेस्ट' की प्रिंसिपल श्रीमती घीजेला सन् 72 की ऐन दीवाली पर, उदयपुर आई। उन्हें शहर तथा यहां की पारंपरिक बस्तियों की दीवाली दिखाई गई।
मिट्टी के झिलमिलाते दीपों को देखकर पीजेला ने कहा कि उनके उधर भी कुछ बस्तियां इसी प्रकार का माटी दीपों का त्यौहार मनाती हैं। उन्हें जय तीर्थयात्रा से लौटने पर पथवारी पूजा और पथवारी के संबंध में बताया गया तो यही प्रथा उधर भी प्रचलित है, जाना। प्रात: काल जय बहुत जल्दी कार्तिक नहाती महिलाओं से उन्हें कहानियां सुनवाई गई तो धीजेला ने कहा कि ठीक यही प्रथा उधर भी प्रचलित है। वहां भी महीने महीने भर औरतें प्रातः इसी प्रकार नहाती हैं, पूजा करती हैं और कहानियां कहती हैं इसी दौरान जब उन्हें कुछ लोरीगीत टेप कराये गए और उनका भावार्थ बताया गया तो उधर भी ऐसे ही लोरीगीतों का प्रभाव होना पाया गया। दशामाता जैसी व्रतकथाएं उधर भी प्रचलित हैं। मेरी सुपुत्री डॉ. कविता मेहता ने दशामाता व्रतकथाओं के सांस्कृतिक अध्ययन पर पी-एच.डी. की। फ्रांस की फेडेरीका बोस्केटी भी मेरे से मिलीं जो दशामाता की कथाओं पर शोध कर रही हैं।
काष्ठकला की दृष्टि से कावड़ का बड़ा नाम है। कोई दस पीढ़ी से चित्तौड़ जिले का बसी गांव इस कला का मुख्य स्थल बना हुआ है। यहां के खैरादी अपने कावड़ चित्रांकन द्वारा देश-देशांतर में नाम किये हैं। ये लोग नागौर से यहां आकर बसे हैं। पहला परिवार पोलूरामजी
का था ।
कावड़ विविध कपाटों का एक चलमंदिर है, जिसके हर कपाट पर
हीरक जयन्ती स्मारिका
Jain Education International
तरह-तरह की चित्रावली की जाती है। इन चित्रों में रामजीवन की बहुलता रहने के कारण इसे 'रामजी की कावड़' भी कहते हैं। कावड़िया भाट इसे अपनी बगल में दबाये गांव-गांव घर-घर घुमाता है और कपाट खोलता हुआ चित्रों से संबंधित गाथा पंक्ति का वाचन करता है। लोग कावड़ में चित्रित महापुरुषों, देवी-देवताओं, भक्तों, तीर्थों आदि के दर्शन कर अपना जीवन सार्थक करते हैं। कावड़िया की यही आजीविका है। लोग कावड़ दर्शन पर धानचून आदि की भेंट भेंटावण देते हैं।
इस कावड़ चितरावण में यहां के मांगीलाल मित्री ने बड़े अच्छे प्रयोग किये। मिस्त्री ने महाभारत, कृष्णलीला, गांधी चरितावली, प्रताप, मीरांबाई, गोपीचन्द्र, ढोलामारू, प्रौढशिक्षा, उन्नत खेती, स्वर्ग-नर्क आदि को लेकर कई कावड़ें बनाईं जो देश में ही नहीं, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, स्वीट्जरलैंड आदि में भी ले जाई गई जो वहां के संग्रहालयों की शोभा बनी हुई हैं।
पोलैंड के यूज विश्वविद्यालय के कल्चरल एन्थ्रोपोलोजी के प्रोफेसर डॉ. वोलस्की ने कलामण्डल के संग्रहालय के आदिवासी कक्ष में भीली महिला को घेरदार घाघरा चोली तथा गले व हाथ पांवों को आभूषणों से लदा पाया तो कह उठे कि उधर की आदिवासी औरतें भी ऐसा ही पहनावा पहनती हैं बड़ा घेरदार घाघरा चोली, बड़ी चोटी, गले में चांदी के बड़े हार, माथे पर झेले, पांवों में घुंघरूदार झांझर और हाथों में बीस-बीस चांदी की चूड़ियां उन्होंने बताया कि उधर करीब 6 हजार आदिवासी हैं। ये आदिवासी महिलाएं सिंगाका कहलाती हैं। इधर के आदिवासियों की तरह उधर भी गूदनों के अंकन बड़े लोकप्रिय हैं।
डॉ. वोलस्की ने यह भी बताया कि जैसे इधर सड़क के किनारे बैठकर महिला - पुरुष राह चलते व्यक्तियों को आकर्षित कर उनका भविष्य बताते हैं, ठीक इसी तरह उधर भी महिलाएं ताश के पत्तों के माध्यम से राह चलते मुसाफिर को आवाज दे देकर उसका भविष्य बताती हैं। आदिवासियों में कुछ लोकगीत तो ऐसे लगे जो इधर भी प्रचलित हैं और समानभावी हैं। एक गीत उन्होंने बताया जिसका आशय था- 'मैं अपनी राह पर अकेली जा रही। लड़के ने देखा मुझे। छुप-छुपकर घूर रहा था वो। ओ भगवान ! मैं तो मर गई।' लड़की का यह गीत मिलाइये इधर के गीत से - 'म्हूं तो म्हारे गैले जाती । छेले छाने देखीरे, क मरगी म्हूं तो लाज में, के लाज्यां मरगी रे ।'
प्रसिद्ध तीर्थ हल्दीघाटी के पास मौलेला नामक गांव में लोक देवी-देवताओं की जो मिट्टी की मूर्तियां वहां के कुम्हारों द्वारा बनाई जाकर देव-देवरों में प्रतिष्ठित की जाती हैं वैसे ही मेक्सिको के मातामुरोज नामक गांव में माटी की मूर्तियां बनाई जाती हैं जिन पर नाना प्रकार के वृक्षलता तथा पशुपक्षियों की आकृतियां उकेरी जाती हैं। ये मूर्तियां ईसाई संतों की होती हैं जो बिना किसी सांचे से बनाई जाती हैं और आग में पकाने के बाद लाल रंग से रंग दी जाती हैं।
ब्रिटेन एवं ग्रीस में गेहूं के, घास के वैसे ही गजरे तथा अन्य कलात्मक चीजें बनाई जाती हैं जैसी राजस्थान के किसान और ग्राम्यवासी बनाते
For Private & Personal Use Only
विद्वत् खण्ड / २९
www.jainelibrary.org