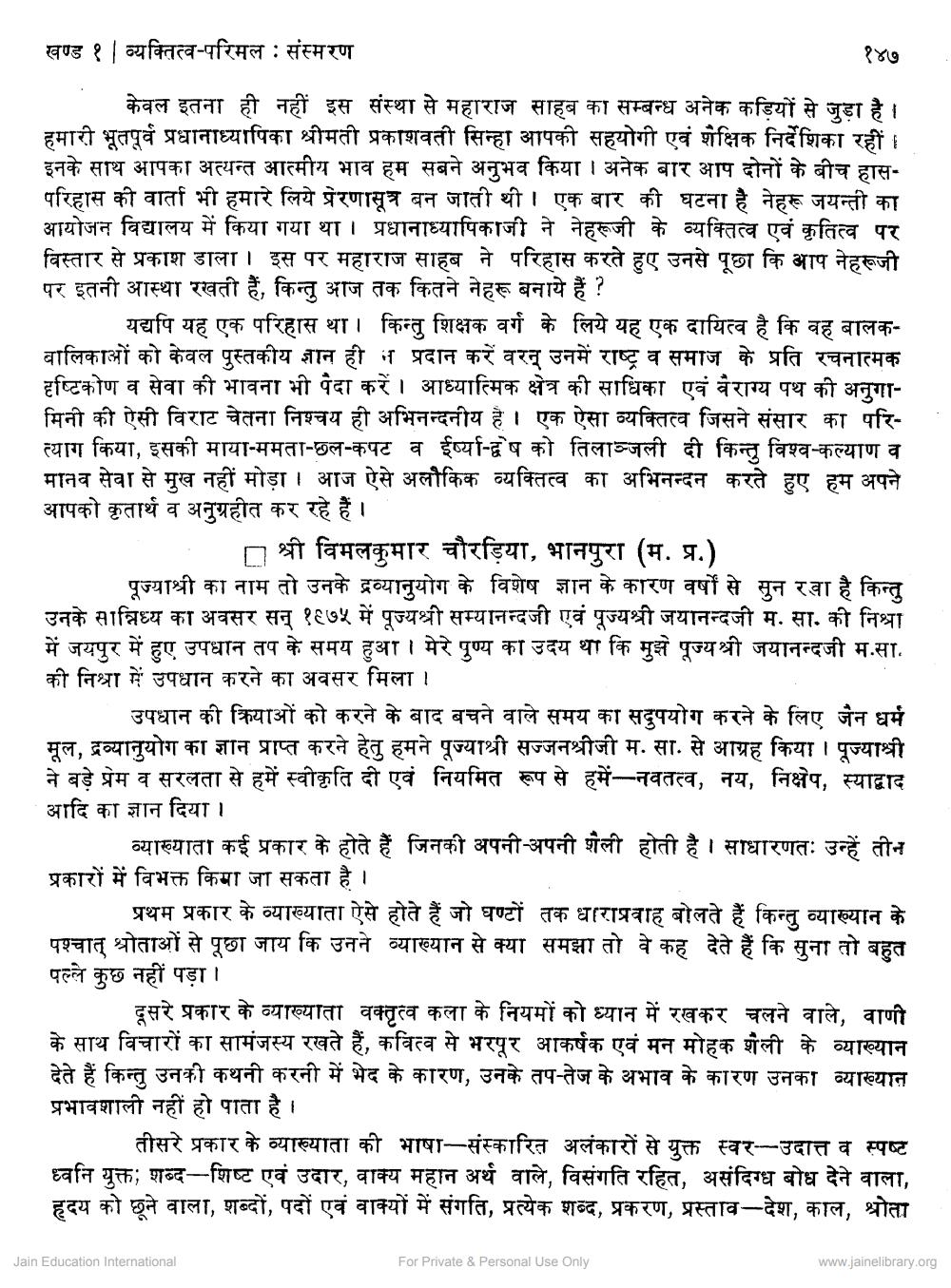________________
१४७
खण्ड १ | व्यक्तित्व - परिमल : संस्मरण
केवल इतना ही नहीं इस संस्था से महाराज साहब का सम्बन्ध अनेक कड़ियों से जुड़ा है । हमारी भूतपूर्व प्रधानाध्यापिका श्रीमती प्रकाशवती सिन्हा आपकी सहयोगी एवं शैक्षिक निर्देशिका रहीं । इनके साथ आपका अत्यन्त आत्मीय भाव हम सबने अनुभव किया । अनेक बार आप दोनों के बीच हासपरिहास की वार्ता भी हमारे लिये प्रेरणासूत्र बन जाती थी। एक बार की घटना है नेहरू जयन्ती का आयोजन विद्यालय में किया गया था। प्रधानाध्यापिकाजी ने नेहरूजी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस पर महाराज साहब ने परिहास करते हुए उनसे पूछा कि आप नेहरूजी पर इतनी आस्था रखती हैं, किन्तु आज तक कितने नेहरू बनाये हैं ? यद्यपि यह एक परिहास था । किन्तु शिक्षक वर्ग के लिये यह एक दायित्व है कि वह बालकबालिकाओं को केवल पुस्तकीय ज्ञान ही न प्रदान करें वरन् उनमें राष्ट्र व समाज के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण व सेवा की भावना भी पैदा करें । आध्यात्मिक क्षेत्र की साधिका एवं वैराग्य पथ की अनुगामिनी की ऐसी विराट चेतना निश्चय ही अभिनन्दनीय है । एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने संसार का परित्याग किया, इसकी माया - ममता - छल-कपट व ईर्ष्या-द्व ेष को तिलाञ्जली दी किन्तु विश्व कल्याण व मानव सेवा से मुख नहीं मोड़ा। आज ऐसे अलौकिक व्यक्तित्व का अभिनन्दन करते हुए हम अपने आपको कृतार्थ व अनुग्रहीत कर रहे हैं ।
श्री विमलकुमार चौरड़िया, भानपुरा (म. प्र. )
पूज्याश्री का नाम तो उनके द्रव्यानुयोग के विशेष ज्ञान के कारण वर्षों से सुन रखा है किन्तु उनके सान्निध्य का अवसर सन् १९७५ में पूज्यश्री सम्यानन्दजी एवं पूज्यश्री जयानन्दजी म. सा. की निश्रा में जयपुर में हुए उपधान तप के समय हुआ । मेरे पुण्य का उदय था कि मुझे पूज्य श्री जयानन्दजी म. सा. की निश्रा में उपधान करने का अवसर मिला ।
उपधान की क्रियाओं को करने के बाद बचने वाले समय का सदुपयोग करने के लिए जैन धर्म मूल, द्रव्यानुयोग का ज्ञान प्राप्त करने हेतु हमने पूज्याश्री सज्जन श्रीजी म. सा. से आग्रह किया । पूज्याश्री ने बड़े प्रेम व सरलता से हमें स्वीकृति दी एवं नियमित रूप से हमें - नवतत्व, नय, निक्षेप, स्याद्वाद आदि का ज्ञान दिया ।
व्याख्याता कई प्रकार के होते हैं जिनकी अपनी अपनी शैली होती है । साधारणतः उन्हें तीन प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है ।
प्रथम प्रकार के व्याख्याता ऐसे होते हैं जो घण्टों तक धाराप्रवाह बोलते हैं किन्तु व्याख्यान के पश्चात् श्रोताओं से पूछा जाय कि उनने व्याख्यान से क्या समझा तो वे कह देते हैं कि सुना तो बहुत पल्ले कुछ नहीं पड़ा ।
दूसरे प्रकार के व्याख्याता वक्तृत्व कला के नियमों को ध्यान में रखकर चलने वाले, वाणी के साथ विचारों का सामंजस्य रखते हैं, कवित्व से भरपूर आकर्षक एवं मन मोहक शैली के व्याख्यान देते हैं किन्तु उनकी कथनी करनी में भेद के कारण, उनके तप तेज के अभाव के कारण उनका व्याख्यान प्रभावशाली नहीं हो पाता है ।
तीसरे प्रकार के व्याख्याता की भाषा - संस्कारित अलंकारों से युक्त स्वर-उदात्त व स्पष्ट ध्वनि युक्त; शब्द - शिष्ट एवं उदार, वाक्य महान अर्थ वाले विसंगति रहित, असंदिग्ध बोध देने वाला, हृदय को छूने वाला, शब्दों, पदों एवं वाक्यों में संगति, प्रत्येक शब्द, प्रकरण, प्रस्ताव - देश, काल, श्रोता
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org