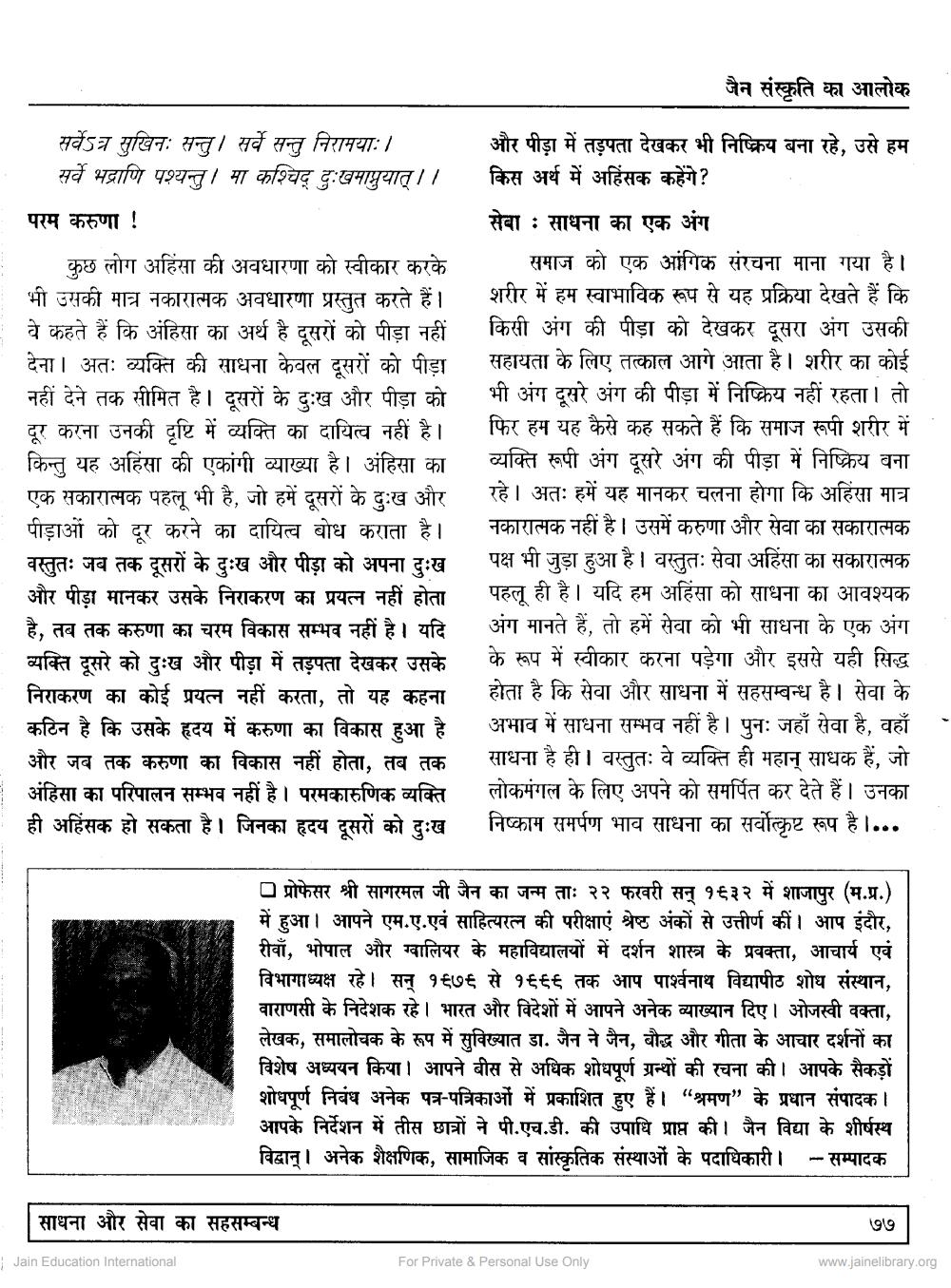________________
जैन संस्कृति का आलोक
सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु। सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चिद् दुःखमाप्नुयात् ।। परम करुणा !
कुछ लोग अहिंसा की अवधारणा को स्वीकार करके भी उसकी मात्र नकारात्मक अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि अंहिसा का अर्थ है दूसरों को पीडा नहीं देना। अतः व्यक्ति की साधना केवल दूसरों को पीड़ा नहीं देने तक सीमित है। दूसरों के दःख और पीडा को दर करना उनकी दृष्टि में व्यक्ति का दायित्व नहीं है। किन्तु यह अहिंसा की एकांगी व्याख्या है। अंहिसा का एक सकारात्मक पहलू भी है, जो हमें दूसरों के दुःख और पीड़ाओं को दूर करने का दायित्व बोध कराता है। वस्तुतः जब तक दूसरों के दुःख और पीड़ा को अपना दुःख
और पीड़ा मानकर उसके निराकरण का प्रयत्न नहीं होता है, तब तक करुणा का चरम विकास सम्भव नहीं है। यदि व्यक्ति दूसरे को दुःख और पीड़ा में तड़पता देखकर उसके निराकरण का कोई प्रयत्न नहीं करता, तो यह कहना कठिन है कि उसके हृदय में करुणा का विकास हुआ है और जब तक करुणा का विकास नहीं होता, तब तक अंहिसा का परिपालन सम्भव नहीं है। परमकारुणिक व्यक्ति ही अहिंसक हो सकता है। जिनका हृदय दूसरों को दुःख
और पीड़ा में तड़पता देखकर भी निष्क्रिय बना रहे, उसे हम किस अर्थ में अहिंसक कहेंगे? सेवा : साधना का एक अंग
समाज को एक आंगिक संरचना माना गया है। शरीर में हम स्वाभाविक रूप से यह प्रक्रिया देखते हैं कि किसी अंग की पीड़ा को देखकर दूसरा अंग उसकी सहायता के लिए तत्काल आगे आता है। शरीर का कोई भी अंग दूसरे अंग की पीड़ा में निष्क्रिय नहीं रहता। तो फिर हम यह कैसे कह सकते हैं कि समाज रूपी शरीर में व्यक्ति रूपी अंग दूसरे अंग की पीड़ा में निष्क्रिय बना रहे। अतः हमें यह मानकर चलना होगा कि अहिंसा मात्र नकारात्मक नहीं है। उसमें करुणा और सेवा का सकारात्मक पक्ष भी जुड़ा हुआ है। वस्तुतः सेवा अहिंसा का सकारात्मक पहलू ही है। यदि हम अहिंसा को साधना का आवश्यक अंग मानते हैं, तो हमें सेवा को भी साधना के एक अंग के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा और इससे यही सिद्ध होता है कि सेवा और साधना में सहसम्बन्ध है। सेवा के अभाव में साधना सम्भव नहीं है। पुनः जहाँ सेवा है, वहाँ साधना है ही। वस्तुतः वे व्यक्ति ही महान् साधक हैं, जो लोकमंगल के लिए अपने को समर्पित कर देते हैं। उनका निष्काम समर्पण भाव साधना का सर्वोत्कृष्ट रूप है।...
प्रोफेसर श्री सागरमल जी जैन का जन्म ताः २२ फरवरी सन् १६३२ में शाजापुर (म.प्र.) में हुआ। आपने एम.ए.एवं साहित्यरत्न की परीक्षाएं श्रेष्ठ अंकों से उत्तीर्ण की। आप इंदौर, रीवाँ, भोपाल और ग्वालियर के महाविद्यालयों में दर्शन शास्त्र के प्रवक्ता, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष रहे। सन १९७६ से १६६६ तक आप पार्श्वनाथ विद्यापीठ शोध संस्थान, वाराणसी के निदेशक रहे। भारत और विदेशों में आपने अनेक व्याख्यान दिए। ओजस्वी वक्ता, लेखक, समालोचक के रूप में सुविख्यात डा. जैन ने जैन, बौद्ध और गीता के आचार दर्शनों का विशेष अध्ययन किया। आपने बीस से अधिक शोधपूर्ण ग्रन्थों की रचना की। आपके सैकड़ों शोधपूर्ण निबंध अनेक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। "श्रमण" के प्रधान संपादक। आपके निर्देशन में तीस छात्रों ने पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की। जैन विद्या के शीर्षस्थ विद्वान् । अनेक शैक्षणिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संस्थाओं के पदाधिकारी। - सम्पादक
| साधना और सेवा का सहसम्बन्ध
७७
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org