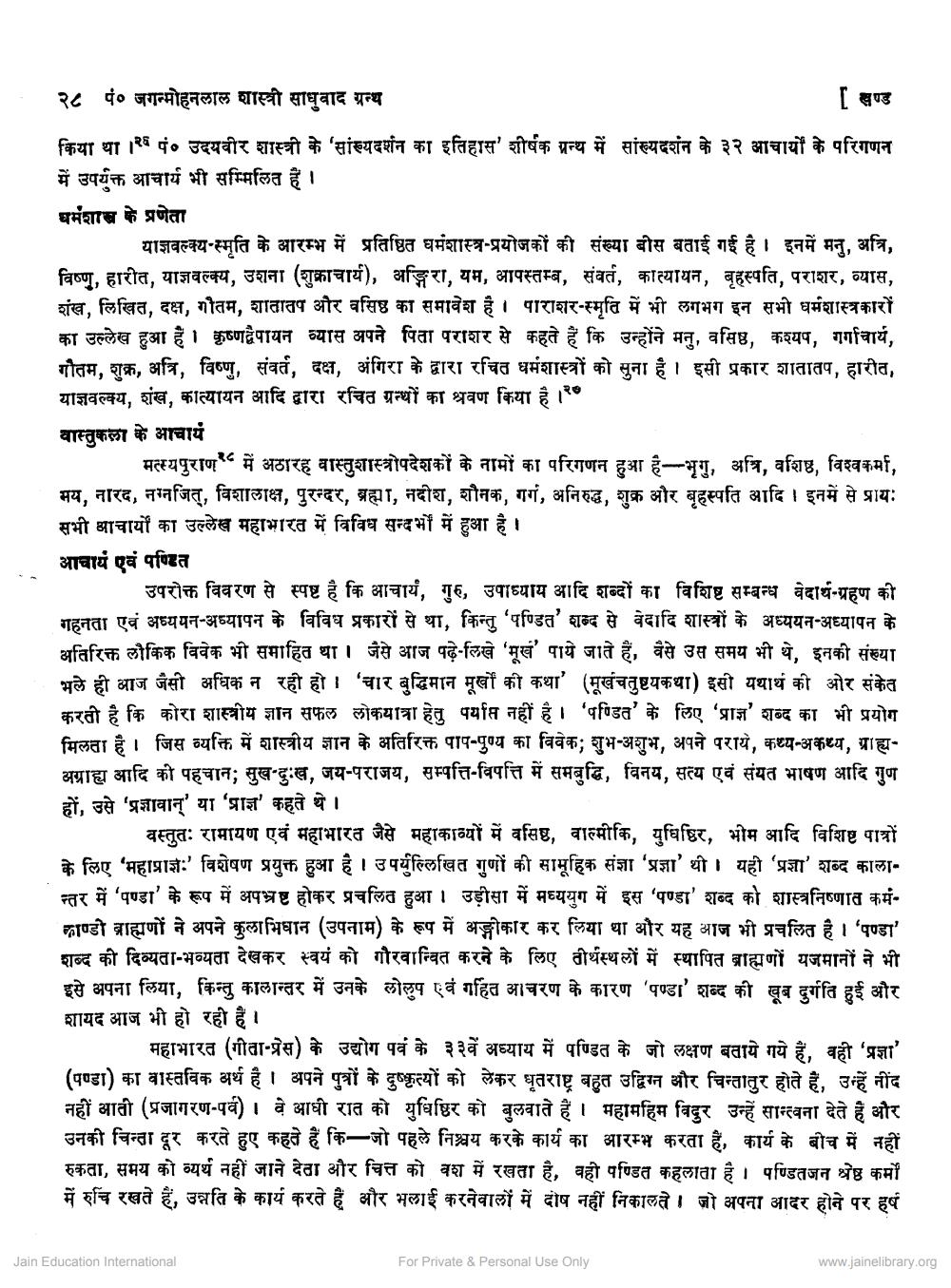________________
२८ पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ
[ खण्ड
किया था । २६ पं० उदयवीर शास्त्री के 'सांख्यदर्शन का इतिहास' शीर्षक ग्रन्थ में सांख्यदर्शन के ३२ आचार्यों के परिगणन में उपर्युक्त आचार्य भी सम्मिलित हैं । धर्मशास्त्र के प्रणेता
याज्ञवल्क्य स्मृति के आरम्भ में प्रतिष्ठित धर्मशास्त्र - प्रयोजकों की संख्या बीस बताई गई है। इनमें मनु, अत्रि, विष्णु, हारीत, याज्ञवल्क्य, उशना (शुक्राचार्य), अङ्गिरा, यम, आपस्तम्ब, संवर्त, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शंख, लिखित, दक्ष, गौतम, शातातप और वसिष्ठ का समावेश है । पाराशर स्मृति में भी लगभग इन सभी धर्मशास्त्रकारों का उल्लेख हुआ हैं | कृष्णद्वैपायन व्यास अपने पिता पराशर से कहते हैं कि उन्होंने मनु, वसिष्ठ, कश्यप, गर्गाचार्य, गौतम, शुक्र, अत्रि, विष्णु, संवर्त, दक्ष, अंगिरा के द्वारा रचित धर्मशास्त्रों को सुना है । इसी प्रकार शातातप, हारीत, याज्ञवल्क्य, शंख, कात्यायन आदि द्वारा रचित ग्रन्थों का श्रवण किया है । २०
वास्तुकला के आचार्य
मत्स्यपुराण" में अठारह वास्तुशास्त्रोपदेशकों के नामों का परिगणन हुआ है-भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नारद, नग्नजित्, विशालाक्ष, पुरन्दर, ब्रह्मा, नदीश, शौनक, गर्ग, अनिरुद्ध, शुक्र और बृहस्पति आदि । इनमें से प्रायः सभी आचार्यों का उल्लेख महाभारत में विविध सन्दर्भों में हुआ है ।
आचार्य एवं पण्डित
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आचार्य, गुरु, उपाध्याय आदि शब्दों का विशिष्ट सम्बन्ध वेदार्थ-ग्रहण की गहनता एवं अध्ययन-अध्यापन के विविध प्रकारों से था, किन्तु 'पण्डित' शब्द से वेदादि शास्त्रों के अध्ययन-अध्यापन के अतिरिक्त लौकिक विवेक भी समाहित था । जैसे आज पढ़े-लिखे 'मूर्ख' पाये जाते हैं, वैसे उस समय भी थे, इनकी संख्या भले ही आज जैसी अधिक न रही हो । 'चार बुद्धिमान मूर्खों की कथा' (मूर्खचतुष्टयकथा ) इसी यथार्थ की ओर संकेत करती है कि कोरा शास्त्रीय ज्ञान सफल लोकयात्रा हेतु पर्याप्त नहीं है । 'पण्डित' के लिए 'प्राज्ञ' शब्द का भी प्रयोग मिलता है । जिस व्यक्ति में शास्त्रीय ज्ञान के अतिरिक्त पाप-पुण्य का विवेक; शुभ-अशुभ, अपने पराये, कथ्य-अकथ्य, ग्राह्यअग्राह्य आदि की पहचान; सुख-दुःख, जय-पराजय, सम्पत्ति - विपत्ति में समबुद्धि, विनय, सत्य एवं संयत भाषण आदि गुण हों, उसे 'प्रज्ञावान्' या 'प्राज्ञ' कहते थे ।
भीम आदि विशिष्ट पात्रों
।
वस्तुतः रामायण एवं महाभारत जैसे महाकाव्यों में वसिष्ठ, वाल्मीकि, युधिष्ठिर, के लिए 'महाप्राज्ञः' विशेषण प्रयुक्त हुआ है । उपर्युल्लिखित गुणों की सामूहिक संज्ञा 'प्रज्ञा' थी यही 'प्रज्ञा' शब्द कालाअन्तर में 'पण्डा' के रूप में अपभ्रष्ट होकर प्रचलित हुआ । उड़ीसा में मध्ययुग में इस 'पण्डा' शब्द को शास्त्रनिष्णात कर्मब्राह्मणों ने अपने कुलाभिधान (उपनाम) के रूप में अङ्गीकार कर लिया था और यह आज भी प्रचलित है । 'पण्डा' शब्द की दिव्यता - भव्यता देखकर स्वयं को गौरवान्वित करने के लिए तीर्थस्थलों में स्थापित ब्राह्मणों यजमानों ने भी इसे अपना लिया, किन्तु कालान्तर में उनके लोलुप एवं गर्हित आचरण के कारण 'पण्डा' शब्द की खूब दुर्गति हुई और शायद आज भी हो रही हैं ।
महाभारत (गीता प्रेस) के उद्योग पर्व के ३३ वें अध्याय में पण्डित के जो लक्षण बताये गये हैं, वही 'प्रज्ञा' (पण्डा) का वास्तविक अर्थ है । अपने पुत्रों के दुष्कृत्यों को लेकर धृतराष्ट्र बहुत उद्विग्न और चिन्तातुर होते हैं, उन्हें नींद
महामहिम विदुर उन्हें सान्त्वना देते हैं और
नहीं आती (प्रजागरण - पर्व) । वे आधी रात को युधिष्ठिर को बुलवाते हैं । उनकी चिन्ता दूर करते हुए कहते हैं कि जो पहले निश्चय करके कार्य का आरम्भ करता हैं, कार्य के बीच में नहीं रुकता, समय को व्यर्थ नहीं जाने देता और चित्त को वश में रखता है, वही पण्डित कहलाता है । पण्डितजन श्रेष्ठ कर्मों में रुचि रखते हैं, उन्नति के कार्य करते हैं और भलाई करनेवालों में दोष नहीं निकालते । जो अपना आदर होने पर हर्ष
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org