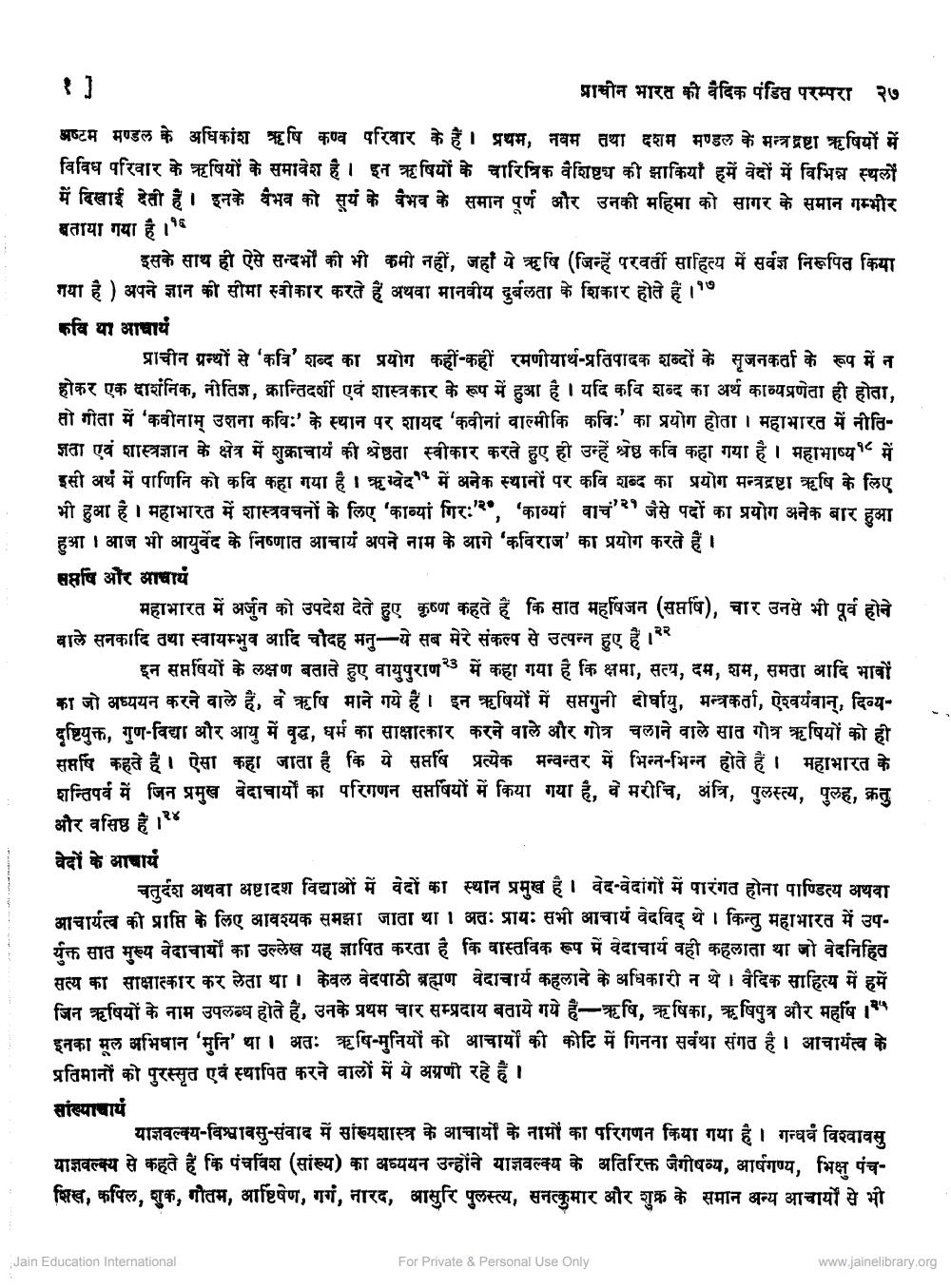________________
प्राचीन भारत की वैदिक पंडित परम्परा २७ अष्टम मण्डल के अधिकांश ऋषि कण्व परिवार के हैं। प्रथम, नवम तथा दशम मण्डल के मन्त्र द्रष्टा ऋषियों में विविध परिवार के ऋषियों के समावेश है। इन ऋषियों के चारित्रिक वैशिष्टय की झाकियां हमें वेदों में विभिन्न स्थलों में दिखाई देती है। इनके वैभव को सूर्य के वैभव के समान पूर्ण और उनकी महिमा को सागर के समान गम्भीर बताया गया है।
इसके साथ ही ऐसे सन्दर्भो की भी कमी नहीं, जहां ये ऋषि (जिन्हें परवर्ती साहित्य में सर्वज्ञ निरूपित किया गया है ) अपने ज्ञान की सीमा स्वीकार करते हैं अथवा मानवीय दुर्बलता के शिकार होते हैं । १७ कवि या आचार्य
प्राचीन ग्रन्थों से 'कवि' शब्द का प्रयोग कहीं-कहीं रमणीयार्थ-प्रतिपादक शब्दों के सृजनकर्ता के रूप में न होकर एक दार्शनिक, नीतिज्ञ, क्रान्तिदर्शी एवं शास्त्रकार के रूप में हुआ है । यदि कवि शब्द का अर्थ काव्यप्रणेता ही होता, तो गीता में 'कवीनाम् उशना कविः' के स्थान पर शायद 'कवीनां वाल्मीकि कविः' का प्रयोग होता । महाभारत में नीतिज्ञता एवं शास्त्रज्ञान के क्षेत्र में शुक्राचार्य की श्रेष्ठता स्वीकार करते हुए ही उन्हें श्रेष्ठ कवि कहा गया है । महाभाष्य१८ में इसी अर्थ में पाणिनि को कवि कहा गया है। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर कवि शब्द का प्रयोग मन्त्रद्रष्टा ऋषि के लिए भी हुआ है। महाभारत में शास्त्रवचनों के लिए 'काव्यां गिरः२९, 'काव्यां वाचं'" जैसे पदों का प्रयोग अनेक बार हा हुआ । आज भी आयुर्वेद के निष्णात आचार्य अपने नाम के आगे 'कविराज' का प्रयोग करते हैं। सप्तषि और आचार्य
महाभारत में अर्जुन को उपदेश देते हुए कृष्ण कहते हैं कि सात महर्षिजन (सप्तर्षि), चार उनसे भी पूर्व होने वाले सनकादि तथा स्वायम्भुव आदि चौदह मनु-ये सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं । २२
इन सप्तर्षियों के लक्षण बताते हुए वायुपुराण में कहा गया है कि क्षमा, सत्य, दम, शम, समता आदि भावों का जो अध्ययन करने वाले हैं, वे ऋषि माने गये हैं। इन ऋषियों में सप्तगुनी दीर्घायु, मन्त्रकर्ता, ऐश्वर्यवान्, दिव्यदृष्टियुक्त, गुण-विद्या और आयु में वृद्ध, धर्म का साक्षात्कार करने वाले और गोत्र चलाने वाले सात गोत्र ऋषियों को ही सप्तर्षि कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये सप्तर्षि प्रत्येक मन्वन्तर में भिन्न-भिन्न होते हैं। महाभारत के शन्तिपर्व में जिन प्रमुख वेदाचार्यों का परिगणन सप्तर्षियों में किया गया है, वे मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु और वसिष्ठ है ।२४ वेदों के आचार्य
चतर्दश अथवा अष्टादश विद्याओं में वेदों का स्थान प्रमुख है। वेद-वेदांगों में पारंगत होना पाण्डित्य अथवा आचार्यत्व की प्राप्ति के लिए आवश्यक समझा जाता था । अतः प्रायः सभी आचार्य वेदविद् थे। किन्तु महाभारत में उप. र्युक्त सात मुख्य वेदाचार्यों का उल्लेख यह ज्ञापित करता है कि वास्तविक रूप में वेदाचार्य वही कहलाता था जो वेदनिहित सत्य का साक्षात्कार कर लेता था। केवल वेदपाठी ब्रह्मण वेदाचार्य कहलाने के अधिकारी न थे। वैदिक साहित्य में हमें जिन ऋषियों के नाम उपलब्ध होते हैं, उनके प्रथम चार सम्प्रदाय बताये गये है-ऋषि, ऋषिका, ऋषिपुत्र और महर्षि ।२५ इनका मूल अभिधान 'मुनि' था। अतः ऋषि-मुनियों को आचार्यों की कोटि में गिनना सर्वथा संगत है। आचार्यत्व के प्रतिमानों को पुरस्सृत एवं स्थापित करने वालों में ये अग्रणी रहे है। सांख्याचार्य
याज्ञवल्क्य-विश्वावसु-संवाद में सांख्यशास्त्र के आचार्यों के नामों का परिगणन किया गया है। गन्धर्व विश्वावसु याज्ञवल्क्य से कहते हैं कि पंचविंश (सांख्य) का अध्ययन उन्होंने याज्ञवल्क्य के अतिरिक्त जैगीषव्य, आर्षगण्य, भिक्षु पंचशिख, कपिल, शुक, गौतम, आष्टिषेण, गर्ग, नारद, आसुरि पुलस्त्य, सनत्कुमार और शुक्र के समान अन्य आचार्यों से भी
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org