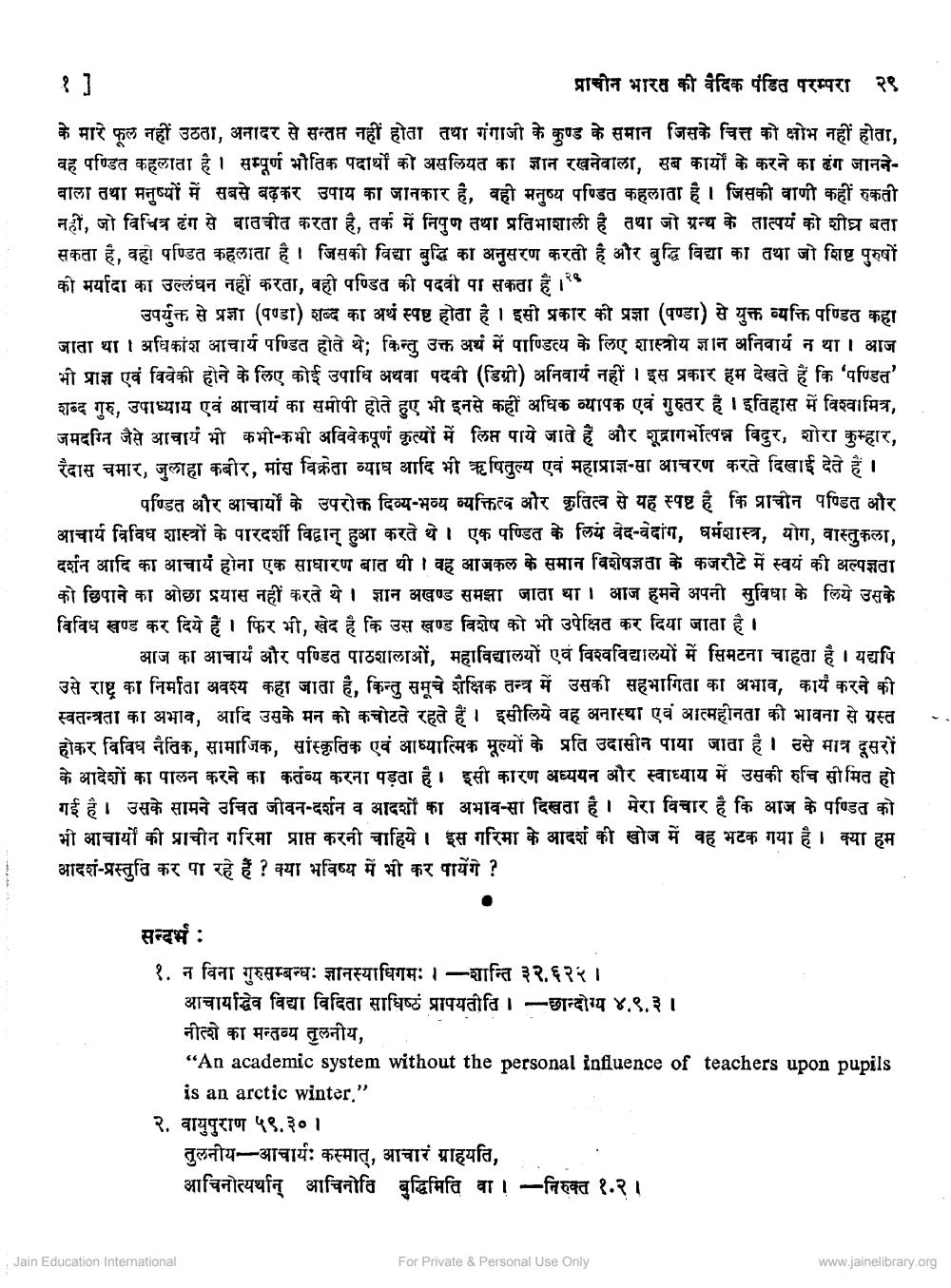________________
प्राचीन भारत की वैदिक पंडित परम्परा २९ के मारे फूल नहीं उठता, अनादर से सन्तप्त नहीं होता तथा गंगाजी के कुण्ड के समान जिसके चित्त को क्षोभ नहीं होता, वह पण्डित कहलाता है । सम्पूर्ण भौतिक पदार्थों को असलियत का ज्ञान रखनेवाला, सब कार्यों के करने का ढंग जाननेवाला तथा मनुष्यों में सबसे बढ़कर उपाय का जानकार है, वही मनुष्य पण्डित कहलाता है । जिसकी वाणी कहीं रुकती नहीं, जो विचित्र ढंग से बातचीत करता है, तर्क में निपुण तथा प्रतिभाशाली है तथा जो ग्रन्थ के तात्पर्य को शीघ्र बता सकता है, वही पण्डित कहलाता है। जिसकी विद्या बुद्धि का अनुसरण करती है और बुद्धि विद्या का तथा जो शिष्ट पुरुषों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, वही पण्डित की पदवी पा सकता है ।
उपर्युक्त से प्रज्ञा (पण्डा) शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है । इसी प्रकार की प्रज्ञा (पण्डा) से युक्त व्यक्ति पण्डित कहा जाता था। अधिकांश आचार्य पण्डित होते थे; किन्तु उक्त अर्थ में पाण्डित्य के लिए शास्त्रीय ज्ञान अनिवार्य न था। आज भी प्राज्ञ एवं विवेकी होने के लिए कोई उपाधि अथवा पदवी (डिग्री) अनिवार्य नहीं । इस प्रकार हम देखते हैं कि 'पण्डित' शब्द गुरु, उपाध्याय एवं आचार्य का समीपी होते हुए भी इनसे कहीं अधिक व्यापक एवं गुरुतर है । इतिहास में विश्वामित्र, जमदग्नि जैसे आचार्य भी कभी-कभी अविवेकपूर्ण कृत्यों में लिप्त पाये जाते हैं और शूद्रागर्भोत्पन्न विदुर, शोरा कुम्हार, रैदास चमार, जुलाहा कबीर, मांस विक्रेता व्याध आदि भी ऋषितुल्य एवं महाप्राज्ञ-सा आचरण करते दिखाई देते हैं ।
पण्डित और आचार्यों के उपरोक्त दिव्य-भव्य व्यक्तित्व और कृतित्व से यह स्पष्ट है कि प्राचीन पण्डित और आचार्य विविध शास्त्रों के पारदर्शी विद्वान् हुआ करते थे। एक पण्डित के लिये वेद-वेदांग, धर्मशास्त्र, योग, वास्तुकला, दर्शन आदि का आचार्य होना एक साधारण बात थी। वह आजकल के समान विशेषज्ञता के कजरौटे में स्वयं की अल्पज्ञता को छिपाने का ओछा प्रयास नहीं करते थे। ज्ञान अखण्ड समझा जाता था। आज हमने अपनी सुविधा के लिये उसके विविध खण्ड कर दिये हैं । फिर भी, खेद है कि उस खण्ड विशेष को भी उपेक्षित कर दिया जाता है।
__ आज का आचार्य और पण्डित पाठशालाओं, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में सिमटना चाहता है । यद्यपि उसे राष्ट्र का निर्माता अवश्य कहा जाता है, किन्तु समूचे शैक्षिक तन्त्र में उसकी सहभागिता का अभाव, कार्य करने की स्वतन्त्रता का अभाव, आदि उसके मन को कचोटते रहते हैं। इसीलिये वह अनास्था एवं आत्महीनता की भावना से ग्रस्त होकर विविध नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति उदासीन पाया जाता है। उसे मात्र दूसरों के आदेशों का पालन करने का कर्तव्य करना पड़ता है। इसी कारण अध्ययन और स्वाध्याय में उसकी रुचि सीमित हो गई है। उसके सामने उचित जीवन-दर्शन व आदर्शों का अभाव-सा दिखता है। मेरा विचार है कि आज के पण्डित को भी आचार्यों की प्राचीन गरिमा प्राप्त करनी चाहिये। इस गरिमा के आदर्श की खोज में वह भटक गया है। क्या हम आदर्श-प्रस्तुति कर पा रहे हैं ? क्या भविष्य में भी कर पायेंगे ?
..
सन्दर्भ: १. न विना गुरुसम्बन्धः ज्ञानस्याधिगमः । -शान्ति ३२.६२२ ।
आचार्याद्धव विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापयतीति। -छान्दोग्य ४.९.३ । नीत्शे का मन्तव्य तुलनीय, "An academic system without the personal influence of teachers upon pupils
is an arctic winter." २. वायुपुराण ५९.३०।
तुलनीय-आचार्यः कस्मात, आचारं ग्राहयति, आचिनोत्यर्थान् आचिनोति बुद्धिमिति वा। -निरुक्त १.२ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org