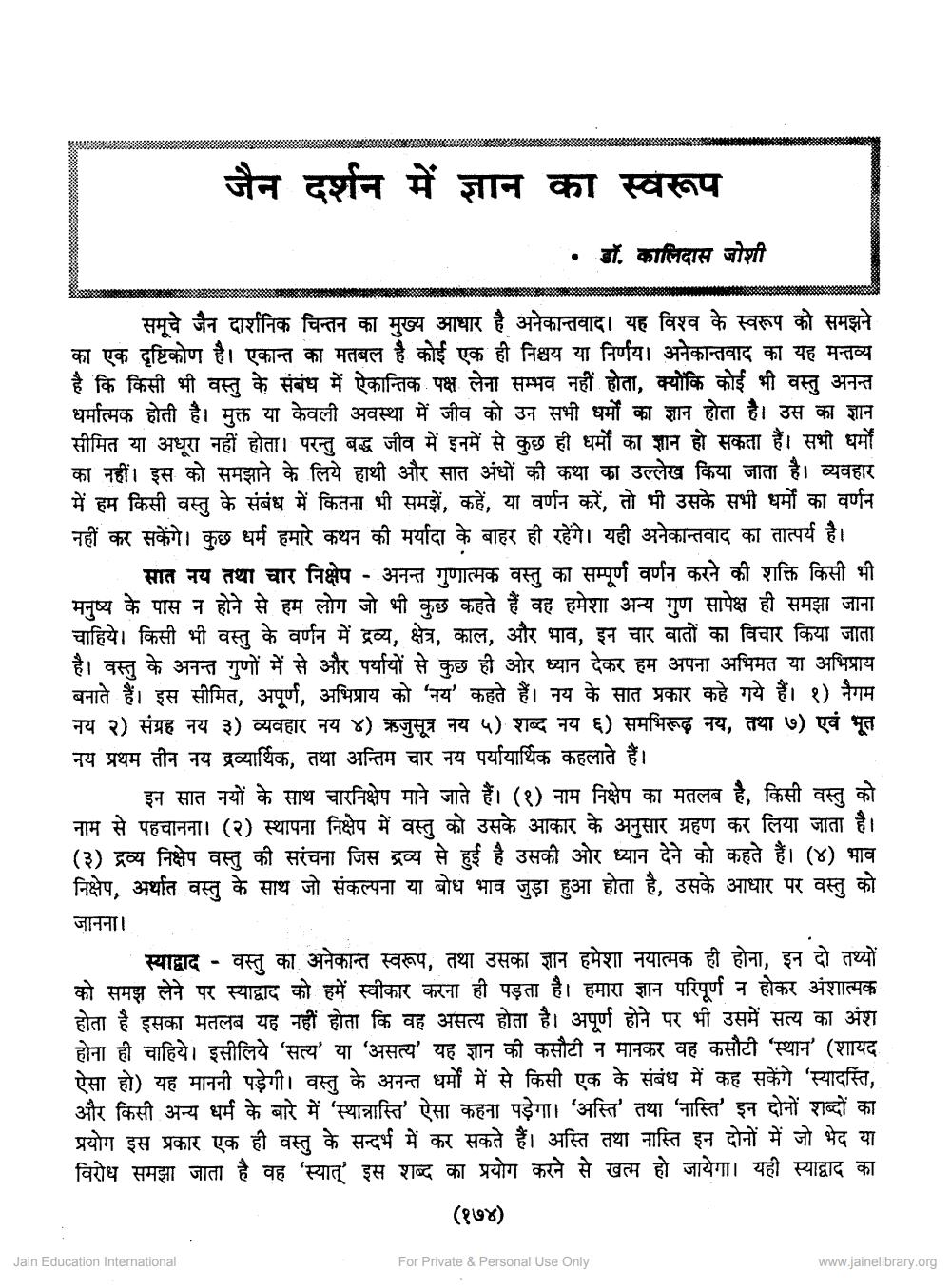________________
जैन दर्शन में ज्ञान का स्वरूप
• डॉ. कालिदास जोशी
3588888888888880000888
समूचे जैन दार्शनिक चिन्तन का मुख्य आधार है अनेकान्तवाद। यह विश्व के स्वरूप को समझने का एक दृष्टिकोण है। एकान्त का मतबल है कोई एक ही निश्चय या निर्णय। अनेकान्तवाद का यह मन्तव्य है कि किसी भी वस्तु के संबंध में ऐकान्तिक पक्ष लेना सम्भव नहीं होता, क्योंकि कोई भी वस्तु अनन्त धर्मात्मक होती है। मुक्त या केवली अवस्था में जीव को उन सभी धर्मों का ज्ञान होता है। उस का ज्ञान सीमित या अधूरा नहीं होता। परन्तु बद्ध जीव में इनमें से कुछ ही धर्मों का ज्ञान हो सकता हैं। सभी धर्मों का नहीं। इस को समझाने के लिये हाथी और सात अंधों की कथा का उल्लेख किया जाता है। व्यवहार में हम किसी वस्तु के संबंध में कितना भी समझें, कहें, या वर्णन करें, तो भी उसके सभी धर्मों का वर्णन नहीं कर सकेंगे। कुछ धर्म हमारे कथन की मर्यादा के बाहर ही रहेंगे। यही अनेकान्तवाद का तात्पर्य है।
. सात नय तथा चार निक्षेप - अनन्त गुणात्मक वस्तु का सम्पूर्ण वर्णन करने की शक्ति किसी भी मनुष्य के पास न होने से हम लोग जो भी कुछ कहते हैं वह हमेशा अन्य गुण सापेक्ष ही समझा जाना चाहिये। किसी भी वस्तु के वर्णन में द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भाव, इन चार बातों का विचार किया जाता है। वस्तु के अनन्त गुणों में से और पर्यायों से कुछ ही ओर ध्यान देकर हम अपना अभिमत या अभिप्राय बनाते हैं। इस सीमित, अपूर्ण, अभिप्राय को 'नय' कहते हैं। नय के सात प्रकार कहे गये हैं। १) नैगम नय २) संग्रह नय ३) व्यवहार नय ४) ऋजुसूत्र नय ५) शब्द नय ६) समभिरूढ़ नय, तथा ७) एवं भूत नय प्रथम तीन नय द्रव्यार्थिक, तथा अन्तिम चार नय पर्यायार्थिक कहलाते हैं।
इन सात नयों के साथ चारनिक्षेप माने जाते हैं। (१) नाम निक्षेप का मतलब है, किसी वस्तु को नाम से पहचानना। (२) स्थापना निक्षेप में वस्तु को उसके आकार के अनुसार ग्रहण कर लिया जाता है। (३) द्रव्य निक्षेप वस्तु की सरंचना जिस द्रव्य से हुई है उसकी ओर ध्यान देने को कहते हैं। (४) भाव निक्षेप, अर्थात वस्तु के साथ जो संकल्पना या बोध भाव जुड़ा हुआ होता है, उसके आधार पर वस्तु को जानना।
स्याद्वाद - वस्तु का अनेकान्त स्वरूप, तथा उसका ज्ञान हमेशा नयात्मक ही होना, इन दो तथ्यों को समझ लेने पर स्याद्वाद को हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। हमारा ज्ञान परिपूर्ण न होकर अंशात्मक होता है इसका मतलब यह नहीं होता कि वह असत्य होता है। अपूर्ण होने पर भी उसमें सत्य का अंश होना ही चाहिये। इसीलिये 'सत्य' या 'असत्य' यह ज्ञान की कसौटी न मानकर वह कसौटी “स्थान' (शायद ऐसा हो) यह माननी पड़ेगी। वस्तु के अनन्त धर्मों में से किसी एक के संबंध में कह सकेंगे 'स्यादस्ति,
और किसी अन्य धर्म के बारे में 'स्थान्नास्ति' ऐसा कहना पड़ेगा। 'अस्ति' तथा 'नास्ति' इन दोनों शब्दों का प्रयोग इस प्रकार एक ही वस्तु के सन्दर्भ में कर सकते हैं। अस्ति तथा नास्ति इन दोनों में जो भेद या विरोध समझा जाता है वह ‘स्यात्' इस शब्द का प्रयोग करने से खत्म हो जायेगा। यही स्याद्वाद का
(१७४)
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org