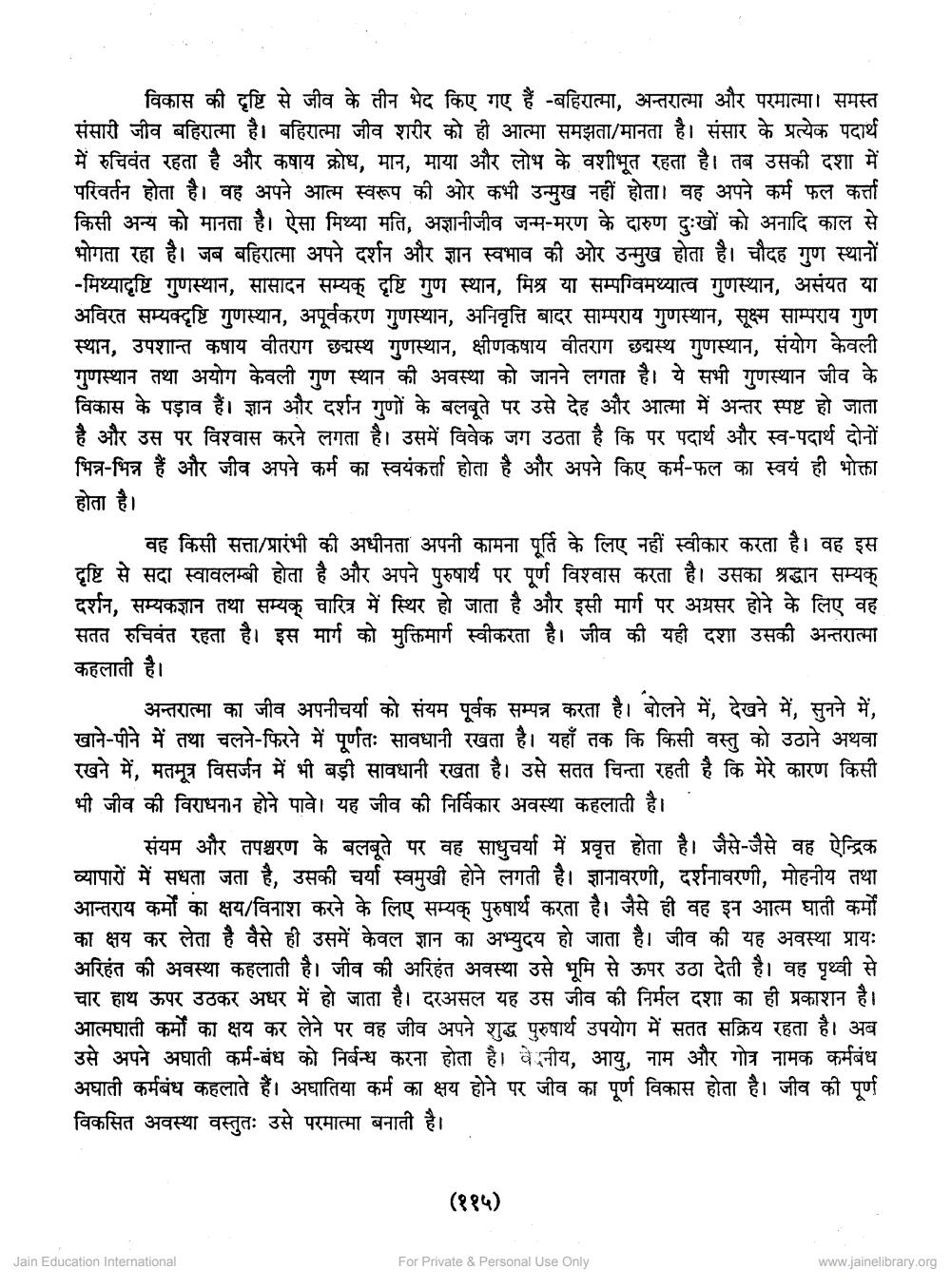________________
विकास की दृष्टि से जीव के तीन भेद किए गए हैं -बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा। समस्त संसारी जीव बहिरात्मा है। बहिरात्मा जीव शरीर को ही आत्मा समझता/मानता है। संसार के प्रत्येक पदार्थ में रुचिवंत रहता है और कषाय क्रोध, मान, माया और लोभ के वशीभूत रहता है। तब उसकी दशा में परिवर्तन होता है। वह अपने आत्म स्वरूप की ओर कभी उन्मुख नहीं होता। वह अपने कर्म फल कर्ता किसी अन्य को मानता है। ऐसा मिथ्या मति, अज्ञानीजीव जन्म-मरण के दारुण दुःखों को अनादि काल से भोगता रहा है। जब बहिरात्मा अपने दर्शन और ज्ञान स्वभाव की ओर उन्मुख होता है। चौदह गुण स्थानों -मिथ्यादृष्टि गुणस्थान, सासादन सम्यक् दृष्टि गुण स्थान, मिश्र या सम्पग्विमथ्यात्व गुणस्थान, असंयत या अविरत सम्यक्दृष्टि गुणस्थान, अपूर्वकरण गुणस्थान, अनिवृत्ति बादर साम्पराय गुणस्थान, सूक्ष्म साम्पराय गुण स्थान, उपशान्त कषाय वीतराग छद्मस्थ गुणस्थान, क्षीणकषाय वीतराग छद्मस्थ गुणस्थान, संयोग केवली गुणस्थान तथा अयोग केवली गुण स्थान की अवस्था को जानने लगता है। ये सभी गुणस्थान जीव के विकास के पड़ाव हैं। ज्ञान और दर्शन गुणों के बलबूते पर उसे देह और आत्मा में अन्तर स्पष्ट हो जाता है और उस पर विश्वास करने लगता है। उसमें विवेक जग उठता है कि पर पदार्थ और स्व-पदार्थ दोनों भिन्न-भिन्न हैं और जीव अपने कर्म का स्वयंकर्ता होता है और अपने किए कर्म-फल का स्वयं ही भोक्ता
होता है।
वह किसी सत्ता/प्रारंभी की अधीनता अपनी कामना पूर्ति के लिए नहीं स्वीकार करता है। वह इस दृष्टि से सदा स्वावलम्बी होता है और अपने पुरुषार्थ पर पूर्ण विश्वास करता है। उसका श्रद्धान सम्यक् दर्शन, सम्यकज्ञान तथा सम्यक् चारित्र में स्थिर हो जाता है और इसी मार्ग पर अग्रसर होने के लिए वह सतत रुचिवंत रहता है। इस मार्ग को मुक्तिमार्ग स्वीकरता है। जीव की यही दशा उसकी अन्तरात्मा कहलाती है।
अन्तरात्मा का जीव अपनीचर्या को संयम पूर्वक सम्पन्न करता है। बोलने में, देखने में, सुनने में, खाने-पीने में तथा चलने-फिरने में पूर्णतः सावधानी रखता है। यहाँ तक कि किसी वस्तु को उठाने अथवा रखने में, मतमूत्र विसर्जन में भी बड़ी सावधानी रखता है। उसे सतत चिन्ता रहती है कि मेरे कारण किसी भी जीव की विराधनान होने पावे। यह जीव की निर्विकार अवस्था कहलाती है।
संयम और तपश्चरण के बलबूते पर वह साधुचर्या में प्रवृत्त होता है। जैसे-जैसे वह ऐन्द्रिक व्यापारों में सधता जता है, उसकी चर्या स्वमुखी होने लगती है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय तथा आन्तराय कर्मों का क्षय/विनाश करने के लिए सम्यक् पुरुषार्थ करता है। जैसे ही वह इन आत्म घाती कर्मों का क्षय कर लेता है वैसे ही उसमें केवल ज्ञान का अभ्युदय हो जाता है। जीव की यह अवस्था प्रायः अरिहंत की अवस्था कहलाती है। जीव की अरिहंत अवस्था उसे भूमि से ऊपर उठा देती है। वह पृथ्वी से चार हाथ ऊपर उठकर अधर में हो जाता है। दरअसल यह उस जीव की निर्मल दशा का ही प्रकाशन है। आत्मघाती कर्मों का क्षय कर लेने पर वह जीव अपने शुद्ध पुरुषार्थ उपयोग में सतत सक्रिय रहता है। अब उसे अपने अघाती कर्म-बंध को निर्बन्ध करना होता है। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र नामक कर्मबंध
अघाती कर्मबंध कहलाते हैं। अघातिया कर्म का क्षय होने पर जीव का पूर्ण विकास होता है। जीव की पूर्ण विकसित अवस्था वस्तुतः उसे परमात्मा बनाती है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org