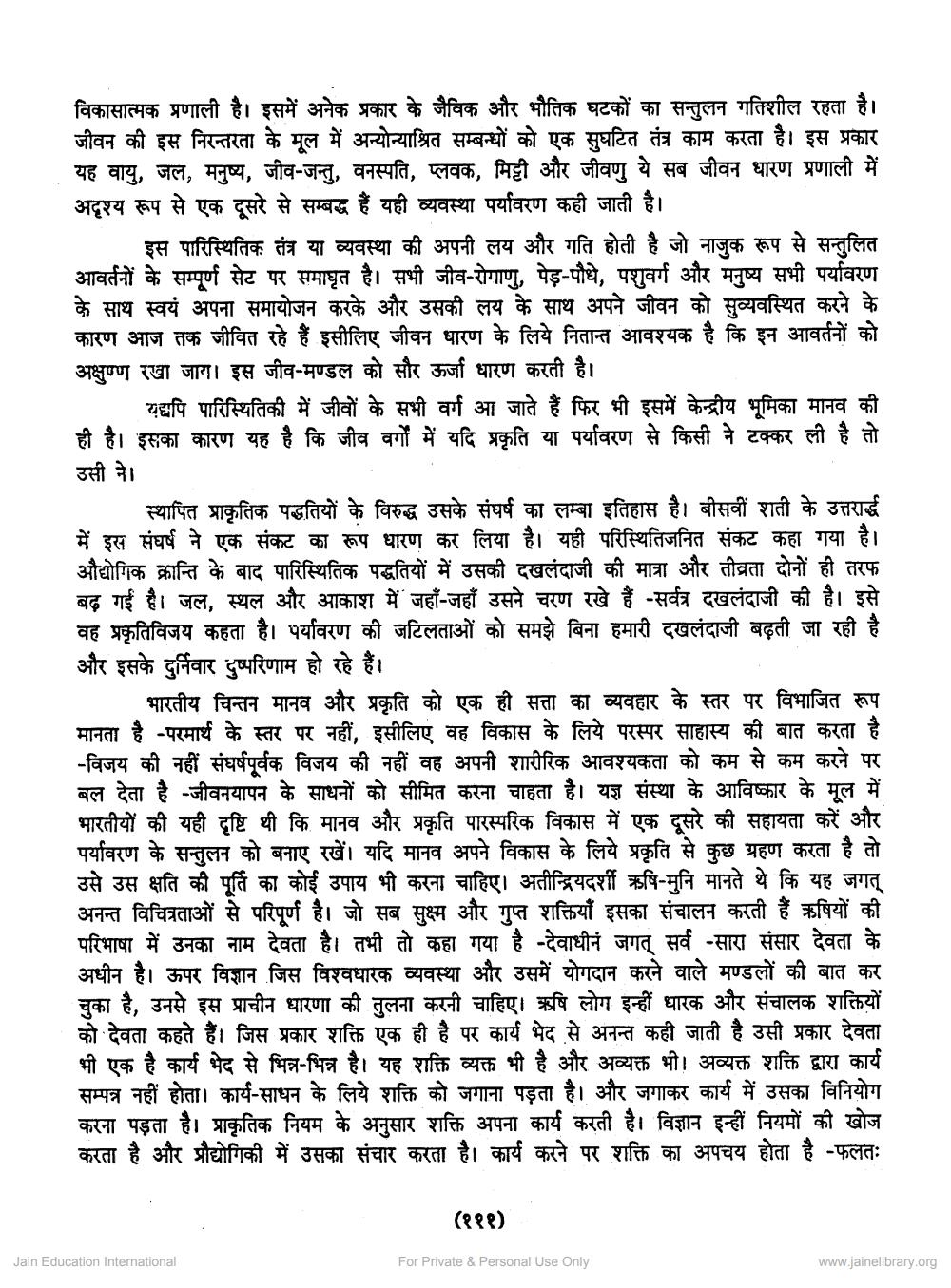________________
विकासात्मक प्रणाली है। इसमें अनेक प्रकार के जैविक और भौतिक घटकों का सन्तुलन गतिशील रहता है। जीवन की इस निरन्तरता के मूल में अन्योन्याश्रित सम्बन्धों को एक सुघटित तंत्र काम करता है। इस प्रकार यह वायु, जल, मनुष्य, जीव-जन्तु, वनस्पति, प्लवक, मिट्टी और जीवणु ये सब जीवन धारण प्रणाली में अदृश्य रूप से एक दूसरे से सम्बद्ध हैं यही व्यवस्था पर्यावरण कही जाती है।
__इस पारिस्थितिक तंत्र या व्यवस्था की अपनी लय और गति होती है जो नाजुक रूप से सन्तुलित आवर्तनों के सम्पूर्ण सेट पर समाघृत है। सभी जीव-रोगाणु, पेड़-पौधे, पशुवर्ग और मनुष्य सभी पर्यावरण के साथ स्वयं अपना समायोजन करके और उसकी लय के साथ अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने के कारण आज तक जीवित रहे हैं इसीलिए जीवन धारण के लिये नितान्त आवश्यक है कि इन आवर्तनों को अक्षुण्ण रखा जाग। इस जीव-मण्डल को सौर ऊर्जा धारण करती है।
यद्यपि पारिस्थितिकी में जीवों के सभी वर्ग आ जाते हैं फिर भी इसमें केन्द्रीय भूमिका मानव की ही है। इसका कारण यह है कि जीव वर्गों में यदि प्रकृति या पर्यावरण से किसी ने टक्कर ली है तो उसी ने।
स्थापित प्राकृतिक पद्धतियों के विरुद्ध उसके संघर्ष का लम्बा इतिहास है। बीसवीं शती के उत्तरार्द्ध में इस संघर्ष ने एक संकट का रूप धारण कर लिया है। यही परिस्थितिजनित संकट कहा गया है।
औद्योगिक क्रान्ति के बाद पारिस्थितिक पद्धतियों में उसकी दखलंदाजी की मात्रा और तीव्रता दोनों ही तरफ बढ़ गई है। जल, स्थल और आकाश में जहाँ-जहाँ उसने चरण रखे हैं -सर्वत्र दखलंदाजी की है। इसे वह प्रकृतिविजय कहता है। पर्यावरण की जटिलताओं को समझे बिना हमारी दखलंदाजी बढ़ती जा रही है और इसके दुर्निवार दुष्परिणाम हो रहे हैं।
भारतीय चिन्तन मानव और प्रकृति को एक ही सत्ता का व्यवहार के स्तर पर विभाजित रूप मानता है -परमार्थ के स्तर पर नहीं, इसीलिए वह विकास के लिये परस्पर साहास्य की बात करता है -विजय की नहीं संघर्षपूर्वक विजय की नहीं वह अपनी शारीरिक आवश्यकता को कम से कम करने पर बल देता है -जीवनयापन के साधनों को सीमित करना चाहता है। यज्ञ संस्था के आविष्कार के मूल में भारतीयों की यही दृष्टि थी कि मानव और प्रकृति पारस्परिक विकास में एक दूसरे की सहायता करें और पर्यावरण के सन्तुलन को बनाए रखें। यदि मानव अपने विकास के लिये प्रकृति से कुछ ग्रहण करता है तो उसे उस क्षति की पूर्ति का कोई उपाय भी करना चाहिए। अतीन्द्रियदर्शी ऋषि-मुनि मानते थे कि यह जगत् अनन्त विचित्रताओं से परिपूर्ण है। जो सब सुक्ष्म और गुप्त शक्तियाँ इसका संचालन करती हैं ऋषियों की परिभाषा में उनका नाम देवता है। तभी तो कहा गया है -देवाधीनं जगत् सर्व -सारा संसार देवता के अधीन है। ऊपर विज्ञान जिस विश्वधारक व्यवस्था और उसमें योगदान करने वाले मण्डलों की बात कर चुका है, उनसे इस प्राचीन धारणा की तुलना करनी चाहिए। ऋषि लोग इन्हीं धारक और संचालक शक्तियों को देवता कहते हैं। जिस प्रकार शक्ति एक ही है पर कार्य भेद से अनन्त कही जाती है उसी प्रकार देवता भी एक है कार्य भेद से भिन्न-भिन्न है। यह शक्ति व्यक्त भी है और अव्यक्त भी। अव्यक्त शक्ति द्वारा कार्य सम्पन्न नहीं होता। कार्य-साधन के लिये शक्ति को जगाना पड़ता है। और जगाकर कार्य में उसका विनियोग करना पड़ता है। प्राकृतिक नियम के अनुसार शक्ति अपना कार्य करती है। विज्ञान इन्हीं नियमों की खोज करता है और प्रौद्योगिकी में उसका संचार करता है। कार्य करने पर शक्ति का अपचय होता है -फलतः
(१११)
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org