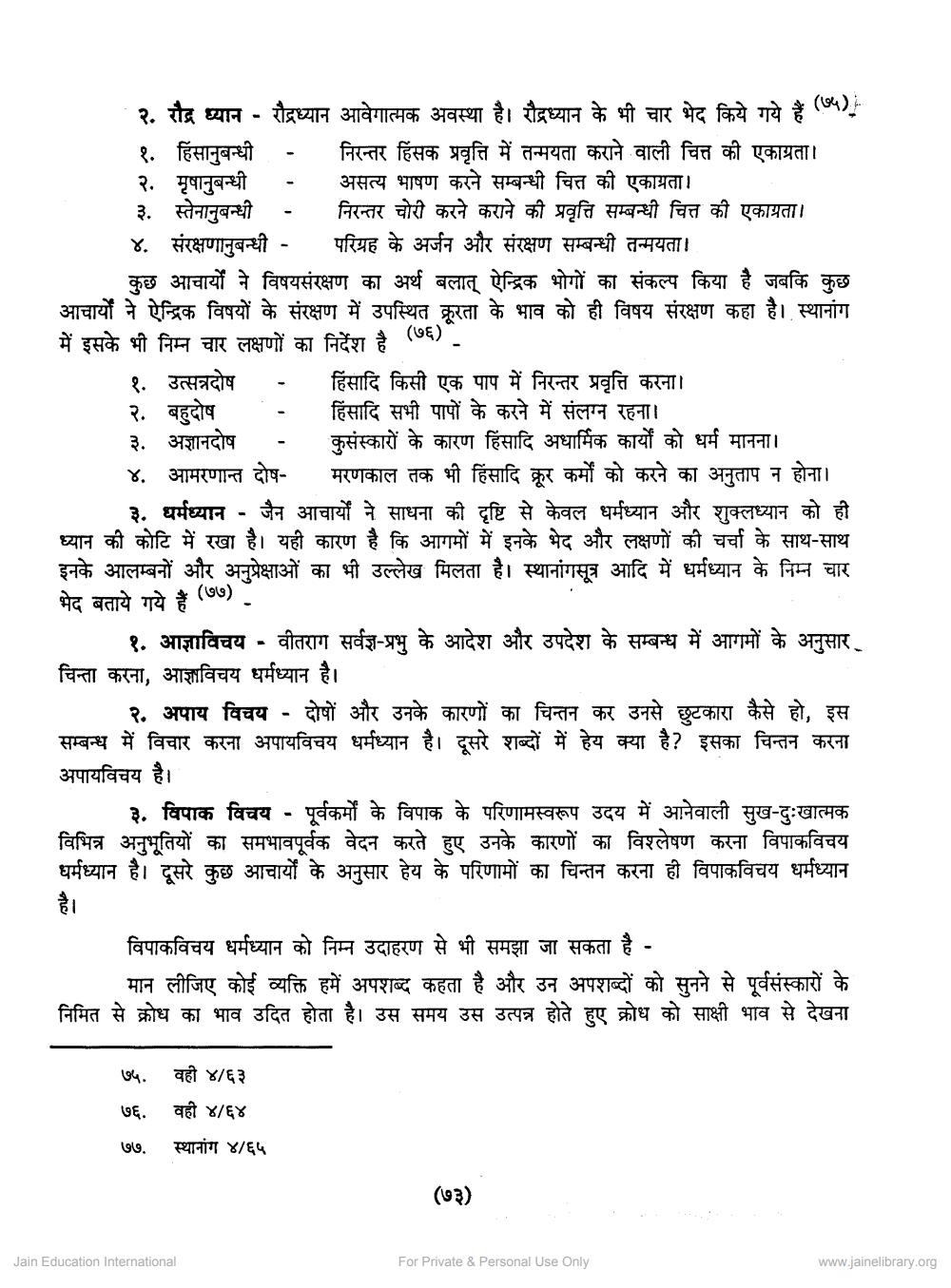________________
२. रौद्र ध्यान - रौद्रध्यान आवेगात्मक अवस्था है। रौद्रध्यान के भी चार भेद किये गये हैं (७५). १. हिंसानुबन्धी . निरन्तर हिंसक प्रवृत्ति में तन्मयता कराने वाली चित्त की एकाग्रता। २. मृषानुबन्धी - असत्य भाषण करने सम्बन्धी चित्त की एकाग्रता। ३. स्तेनानुबन्धी - निरन्तर चोरी करने कराने की प्रवृत्ति सम्बन्धी चित्त की एकाग्रता। ४. संरक्षणानुबन्धी - परिग्रह के अर्जन और संरक्षण सम्बन्धी तन्मयता।
कुछ आचार्यों ने विषयसंरक्षण का अर्थ बलात् ऐन्द्रिक भोगों का संकल्प किया है जबकि कुछ आचार्यों ने ऐन्द्रिक विषयों के संरक्षण में उपस्थित क्रूरता के भाव को ही विषय संरक्षण कहा है। स्थानांग में इसके भी निम्न चार लक्षणों का निर्देश है (७५) -
१. उत्सत्रदोष . हिंसादि किसी एक पाप में निरन्तर प्रवृत्ति करना। २. बहुदोष - हिंसादि सभी पापों के करने में संलग्न रहना। ३. अज्ञानदोष - कुसंस्कारों के कारण हिंसादि अधार्मिक कार्यों को धर्म मानना। ४. आमरणान्त दोष- मरणकाल तक भी हिंसादि क्रूर कर्मों को करने का अनुताप न होना।
३. धर्मध्यान - जैन आचार्यों ने साधना की दृष्टि से केवल धर्मध्यान और शुक्लध्यान को ही ध्यान की कोटि में रखा है। यही कारण है कि आगमों में इनके भेद और लक्षणों की चर्चा के साथ-साथ इनके आलम्बनों और अनुप्रेक्षाओं का भी उल्लेख मिलता है। स्थानांगसूत्र आदि में धर्मध्यान के निम्न चार भेद बताये गये हैं (७७) -
१. आज्ञाविचय - वीतराग सर्वज्ञ-प्रभु के आदेश और उपदेश के सम्बन्ध में आगमों के अनुसार, चिन्ता करना, आज्ञाविचय धर्मध्यान है।
२. अपाय विचय - दोषों और उनके कारणों का चिन्तन कर उनसे छुटकारा कैसे हो, इस सम्बन्ध में विचार करना अपायविचय धर्मध्यान है। दूसरे शब्दों में हेय क्या है? इसका चिन्तन करना अपायविचय है।
३. विपाक विचय - पूर्वकर्मों के विपाक के परिणामस्वरूप उदय में आनेवाली सुख-दुःखात्मक विभिन्न अनुभूतियों का समभावपूर्वक वेदन करते हुए उनके कारणों का विश्लेषण करना विपाकविचय धर्मध्यान है। दूसरे कुछ आचार्यों के अनुसार हेय के परिणामों का चिन्तन करना ही विपाकविचय धर्मध्यान
विपाकविचय धर्मध्यान को निम्न उदाहरण से भी समझा जा सकता है -
मान लीजिए कोई व्यक्ति हमें अपशब्द कहता है और उन अपशब्दों को सुनने से पूर्वसंस्कारों के निमित से क्रोध का भाव उदित होता है। उस समय उस उत्पन्न होते हुए क्रोध को साक्षी भाव से देखना
७५. वही ४/६३ ७६. वही ४/६४ ७७. स्थानांग ४/६५
(७३)
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org