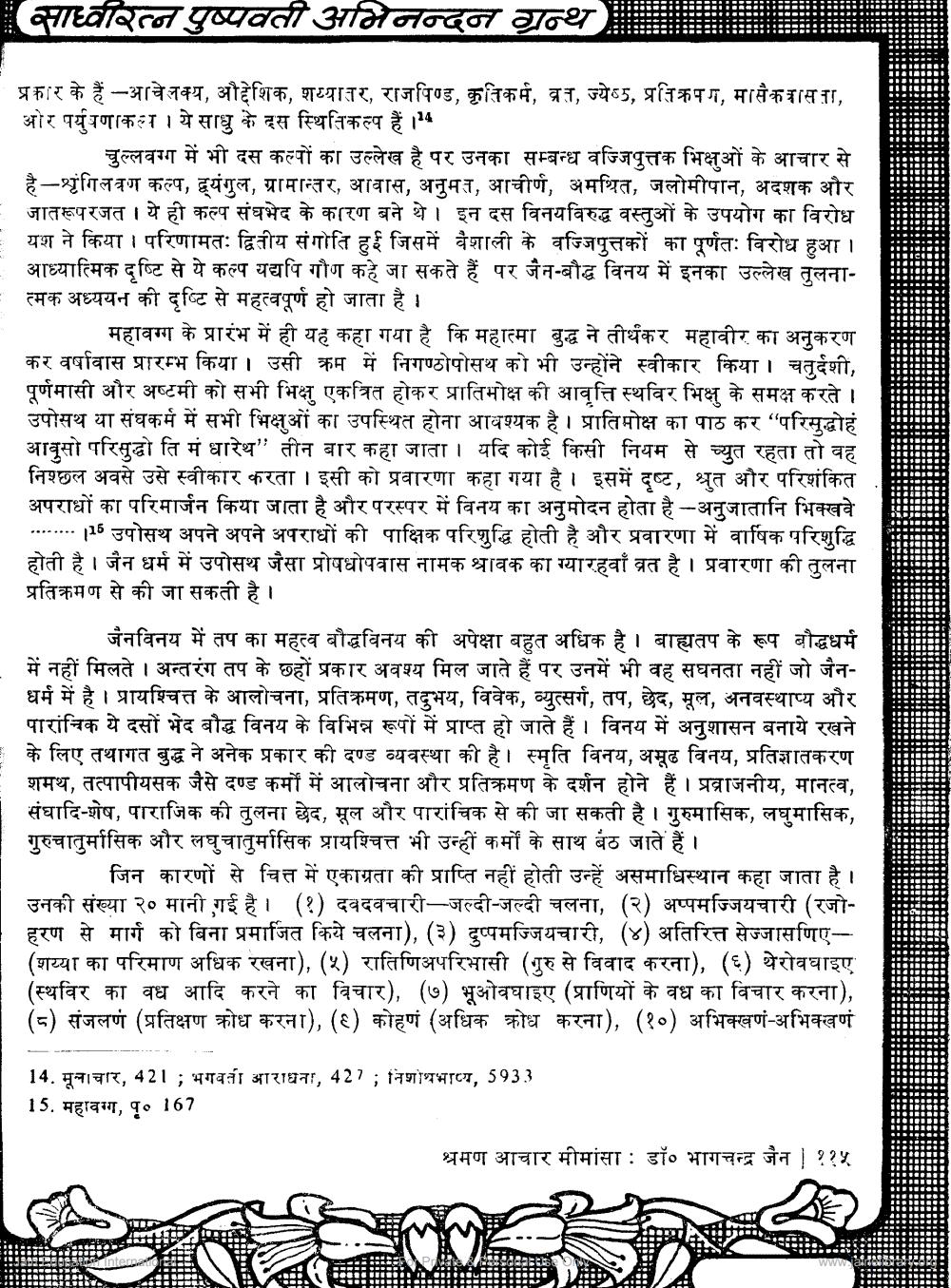________________
साध्वीरत्नपुष्पवती अभिनन्दन ग्रन्थ
प्रकार के हैं -आचेलक्य, औदेशिक, शय्यातर, राजपिण्ड, कृतिकर्म, व्रत, ज्येष्ठ, प्रतिक्रमम, मासैकवासता, ओर पर्युषणाकल । ये साधु के दस स्थितिकल्प हैं ।
चुल्लवग्ग में भी दस कल्पों का उल्लेख है पर उनका सम्बन्ध वज्जिपुत्तक भिक्षुओं के आचार से है-शृंगिलवण कल्प, व्यंगुल, ग्रामान्तर, आवास, अनुमत, आचीर्ण, अमथित, जलोमीपान, अदशक और जातरूपरजत । ये ही कल्प संघभेद के कारण बने थे। इन दस विनयविरुद्ध वस्तुओं के उपयोग का विरोध यश ने किया। परिणामतः द्वितीय संगोति हुई जिसमें वैशाली के वज्जिपुत्तकों का पूर्णतः विरोध हुआ। आध्यात्मिक दृष्टि से ये कल्प यद्यपि गौण कहे जा सकते हैं पर जैन-बौद्ध विनय में इनका उल्लेख तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है।
महावग्ग के प्रारंभ में ही यह कहा गया है कि महात्मा बुद्ध ने तीर्थंकर महावीर का अनुकरण कर वर्षावास प्रारम्भ किया। उसी क्रम में निगण्ठोपोसथ को भी उन्होंने स्वीकार किया। चतुर्दशी, पूर्णमासी और अष्टमी को सभी भिक्षु एकत्रित होकर प्रातिमोक्ष की आवृत्ति स्थविर भिक्षु के समक्ष करते। उपोसथ या संघकर्म में सभी भिक्षुओं का उपस्थित होना आवश्यक है। प्रातिमोक्ष का पाठ कर “परिसुद्धोहं आवूसो परिसुद्धो ति मंधारेथ" तीन बार कहा जाता। यदि कोई किसी नियम से च्युत रहता तो वह निश्छल अवसे उसे स्वीकार करता । इसी को प्रवारणा कहा गया है। इसमें दष्ट, श्रत और परिशंकित अपराधों का परिमार्जन किया जाता है और परस्पर में विनय का अनुमोदन होता है -अनुजातानि भिक्खवे ......... 115 उपोसथ अपने अपने अपराधों की पाक्षिक परिशुद्धि होती है और प्रवारणा में वार्षिक परिशुद्धि होती है । जैन धर्म में उपोसथ जैसा प्रोषधोपवास नामक श्रावक का ग्यारहवाँ व्रत है। प्रवारणा की तुलना प्रतिक्रमण से की जा सकती है।
जैनविनय में तप का महत्व बौद्धविनय की अपेक्षा बहुत अधिक है। बाह्यतप के रूप बौद्धधर्म में नहीं मिलते । अन्तरंग तप के छहों प्रकार अवश्य मिल जाते हैं पर उनमें भी वह सघनता नहीं जो जैनधर्म में है। प्रायश्चित्त के आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, मूल, अनवस्थाप्य और पारांचिक ये दसों भेद बौद्ध विनय के विभिन्न रूपों में प्राप्त हो जाते हैं। विनय में अनुशासन बनाये रखने के लिए तथागत बुद्ध ने अनेक प्रकार की दण्ड व्यवस्था की है। स्मृति विनय, अमूढ विनय, प्रतिज्ञातकरण
मथ, तत्पापीयसक जैसे दण्ड कर्मों में आलोचना और प्रतिक्रमण के दर्शन होने हैं। प्रव्राजनीय, मानत्व संघादि-शेष, पाराजिक की तुलना छेद, मूल और पारांचिक से की जा सकती है । गुरुमासिक, लघुमासिक, गुरुचातुर्मासिक और लघुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त भी उन्हीं कर्मों के साथ बैठ जाते हैं।
जिन कारणों से चित्त में एकाग्रता की प्राप्ति नहीं होती उन्हें असमाधिस्थान कहा जाता है। उनकी संख्या २० मानी गई है। (१) दवदवचारी-जल्दी-जल्दी चलना, (२) अप्पम हरण से मार्ग को बिना प्रमार्जित किये चलना), (३) दुप्पमज्जियचारी, (४) अतिरित्त सेज्जासहिए(शय्या का परिमाण अधिक रखना), (५) रातिणिअपरिभासी (गुरु से विवाद करना), (६) थेरोवघाइए (स्थविर का वध आदि करने का विचार), (७) भूओवघाइए (प्राणियों के वध का विचार करना), (८) संजलणं (प्रतिक्षण क्रोध करना), (६) कोहणं (अधिक क्रोध करना), (१०) अभिक्खणं-अभिक्खणं
14. मूलाचार, 421 ; भगवती आराधना, 427 ; निशोथभाष्य, 5933 15. महावग्ग, पृ० 167
श्रमण आचार मीमांसा : डॉ० भागचन्द्र जैन | ११५