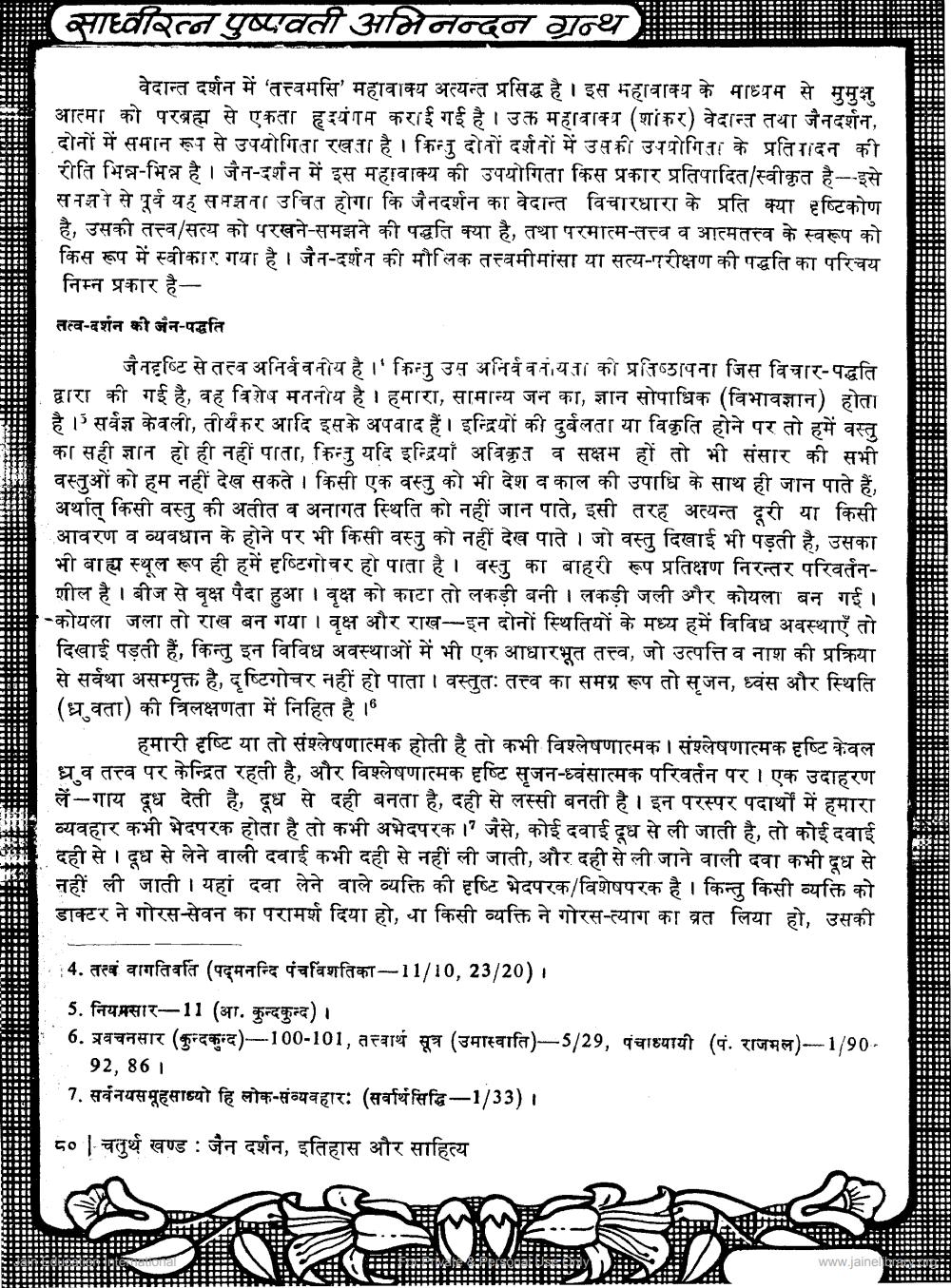________________
साध्वी रत्न पुष्पवती अभिनन्दन ग्रन्थ
वेदान्त दर्शन में 'तत्त्वमसि' महावाक्य अत्यन्त प्रसिद्ध है । इस महावाक्य के माध्यम से मुमुक्षु आत्मा को परब्रह्म से एकता हृदयंगम कराई गई है । उक्त महावाक्य (शांकर) वेदान्त तथा जैनदर्शन, दोनों में समान रूप से उपयोगिता रखता । किन्तु दोनों दर्शनों में उसकी उपयोगिता के प्रतिपादन की रीति भिन्न-भिन्न है । जैन दर्शन में इस महावाक्य की उपयोगिता किस प्रकार प्रतिपादित / स्वीकृत है - इसे समझने से पूर्व यह समझना उचित होगा कि जैनदर्शन का वेदान्त विचारधारा के प्रति क्या दृष्टिकोण है, उसकी तत्त्व/ सत्य को परखने-समझने की पद्धति क्या है, तथा परमात्म-तत्त्व व आत्मतत्त्व के स्वरूप को किस रूप में स्वीकार गया है। जैन दर्शन की मौलिक तत्त्वमीमांसा या सत्य-परीक्षण की पद्धति का परिचय निम्न प्रकार है
तत्व-दर्शन की जैन-पद्धति
दृष्टि से तत्व अनिर्ववतीय है ।' किन्तु उस अनिवर्तयता की प्रतिष्ठापना जिस विचार पद्धति द्वारा की गई है, वह विशेष मननीय है । हमारा सामान्य जन का ज्ञान सोपाधिक (विभावज्ञान) होता है । सर्वज्ञ केवली, तीर्थंकर आदि इसके अपवाद हैं । इन्द्रियों की दुर्बलता या विकृति होने पर तो हमें वस्तु का सही ज्ञान हो ही नहीं पाता, किन्तु यदि इन्द्रियाँ अविकृत व सक्षम हों तो भी संसार की सभी वस्तुओं को हम नहीं देख सकते । किसी एक वस्तु को भी देश व काल की उपाधि के साथ ही जान पाते हैं, अर्थात् किसी वस्तु की अतीत व अनागत स्थिति को नहीं जान पाते, इसी तरह अत्यन्त दूरी या किसी आवरण व व्यवधान के होने पर भी किसी वस्तु को नहीं देख पाते । जो वस्तु दिखाई भी पड़ती है, उसका भी बाह्य स्थूल रूप ही हमें दृष्टिगोचर हो पाता है । वस्तु का बाहरी रूप प्रतिक्षण निरन्तर परिवर्तनशील है । बीज से वृक्ष पैदा हुआ । वृक्ष को काटा तो लकड़ी बनी । लकड़ी जली और कोयला बन गई। - कोयला जला तो राख बन गया । वृक्ष और राख - इन दोनों स्थितियों के मध्य हमें विविध अवस्थाएँ तो दिखाई पड़ती हैं, किन्तु इन विविध अवस्थाओं में भी एक आधारभूत तत्त्व, जो उत्पत्ति व नाश की प्रक्रिया से सर्वथा असम्पृक्त है, दृष्टिगोचर नहीं हो पाता । वस्तुतः तत्त्व का समग्र रूप तो सृजन, ध्वंस और स्थिति ( ध्रुवता ) की विलक्षणता में निहित है ।"
हमारी दृष्टि या तो संश्लेषणात्मक होती है तो कभी विश्लेषणात्मक । संश्लेषणात्मक दृष्टि केवल ध्रुव तत्त्व पर केन्द्रित रहती है, और विश्लेषणात्मक दृष्टि सृजन-ध्वंसात्मक परिवर्तन पर । एक उदाहरण लें - गाय दूध देती है, दूध से दही बनता है, दही से लस्सी बनती है । इन परस्पर पदार्थों में हमारा व्यवहार कभी भेदपरक होता है तो कभी अभेदपरक । जैसे, कोई दवाई दूध से ली जाती है, तो कोई दवाई दही से । दूध से लेने वाली दवाई कभी दही से नहीं ली जाती, और दही से ली जाने वाली दवा कभी दूध नहीं ली जाती। यहां दवा लेने वाले व्यक्ति की दृष्टि भेदपरक / विशेषपरक है । किन्तु किसी व्यक्ति को डाक्टर ने गोरस सेवन का परामर्श दिया हो, या किसी व्यक्ति ने गोरस-त्याग का व्रत लिया हो, उसकी
4. तत्वं वागतिवति (पद्मनन्दि पंचविशतिका - 11 / 10, 23/20)।
5. नियमसार - 11 ( आ. कुन्दकुन्द) ।
6. प्रवचनसार (कुन्दकुन्द ) - 100-101, तत्त्वार्थ सूत्र ( उमास्वाति ) - 5 / 29, पंचाध्यायी (पं. राजमल ) -- 1 /9092, 86 1
7. सर्वनयसमूहसाध्यो हि लोक-संव्यवहार : ( सर्वार्थ सिद्धि – 1 / 33 ) ।
८० | चतुर्थ खण्ड : जैन दर्शन, इतिहास और साहित्य
www.jainel