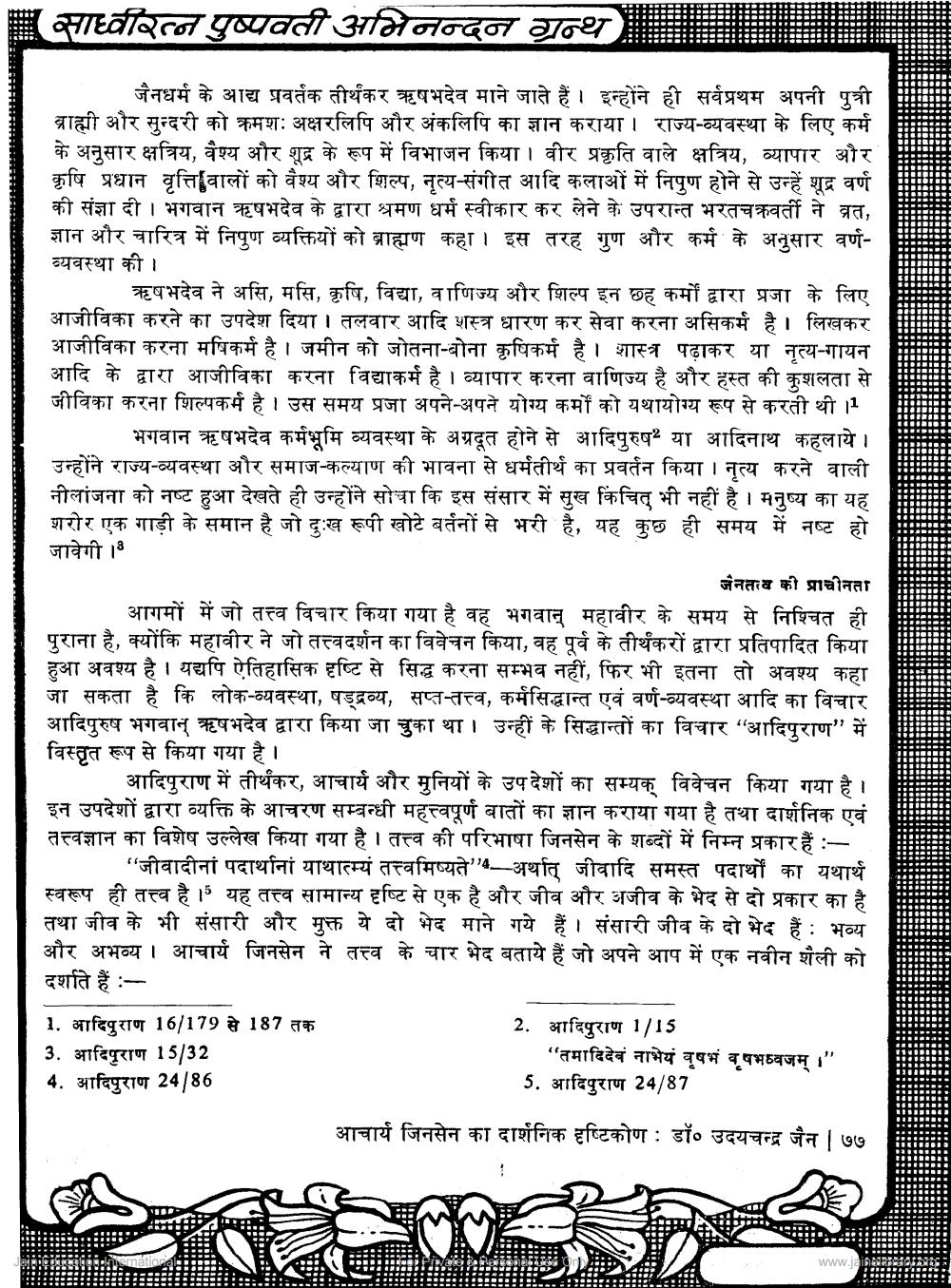________________
साध्वीरत्न पुष्पवती अभिनन्दन ग्रन्थ
जैनधर्म के आद्य प्रवर्तक तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम अपनी पुत्री ब्राह्मी और सुन्दरी को क्रमशः अक्षरलिपि और अंकलिपि का ज्ञान कराया। राज्य-व्यवस्था के लिए कर्म के अनुसार क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में विभाजन किया। वीर प्रकृति वाले क्षत्रिय, व्यापार और कृषि प्रधान वृत्ति वालों को वैश्य और शिल्प, नृत्य-संगीत आदि कलाओं में निपुण होने से उन्हें शूद्र वर्ण की संज्ञा दी। भगवान ऋषभदेव के द्वारा श्रमण धर्म स्वीकार कर लेने के उपरान्त भरतचक्रवर्ती ने व्रत, ज्ञान और चारित्र में निपुण व्यक्तियों को ब्राह्मण कहा। इस तरह गुण और कर्म के अनुसार वर्णव्यवस्था की।
ऋषभदेव ने असि, मसि, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प इन छह कर्मों द्वारा प्रजा के लिए आजीविका करने का उपदेश दिया। तलवार आदि शस्त्र धारण कर सेवा करना असिकर्म है। लिखकर आजीविका करना मषिकर्म है। जमीन को जोतना-बोना कृषिकर्म है। शास्त्र पढाकर आदि के द्वारा आजीविका करना विद्याकर्म है। व्यापार करना वाणिज्य है और हस्त की कुशलता से जीविका करना शिल्पकर्म है। उस समय प्रजा अपने-अपने योग्य कर्मों को यथायोग्य रूप से करती थी।1
भगवान ऋषभदेव कर्मभूमि व्यवस्था के अग्रदूत होने से आदिपुरुष या आदिनाथ कहलाये। उन्होंने राज्य-व्यवस्था और समाज-कल्याण की भावना से धर्मतीर्थ का प्रवर्तन किया । नृत्य करने वाली नीलांजना को नष्ट हुआ देखते ही उन्होंने सोचा कि इस संसार में सुख किंचित् भी नहीं है । मनुष्य का यह शरीर एक गाड़ी के समान है जो दुःख रूपी खोटे बर्तनों से भरी है, यह कुछ ही समय में नष्ट हो जावेगी।
जैनतत्व की प्राचीनता आगमों में जो तत्त्व विचार किया गया है वह भगवान महावीर के समय से निश्चित ही पुराना है, क्योंकि महावीर ने जो तत्त्वदर्शन का विवेचन किया, वह पूर्व के तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित किया हुआ अवश्य है । यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टि से सिद्ध करना सम्भव नहीं, फिर भी इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि लोक-व्यवस्था, षड्द्रव्य, सप्त-तत्त्व, कर्मसिद्धान्त एवं वर्ण-व्यवस्था आदि का विचार आदिपुरुष भगवान् ऋषभदेव द्वारा किया जा चुका था। उन्हीं के सिद्धान्तों का विचार "आदिपुराण" में विस्तृत रूप से किया गया है।
__ आदिपुराण में तीर्थंकर, आचार्य और मुनियों के उपदेशों का सम्यक् विवेचन किया गया है। इन उपदेशों द्वारा व्यक्ति के आचरण सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण बातों का ज्ञान कराया गया है तथा दार्शनिक एवं तत्त्वज्ञान का विशेष उल्लेख किया गया है। तत्त्व की परिभाषा जिनसेन के शब्दों में निम्न प्रकार हैं :
"जीवादीनां पदार्थानां याथात्म्यं तत्त्वमिष्यते"4-अर्थात् जीवादि समस्त पदार्थों का यथार्थ स्वरूप ही तत्त्व है। यह तत्त्व सामान्य दृष्टि से एक है और जीव और अजीव के भेद से दो प्रकार का है तथा जीव के भी संसारी और मुक्त ये दो भेद माने गये हैं। संसारी जीव के दो भेद हैं : भव्य
और अभव्य । आचार्य जिनसेन ने तत्त्व के चार भेद बताये हैं जो अपने आप में एक नवीन शैली को दर्शाते हैं :
1. आदिपुराण 16/179 से 187 तक 3. आदिपुराण 15/32 4. आदिपुराण 24/86
2. आदिपुराण 1/15
"तमादिदेव नाभेयं वृषभं वृषभध्वजम् ।" 5. आदिपुराण 24/87
आचार्य जिनसेन का दार्शनिक दृष्टिकोण : डॉ० उदयचन्द्र जैन | ७७
www.IE