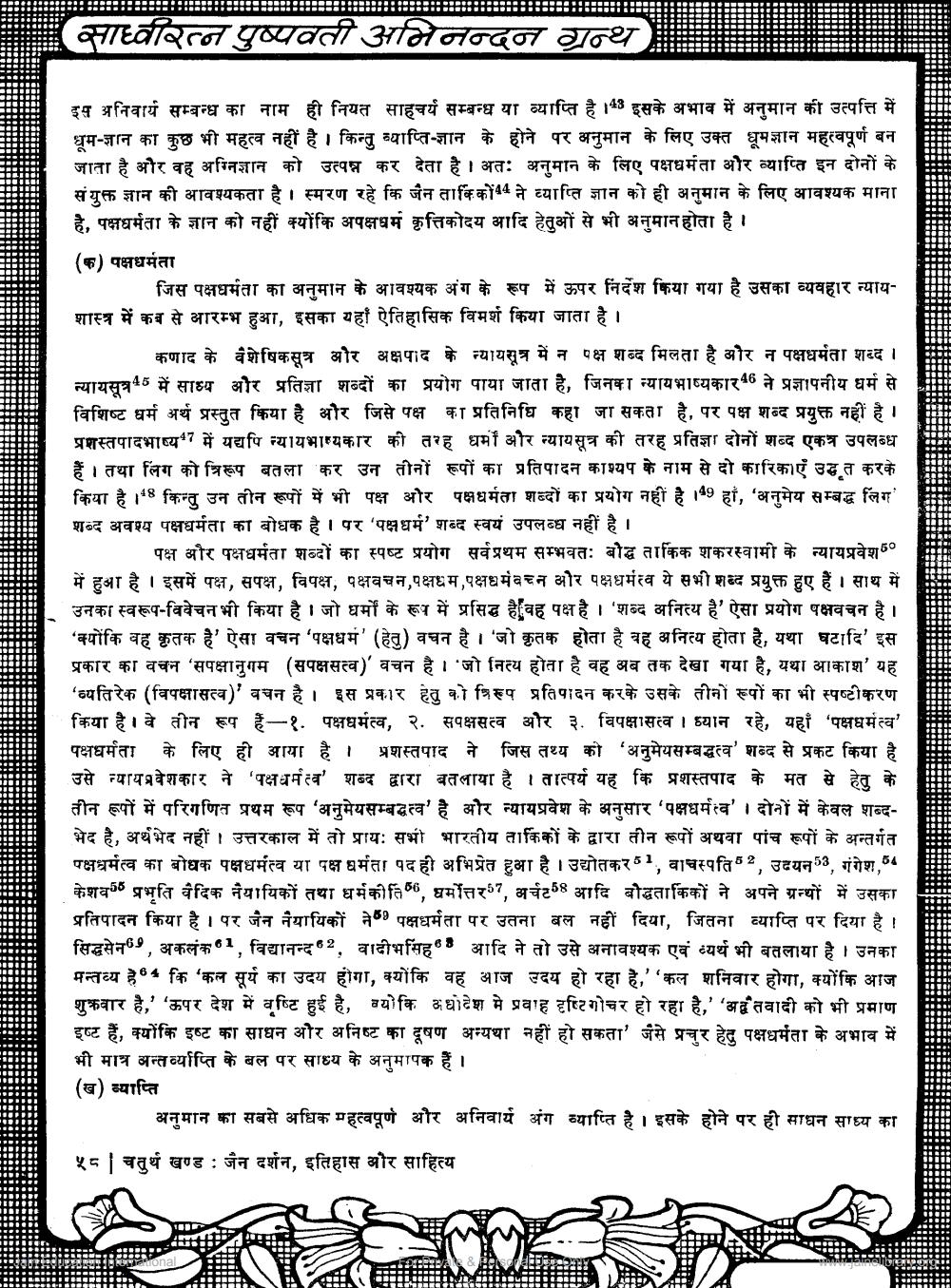________________
साध्वीरत्नपुष्पवती अभिनन्दन ग्रन्थ
इस अनिवार्य सम्बन्ध का नाम ही नियत साहचर्य सम्बन्ध या व्याप्ति है।43 इसके अभाव में अनुमान की उत्पत्ति में धूम-ज्ञान का कुछ भी महत्व नहीं है। किन्तु व्याप्ति-ज्ञान के होने पर अनुमान के लिए उक्त धूम ज्ञान महत्वपूर्ण बन जाता है और वह अग्निज्ञान को उत्पन्न कर देता है। अतः अनुमान के लिए पक्षधर्मता और व्याप्ति इन दोनों के संयुक्त ज्ञान की आवश्यकता है। स्मरण रहे कि जैन ताकिकों ने व्याप्ति ज्ञान को ही अनुमान के लिए आवश्यक माना है, पक्षधर्मता के ज्ञान को नहीं क्योंकि अपक्षधर्म कृत्तिकोदय आदि हेतुओं से भी अनुमान होता है । (क) पक्षधर्मता
जिस पक्षधर्मता का अनुमान के आवश्यक अंग के रूप में ऊपर निर्देश किया गया है उसका व्यवहार न्यायशास्त्र में कब से आरम्भ हुआ, इसका यहाँ ऐतिहासिक विमर्श किया जाता है।
कणाद के वैशेषिकसूत्र और अक्षपाद के न्यायसूत्र में न पक्ष शब्द मिलता है और न पक्षधर्मता शब्द । न्यायसूत्र45 में साध्य और प्रतिज्ञा शब्दों का प्रयोग पाया जाता है, जिनका न्यायभाष्यकार46 ने प्रज्ञापनीय धर्म से विशिष्ट धर्म अर्थ प्रस्तुत किया है और जिसे पक्ष का प्रतिनिधि कहा जा सकता है, पर पक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं है। प्रशस्तपादभाष्य'7 में यद्यपि न्यायभाष्यकार की तरह धर्मों और न्यायसूत्र की तरह प्रतिज्ञा दोनों शब्द एकत्र उपलब्ध हैं। तथा लिंग को त्रिरूप बतला कर उन तीनों रूपों का प्रतिपादन काश्यप के नाम से दो कारिकाएं उद्धत करके किया है। 8 किन्तु उन तीन रूपों में भी पक्ष और पक्षधर्मता शब्दों का प्रयोग नहीं है ।49 हाँ, 'अनुमेय सम्बद्ध लिंग' शब्द अवश्य पक्षधर्मता का बोधक है । पर 'पक्षधर्म' शब्द स्वयं उपलब्ध नहीं है।
पक्ष और पक्षधर्मता शब्दों का स्पष्ट प्रयोग सर्वप्रथम सम्भवतः बौद्ध ताकिक शकरस्वामी के न्यायप्रवेश में हुआ है । इसमें पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, पक्षवचन,पक्षधम,पक्षधर्मवचन और पक्षधर्मत्व ये सभी शब्द प्रयुक्त हुए हैं। साथ में उनका स्वरूप-विवेचन भी किया है । जो धर्मों के रूप में प्रसिद्ध है वह पक्ष है । 'शब्द अनित्य है' ऐसा प्रयोग पक्षवचन है। 'क्योंकि वह कृतक है' ऐसा वचन 'पक्षधर्म' (हेतु) वचन है । 'जो कृतक होता है वह अनित्य होता है, यथा घटादि' इस प्रकार का वचन ‘सपक्षानुगम (सपक्षसत्व) वचन है। जो नित्य होता है वह अब तक देखा गया है, यथा आकाश' यह 'व्यतिरेक (विपक्षासत्व) वचन है। इस प्रकार हेतु को त्रिरूप प्रतिपादन करके उसके तीनों रूपों का भी स्पष्टीकरण किया है। वे तीन रूप हैं-१. पक्षधर्मत्व, २. सपक्षसत्व और ३. विपक्षासत्व । ध्यान रहे, यहाँ 'पक्षधर्मत्व' पक्षधर्मता के लिए ही आया है। प्रशस्तपाद ने जिस तथ्य को 'अनुमेयसम्बद्धत्व' शब्द से प्रकट किया है उसे न्यायप्रवेशकार ने 'पक्षधर्मत्व' शब्द द्वारा बतलाया है । तात्पर्य यह कि प्रशस्तपाद के मत से हेतु के तीन रूपों में परिगणित प्रथम रूप 'अनुमेयसम्बद्धत्व' है और न्यायप्रवेश के अनुसार 'पक्षधर्मत्व' । दोनों में केवल शब्दभेद है, अर्थभेद नहीं। उत्तरकाल में तो प्रायः सभी भारतीय ताकिकों के द्वारा तीन रूपों अथवा पांच रूपों के अन्तर्गत पक्षधर्मत्व का बोधक पक्षधर्मत्व या पक्ष धर्मता पद ही अभिप्रेत हुआ है । उद्योतकर 1, वाचस्पति 52, उदयन53, गंगेश,54 केशव प्रभति वैदिक नैयायिकों तथा धर्मकीति, धर्मोत्तर67, अर्चट58 आदि बौद्धताकिकों ने अपने ग्रन्थों में उसका प्रतिपादन किया है । पर जैन नैयायिकों ने पक्षधर्मता पर उतना बल नहीं दिया, जितना व्याप्ति पर दिया है। सिद्धसेन69, अकलंक 61, विद्यानन्द, वादीभसिंह आदि ने तो उसे अनावश्यक एवं व्यर्थ भी बतलाया है। उनका मन्तव्य है कि 'कल सूर्य का उदय होगा, क्योंकि वह आज उदय हो रहा है, 'कल शनिवार होगा, क्योंकि आज शुक्रवार है,' 'ऊपर देश में वृष्टि हुई है, क्योकि अधोदेश मे प्रवाह दृष्टिगोचर हो रहा है, 'अद्वैतवादी को भी प्रमाण इष्ट हैं, क्योंकि इष्ट का साधन और अनिष्ट का दूषण अन्यथा नहीं हो सकता' जैसे प्रचर हेतु पक्षधर्मता के अभाव में भी मात्र अन्तर्व्याप्ति के बल पर साध्य के अनुमापक हैं। (ख) व्याप्ति
अनुमान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और अनिवार्य अंग व्याप्ति है । इसके होने पर ही साधन साध्य का ५८ | चतुर्थ खण्ड : जैन दर्शन, इतिहास और साहित्य
मा.
........: AMAtional
H
.Di.
.