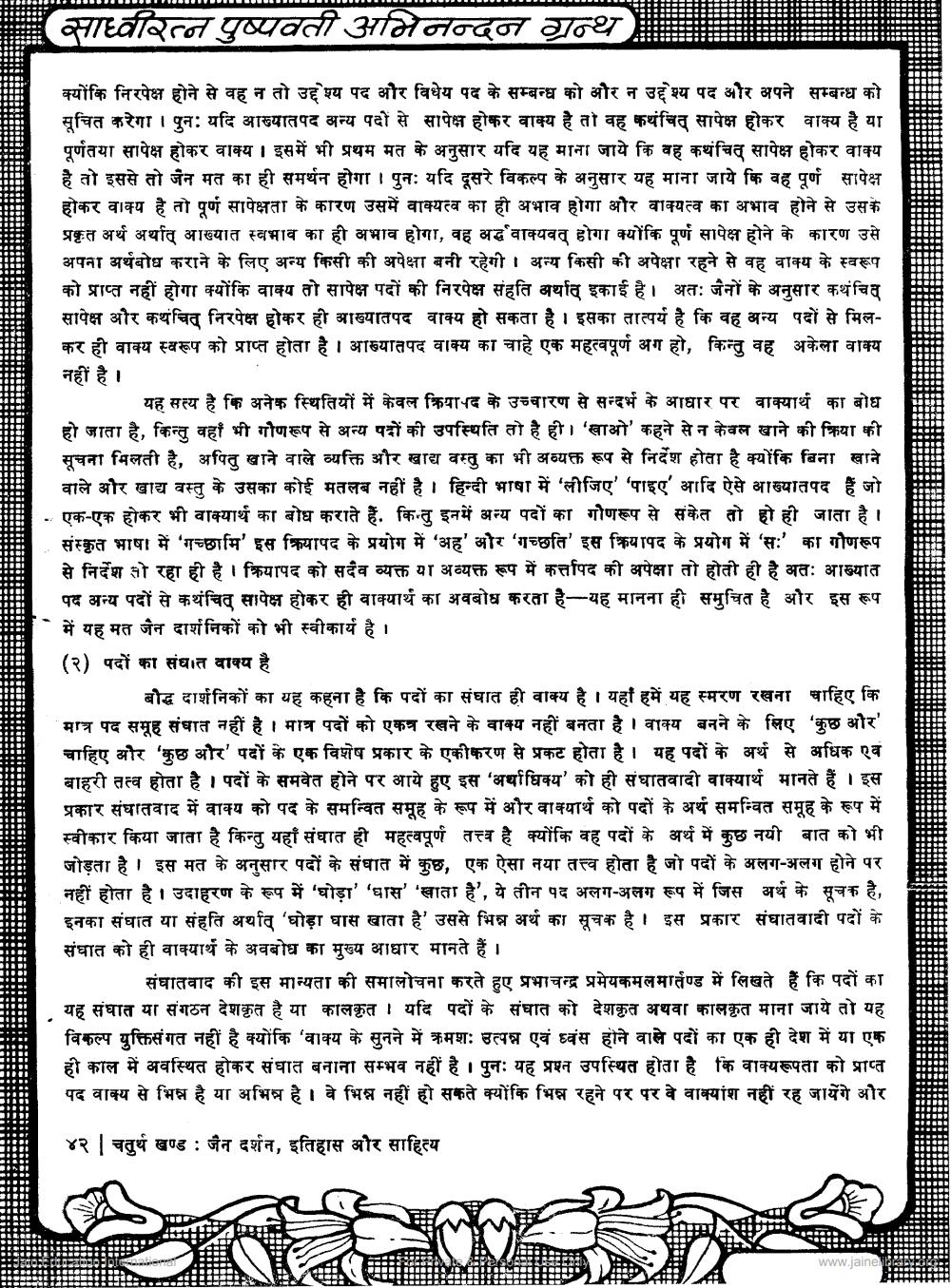________________
साध्वीरत्न पुष्पवती अभिनन्दन ग्रन्थ
क्योंकि निरपेक्ष होने से वह न तो उद्देश्य पद और विधेय पद के सम्बन्ध को और न उद्देश्य पद और अपने सम्बन्ध को सूचित करेगा । पुनः यदि आख्यातपद अन्य पदों से सापेक्ष होकर वाक्य है तो वह कथंचित् सापेक्ष होकर वाक्य है या पूर्णतया सापेक्ष होकर वाक्य। इसमें भी प्रथम मत के अनुसार यदि यह माना जाये कि वह कथंचित् सापेक्ष होकर वाक्य है तो इससे तो जैन मत का ही समर्थन होगा । पुनः यदि दूसरे विकल्प के अनुसार यह माना जाये कि वह पूर्ण सापेक्ष होकर वाक्य है तो पूर्ण सापेक्षता के कारण उसमें वाक्यत्व का ही अभाव होगा और वाक्यत्व का अभाव होने से उसके प्रकृत अर्थ अर्थात् आख्यात स्वभाव का ही अभाव होगा, वह अर्द्ध वाक्यवत् होगा क्योंकि पूर्ण सापेक्ष होने के कारण उसे अपना अर्थबोध कराने के लिए अन्य किसी की अपेक्षा बनी रहेगी । अन्य किसी की अपेक्षा रहने से वह वाक्य के स्वरूप को प्राप्त नहीं होगा क्योंकि वाक्य तो सापेक्ष पदों की निरपेक्ष संहति अर्थात् इकाई है। अतः जैनों के अनुसार कथंचित् सापेक्ष और कथंचित् निरपेक्ष होकर ही आख्यातपद वाक्य हो सकता है । इसका तात्पर्य है कि वह अन्य पदों से मिलकर ही वाक्य स्वरूप को प्राप्त होता है। आख्यातपद वाक्य का चाहे एक महत्वपूर्ण अंग हो, किन्तु वह अकेला वाक्य नहीं है ।
यह सत्य है कि अनेक स्थितियों में केवल क्रियापद के उच्चारण से सन्दर्भ के आधार पर वाक्यार्थ का बोध हो जाता है, किन्तु वहाँ भी गौणरूप से अन्य पत्रों की उपस्थिति तो है ही 'खाओ' कहने से न केवल खाने की क्रिया की सूचना मिलती है, अपितु खाने वाले व्यक्ति और खाद्य वस्तु का भी अव्यक्त रूप से निर्देश होता है क्योंकि बिना खाने वाले और खाद्य वस्तु के उसका कोई मतलब नहीं है। हिन्दी भाषा में 'लीजिए' 'पाइए' आदि ऐसे आख्यातपद हैं जो - एक-एक होकर भी वाक्यार्थ का बोध कराते हैं. किन्तु इनमें अन्य पदों का गौणरूप से संकेत तो हो ही जाता है। संस्कृत भाषा में 'गच्छामि' इस क्रियापद के प्रयोग में 'अह' और 'गच्छति' इस क्रियापद के प्रयोग में 'सः' का गौणरूप से निर्देश सो रहा ही है । क्रियापद को सदैव व्यक्त या अव्यक्त रूप में कर्त्तापद की अपेक्षा तो होती ही है अतः आख्यात पद अन्य पदों से कथंचित् सापेक्ष होकर ही वाक्यार्थ का अवबोध करता है - यह मानना ही समुचित है और इस रूप में यह मत जैन दार्शनिकों को भी स्वीकार्य है ।
(२) पदों का संघात वाक्य है
बौद्ध दार्शनिकों का यह कहना है कि पदों का संघात ही वाक्य है। यहाँ हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि मात्र पद समूह संघात नहीं है । मात्र पदों को एकत्र रखने के वाक्य नहीं बनता है । वाक्य बनने के लिए 'कुछ और' चाहिए और 'कुछ और पदों के एक विशेष प्रकार के एकीकरण से प्रकट होता है। यह पदों के अर्थ से अधिक एवं बाहरी तत्व होता है । पदों के समवेत होने पर आये हुए इस 'अर्थाधिक्य' को ही संघातवादी वाक्यार्थ मानते हैं । इस प्रकार संघातवाद में वाक्य को पद के समन्वित समूह के रूप में और वाक्यार्थ को पदों के अर्थ समन्वित समूह के रूप में स्वीकार किया जाता है किन्तु यहाँ संघात ही महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि वह पदों के अर्थ में कुछ नयी बात को भी जोड़ता है। इस मत के अनुसार पदों के संघात में कुछ एक ऐसा नया तत्व होता है जो पदों के अलग-अलग होने पर नहीं होता है । उदाहरण के रूप में 'घोड़ा' 'घास' 'खाता है', ये तीन पद अलग-अलग रूप में जिस अर्थ के सूचक है, इनका संघात या संहति अर्थात् 'घोड़ा घास खाता है' उससे भिन्न अर्थ का सूचक है । इस प्रकार संघातवादी पदों के संघात को ही वाक्यार्थ के अवबोध का मुख्य आधार मानते हैं ।
संघातवाद की इस मान्यता की समालोचना करते हुए प्रभाचन्द्र प्रमेयकमल मार्तण्ड में लिखते हैं कि पदों का यह संघात या संगठन देशकृत है या कालकृत यदि पदों के संघात को देशकृत अथवा कालकृत माना जाये तो यह विकल्प युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि 'वाक्य के सुनने में क्रमशः उत्पन्न एवं ध्वंस होने वाले पदों का एक ही देश में या एक ही काल में अवस्थित होकर संघात बनाना सम्भव नहीं है । पुनः यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वाक्यरूपता को प्राप्त पद वाक्य से भिन्न है या अभि है। वे भिन्न नहीं हो सकते क्योंकि भिन्न रहने पर पर वे वाक्यांश नहीं रह जायेंगे और
४२ | चतुर्थ खण्ड: जैन दर्शन, इतिहास और साहित्य
www.jaine iters