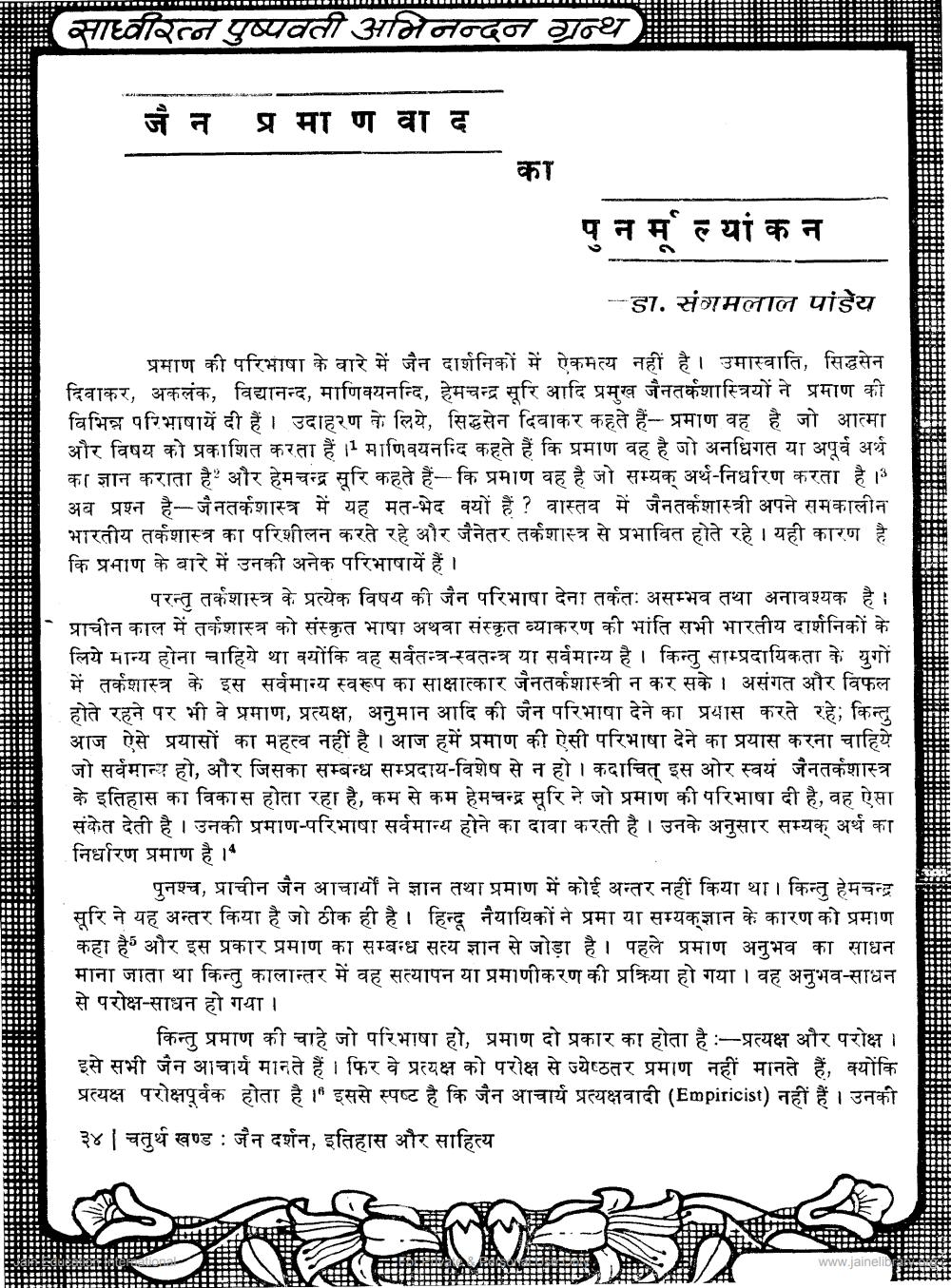________________
.....
.
.
.....
..
.......
.
..
.
.
..
.
...
....
साध्वीरत्नपुष्पवती अभिनन्दन ग्रन्थ
जैन प्रमाण वा द
-
-
का
पुन मूल्यांकन
TIT DOT
डा. संगमलाल पांडेय
...
प्रमाण की परिभाषा के बारे में जैन दार्शनिकों में ऐकमत्य नहीं है। उमास्वाति, सिद्धसेन दिवाकर, अकलंक, विद्यानन्द, माणिक्यनन्दि, हेमचन्द्र सूरि आदि प्रमुख जैनतर्कशास्त्रियों ने प्रमाण की विभिन्न परिभाषायें दी हैं। उदाहरण के लिये, सिद्धसेन दिवाकर कहते हैं-प्रमाण वह है जो आत्मा और विषय को प्रकाशित करता हैं । माणिवयनन्दि कहते हैं कि प्रमाण वह है जो अनधिगत या अपूर्व अर्थ का ज्ञान कराता है और हेमचन्द्र सूरि कहते हैं कि प्रमाण वह है जो सम्यक् अर्थ-निर्धारण करता है। अब प्रश्न है--जैनतर्कशास्त्र में यह मत-भेद क्यों हैं? वास्तव में जैन तर्कशास्त्री अपने समकालीन भारतीय तर्कशास्त्र का परिशीलन करते रहे और जैनेतर तर्कशास्त्र से प्रभावित होते रहे । यही कारण है कि प्रमाण के बारे में उनकी अनेक परिभाषायें हैं।
परन्त तर्कशास्त्र के प्रत्येक विषय की जैन परिभाषा देना तर्कतः असम्भव तथा अनावश्यक है। प्राचीन काल में तर्कशास्त्र को संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत व्याकरण की भांति सभी भारतीय दार्शनिकों के लिये मान्य होना चाहिये था क्योंकि वह सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र या सर्वमान्य है। किन्तु साम्प्रदायिकता के यूगों में तर्कशास्त्र के इस सर्वमान्य स्वरूप का साक्षात्कार जैनतर्कशास्त्री न कर सके। असंगत और विफल होते रहने पर भी वे प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान आदि की जैन परिभाषा देने का प्रयास करते रहे; किन्तु आज ऐसे प्रयासों का महत्व नहीं है । आज हमें प्रमाण की ऐसी परिभाषा देने का प्रयास करना चाहिये जो सर्वमान्य हो, और जिसका सम्बन्ध सम्प्रदाय-विशेष से न हो । कदाचित् इस ओर स्वयं जैनतर्कशास्त्र के इतिहास का विकास होता रहा है, कम से कम हेमचन्द्र सूरि ने जो प्रमाण की परिभाषा दी है, वह ऐसा संकेत देती है । उनकी प्रमाण-परिभाषा सर्वमान्य होने का दावा करती है । उनके अनुसार सम्यक् अर्थ का निर्धारण प्रमाण है।
पुनश्च, प्राचीन जैन आचार्यों ने ज्ञान तथा प्रमाण में कोई अन्तर नहीं किया था। किन्तु हेमचन्द्र सूरि ने यह अन्तर किया है जो ठीक ही है। हिन्दू नैयायिकों ने प्रमा या सम्यक् ज्ञान के कारण को प्रमाण कहा है और इस प्रकार प्रमाण का सम्बन्ध सत्य ज्ञान से जोड़ा है। पहले प्रमाण अनुभव का साधन माना जाता था किन्तु कालान्तर में वह सत्यापन या प्रमाणीकरण की प्रक्रिया हो गया। वह अनुभव-साधन से परोक्ष-साधन हो गया।
किन्तु प्रमाण की चाहे जो परिभाषा हो, प्रमाण दो प्रकार का होता है :-प्रत्यक्ष और परोक्ष । इसे सभी जैन आचार्य मानते हैं । फिर वे प्रत्यक्ष को परोक्ष से ज्येष्ठतर प्रमाण नहीं मानते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष परोक्षपूर्वक होता है। इससे स्पष्ट है कि जैन आचार्य प्रत्यक्षवादी (Empiricist) नहीं हैं। उनकी ३४ | चतुर्थ खण्ड : जैन दर्शन, इतिहास और साहित्य
www.jainelib