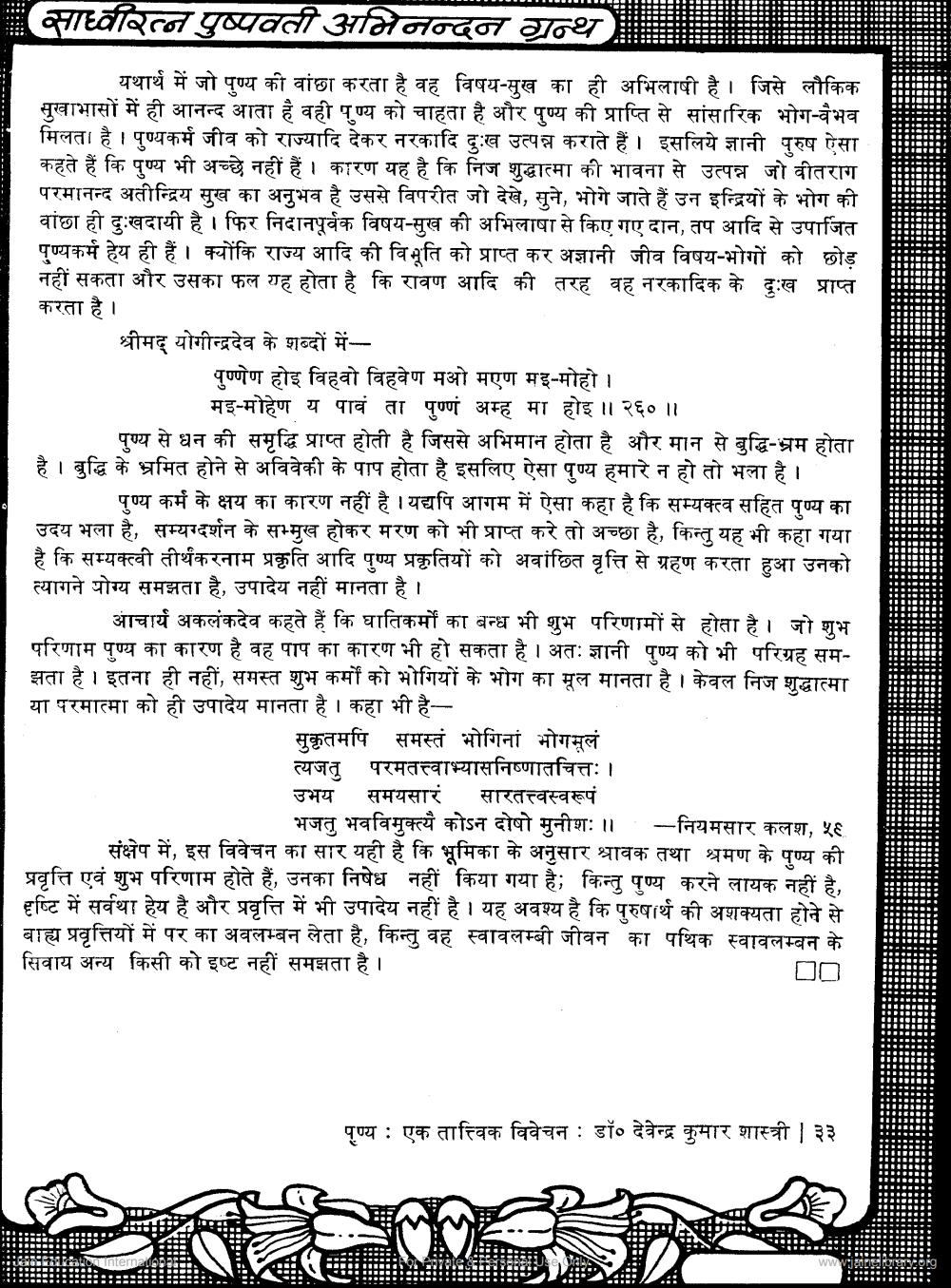________________
साध्वीरत्न पुष्पवती अभिनन्दन ग्रन्थ
यथार्थ में जो पुण्य की वांछा करता है वह विषय-सुख का ही अभिलाषी है । जिसे लौकिक सुखाभासों में ही आनन्द आता है वही पुण्य को चाहता है और पुण्य की प्राप्ति से सांसारिक भोग- वैभव मिलता है । पुण्यकर्म जीव को राज्यादि देकर नरकादि दुःख उत्पन्न कराते हैं । इसलिये ज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि पुण्य भी अच्छे नहीं हैं । कारण यह है कि निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न जो वीतराग परमानन्द अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है उससे विपरीत जो देखे, सुने, भोगे जाते हैं उन इन्द्रियों के भोग की ही दुःखदायी है । फिर निदानपूर्वक विषय - सुख की अभिलाषा से किए गए दान, तप आदि से उपार्जित पुण्यकर्म । क्योंकि राज्य आदि की विभूति को प्राप्त कर अज्ञानी जीव विषय-भोगों को छोड़ नहीं सकता और उसका फल यह होता है कि रावण आदि की तरह वह नरकादिक के दुःख प्राप्त करता है ।
श्रीमद् योगीन्द्रदेव के शब्दों में
२६० ॥
पुणेण होइ विहवो विहवेण मओ मएण मइ-मोहो । मइ - मोहेण य पावं ता पुण्णं अम्ह मा होइ ॥ पुण्य से धन की समृद्धि प्राप्त होती है जिससे अभिमान होता है और मान से बुद्धि-भ्रम होता है । बुद्धि के भ्रमित होने से अविवेकी के पाप होता है इसलिए ऐसा पुण्य हमारे न हो तो भला है । पुण्य कर्म के क्षय का कारण नहीं है । यद्यपि आगम में ऐसा कहा है कि सम्यक्त्व सहित पुण्य का उदय भला है, सम्यग्दर्शन के सम्मुख होकर मरण को भी प्राप्त करे तो अच्छा है, किन्तु यह भी कहा गया है कि सम्यक्त्वी तीर्थंकरनाम प्रकृति आदि पुण्य प्रकृतियों को अवांछित वृत्ति से ग्रहण करता हुआ उनको त्यागने योग्य समझता है, उपादेय नहीं मानता है ।
आचार्य अकलंकदेव कहते हैं कि घातिकर्मों का बन्ध भी शुभ परिणामों से होता है । जो शुभ परिणाम पुण्य का कारण है वह पाप का कारण भी हो सकता है । अतः ज्ञानी पुण्य को भी परिग्रह समझता है । इतना ही नहीं, समस्त शुभ कर्मों को भोगियों के भोग का मूल मानता है । केवल निज शुद्धात्मा या परमात्मा को ही उपादेय मानता है । कहा भी है
सुकृतमपि समस्तं भोगिनां भोगमूलं त्यजतु परमतत्त्वाभ्यासनिष्णातचित्तः । उभय समयसारं सारतत्त्वस्वरूपं भजतु भवविमुक्त्यै कोऽन दोषो मुनीशः ॥
- नियमसार कलश, ५६.
संक्षेप में, इस विवेचन का सार यही है कि भूमिका के अनुसार श्रावक तथा श्रमण के पुण्य की प्रवृत्ति एवं शुभ परिणाम होते हैं, उनका निषेध नहीं किया गया है; किन्तु पुण्य करने लायक नहीं है, दृष्टि में सर्वथा है और प्रवृत्ति में भी उपादेय नहीं है । यह अवश्य है कि पुरुषार्थ की अशक्यता होने से बाह्य प्रवृत्तियों में पर का अवलम्बन लेता है, किन्तु वह स्वावलम्बी जीवन का पथिक स्वावलम्बन के सिवाय अन्य किसी को इष्ट नहीं समझता है ।
पुण्य : एक तात्त्विक विवेचन : डॉ० देवेन्द्र कुमार शास्त्री | ३३