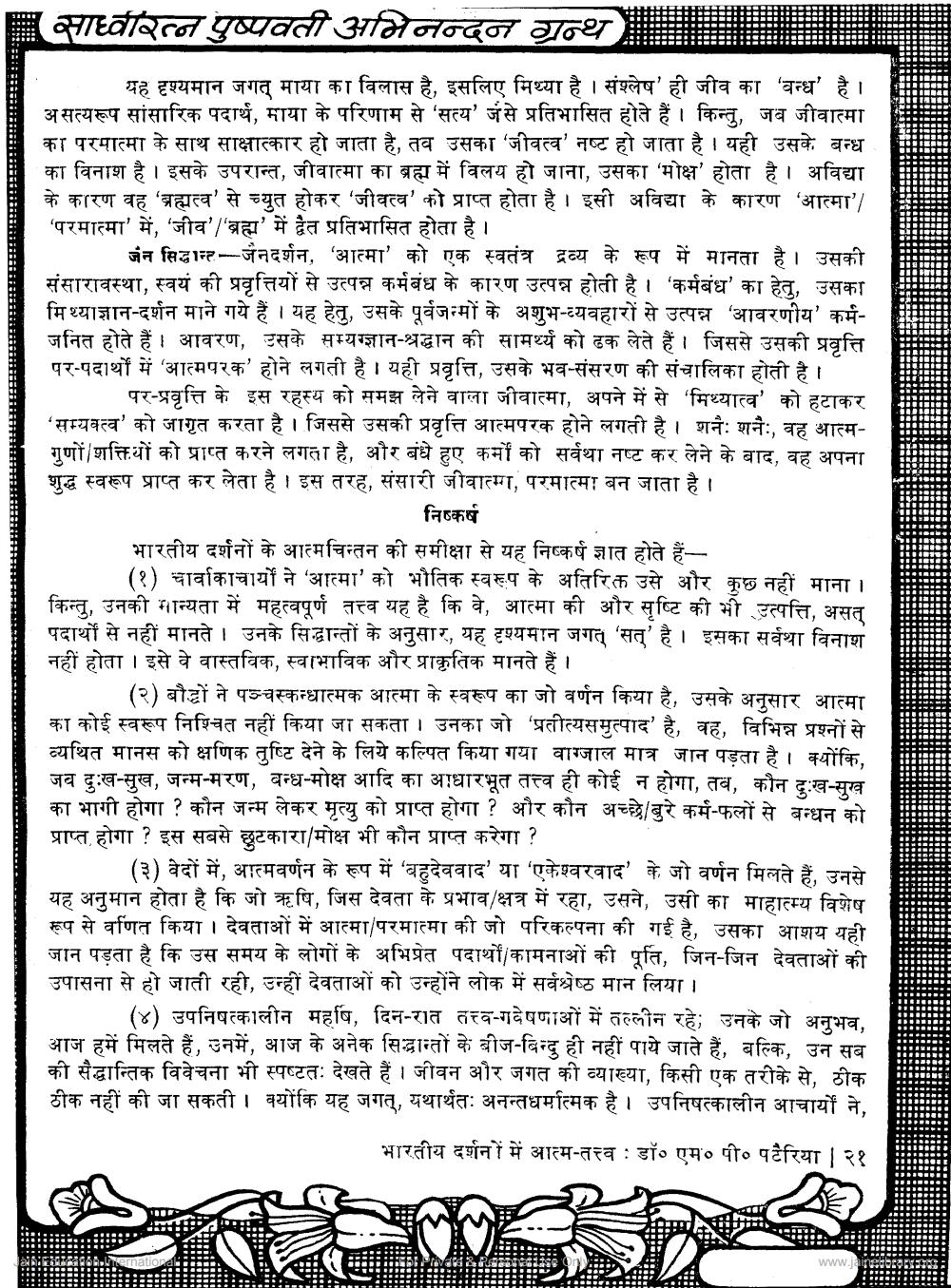________________
साध्वीरत्नपुष्पवती अभिनन्दन ग्रन्थ
यह दृश्यमान जगत् माया का विलास है, इसलिए मिथ्या है । संश्लेष' ही जीव का 'वन्ध' है। असत्यरूप सांसारिक पदार्थ, माया के परिणाम से 'सत्य' जैसे प्रतिभासित होते हैं। किन्तु, जब जीवात्मा का परमात्मा के साथ साक्षात्कार हो जाता है, तव उसका 'जीवत्व' नष्ट हो जाता है । यही उसके बन्ध का विनाश है । इसके उपरान्त, जीवात्मा का ब्रह्म में विलय हो जाना, उसका 'मोक्ष' होता है। अविद्या के कारण वह 'ब्रह्मत्व' से च्यूत होकर 'जीवत्व' को प्राप्त होता है। इसी अविद्या के कारण 'आत्मा'। 'परमात्मा' में, 'जीव'/'ब्रह्म' में द्वैत प्रतिभासित होता है।
जैन सिद्धान्त-जैनदर्शन, 'आत्मा' को एक स्वतंत्र द्रव्य के रूप में मानता है। उसकी संसारावस्था, स्वयं की प्रवृत्तियों से उत्पन्न कर्मबंध के कारण उत्पन्न होती है। 'कर्मबंध' का हेतु, उसका मिथ्याज्ञान-दर्शन माने गये हैं । यह हेतु, उसके पूर्वजन्मों के अशुभ-व्यवहारों से उत्पन्न 'आवरणीय' कर्मजनित होते हैं। आवरण, उसके सम्यग्ज्ञान-श्रद्धान की सामर्थ्य को ढक लेते हैं। जिससे उसकी प्र पर-पदार्थों में 'आत्मपरक' होने लगती है। यही प्रवृत्ति, उसके भव-संसरण की संचालिका होती है।
पर-प्रवत्ति के इस रहस्य को समझ लेने वाला जीवात्मा, अपने में से 'मिथ्यात्व' को हटाकर 'सम्यक्त्व' को जागृत करता है। जिससे उसकी प्रवृत्ति आत्मपरक होने लगती है। शनैः शनैः, वह आत्मगुणों शक्तियों को प्राप्त करने लगता है, और बंधे हुए कर्मों को सर्वथा नष्ट कर लेने के बाद, वह अपना शुद्ध स्वरूप प्राप्त कर लेता है । इस तरह, संसारी जीवात्म्ग, परमात्मा बन जाता है।
निष्कर्ष भारतीय दर्शनों के आत्मचिन्तन की समीक्षा से यह निष्कर्ष ज्ञात होते हैं
(१) चार्वाकाचार्यों ने 'आत्मा' को भौतिक स्वरूप के अतिरिक्त उसे और कुछ नहीं माना। किन्तु, उनकी मान्यता में महत्वपूर्ण तत्त्व यह है कि वे, आत्मा की और सृष्टि की भी उत्पत्ति, असत पदार्थों से नहीं मानते । उनके सिद्धान्तों के अनुसार, यह दृश्यमान जगत् 'सत्' है। इसका सर्वथा विनाश नहीं होता । इसे वे वास्तविक, स्वाभाविक और प्राकृतिक मानते हैं ।
(२) बौद्धों ने पञ्चस्कन्धात्मक आत्मा के स्वरूप का जो वर्णन किया है, उसके अनुसार आत्मा का कोई स्वरूप निश्चित नहीं किया जा सकता। उनका जो 'प्रतीत्यसमुत्पाद' है, वह, विभिन्न प्रश्नों से व्यथित मानस को क्षणिक तुष्टि देने के लिये कल्पित किया गया वाग्जाल मात्र जान पड़ता है। क्योंकि. जब दुःख-सुख, जन्म-मरण, बन्ध-मोक्ष आदि का आधारभूत तत्त्व ही कोई न होगा, तब, कौन दुःख-सुख का भागी होगा ? कौन जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त होगा? और कौन अच्छे बुरे कर्म-फलों से बन्धन को प्राप्त होगा ? इस सबसे छुटकारा/मोक्ष भी कौन प्राप्त करेगा?
(३) वेदों में, आत्मवर्णन के रूप में 'बहुदेववाद' या 'एकेश्वरवाद' के जो वर्णन मिलते हैं, उनसे यह अनुमान होता है कि जो ऋषि, जिस देवता के प्रभाव/क्षत्र में रहा, उसने, उसी का माहात्म्य विशेष रूप से वणित किया। देवताओं में आत्मा/परमात्मा की जो परिकल्पना की गई है, उसका आशय यही जान पड़ता है कि उस समय के लोगों के अभिप्रेत पदार्थो कामनाओं की पूति, जिन-जिन देवताओं की उपासना से हो जाती रही, उन्हीं देवताओं को उन्होंने लोक में सर्वश्रेष्ठ मान लिया।
(४) उपनिषत्कालीन महर्षि, दिन-रात तत्त्व-गवेषणाओं में तल्लीन रहे; उनके जो अनुभव, आज हमें मिलते हैं, उनमें, आज के अनेक सिद्धान्तों के बीज-बिन्दु ही नहीं पाये जाते हैं, बल्कि, उन सब की सैद्धान्तिक विवेचना भी स्पष्टतः देखते हैं । जीवन और जगत की व्याख्या, किसी एक तरीके से, ठीक ठीक नहीं की जा सकती। क्योंकि यह जगत्, यथार्थतः अनन्तधर्मात्मक है। उपनिषत्कालीन आचार्यों ने,
भारतीय दर्शनों में आत्म-तत्त्व : डॉ० एम० पी० पटैरिया | २१
Nok
www.