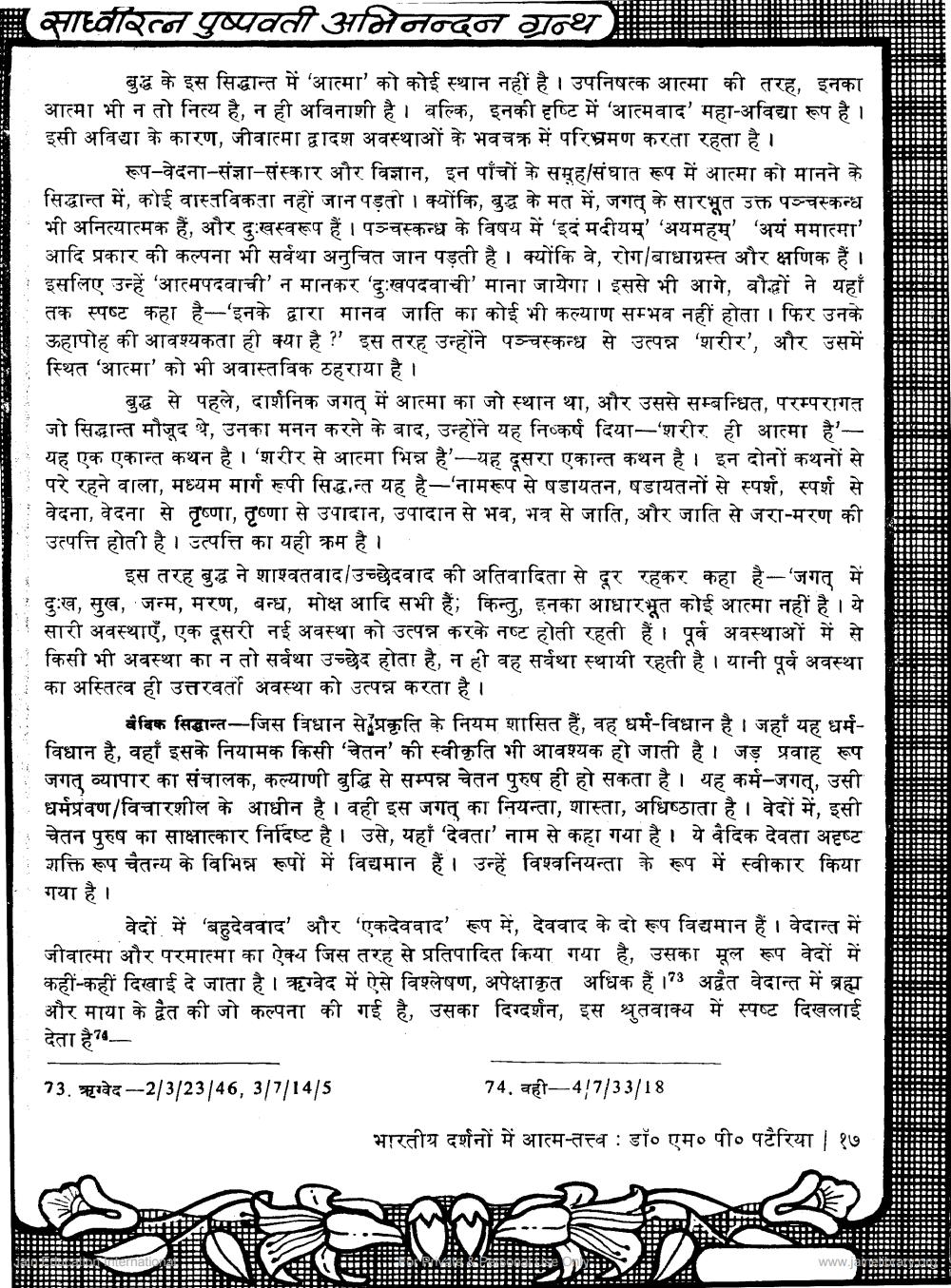________________
साध्वीरत्न पुष्पवती अभिनन्दन ग्रन्थ
-..-.
..---------
----
-
-
--------
-
-----
--
बुद्ध के इस सिद्धान्त में 'आत्मा' को कोई स्थान नहीं है। उपनिषत्क आत्मा की तरह, इनका आत्मा भी न तो नित्य है, न ही अविनाशी है। बल्कि, इनकी दृष्टि में 'आत्मवाद' महा-अविद्या रूप है। इसी अविद्या के कारण, जीवात्मा द्वादश अवस्थाओं के भवचक्र में परिभ्रमण करता रहता है।
रूप-वेदना-संज्ञा-संस्कार और विज्ञान, इन पाँचों के समह/संघात रूप में आत्मा को मानने के सिद्धान्त में, कोई वास्तविकता नहीं जान पड़तो। क्योंकि, बुद्ध के मत में, जगत् के सारभूत उक्त पञ्चस्कन्ध भी अनित्यात्मक हैं, और दुःखस्वरूप हैं। पञ्चस्कन्ध के विषय में 'इदं मदीयम्' 'अयमहम्' 'अयं ममात्मा' आदि प्रकार की कल्पना भी सर्वथा अनुचित जान पड़ती है। क्योंकि वे, रोग/बाधाग्रस्त और क्षणिक हैं। इसलिए उन्हें 'आत्मपदवाची' न मानकर 'दुःखपदवाची' माना जायेगा। इससे भी आगे, बौद्धों ने यहाँ तक स्पष्ट कहा है-'इनके द्वारा मानव जाति का कोई भी कल्याण सम्भव नहीं होता । फिर उनके ऊहापोह की आवश्यकता ही क्या है ?' इस तरह उन्होंने पञ्चस्कन्ध से उत्पन्न 'शरीर', और उसमें स्थित 'आत्मा' को भी अवास्तविक ठहराया है।
बुद्ध से पहले, दार्शनिक जगत् में आत्मा का जो स्थान था, और उससे सम्बन्धित, परम्परागत जो सिद्धान्त मौजूद थे, उनका मनन करने के बाद, उन्होंने यह निष्कर्ष दिया-'शरीर ही आत्मा है'यह एक एकान्त कथन है। 'शरीर से आत्मा भिन्न है'-यह दूसरा एकान्त कथन है। इन दोनों कथनों से परे रहने वाला, मध्यम मार्ग रूपी सिद्धान्त यह है-'नामरूप से षडायतन, षडायतनों से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से भव, भव से जाति, और जाति से जरा-मरण की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति का यही क्रम है।
इस तरह बुद्ध ने शाश्वतवाद उच्छेदवाद की अतिवादिता से दूर रहकर कहा है- 'जगत् में दुःख, सुख, जन्म, मरण, बन्ध, मोक्ष आदि सभी हैं; किन्तु, इनका आधारभूत कोई आत्मा नहीं है । ये सारी अवस्थाएँ, एक दूसरी नई अवस्था को उत्पन्न करके नष्ट होती रहती हैं। पूर्व अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था का न तो सर्वथा उच्छेद होता है, न ही वह सर्वथा स्थायी रहती है । यानी पूर्व अवस्था का अस्तित्व ही उत्तरवर्तो अवस्था को उत्पन्न करता है ।
वैविक सिद्धान्त-जिस विधान से प्रकृति के नियम शासित हैं, वह धर्म-विधान है । जहाँ यह धर्मविधान है, वहाँ इसके नियामक किसी 'चेतन' की स्वीकृति भी आवश्यक हो जाती है। जड़ प्रवाह रूप जगत् व्यापार का संचालक, कल्याणी बुद्धि से सम्पन्न चेतन पुरुष ही हो सकता है। यह कर्म-जगत्, उसी धर्मप्रवण/विचारशील के आधीन है। वही इस जगत् का नियन्ता, शास्ता, अधिष्ठाता है । वेदों में, इसी चेतन पुरुष का साक्षात्कार निर्दिष्ट है। उसे, यहाँ 'देवता' नाम से कहा गया है। ये वैदिक देवता अदृष्ट शक्ति रूप चैतन्य के विभिन्न रूपों में विद्यमान हैं। उन्हें विश्वनियन्ता के रूप में स्वीकार किया गया है।
वेदों में 'बहुदेववाद' और 'एकदेववाद' रूप में, देववाद के दो रूप विद्यमान हैं । वेदान्त में जीवात्मा और परमात्मा का ऐक्य जिस तरह से प्रतिपादित किया गया है, उसका मूल रूप वेदों में कहीं-कहीं दिखाई दे जाता है । ऋग्वेद में ऐसे विश्लेषण, अपेक्षाकृत अधिक हैं ।73 अद्वैत वेदान्त में ब्रह्म और माया के द्वैत की जो कल्पना की गई है, उसका दिग्दर्शन, इस श्रुतवाक्य में स्पष्ट दिखलाई देता है
-
73. ऋग्वेद--2/3/23/46, 3/7/14/5
74. वही-4/7/33/18
भारतीय दर्शनों में आत्म-तत्त्व : डॉ० एम० पी० पटैरिया | १७