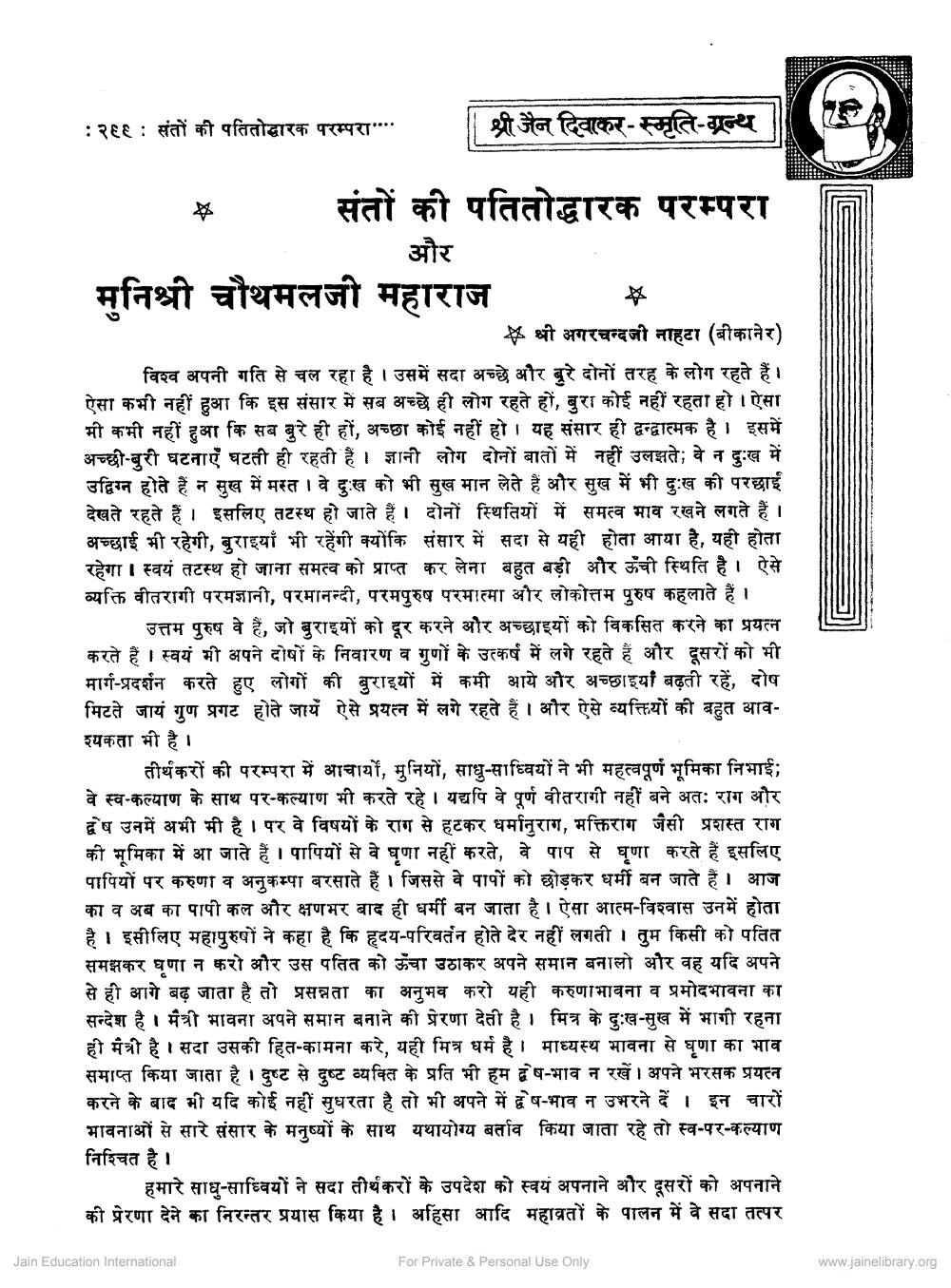________________
: २६६ : संतों की पतितोद्धारक परम्परा
श्री जैन दिवाकर-स्मृति-ठान्थ ||
*
संतों की पतितोद्धारक परम्परा
और मनिश्री चौथमलजी महाराज
श्री अगरचन्दजी नाहटा (बीकानेर) विश्व अपनी गति से चल रहा है । उसमें सदा अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग रहते हैं। ऐसा कभी नहीं हआ कि इस संसार में सब अच्छे ही लोग रहते हों, बुरा कोई नहीं रहता हो। भी कभी नहीं हुआ कि सब बुरे ही हों, अच्छा कोई नहीं हो। यह संसार ही द्वन्द्वात्मक है। इसमें अच्छी-बुरी घटनाएं घटती ही रहती हैं। ज्ञानी लोग दोनों बातों में नहीं उलझते; वे न दुःख में उद्विग्न होते हैं न सुख में मस्त । वे दुःख को भी सुख मान लेते हैं और सुख में भी दुःख की परछाई देखते रहते हैं। इसलिए तटस्थ हो जाते हैं। दोनों स्थितियों में समत्व भाव रखने लगते हैं । अच्छाई भी रहेगी, बुराइयाँ भी रहेंगी क्योंकि संसार में सदा से यही होता आया है, यही होता रहेगा । स्वयं तटस्थ हो जाना समत्व को प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी और ऊंची स्थिति है। ऐसे व्यक्ति वीतरागी परमज्ञानी, परमानन्दी, परमपुरुष परमात्मा और लोकोत्तम पुरुष कहलाते हैं ।
उत्तम पुरुष वे हैं, जो बुराइयों को दूर करने और अच्छाइयों को विकसित करने का प्रयत्न करते हैं । स्वयं भी अपने दोषों के निवारण व गुणों के उत्कर्ष में लगे रहते हैं और दूसरों को भी मार्ग-प्रदर्शन करते हुए लोगों की बुराइयों में कमी आये और अच्छाइयां बढ़ती रहें, दोष मिटते जायं गुण प्रगट होते जायें ऐसे प्रयत्न में लगे रहते हैं। और ऐसे व्यक्तियों की बहुत आवश्यकता भी है।
तीर्थकरों की परम्परा में आचार्यों, मुनियों, साधु-साध्वियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे स्व-कल्याण के साथ पर-कल्याण भी करते रहे । यद्यपि वे पूर्ण वीतरागी नहीं बने अतः राग और द्वेष उनमें अभी भी है। पर वे विषयों के राग से हटकर धर्मानुराग, भक्तिराग जैसी प्रशस्त राग की भूमिका में आ जाते हैं । पापियों से वे घृणा नहीं करते, वे पाप से घृणा करते हैं इसलिए पापियों पर करुणा व अनुकम्पा बरसाते हैं। जिससे वे पापों को छोड़कर धर्मी बन जाते हैं। आज का व अब का पापी कल और क्षणभर बाद ही धर्मी बन जाता है। ऐसा आत्म-विश्वास उनमें होता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि हृदय-परिवर्तन होते देर नहीं लगती। तुम किसी को पतित समझकर घणा न करो और उस पतित को ऊंचा उठाकर अपने समान बनालो और वह यदि अपने से ही आगे बढ़ जाता है तो प्रसन्नता का अनुभव करो यही करुणाभावना व प्रमोदभावना का सन्देश है । मैत्री भावना अपने समान बनाने की प्रेरणा देती है। मित्र के दुःख-सुख में भागी रहना ही मैत्री है । सदा उसकी हित-कामना करे, यही मित्र धर्म है। माध्यस्थ भावना से घृणा का भाव समाप्त किया जाता है। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के प्रति भी हम द्वेष-भाव न रखें। अपने भरसक प्रयत्न करने के बाद भी यदि कोई नहीं सुधरता है तो भी अपने में द्वेष-भाव न उभरने दें । इन चारों भावनाओं से सारे संसार के मनुष्यों के साथ यथायोग्य बर्ताव किया जाता रहे तो स्व-पर-कल्याण निश्चित है।
हमारे साधु-साध्वियों ने सदा तीर्थंकरों के उपदेश को स्वयं अपनाने और दूसरों को अपनाने की प्रेरणा देने का निरन्तर प्रयास किया है। अहिंसा आदि महाव्रतों के पालन में वे सदा तत्पर
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org