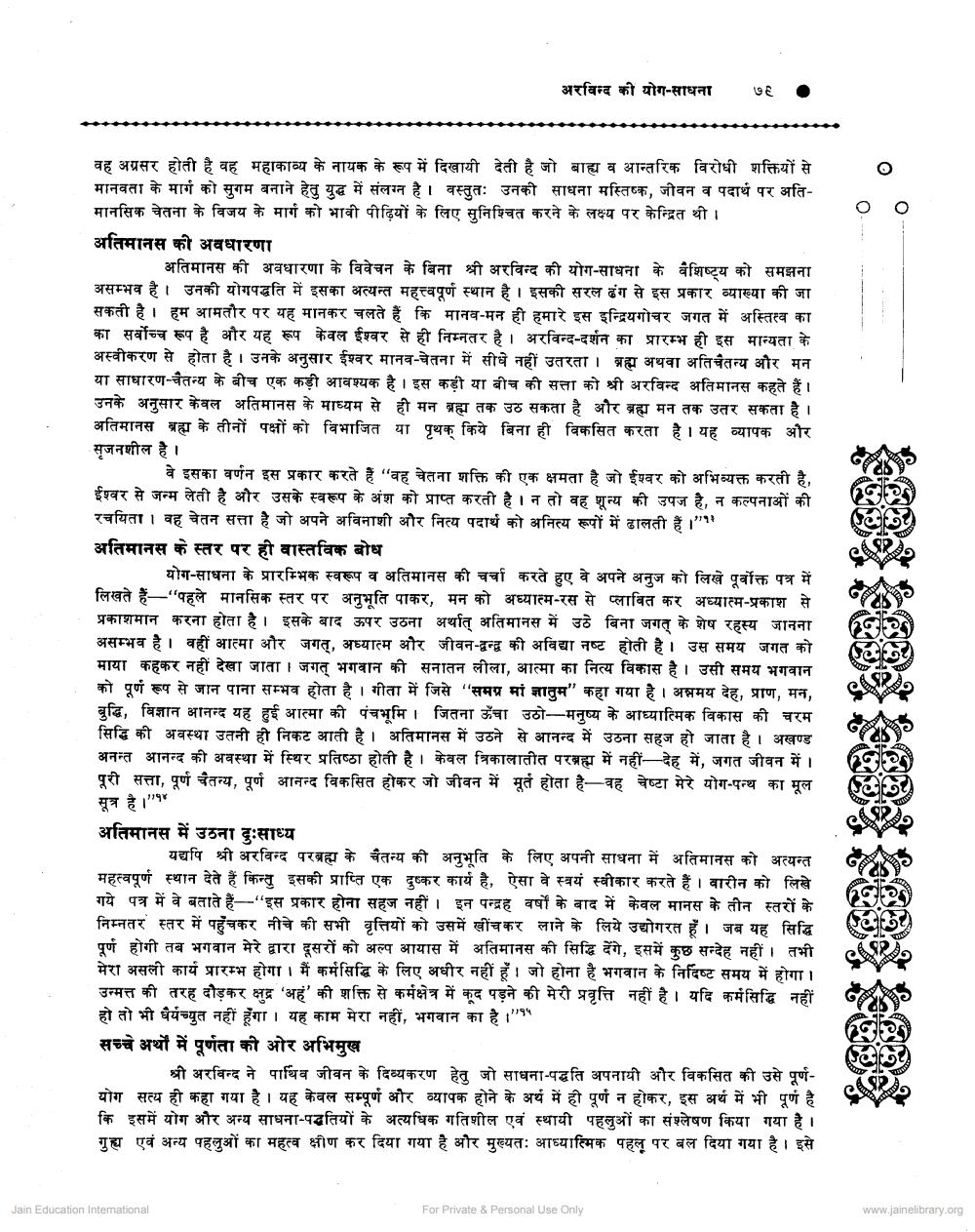________________
अरविन्द की योग-साधना
७६
वह अग्रसर होती है वह महाकाव्य के नायक के रूप में दिखायी देती है जो बाह्य व आन्तरिक विरोधी शक्तियों से मानवता के मार्ग को सुगम बनाने हेतु युद्ध में संलग्न है। वस्तुतः उनकी साधना मस्तिष्क, जीवन व पदार्थ पर अतिमानसिक चेतना के विजय के मार्ग को भावी पीढ़ियों के लिए सुनिश्चित करने के लक्ष्य पर केन्द्रित थी। अतिमानस की अवधारणा
अतिमानस की अवधारणा के विवेचन के बिना श्री अरविन्द की योग-साधना के वैशिष्ट्य को समझना असम्भव है। उनकी योगपद्धति में इसका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसकी सरल ढंग से इस प्रकार व्याख्या की जा सकती है। हम आमतौर पर यह मानकर चलते हैं कि मानव-मन ही हमारे इस इन्द्रियगोचर जगत में अस्तित्व का का सर्वोच्च रूप है और यह रूप केवल ईश्वर से ही निम्नतर है। अरविन्द-दर्शन का प्रारम्भ ही इस मान्यता के अस्वीकरण से होता है। उनके अनुसार ईश्वर मानव-चेतना में सीधे नहीं उतरता। ब्रह्म अथवा अतिचैतन्य और मन या साधारण-चैतन्य के बीच एक कड़ी आवश्यक है। इस कड़ी या बीच की सत्ता को श्री अरविन्द अतिमानस कहते हैं। उनके अनुसार केवल अतिमानस के माध्यम से ही मन ब्रह्म तक उठ सकता है और ब्रह्म मन तक उतर सकता है। अतिमानस ब्रह्म के तीनों पक्षों को विभाजित या पृथक् किये बिना ही विकसित करता है। यह व्यापक और सृजनशील है।
वे इसका वर्णन इस प्रकार करते हैं "वह चेतना शक्ति की एक क्षमता है जो ईश्वर को अभिव्यक्त करती है, ईश्वर से जन्म लेती है और उसके स्वरूप के अंश को प्राप्त करती है। न तो वह शून्य की उपज है, न कल्पनाओं की रचयिता । वह चेतन सत्ता है जो अपने अविनाशी और नित्य पदार्थ को अनित्य रूपों में ढालती हैं।" अतिमानस के स्तर पर ही वास्तविक बोध
योग-साधना के प्रारम्भिक स्वरूप व अतिमानस की चर्चा करते हुए वे अपने अनुज को लिखे पूर्वोक्त पत्र में लिखते हैं-"पहले मानसिक स्तर पर अनुभूति पाकर, मन को अध्यात्म-रस से प्लावित कर अध्यात्म-प्रकाश से प्रकाशमान करना होता है। इसके बाद ऊपर उठना अर्थात् अतिमानस में उठे बिना जगत् के शेष रहस्य जानना असम्भव है। वहीं आत्मा और जगत्, अध्यात्म और जीवन-द्वन्द्व की अविद्या नष्ट होती है। उस समय जगत को माया कहकर नहीं देखा जाता । जगत् भगवान की सनातन लीला, आत्मा का नित्य विकास है। उसी समय भगवान को पूर्ण रूप से जान पाना सम्भव होता है । गीता में जिसे "समग्र मां ज्ञातुम" कहा गया है। अन्नमय देह, प्राण, मन, बुद्धि, विज्ञान आनन्द यह हुई आत्मा की पंचभूमि । जितना ऊँचा उठो-मनुष्य के आध्यात्मिक विकास की चरम सिद्धि की अवस्था उतनी ही निकट आती है। अतिमानस में उठने से आनन्द में उठना सहज हो जाता है। अखण्ड अनन्त आनन्द की अवस्था में स्थिर प्रतिष्ठा होती है। केवल त्रिकालातीत परब्रह्म में नहीं-देह में, जगत जीवन में। पूरी सत्ता, पूर्ण चैतन्य, पूर्ण आनन्द विकसित होकर जो जीवन में मूर्त होता है-वह चेष्टा मेरे योग-पन्थ का मूल सूत्र है।" अतिमानस में उठना दुःसाध्य
यद्यपि श्री अरविन्द परब्रह्म के चैतन्य की अनुभूति के लिए अपनी साधना में अतिमानस को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान देते हैं किन्तु इसकी प्राप्ति एक दुष्कर कार्य है, ऐसा वे स्वयं स्वीकार करते हैं। वारीन को लिखे गये पत्र में वे बताते हैं-"इस प्रकार होना सहज नहीं। इन पन्द्रह वर्षों के बाद में केवल मानस के तीन स्तरों के निम्नतर स्तर में पहुंचकर नीचे की सभी वृत्तियों को उसमें खींचकर लाने के लिये उद्योगरत हूँ। जब यह सिद्धि पूर्ण होगी तब भगवान मेरे द्वारा दूसरों को अल्प आयास में अतिमानस की सिद्धि देंगे, इसमें कुछ सन्देह नहीं। तभी मेरा असली कार्य प्रारम्भ होगा। मैं कर्मसिद्धि के लिए अधीर नहीं हूँ। जो होना है भगवान के निर्दिष्ट समय में होगा। उन्मत्त की तरह दौड़कर क्षुद्र 'अहं' की शक्ति से कर्मक्षेत्र में कूद पड़ने की मेरी प्रवृत्ति नहीं है। यदि कर्मसिद्धि नहीं हो तो भी धैर्यच्युत नहीं हूँगा। यह काम मेरा नहीं, भगवान का है।"१५ सच्चे अर्थों में पूर्णता को ओर अभिमुख
श्री अरविन्द ने पार्थिव जीवन के दिव्यकरण हेतु जो साधना-पद्धति अपनायी और विकसित की उसे पूर्णयोग सत्य ही कहा गया है। यह केवल सम्पूर्ण और व्यापक होने के अर्थ में ही पूर्ण न होकर, इस अर्थ में भी पूर्ण है कि इसमें योग और अन्य साधना-पद्धतियों के अत्यधिक गतिशील एवं स्थायी पहलुओं का संश्लेषण किया गया है। गुह्य एवं अन्य पहलुओं का महत्व क्षीण कर दिया गया है और मुख्यतः आध्यात्मिक पहल पर बल दिया गया है। इसे
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org