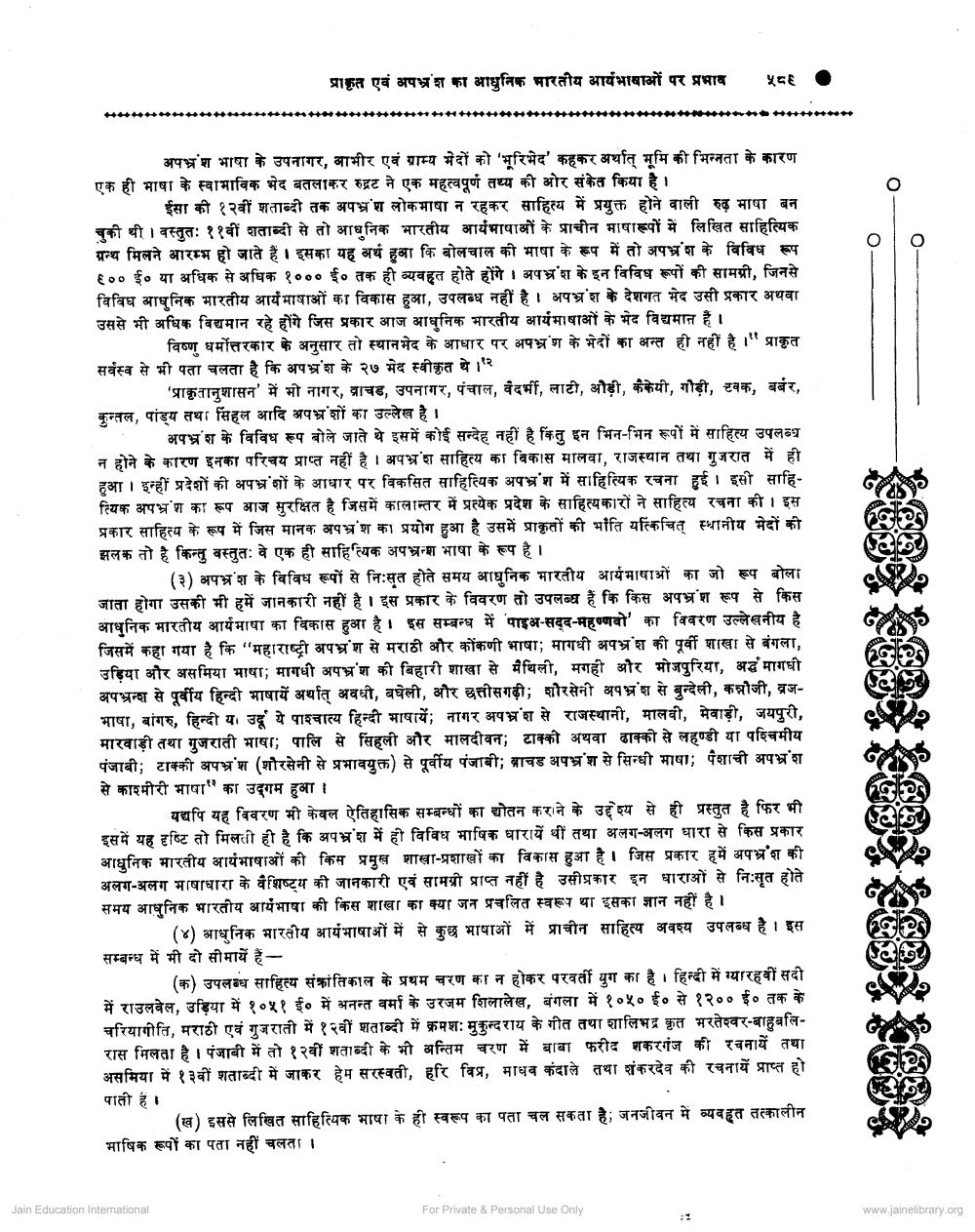________________
***
प्राकृत एवं अपभ्रंश का आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं पर प्रभाव ५८६
अपश भाषा के उपनागर, आभीर एवं ग्राम्य भेदों को 'भूरिभेद' कहकर अर्थात् भूमि की भिन्नता के कारण एक ही भाषा के स्वाभाविक भेद बतलाकर रुद्रट ने एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर संकेत किया है।
ईसा की १२वीं शताब्दी तक अपभ्रंश लोकभाषा न रहकर साहित्य में प्रयुक्त होने वाली रुढ़ भाषा बन चुकी थी । वस्तुतः ११वीं शताब्दी से तो आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं के प्राचीन भाषारूपों में लिखित साहित्यिक ग्रन्थ मिलने आरम्भ हो जाते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि बोलचाल की भाषा के रूप में तो अपभ्रंश के विविध रूप ६०० ई० या अधिक से अधिक १००० ई० तक ही व्यवहृत होते होंगे। अपभ्रंश के इन विविध रूपों की सामग्री, जिनसे विविध आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ, उपलब्ध नहीं है। अपभ्रंश के देशगत भेद उसी प्रकार अथवा उससे भी अधिक विद्यमान रहे होंगे जिस प्रकार आज आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं के भेद विद्यमान हैं ।
विष्णु धर्मोत्तरकार के अनुसार तो स्थानभेद के आधार पर अपभ्रंश के भेदों का अन्त ही नहीं है ।" प्राकृत सर्वस्व से भी पता चलता है कि अपभ्रंश के २७ भेद स्वीकृत थे । १२
'प्राकृतानुशासन' में भी नागर, व्राचड, उपनागर, पंचाल, वैदर्भी, लाटी, ओड़ी, कैकेयी, गौड़ी, टवक, बर्बर, कुन्तल, पांड्य तथा सिंहल आदि अपभ्रंशों का उल्लेख है ।
अपभ्रंश के विविध रूप बोले जाते थे इसमें कोई सन्देह नहीं है किंतु इन मिन-भिन्न रूपों में साहित्य उपलब्ध न होने के कारण इनका परिचय प्राप्त नहीं है । अपभ्रंश साहित्य का विकास मालवा, राजस्थान तथा गुजरात में ही हुआ । इन्हीं प्रदेशों की अपभ्रंशों के आधार पर विकसित साहित्यिक अपभ्रंश में साहित्यिक रचना हुई। इसी साहि त्यिक अपभ्रंश का रूप आज सुरक्षित है जिसमें कालान्तर में प्रत्येक प्रदेश के साहित्यकारों ने साहित्य रचना की। इस प्रकार साहित्य के रूप में जिस मानक अपभ्रंश का प्रयोग हुआ है उसमें प्राकृतों की भाँति यत्किचित् स्थानीय भेदों की झलक तो है किन्तु वस्तुतः वे एक ही साहित्यिक अपभ्रन्श भाषा के रूप है ।
(३) अपभ्रंश के विविध रूपों से निःसृत होते समय आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं का जो रूप बोला जाता होगा उसकी भी हमें जानकारी नहीं है। इस प्रकार के विवरण तो उपलब्ध हैं कि किस अपभ्रंश रूप से किस आधुनिक भारतीय आर्यभाषा का विकास हुआ है। इस सम्बन्ध में पाइअ सद्द-महण्णवो' का विवरण उल्लेखनीय है जिसमें कहा गया है कि "महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी और कोंकणी भाषा; मागधी अपभ्रंश की पूर्वी शाखा से बंगला, उड़िया और असमिया माया, मागधी अपभ्रंश की बिहारी शाखा से मैथिली, मगही और भोजपुरिया, बहंगामधी अपभ्रन्ा से पूर्वीय हिन्दी भाषायें अर्थात् अवधी, बघेली, और छत्तीसगढ़ी; शौरसेनी अपभ्रंश से बुन्देली, कन्नौजी, व्रजभाषा, बांगरु, हिन्दी य उर्दू ये पाश्चात्य हिन्दी भाषायें; नागर अपभ्रंश से राजस्थानी, मालवी, मेवाड़ी, जयपुरी, मारवाड़ी तथा गुजराती भाषा; पालि से सिंहली और मालदीवन; टाक्की अथवा ढाक्की से लहण्डी या पश्चिमीय पंजाबी; टाक्की अपभ्रंश (शौरसेनी से प्रभावयुक्त) से पूर्वीय पंजाबी; ब्राचड अपभ्रंश से सिन्धी भाषा; पैशाची अपभ्रंश से काश्मीरी भाषा" का उद्गम हुआ ।
यद्यपि यह विवरण भी केवल ऐतिहासिक सम्बन्धों का द्योतन करने के उद्देश्य से ही प्रस्तुत है फिर भी इसमें यह दृष्टि तो मिलती ही है कि अपभ्रंश में ही विविध भाषिक धारायें थीं तथा अलग-अलग धारा से किस प्रकार आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं की किस प्रमुख शाखा प्रशाखों का विकास हुआ है । जिस प्रकार हमें अपभ्रंश की अलग-अलग भाषाधारा के वैशिष्ट्य की जानकारी एवं सामग्री प्राप्त नहीं है उसीप्रकार इन धाराओं से निःसृत होते समय आधुनिक भारतीय आर्यभाषा की किस शाखा का क्या जन प्रचलित स्वरूप था इसका ज्ञान नहीं है।
(४) आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं में से कुछ भाषाओं में प्राचीन साहित्य अवश्य उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में भी दो सीमायें हैं
(क) उपलब्ध साहित्य संक्रांतिकाल के प्रथम चरण का न होकर परवर्ती युग का है। हिन्दी में ग्यारहवीं सदी में राउलवेल, उड़िया में १०५१ ई० में अनन्त वर्मा के उरजम शिलालेख, बंगला में १०५० ई० से १२०० ई० तक के चरियागीति, मराठी एवं गुजराती में १२वीं शताब्दी में क्रमशः मुकुन्दराय के गीत तथा शालिभद्र कृत भरतेश्वर बाहुबलि - रास मिलता है। पंजाबी में तो १२वीं शताब्दी के भी अन्तिम चरण में बाबा फरीद शकरगंज की रचनायें तथा असमिया में १३वीं शताब्दी में जाकर हेम सरस्वती, हरि विप्र माधव कंदाले तथा शंकरदेव की रचनायें प्राप्त हो
पाती हैं।
(ख) इससे लिखित साहित्यिक भाषा के ही स्वरूप का पता चल सकता है; जनजीवन में व्यवहृत तत्कालीन भाषिक रूपों का पता नहीं चलता ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org